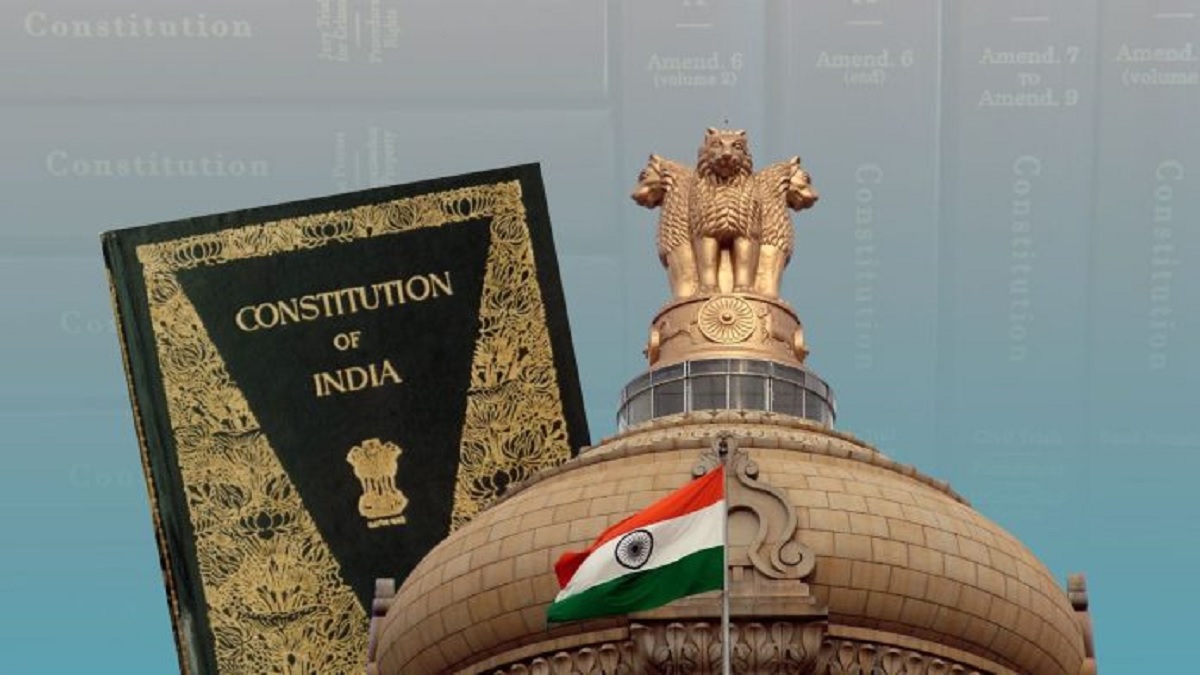जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चुनाव का बहुत महत्व होता है। हम सब हर पल किसी-न-किसी तरह के चुनाव में लगे रहते हैं। सब से ज्यादा चुनावी पल मोबाइल के साथ जुड़ा दिखता है। चुनाव विकल्पों में से किसी एक को चुनने का अवसर देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उपलब्ध विकल्प असल में विकल्प होते ही नहीं हैं। फिर भी चुनने के अवसर का अपने-आप में महत्वपूर्ण होता है।
दैनंदिन जीवन के अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि सब से ज्यादा खिचखिच सब्जी और कपड़ा बाजार में होता है। उदाहरण के लिए कपड़ा बाजार की बात कर सकते हैं। कपड़ा खरीदने में सब से ज्यादा खिचखिच रंग और रूप यानी ‘कलर और डिजाइन’ को लेकर होती है। ध्यान देने की बात है कि ‘कलर और डिजाइन’ के बाद ही मूल वस्तु की गुणवत्ता का नंबर आता है। कपड़ों की खरीद के मामले में अदल-बदल की गुंजाइश की रहती है, अमूमन पांच-छः महीने में अगली खरीद का मौका भी आ ही जाता है। फिर भी हम खरीद में आश्चर्यजनक सावधानी बरतते हैं।
एक चुनाव ऐसा भी होता है जिस में अदल-बदल की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अगला मौका पांच साल बाद मिलने का संवैधानिक प्रावधान होता है। कहना न होगा कि जीवन स्थिति और परिस्थिति के लिए ऐसे अतिमहत्वपूर्ण चुनाव में कई बार हम आश्चर्यजनक लापरवाही बरतने के दोषी होते हैं! अपने वर्तमान और प्रत्याशित जन-प्रतिनिधि के काम और इरादों पर न तो ठीक से नजर रखते हैं, न उनके वास्तविक आकलन की ही कोई कोशिश करते हैं। अपवाद की गुंजाइश सभी जगह होती है, यहां भी है। आज का समय नजरदारी का समय है।
प्रत्येक घटना को घटते हुए देखने की अदम्य लालसाओं ने हमारे नैतिक संकाय को बहुत निकृष्ट अर्थ में गछार लिया है, जैसे अनचाही लताएं वृक्ष को लपेट लेती हैं। शब्द संकेत मात्र बनकर रह गये हैं और दृश्य लगभग अकाट्य और सर्वसंतोषी प्रमाण बन गये हैं। शब्द-दृश्य पदबंध मं ‘शब्द’ कमजोर पड़ते जा रहे हैं। कहने का आशय यह है कि ‘शब्द’ का महत्व सांकेतिक बनकर रह गया है जबकि ‘दृश्य’ का महत्व प्रामाणिक किस्म का बन गया है। यह प्रवृत्ति व्यक्ति, समाज और राज सभी जगह बढ़ रही है। ऐसे में निजता और सार्वजनिकता के बीच का फर्क मिटता चला जा रहा है।
‘घर में घुसकर देखने’ की अदम्य प्रवृत्ति का स्वाभाविक विस्तार ‘घर में घुसकर मारने’ तक हो जाता है। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र, न्यायपत्र में ‘निजता के अधिकार’ की बात कही है और ‘निजता की रक्षा’ का आश्वासन दिया है तो उसके व्यापक महत्व को नागरिक जीवन की स्वतंत्रता के महत्व से जोड़कर ही समझा जा सकता है। कहने का आशय यह है कि आज के डीजिटल दौर में ‘निजता के अधिकार’ और ‘निजता की रक्षा’ की जरूरत राज्य व्यवस्था के नाभिक केंद्र में बैठे व्यवस्थापक व्यक्ति को तो होती ही है, सामाजिक हाशिए की अंतिम परिधि पर खड़े व्यक्ति को भी होती है।
समाज और राज्य व्यवस्था के सुचारु रहने के साथ ही, व्यक्ति की गरिमा के लिए भी पारदर्शी नैतिकता और नैतिक नजरदारी या निगरानी (Ethical Surveillance) की अनिवार्यता से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पारदर्शिता और निजता का सवाल आज के दौर की कई महत्वपूर्ण जटिलताओं में से एक है। अनैतिक उद्देश्यों से नैतिक नजरदारी या निगरानी की प्रवृत्ति के अपने खतरे हैं। इन खतरों में ‘घर में घुसकर देखने’ और ‘घर में घुसकर मारने’ के इरादे को भी शामिल समझना चाहिए। कहना न होगा कि जीवन में पारदर्शिता और अपारदर्शिता की ऊहापोह के चलते डिजिटल के दायरे के विस्तार से दुश्चिंता, खतरा, भयदोहन, शोषण, विभिन्न तरह की विषमताओं, अन्याय और हिंसा का भी दायरा बढ़ा है।
ज्ञान, अधिकार और शक्ति के बीच हमेशा खींचतान लगा रहता है। इन के पारस्परिक संबंधों में संतुलन और असंतुलन का प्रभाव दैनंदिन के कामकाज पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। ज्ञान, अधिकार और शक्ति के बीच सार्वकालिक और सार्वदेशिक संतुलन हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन पर हमेशा चौकस नजर रखना और समस्याओं को निवारण करते रहना ही एक मात्र उपाय हो सकता है। कार्य और शक्ति के पारंपरिक संबंधों की पारस्परिकता में भारी उथल-पुथल भविष्य के प्रति शंकालु बनाता है। ऐसे में ‘जो है, जैसा है, यथा-समय मौज करो’ की मानसिकता जीवन को ‘तदर्थ’ की गिरफ्त में डाल देता है। जीवन का ‘तदर्थ’ की गिरफ्त में पड़ जाना भयानक होता है।
लोकतंत्र में चुनाव ‘वैकल्पिक आत्मीयता’ का महत्व होता है। लोकतांत्रिक चुनाव में आत्मीयता के उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक को चुनने का अवसर होता है। इस तरह जनप्रतिनिधियों के चुनाव में लोकतांत्रिक आत्मीयता का एक अनिवार्य तत्व अवश्य ही होना चाहिए। मगर होता नहीं है। ‘लोकतांत्रिक आत्मीयता’ के बने रहने की कोशिश ‘शक्ति से संपन्न’ होती है। इसलिए यह मुख्य रूप से सत्ता पक्ष का दायित्व और विपक्ष की भाव-भंगिमा का विषय है। प्रसंगवश, भंग करने का अर्थ तोड़ना और भंगिमा का अर्थ तोड़ने की कला होता है। नाट्य में भाव-भंगिमा का बहुत महत्व होता है। आहत किये बिना किसी भाव से अलग होना और करना भाव-भंगिमा है।
दुर्भाग्यजनक है कि भारत में चुनाव लगभग नागरिक युद्ध में बदल जाता है, इस बार तो यह कुछ ज्यादा ही होने के आसार हैं। माहौलबंदी के लिए चुनाव में जनविद्वेषी बयानबाजी (Hate Speech) का अटूट सिलसिला चल निकलता है। इस अटूट सिलसिला के चलते आत्मीयता बार-बार खंडित होती रहती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खंडित आत्मीयता विष की तरह होती है। ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए सब से बड़ा हथियार यह खंडित आत्मीयता ही तो होती है!
खंडित आत्मीयता का आयुधीकरण आसान होता है या आयुधीकरण के लिए आत्मीयता को खंडित करने का लोकतांत्रिक विरोधी रुझान ‘लोकतंत्र के पर्व’ में अपने कपट के साथ प्रकट होता है! कहना बहुत मुश्किल है, समझना शायद उतना मुश्किल न हो। महाभारत में आत्मीयता के आयुधीकरण का एक प्रसंग चाचा धृतराष्ट्र का भीम को गले लगाने की इच्छा में देखने को मिलता है। इस प्रसंग में कृष्ण आत्मीयता के आयुधीकरण के खतरे को भांपकर भीम को सावधान न किया होता तो उनकी लीला वहीं समाप्त हो गई होती।
लोकलुभावन राजनीति काल्पनिक अतीत के स्वर्ण युग के प्रतिपक्षी राजनीति के कारण विनष्ट हो जाने का हल्ला मचाती है। ‘सोने के हिरन’ को पाने की जिद को लोक चेतना से जोड़ देती है। फिर क्या होता है! जो नहीं होना चाहिए किसी सभ्य समाज में, किसी भी काल में! लोकलुभावन राजनीति अनुमानित भविष्य में अतिरेकी सुख-दुख के प्रति स्वाभाविक चिंता में निहित अनावश्यक उन्माद की तीव्रता की आंच बढ़ाती रहती है। लोकलुभावन राजनीति वर्तमान और भविष्य में विभिन्न तरह के खतरों और हिंसा की आशंकाओं की हवा लोकमन में भरती रहती है।
लोकमन में अपनी विश्वसनीयता बनाये रखने की ‘परियोजना’ के अंतर्गत लोकलुभावन राजनीति दंगा-फसाद कराने से भी नहीं बाज आती है। जरा-सा मौका मिलते ही दंगा-फसाद का माहौल बनाने के लिए उकसावा देती है। स्पष्टता से कहा जाये तो, लोकलुभावन राजनीति अपनी विश्वसनीयता के लिए खतरों और हिंसा की आशंकाओं को वास्तविक साबित करने के लिए किसी भी तरह की निकृष्टता से परहेज नहीं करती है।
चुनाव का मिजाज परिवार के बल पर नहीं तय होता है। आज-कल चुनावी राजनीति में गलत इरादे से परिवारवाद की बेसुरा तान छेड़ने में सतरू (सत्तारूढ़) पक्ष के लोग लगे हुए हैं। परिवार चुनाव से नहीं बनता है। हम न मां-बाप को चुनते हैं। न भाई-बहन को! फिर भी कौन इनकार कर सकता है कि हम उन के लिए जीते-मरते हैं! हम न परिवार को चुनते हैं, न परिवार हमें चुनता है। परिवार एक मिली हुई परिस्थिति है। परिवार में उत्तराधिकार और उत्तरजीविता (पहले के जीवित के अर्जित का बाद में जीवित को मिलनेवाला लाभ) का नैतिक एवं संवैधानिक महत्व है। भारतीय जनता पार्टी और उस के बड़े से बड़े नेता जिस तरह से परिवारवाद की खिल्ली उड़ाते हैं, उन्हें उत्तराधिकार और उत्तरजीविता के बारे में अपना रुख साफ-साफ रखना चाहिए।
अद्भुत है, पूरे तंत्र को एकाधिकार में लेने को आतुर ‘एकोअहं’ की धमाचौकड़ी मचाते हुए बात-बात में परिवारवाद की बात करना! मनुष्य के जीवन में व्यक्ति का भी महत्व है परिवार, समाज और राज का भी महत्व है। इस महत्व के सार को समझने के लिए जरूरी है कि इन्हें एक दूसरे के जुड़ाव और संभाव में देखा जाये। राजनीति और लोकतंत्र परिवारविहीन या संन्यासियों का न तो कुरुक्षेत्र है और न धर्मक्षेत्र है। परिवारवाद से मुक्त होने के लिए उत्तराधिकार के कानून को बदले जाने की बात कीजिए तो पता चल जायेगा कि कौन कितने पानी में है। यहां तो कई लोग अनी ही तीसरी पीढ़ी के ऊपर के नाम तक नहीं जानते और जिस पर परिवारवादी होने का आरोप लगाते हैं, श्रीमान उसकी पांच-छः पीढ़ी ऊपर के लोगों को इतिहास याद रखे हुए है।
फिर कहें, लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्व होता है। संसदीय लोकतंत्र में चुनाव का समय नागरिक के लिए बहुत कुछ सीखने का अवसर लेकर आता है। कुछ-कुछ करते रहना और इस के साथ कुछ-न-कुछ सीखते रहना मनुष्य के जीवंत बने रहने के लिए जरूरी होता है। हर नागरिक को अपने और देश के तात्कालिक और दीर्घकालिक हित में जनप्रतिनिधियों को चुनते समय बहुत अधिक सावधानी से काम लेने के महत्व को समझना होगा। यही वह सब से माकूल समय है जब हमें पहले हिंदू, पहले मुसलमान, पहले बिहारी, पहले मद्रासी आदि के किसी भी तरह के ‘पहले’ होने से बचना होगा।
‘पहले भी’ और ‘बाद में भी’ भारतीय, सिर्फ भारतीय होने के महत्व को पहचानना होगा। डॉ. आंबेडकर की लोकतांत्रिक शिक्षा का अनुसरण लाभप्रद है। ‘पहले कुछ अन्य और बाद में भारतीय’ या ‘पहले भारतीय और बाद में कुछ अन्य’ की सोच की विभक्त निष्ठा से मुक्त हो कर ‘पहले भी भारतीय और अंत में भी भारतीय’ की अविभक्त निष्ठा ही हमारे काम की है।
संसदीय लोकतंत्र के लिए होनेवाले चुनाव में ‘पहले भी भारतीय और अंत में भी भारतीय’ की अविभक्त निष्ठा ही हमारे निर्णय का वास्तविक आधार होना चाहिए। अभी कोई उलझाव नहीं। व्यक्तिवाद परिवारवाद समाजवाद अपनी जगह! चुनाव में चाहिए संविधानवाद! 2024 का आम चुनाव भारतीयों की अविभक्त निष्ठा की सब से बड़ी परीक्षा है। इस कठिन परीक्षा में परीक्षार्थी भी हम हैं। परीक्षक भी हम हैं। फेल या पास भी हमें ही होना है। परिणाम की प्रतीक्षा है।
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)