कृश्न चंदर से मैं आख़िरी बार बंबई अस्पताल में मिला। मैं वहां पांच बजे शाम को गया था। अंदर जाने की मुमानियत (पाबंदी) थी, मगर फिर भी मैं डॉक्टर की नज़र बचाकर एक मिनट के लिए कमरे के अंदर पहुंच गया। कृश्न चंदर पलंग पर तकियों के सहारे लेटे थे। कितनी नलकियां और बिजली की तारें, उनके जिस्म में लगी हुई थीं। टखने की रग के ज़रिए ग्लूकोज़ दिया जा रहा था। नाक में ऑक्सीजन की नलकी लगी हुई थी।
छाती पर बांए तरफ़ को उनकी खाल के नीचे पेसमेकर लगा हुआ था। जो एक बैटरी से चलने वाला आला है। जो दिल की हरकत जब तशवीश (घबराहट) के क़ाबिल हो जाए, तो उसको आपसे आप चालू कर देता है। ग़रज़ कि दिल के मरीज को जितनी मेडिकल सहुलियतें मुमकिन हैं, दी जा रही थीं। दिल की हरकत तारों के ज़रिए एक पर्दे पर उछलती हुई रौशनी की एक नन्हीं सी गेंद की शक्ल में नज़र आती है। उस वक़्त ये रौशन गेंद उछल-कूद कर रही थी। यानी दिल ब-ख़ूबी काम कर रहा था।
फिर भी मुझको कृश्न चंदर के चेहरे पर मायूसी तो नहीं कहूंगा, लेकिन थकन के आसार नज़र आए। पहले जब मैं जाता था, तो वो मेरा इस्तिक़बाल अपनी ख़ूबसूरत और मीठी मुस्कराहट से करते थे। उनकी आंखें चमक उठती थीं। लेकिन उस दिन एक हल्की सी, कड़वी सी, मुस्कराहट उनके चेहरे पर एक पल के लिए उभरी। और फिर धीरे-धीरे फेड आउट (धुंधली) हो गई। आंखों की गहराई में मैंने एक ऐसी बुझती हुई चमक देखी, जो पहले कभी दिखाई न दी थी। मैंने कल न आने की माफ़ी चाही।
“होली का हंगामा इतना था कि हिम्मत न पड़ी घर से निकलने की।”
धीरे से उन्होंने कहा, “कल तो तुम आए थे। साथ में अंदर भी थे, शाम।” (मिसेज इंदिरा बहन भी थीं।)
मैंने कहा, “वो परसो थीं। कल हम लोग न आ सके।”
“नहीं, कल तुम लोग आए थे।”
मैंने सोचा, इनका दिमाग़ कल और परसों का फ़र्क़ भूल गया है। फिर मैंने उस पर बहस नहीं की।
‘अब्बास’ फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, “हम तो अब चले।”
मैंने पुर-ख़ुलूस (उदारता से भरा हुआ) रिया-कारी (ढोंग) से कहा, “नहीं जी, कैसे जा सकते हैं, आप। अभी तो तुम्हें बहुत काम करना है। हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे।”
फिर मैंने कृश्न चंदर का हाथ, अपने हाथ में लिया। ये हाथ जिसने क़लम से क्या-क्या गुल-बूटे (कलियाँ या पौधे) खिलाए थे, उर्दू अदब के चमन में। ये हाथ जिसने ‘तिलिस्म-ए-ख़याल’ लिखा था। अफ़सानों की पहली किताब। अफ़साने, जिन्होंने उर्दू पढ़ने वालों को चौंका दिया था कि अदब के उफु़क़ (क्षितिज) पर एक सूरज और नुमूदार (प्रकट) हुआ।
ये हाथ जिसने ‘अन्नदाता’ और ‘बालकनी’ जैसे ट्रेड मार्क अफ़साने लिखे थे। जिनकी रूह मार्क्सवाद थी। मगर जिनमें उर्दू की बेहतरीन शायरी का सारा हुस्न था। ये हुस्न और शुऊर का इम्तिज़ाज (मिश्रण) कृश्न चंदर की देन थी। आज वो हाथ मेरे हाथ में था। जी चाहता था, उसको न छोड़ूं। अपने हाथ में दबोचे रखूं। उसे अपने हाथों की गर्मी पहुंचा दूं। अपनी ज़िंदगी उस हाथ को दे दूं। ताकि अगर कृश्न चंदर मर भी जाए, तो किसी तरह ये हाथ ज़िंदा रहे। और लिखता रहे।
और उस रात ही कृश्न को बेचैनी शुरू हुई और रात ही को बंबई अस्पताल में दाख़िल कर दिया गया। जिस कमरे में उसने पिछले हार्ट अटैक में लगभग एक महीना काटा था। इत्तिफ़ाक़ से वही कमरा खाली मिल गया। हमें नहीं मालूम कि मौत वहां उसका इंतज़ार कर रही है।
मैंने हाथ को दबाया। दूसरी तरफ़ से भी हल्की सी कोशिश हुई, मेरे हाथ को दबाने की। लेकिन अब उस हाथ में ताक़त ख़त्म हो रही थी। क्या, परवाह है? मैंने सोचा, इस हाथ को फावड़ा चलाना थोड़ा ही है, सिर्फ़ लिखना ही तो है। इतनी ताक़त भी काफ़ी है। नर्स ने मुझे इशारा किया कि अब, तुम जाओ। मैंने बा-दिल-ए-ना-ख़्वास्ता (इच्छा के विरुद्ध) कृश्न चंदर का हाथ छोड़ा। अपने हाथ के अंगूठे को ऊपर करके दो-तीन बार जुंबिश (कंपन) की। ये बैनल-अक़वामी (अंतर्राष्ट्रीय) निशानी है, जीत की। कि हमने अभी हार नहीं मानी है। उसने भी अंगूठा ऊपर करके, बहुत ही हल्के से जुंबिश की।
मैंने समझा, कृश्न कह रहा है कि मैंने हार नहीं मानी है। मैं जीतने की कोशिश करूंगा। ये हमारा बहुत पुराना निशान था। हर बार, जब कृश्न को हार्ट अटैक हुआ, मैं चलते वक़्त ये ही इशारा करता था। और कृश्न भी यही इशारा करता था। मगर आज उसके इशारे में एक दूसरा मतलब छुपा हुआ था। वो गोया अंगूठे से इशारा कर रहा था कि “हम तो अब ऊपर चले।” मगर मैंने अपने दिल को जान-बूझकर धोखा दिया। नहीं जी, वही पुराना मतलब है। अपना यार कृश्न चंदर बहुत हिम्मतवाला है। वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। सीढ़ियां उतर रहा था कि ज़ोए अंसारी ऊपर जाते हुए मिले। उन्होंने पूछा, “कृश्न चंदर कैसे हैं?”
मैंने सफे़द झूठ बोला, “पहले से बहुत बेहतर हैं।”
वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चले गए, मैं नीचे चला गया। मेरा दिल और नीचे जा रहा था। वो पुर-उम्मीद जा रहे थे। मैं उम्मीद के चिराग़ बुझा चुका था।
मैं कृश्न चंदर के लड़के से (जो बाहर बैठा हुआ था) कहकर आया था, “कोई तशवीश-नाक (व्याकुलता भरी) बात हो, तो मुझे फोन कर देना।”
रात भर उस फ़ोन के इंतज़ार में नींद नहीं आई। मैं करवटें बदलता रहा। और मेरे तख़य्युल (कल्पना) के पर्दे पर कृश्न चंदर की मुख़्तलिफ़ झलकियां उभर रही थीं। इक फ़िल्म ‘मोंताज़’ (विभिन्न शॉट्स को एक कड़ी में जोड़कर, एक नया प्रभाव पैदा करने की कोशिश) की तरह आती रहीं-जाती रहीं। शर्बती आंखों वाला कृश्न चंदर उस वक़्त दुबला-पतला नौजवान होता था। दिल्ली के रेडियो स्टेशन में जहां हमारी पहली मुलाक़ात हुई थी। मंटो भी वहां था। (अब मंटो कहां है? कौन से आकाशवाणी से अपने ड्रामे प्रोड्यूस कर रहा है?)
फिर हम बंबई में मिले। जब वो पूना में ‘शालीमार’ में काम कर रहा था। वहां अदबी जमघट था। जोश, अख़्तर-उल-ईमान, इंदर राज आनंद, साग़र निजामी, रामानंद सागर, (जिसमें से अक्सर को कृश्न की तजवीज़ (सुझाव) पर वहां बुलाया गया था।) ‘अंजुमन तरक़्क़ीपसंद मुसन्निफ़ीन’ की मीटिंग्स उन दिनों सज्जाद ज़हीर के फ्लैट में बालकेश्वर रोड पर होती थीं।
बंगाल में उन दिनों अकाल पड़ रहा था। एक दिन ख़बर आई कि कृश्न चंदर पूना से आए हुए हैं और इतवार को ‘अंजुमन तरक़्क़ीपसंद मुसन्निफ़ीन’ में अपना नया अफ़साना सुनाएंगे। अफ़साना तो याद नहीं, कौन सा था? ‘बालकनी’ या ‘अन्नदाता’ मगर ये अब तक याद है कि नीले, चिकने मोटे काग़ज़ के पैड पर लिखा हुआ था। जैसे काग़ज़ों पर कभी हम कॉलेज में प्रेम-पत्र लिखा करते थे। (ये अदा कृश्न चंदर की आख़िरी दिनों तक रही। अब भी उसके कमरे में चिकने, नीले काग़ज़ के कितने ही पैड खाली पड़े उसके क़लम की रवानी का इंतज़ार कर रहे हैं।) मैंने उस काग़ज़ से मरऊब (आतंकित) होकर, कृश्न से कहा,
“तुम तो अफ़साना क्या लिखते हो, एक प्रेम-पत्र लिखते हो?”
मगर उस क़लम की रवानी का मैं क़ायल और आशिक़ हो गया। काश, मेरी क़लम में भी ये रवानी होती। बार-बार मैं, ये सोचता। फिर मुझे कृश्न से ब-यक-वक़्त (एक साथ) मुहब्बत और अदावत हो गई। जहां कहीं उसका कोई अफ़साना नज़र आता, मैं उसे बार-बार पढ़ता। बिल्कुल ऐसे, जैसे कभी किसी के नीले काग़ज़ वाले ख़त पढ़ा करता था। साथ में उसके स्टाइल पर रश्क आता, बल्कि हसद (ईर्ष्या) होता, जलन होती।
और जब कोई अफ़साना लिखने बैठता, तो ये कोशिश होती कि मेरे अफ़साने में भी कृश्न चंदर जैसी झलक आ जाए। उसकी नक्ल तो मैंने आज तक नहीं की, लेकिन ये ख़याल ज़रूर रहता कि कृश्न चंदर इस अफ़साने को पढ़े और पसंद करे, तब बात बने।
आज़ादी आने के बाद उसके क़लम में एक नई ताक़त आ गई। और उसने फ़सादात के बाद जो अफ़साने और नॉवेल लिखे, ‘पांच रुपए की आज़ादी’, ‘फूल सुर्ख़ हैं’ और तेलंगाना तहरीक पर ‘जब खेत जाग उठे’ वगैरह में आज़ादी के तख़य्युल (स्वतंत्रता की कल्पना) की जो इंक़लाबी तस्वीर उसने खींची है, वो किसी और का काम नहीं।
कृश्न चंदर के अफ़साने रूस में और दूसरी सोवियत ज़बानों में तर्जुमा होकर बहुत मक़बूल हुए हैं। “रूस जाकर देखो, तो हिंदुस्तान की तारीफ़ें भूल जाओगे।” मैंने कहा। और हुआ भी यही कि कृश्न चंदर के अफ़सानों की किताबें लाखों की गिनती में रूस और उसकी एशियाई रियासतों में शाए हुईं और वहां के लड़के-लड़कियां अगर फ़िल्में राजकपूर की पसंद करते थे, तो उनका महबूब अदीब कृश्न चंदर था।
और अब अर्थी को शमशान पहुंचा दिया गया है। एक जुलूस ने जिसमें सौ से ज़्यादा आदमी नहीं थे। ज़्यादातर लेखक और अदीब। सारे अदीब ख़िराज-ए-अक़ीदत पेश कर रहे थे।
कोई कहता है, “अदब का शहज़ादा चला गया।”
कोई कहता है, “वो उर्दू अदब का जवाहरलाल था।”
कोई कहता है कि “एक शोले को शोलों के सुपुर्द करने आए हैं।”
मैं कहता हूं कि वो न “अदब का शहज़ादा था”, न “अदब का जवाहरलाल”, वो तो “मेरा हमदम, मेरा दोस्त” था। उसके मरने से मैं खु़द मर गया हूं, अब और क्या कहूं?
“देखो, कृश्न ये सब जमा हैं। सरदार जाफ़री, भारती जी, कमलेश्वर, इंदर राज आनंद, रामानंद सागर, सी. एल. काविश, मजरूह, राजिंदर सिंह बेदी। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे यार। तुम्हारे हम मुशरिफ़ (जानकार)। तुम्हारे हमप्याला, हमनिवाला और आज ये सब तुम्हें जलाने आए हैं।”
ब-क़ौल सरदार जाफ़री, “एक शोले को शोलों के सुपुर्द करने आए हैं।”
“बोलो यार, कुछ तो बोलो।” कुछ नहीं तो हाथ का अंगूठा ऊपर करके कहो, “हम, तो अब चले ऊपर।”
(उर्दू से हिंदी लिप्यंतरण- ज़ाहिद ख़ान और इशरत ग्वालियरी।)






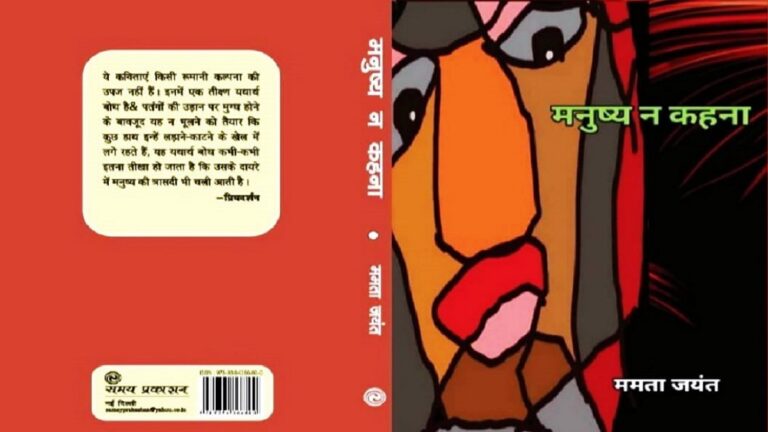





+ There are no comments
Add yours