उर्दू भाषा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान सोशल मीडिया में बहुत सुर्खियाँ बटोर रहा है, उनको लगता है कि उर्दू पढ़ने वाला कठमुल्ला बनता है। नेताओं के ऐसे बयान हलांकि कुछ लोगों को तकलीफ़ देते हैं लेकिन इनकी वजह से जो बहस चलती है उससे अकसर लोगों का फ़ायदा ही होता है। आज उर्दू को लेकर जो बहस हो रही है उससे आम लोगों की जानकारी और समझ में इज़ाफा ही हो रहा है।
उर्दू भले ही भारत में तेज़ी से ख़त्म की जा रही ज़बान है, लेकिन ये ज़बान ऐसी है कि सरकारों के तमाम सौतेले व्यवहारों के बावजूद ख़त्म नहीं हो रही है। मैंने कहा उर्दू तेज़ी से ख़त्म की जा रही ज़बान है, यानि ये ख़त्म हो नहीं रही है, बल्कि ख़त्म हो जाये इसकी कोशिश हो रही है। योगी जी के बयान को इसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए।
दरअसल, हिंदुत्व कि सियासत जिससे नफ़रत करती है उसे पहले मुसलमान से जोड़ती है फ़िर उस पर हमले करती है। जवाहरलाल नेहरू साहब को बार बार मुसलमान साबित करने की कोशिशें भी ऐसी ही हैं। हलांकि उर्दू विशुद्ध रूप से भारतीय भाषा है लेकिन पिछली सदी में उर्दू को भारत की ज़मीन से निकालने की और इसकी जगह हिन्दी को स्थापित करने की भरपूर कोशिश की गयी।
यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि उर्दू और हिन्दी दोनों की अम्मा एक ही भाषा है जिसको पहले हिन्दवी कहा जाता था, लेकिन जब यही ज़बान नागरी लिपि में लिखी जाने लगी तो इसमें संस्कृत के शब्द बढ़ाने और फारसी के शब्द घटाने की लगातार कोशिशों के नतीज़े में जो ज़बान बनी उसे ही आज हम हिन्दी कहते हैं, जबकि नस्तालीक लिपि में लिखी जा रही हिन्दवी आज उर्दू कहलाती है।
उर्दू कब मुसलमानों की ज़बान बना दी गयी ये तो शोध का विषय है, लेकिन ऐसा हो जाने के बाद उर्दू को सप्रयास मिटाने की कोशिशें भी हुईं, लेकिन चूंकि उर्दू को मुसलमान की ज़बान बना दी गयी है इसलिए मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए उर्दू के हक़ में भी सियासत खड़ी होती रही, इसलिए उर्दू किसी हद तक अपना वजूद बचा पायी है।
यहाँ ये स्वीकार करना ज़रूरी है कि नागरी लिपि में उच्चारण की जो आसानियाँ हैं, वो दूसरी लिपियों में नहीं है, इस लिहाज़ से अगर उर्दू के लिए नागरी लिपि का भी इस्तेमाल होता तो ये उर्दू के हक़ में बेहतर होता, आजकल इसकी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सप्रयास किसी ज़बान की हत्या करना तो किसी भी एंगल से जायज़ नहीं है।
उर्दू का विरोध कोई अचानक नहीं हुआ है, इस विरोध का भी एक इतिहास है, लेकिन इस इतिहास से ज़्यादा ज़रूरी है कि उर्दू ज़बान के इतिहास को थोड़ा सा जान लिया जाए।
10 वीं सदी के आसपास भारत में एक मिली जुली ज़बान आकार लेना शुरू करती है, जिसमें फारसी, तुर्की, अरबी, सिन्धी, ब्रज, अवधी और कुछ दूसरी बोलियों के अल्फ़ाज़ होते हैं। दरअसल भाषा या संस्कृति संसर्ग यानि मेल जोल से पैदा होती है, भारत में ये वो दौर था जब अरब, फारस, यूनान और सुदूरवर्ती इलाकों से व्यापार एक ख़ास मुक़ाम हासिल कर चुका था, इसके साथ ही भारत का आन्तरिक व्यापार भी लगातार बढ़ रहा था। व्यापार की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे थे, इसलिए उनकी भाषाएँ एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही थीं, भारत में उर्दू ज़बान इसी मिश्रण का परिणाम है।
ऐसा नहीं है कि अकेले उर्दू ही इस तरह निर्मित हुई, दुनिया की तमाम ज़बानें लगभग इसी तरह पैदा हुई हैं, आज आप किसी भी एक ऐसी भाषा का नाम नहीं ले पाएंगे जिसमें दूसरी भाषाओँ के शब्द न हों, यहाँ तक कि संस्कृत जिसे परिष्कृत भाषा कहा जाता है, उसमें भी पाली के शब्द मौजूद हैं। इस आधार पर शुद्धता के दावे को नासमझी या बदमाशी भी कहा जा सकता है।
बहरहाल 10 वीं सदी में आकार लेना शुरू करती हुई उर्दू ज़बान एकदम से आज की शक्ल में नहीं आयी, बल्कि वक्त के साथ उसके अल्फ़ाज़ और उनके उच्चारण में अंतर आया है, लेकिन जब भारत में मुस्लिम शासकों का दौर आया तो इस ज़बान ने भी अपने विकास में तेज़ी पकड़ी।
मुस्लिम शासकों के दौर में इसे एक समय खड़ी बोली, फ़िर रेख्ता और अंत में हिन्दवी या हिन्दुस्तानी कहा गया। हिन्दवी या हिन्दुस्तानी दरअसल भौगोलिक नाम है, यानि हिन्द वो एरिया जिसे हम भारत कहते हैं और हिन्दवी यानि इस इलाके के लोगों की बोली या भाषा।
अब हिन्द, हिन्दू, इंडस, इंडिया, जैसे अल्फ़ाज़ कब और कैसे बने, इनका मूल क्या है, ये एक अलग कहानी है, लेकिन आपकी जानने की ख्वाहिश हो तो आपका फ़ोन और इन्टरनेट की सुविधा चंद लम्हों में आपको इनकी कहानी बता देंगे। कुछ लोग उर्दू को लश्करी ज़बान, यानि सेनाओं की भाषा भी कहते हैं, लेकिन ये भी एक तरह का दुष्प्रचार ही है, सेनाओं ने इस ज़बान का उसी तरह इस्तेमाल किया है जैसे आन्तरिक और बाहरी व्यापारियों ने, इसलिए इसे सिर्फ़ लश्कर की ज़बान कहना एक ग़लती होगी।
बहरहाल 14 वीं सदी के बाद जैसे जैसे इस देश में मुसलमानों की हुकूमत क़ायम हुई फ़ारसी शासक वर्ग की और उर्दू पढ़े लिखे आम लोगों की भाषा बन गयी, जबकि आम जनता उन बोलियों से काम चलाती रही जिसे क्षेत्र विशेष में बोला जाता है।
यहाँ इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि आज भले ही धर्म के आधार पर उर्दू का विरोध हो रहा है लेकिन मुस्लिम शासकों के दौर में ब्राह्मणों और कायस्थों ने खुले दिल से उर्दू और फ़ारसी को अपनाया क्योंकि शासक वर्ग से जुड़ने के लिए ये ज़रूरी था, ये बिलकुल वैसा ही था जैसे ब्रिटिश हुकूमत के दौर में भारतीय मध्यम और उच्च वर्ग ने अग्रेजी को गले लगाया था या कि आज भी सत्ता प्रतिष्ठानों और बाज़ार में जगह बनाने के लिए जैसे अंग्रेजी भाषा पर मज़बूत पकड़ ज़रूरी है।
बहरहाल, मुस्लिम शासकों के दौर में उर्दू एक भाषा के तौर पर पढ़े लिखों की भाषा बनी तो इसी दौर में उर्दू साहित्य ने भी वो तरक्की हासिल की जिसका असर आज भी न सिर्फ़ उर्दू बल्कि हिन्दी भाषा पर भी देखा जा सकता है। यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि उर्दू भाषा और उर्दू साहित्य के विकास में मुसलमानों के साथ ही हिन्दुओं का भी बड़ा योगदान है, उर्दू अदब या साहित्य की चर्चा इनके नामों को हटा कर करना मुमकिन नहीं है।
19 वीं सदी में हिन्दवी या उर्दू को नागरी लिपि में लिखने की शुरुआत हुई। 1893 में वाराणसी में बनी नागरी प्रचारणी सभा ने नागरी लिपि में लिखने पढ़ने को खूब प्रचारित किया, आज की हिन्दी को ये रूप और आकार देने में इस सभा का बड़ा योगदान है। लेकिन जैसे जैसे हिन्दी विकसित हुई उसी के समानांतर उर्दू का विरोध भी शुरू हुआ और आज़ाद भारत में ये विरोध वक्त के साथ तेज़ होता चला गया, इसी विरोध के क्रम में उर्दू जो भारतीयों की भाषा रही है, उसे मुसलमानों की भाषा के तौर पर प्रचारित किया गया, यानि उर्दू बनाम हिन्दी का विवाद एक साम्प्रदायिक विवाद है और साम्प्रदायिकता कैसे इस देश को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
इस सबके बावजूद चूंकि हिन्दवी हिन्दी और उर्दू दोनों की अम्मा है, इसलिए तमाम कोशिशों के बावजूद उर्दू से हिन्दी और हिन्दी से उर्दू को अलग नहीं किया जा सकता।
(सलमान अरशद का लेख)






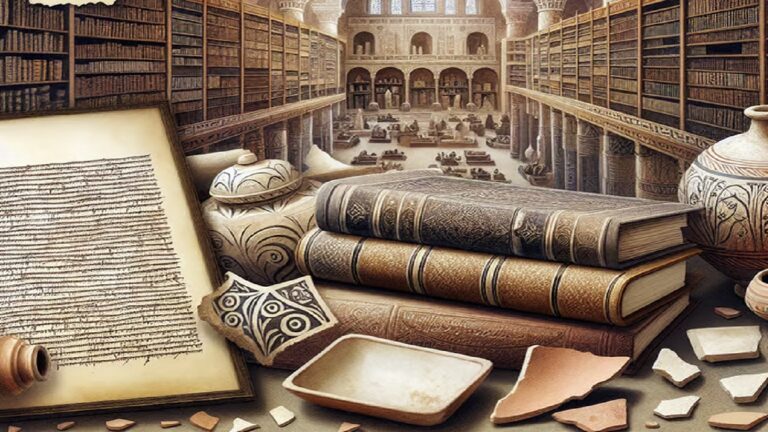
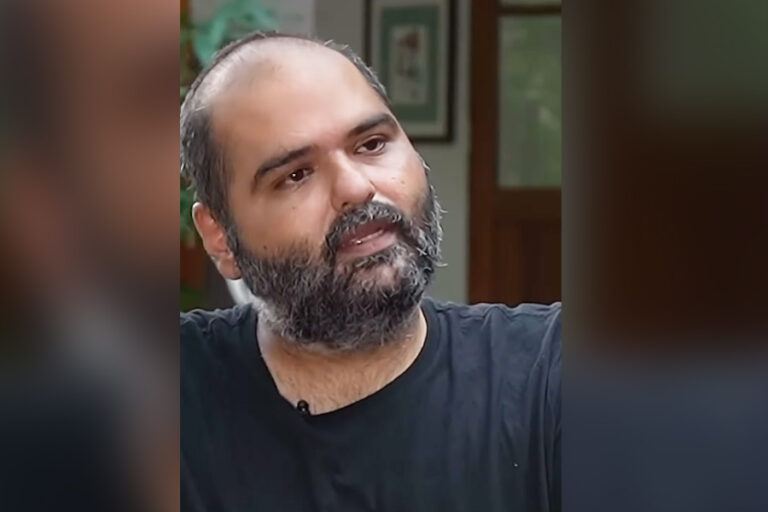




+ There are no comments
Add yours