भारत में वक्फ कानून सिर्फ एक कानूनी ढांचा नहीं, बल्कि मुसलमानों की धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। यह कानून उन संपत्तियों को लेकर बना है, जिन्हें मुसलमान अल्लाह की राह में वक्फ कर देते हैं, यानी हमेशा के लिए दान कर देते हैं, ताकि उनका इस्तेमाल मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, अस्पताल या किसी भी तरह के कल्याणकारी काम में हो सके। ऐसी संपत्ति अब किसी व्यक्ति की निजी मिल्कियत नहीं रहती, बल्कि पूरी कौम की अमानत बन जाती है। भारत में इसका इतिहास अंग्रेजों के ज़माने से शुरू होता है, लेकिन आज़ादी के बाद इसे औपचारिक रूप से कानून का दर्जा दिया गया-पहले 1954 में और फिर 1995 में, जब वक्फ अधिनियम को नया ढांचा मिला।
इसके बाद 2013 में कुछ अहम संशोधन हुए, लेकिन असली हंगामा 2025 में हुआ, जब मोदी सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम लागू किया। इस नए संशोधन ने न सिर्फ मुस्लिम समाज को बेचैन किया, बल्कि सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी। लोगों ने इसे संविधान के खिलाफ बताया, धार्मिक मामलों में दखल माना, और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा।
अब बात करें वक्फ कानून की बुनियादी बातों की, तो सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि वक्फ क्या होता है। कोई भी मुसलमान अपनी चल या अचल संपत्ति को अल्लाह की राह में वक्फ कर सकता है, और फिर वह संपत्ति अल्लाह के नाम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि न तो वह व्यक्ति और न ही उसके वारिस उस संपत्ति को बेच सकते हैं, बांट सकते हैं, या निजी फायदे में ला सकते हैं। उस संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ वही हो सकता है, जो मकसद वक्फ करते वक्त बताया गया हो-जैसे कि मदरसा चलाना, अनाथ बच्चों की परवरिश करना, या अस्पताल बनाना। यानी अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति वक्फ की हुई संपत्ति के मूल स्वरूप को बदल नहीं सकता।
वक्फ की स्थापना दो तरीकों से हो सकती है-एक लिखित दस्तावेज, यानी वक्फनामा के ज़रिए, और दूसरा मौखिक ऐलान के ज़रिए। लेकिन दोनों ही सूरतों में यह साफ ज़ाहिर होना चाहिए कि कौन-सी संपत्ति वक्फ की जा रही है और उसका मकसद क्या है। एक बार अगर कोई चीज़ वक्फ हो गई, तो फिर उसे रद्द नहीं किया जा सकता, सिवाय कुछ बेहद खास सूरतों के।
वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए दो संस्थाएं होती हैं-केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड। केंद्रीय वक्फ परिषद सलाह देती है और नीतियां तय करती है, जबकि राज्य वक्फ बोर्ड हर राज्य में वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख, सर्वे, और विवादों का निपटारा करता है। वक्फ संपत्ति की देखभाल करने वाला व्यक्ति “मुतवली” कहलाता है।
अब कानून में एक अहम बात यह है कि वक्फ संपत्तियों का नियमित सर्वे किया जाता है। 1995 के अधिनियम की धारा 4 कहती है कि राज्य वक्फ बोर्ड के ज़रिए सर्वे किया जाए और हर संपत्ति का रिकॉर्ड रखा जाए। वहीं, धारा 40 वक्फ बोर्ड को यह ताकत देती थी कि वह किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सके, अगर उसे लगे कि वह वाकई वक्फ की है।
वक्फ से जुड़े कानूनी विवादों का निपटारा वक्फ ट्रिब्यूनल करता है, और धारा 85 के मुताबिक, आम अदालतों को वक्फ मामलों में दखल देने का हक नहीं है। सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है।
वक्फ संपत्तियों की एक खास बात यह है कि उन पर कब्जे के मामलों में लिमिटेशन एक्ट की धारा 107 लागू होती है, यानी अगर किसी ने वक्फ की ज़मीन पर कब्जा कर भी लिया है, तो समय की कोई पाबंदी नहीं है-कभी भी उसे हटाया जा सकता है।
अब बात करें 2025 के वक्फ संशोधन कानून की, तो यह सबसे विवादास्पद बदलाव लेकर आया। इसे 8 अप्रैल 2025 से लागू किया गया, और सरकार का दावा है कि यह पारदर्शिता, जवाबदेही, और बेहतर प्रबंधन के लिए है। लेकिन मुस्लिम समाज का कहना है कि इसके पीछे एक सियासी एजेंडा है-वक्फ संपत्तियों को कमजोर करना और धार्मिक मामलों में दखल देना।
इस नए कानून में कई बदलाव हुए। मसलन, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में अब गैर-मुस्लिमों और महिलाओं को भी जगह देने का प्रावधान कर दिया गया है। यह वाक्य मीडिया से लिया गया है; पिछले वाक्य में “भी” एक छलावा है। सच तो यह है कि पहले भी वक्फ बोर्ड में कम से कम दो महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान था, अब अधिक से अधिक दो महिलाएं शामिल हो सकती हैं। इस स्पष्टीकरण की ज़रूरत इसलिए है, ताकि आप जान सकें कि मुख्यधारा की मीडिया कैसे भाषा के साथ एक दल विशेष के पक्ष में छल करती है।
पहले यह शर्त थी कि वक्फ परिषद का हर सदस्य (मंत्री को छोड़कर) मुसलमान होना चाहिए, लेकिन अब सांसद, जज, या प्रतिष्ठित लोग, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, इसमें शामिल हो सकते हैं। यहां यह ध्यान रखना होगा कि हिंदुओं के धर्मार्थ ट्रस्टों आदि में मुसलमान तो छोड़िए, सभी वर्गों के हिंदू भी शामिल नहीं हो सकते। अब यह सवाल चर्चा में है कि सरकार वक्फ बोर्ड, जो मुस्लिम दानकर्ताओं की संपत्ति के प्रबंधन के लिए बना है, में हिंदुओं को शामिल करना क्यों चाहती है।
दूसरा बड़ा बदलाव सर्वे प्रक्रिया में हुआ है। अब वक्फ संपत्तियों का सर्वे ज़िला कलेक्टर करेगा, न कि सर्वेक्षण आयुक्त। यानी अब जो तय करेगा कि कौन-सी संपत्ति वक्फ है या नहीं, वह एक सरकारी अफसर होगा।
तीसरा बड़ा मुद्दा धारा 40 को हटाने का है। पहले वक्फ बोर्ड के पास यह ताकत थी कि वह किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता था, लेकिन अब यह अधिकार राज्य सरकार के किसी नामित अधिकारी को दे दिया गया है। इसका मतलब है कि अब सरकार की मंजूरी के बिना कोई संपत्ति वक्फ नहीं हो सकेगी। यह अंश भी मैंने मीडिया से लिया है।
हकीकत यह है कि आज भी सालों पुरानी बहुत-सी वक्फ संपत्तियां वक्फ के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन उनका किसी न किसी रूप में वक्फ संपत्ति की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर के पैराग्राफ में ऐसी ही संपत्तियों को वक्फ घोषित करने की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि वक्फ के लोग कल नींद से उठें और कह दें कि संसद तो वक्फ संपत्ति है, और हमें हमारी संसद से हाथ धोना पड़े। हालांकि, नफरती सियासत का प्रचार यही कर रहा है।
इसके अलावा, वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, वित्तीय ऑडिट, केंद्रीय पोर्टल, और पारदर्शी प्रबंधन के नाम पर कई नई व्यवस्थाएं लाई गई हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चिंता की वजह बनी, वह यह है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल में मुसलमानों को कानून की समझ रखने वाले सदस्य की जगह एक ज़िला जज और एक संयुक्त सचिव रैंक का अफसर नियुक्त किया जाएगा। इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ के जानकारों की भूमिका लगभग खत्म हो जाएगी।
और शायद सबसे ज्यादा विवाद खड़ा करने वाला नियम यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वक्फ संपत्ति पर 12 साल से ज्यादा समय से कब्जा किए हुए है, तो अब उसे मालिकाना हक भी मिल सकता है। इस प्रावधान को मुसलमानों ने सीधे-सीधे वक्फ संपत्तियों पर हमले के तौर पर देखा है।
इसके अलावा, वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं की अनिवार्य नियुक्ति और बोहरा, आगाखानी जैसे अन्य समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने की व्यवस्था भी इस संशोधन में शामिल है।
अब जब इतना कुछ बदला है, तो सवाल उठता है-क्या यह सब संविधान के मुताबिक है? कई याचिकाकर्ताओं का जवाब है-नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह कहा कि वक्फ संशोधन कानून, 2025 भारत के संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है।
अनुच्छेद 14 के तहत हर नागरिक को समानता का हक है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर हिंदू मंदिर ट्रस्टों या चर्च बोर्डों में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ, तो सिर्फ वक्फ कानून में क्यों? क्या यह मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं है?
अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव से मना करता है, लेकिन यह संशोधन सीधे-सीधे मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों को टारगेट करता है। अन्य समुदायों को कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ वक्फ संपत्तियां ही निशाने पर हैं।
अनुच्छेद 25 धार्मिक आज़ादी का हक देता है। लेकिन अगर वक्फ संपत्तियों के फैसले अब कलेक्टर करेगा, तो क्या यह धार्मिक मामलों में सरकारी दखल नहीं होगा?
अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों का खुद प्रबंधन करने का अधिकार देता है। लेकिन अगर गैर-मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा, तो क्या यह उस हक में सीधा दखल नहीं है?
अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाए रखने का अधिकार देता है। लेकिन यह संशोधन उस पहचान को ही कमजोर करता है।
अनुच्छेद 300A संपत्ति के हक की बात करता है। लेकिन अगर कोई 12 साल से कब्जा करके बैठा है और उसे मालिकाना हक मिल जाए, तो यह वक्फ की मिल्कियत पर हमला नहीं तो और क्या है?
इन सभी सवालों के जवाब अभी सुप्रीम कोर्ट में तलाशे जा रहे हैं। 15 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की और कुछ अंतरिम फैसले भी दिए। सबसे पहली बात, अदालत ने गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी। दूसरी अहम बात यह कि अदालत ने वक्फ “बाय यूज़र” की परंपरा को बरकरार रखा-यानी जो ज़मीनें बरसों से मस्जिद, मदरसे, या कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल होती आ रही हैं, उन्हें वक्फ ही माना जाएगा। तीसरी बात, जब तक फैसला नहीं आता, तब तक किसी भी वक्फ संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। और आखिर में, अदालत ने केंद्र सरकार से सारे संवैधानिक मुद्दों पर विस्तृत जवाब मांगा है।
इन अंतरिम फैसलों से मुस्लिम समाज को कुछ राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। अदालत ने साफ कहा है कि वह जल्दबाज़ी में कोई फैसला नहीं लेगी, बल्कि केंद्र को पूरा मौका देगी अपनी दलीलें पेश करने का।
अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसका असर पूरे देश की सियासत पर भी पड़ रहा है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं, और मुस्लिम संगठन इसे अपने धार्मिक हकों पर हमला मान रहे हैं। यह बहस सिर्फ एक कानून की नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों की धार्मिक पहचान, उनकी संपत्तियों की हिफाज़त, और भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे की असलियत की भी है।
जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून आया है और जिस अंदाज़ में इसके प्रावधान लागू किए जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि मामला सिर्फ सुधार या पारदर्शिता का नहीं है। यह सत्ता की उस सोच को भी ज़ाहिर करता है, जो धार्मिक आज़ादी और सांस्कृतिक अधिकारों को “प्रशासनिक सुधार” के नाम पर सीमित करना चाहती है।
लेकिन क्या भारत जैसे विविधता भरे लोकतंत्र में यह मुमकिन है? क्या अदालतें और जनता इसे चुपचाप स्वीकार कर लेंगी? क्या मुसलमान अपने धार्मिक अधिकारों की हिफाज़त कर पाएंगे, या यह भी एक लंबी अदालती लड़ाई में दब जाएगा?
सवाल बहुत हैं, जवाब धीरे-धीरे सामने आएंगे-लेकिन यह तय है कि वक्फ कानून पर यह बहस भारत के संविधान, धर्मनिरपेक्षता, और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए एक कसौटी बन चुकी है।
(डॉ. सलमान अरशद स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)








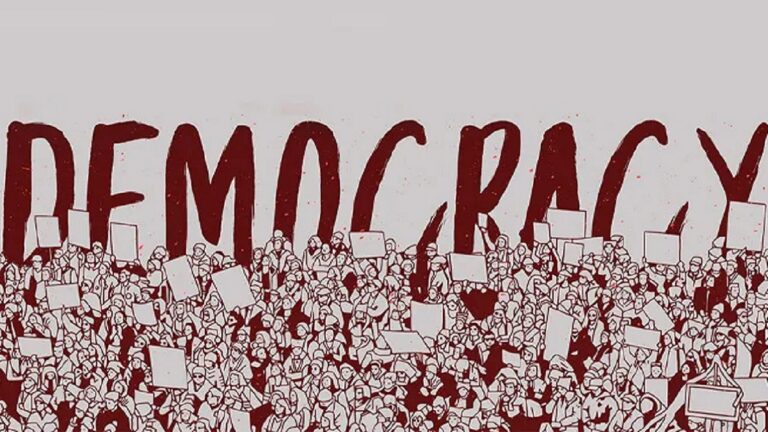



+ There are no comments
Add yours