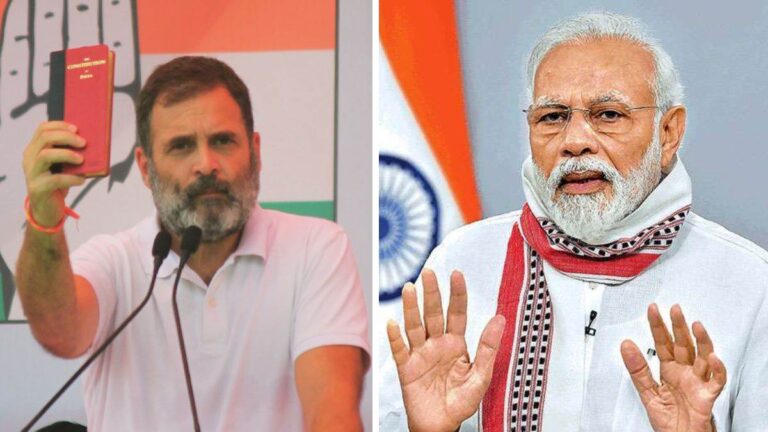साढ़े आठ महीनों से फिलस्तीन के ग़जा में इजराइली नरसंहार जारी है। इसमें 37,400 से अधिक फिलस्तीनी मारे जा चुके हैं। यह आधिकारिक आंकड़ा है। नरसंहार के कारण इलाज सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं के पैदा हुए अभाव से हुई मौतों को भी अगर शामिल करें, तो यह आंकड़ा 45 हजार के ऊपर जाता है। इनमें लगभग दो तिहाई महिलाएं और बच्चे हैं। 77 हजार से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। 15 लाख से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। जाहिर है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद मानवीय अपराध के ऐसे नजारे दुनिया के सामने पेश नहीं आए थे।
कहा जा सकता है कि बीते सात अक्टूबर को हमास ने इजराइली कब्जे वाले इलाकों पर जो हमले किए, उनकी बेहद महंगी कीमत- खासकर ग़जा स्थित फिलस्तीनी आवाम ने चुकाई है। वैसे इसकी जद में पश्चिमी किनारे के निवासी भी आए हैं और आंच लेबनान तक पहुंची है।
अगर सिर्फ इन्हीं बातों को ध्यान में रखा जाए, तो यह धारणा बन सकती है कि हमास ने एक दुस्साहसी कार्रवाई की थी- इस दुस्साहस का कुछ नुकसान उसे भी झेलना पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी कीमत आम फिलस्तीनियों ने चुकाई है। बहरहाल, यह इस कहानी का सिर्फ एक पक्ष है। जबकि अब तकरीबन नौ महीने बाद इस कहानी का दूसरा पक्ष भी उभरता दिख रहा है।
उस पक्ष पर गौर करें, तो हम यह सोचने को भी प्रेरित हो सकते हैं कि हमास ने संभवतः जो गणनाएं (calculations) की थीं, वह सटीक बैठी हैं। अब यह दीगर सवाल है कि क्या किसी संगठन को इतने बड़े पैमाने पर मासूम लोगों की जान को दांव पर लगाते हुए कोई जोखिम मोल लेना चाहिए? परंतु फिलस्तीनियों के नजरिए से देखें, तो जिन लोगों को रोजमर्रा के स्तर पर अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा हो और जिनके आत्म-सम्मान एवं स्वतंत्रताओं का निरंतर उल्लंघन किया जा रहा हो, उनके सामने क्या विकल्प बचता है? एक पूरी आबादी को अगर उसकी परंपरागत जमीन से बेदखल कर दिया गया हो और जिसे आगे अपना कोई भविष्य नज़र नहीं आता हो, तो यह मुमकिन है कि किसी मुकाम पर आकर वह अपना सब कुछ दांव पर लगाने को मजबूर हो जाए।
बेशक हमास ने एक ऐसा दांव लगाया। और अब तकरीबन नौ महीने बाद सूरत यह है कि इजराइल अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट में फंसा दिख रहा है। बल्कि धारणा तो यह बनने लगी है कि जिस Zionist प्रोजेक्ट के तहत एक औपनिवशिक योजना के रूप में इस कृत्रिम देश को स्थापित किया गया था (इजराइल का वजूद ही उकसावे की जड़ है! – जनचौक (janchowk.com)), आज उसका अस्तित्व खतरे में है। और उसके साथ ही पश्चिम एशिया क्षेत्र में उस औपनिवेशिक योजना के सूत्रधारों की भी साख और रसूख डगमगाते दिख रहे हैं। इस योजना का आरंभिक सूत्रधार ब्रिटेन था। बाद में इसे कायम रखने की जिम्मेदारी अमेरिका ने संभाल ली थी।
तो आज सूरत क्या है?
Zionist प्रोजेक्ट के तहत दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बसे इजराइलियों को लाकर फिलस्तीन की जमीन पर यहूदी देश बनाने की योजना को कार्यरूप दिया गया था। लगभग 70 साल तक इसके लिए चले अभियान के बाद 1948 में यह मकसद पूरा हुआ। उसके बाद 75 साल गुजर चुके हैं। इस पूरी अवधि में यहूदी समुदाय के बीच इजराइल के स्वरूप को लेकर उतने गहरे मतभेद कभी नहीं थे, जितने आज नज़र आ रहे हैँ।
वैसे ये मतभेद सात अक्टूबर के पहले ही सड़कों पर जाहिर हो रहे थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके कट्टरपंथी समर्थक इजराइल को धर्मसत्ता (theocracy) में तब्दील करने की राह पर आगे बढ़े हैं। जबकि यहूदियों का एक बड़ा धड़ा राज्य-व्यवस्था को धर्म-निरपेक्ष, उदार और आधुनिक रखना चाहता है। वैसे, जहां तक फिलस्तीनियों को बेदखल करने का मकसद है, उसमें इन दोनों समूहों में पूरी सहमति रही है। मगर एक राष्ट्र-राज्य के रूप में इजराइल के स्वरूप को लेकर उनमें हमेशा ही आपसी मतभेद थे। पहले उदार समूहों के लोग भारी पड़े। लेकिन गुजरे 20-25 वर्षों में कहानी पलट गई है।
इधर, सात अक्टूबर से लेकर अब तक कई अहम घटनाएं हुई हैं। सात अक्टूबर को हमास ने इजराइल के अभेद्य होने का भ्रम तोड़ दिया। इजराइल के खौफ पैदा करने वाली बहुचर्चित खुफिया तंत्र की कमजोरियां और नाकामियां उस रोज जग-जाहिर हो गईं। उसके बाद से इजराइल ने जो बदले की कार्रवाई की, सैनिक उद्देश्य के लिहाज से वह साढ़े आठ महीनों में कहीं नहीं पहुंची है। हमास आज भी मौजूद है। इन घटनाओं ने इजराइली आबादी में मत-विभाजन को अत्यंत तीखा बना दिया है। इस दौर में इजराइल में असुरक्षा एवं भविष्य-हीनता की आशंकाएं इस हद तक गहरा गई हैं कि पांच लाख यहूदी हमेशा के लिए देश छोड़ चले गए हैँ।
धनी इजराइली अपने देश से निवेश को निकालना शुरू कर चुके हैं। हर गुजरते महीने के साथ अपना पैसा और संपत्ति पश्चिमी देशों में ले जाने की रफ्तार तेज होती गई है। एक हालिया सर्वे से सामने आया कि देश के अंदर 80 फीसदी टैक्स देने वाले 20 प्रतिशत धनी इजराइली अपने निवेश को कहीं और ले जाने पर विचार कर रहे हैं। युद्ध पर भारी खर्च और लाल सागर संकट के कारण क्षतिग्रस्त हुए कारोबार की वजह से इजराइल का आर्थिक एवं वित्तीय संकट बेहद बढ़ा है। यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि इजराइल अपने अस्तित्व के लिए अधिक से अधिक अमेरिका पर निर्भर होता जा रहा है। अमेरिका ने 14 बिलियन डॉलर की मदद देने का एलान किया है, लेकिन संकट के परिमाण को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि ये रकम पर्याप्त साबित होगी।
इस बीच नरसंहारी नजरिए के कारण अंतरराष्ट्रीय जगत में इजराइल तेजी से अलग-थलग पड़ता गया है। पश्चिम एशिया के पड़ोसी देशों के साथ संबंध सामान्य होने की प्रक्रिया के आगे बढ़ने की बात तो दूर, अब सामान्य संबंध वाले देशों के साथ भी रिश्तों में अवरोध पैदा हो गए हैं। तुर्किये और कोलंबिया जैसे देशों ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत कर दी है। इस बीच अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने इजराइल के खिलाफ जो टिप्पणियां कीं या जो कदम उठाए हैं, उससे यह जाहिर हुआ कि अब अमेरिकी (या पश्चिमी) कवच इजराइल की हर हाल में रक्षा करने में कमजोर साबित हो रहा है।
असल में कवच प्रदान करने के चक्कर में इन देशों ने अपना बड़ा नुकसान कर लिया है। आज ग्लोबल साउथ में इन देशों का कोई अख़लाक नहीं बचा। लोकतंत्र और मानव अधिकारों का जो डंडा वे चलाते थे, आज उसकी कोई नैतिक साख नहीं बची है। इसके विपरीत इस संकट ने उनके प्रतिद्वंद्वी चीन और रूस की स्वीकार्यता बढ़ाने में योगदान किया है। इसके दूरगामी परिणामों का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।
इजराइल के पक्ष में ग्लोबल साउथ- खास कर पश्चिम एशिया के देशों को लामबंद करने में अमेरिका की नाकामी ने उसकी निष्प्रभावी होती कूटनीतिक क्षमता और घटते रुतबे को रेखांकित किया है। फिलस्तीनियों के समर्थन में यमन स्थित अंसारुल्लाह (हूती) ने जो मुहिम छेड़ी, उसके खिलाफ अमेरिका की नाकामी ने उसकी सैनिक क्षमताओं को भी अधिक संदिग्ध बना दिया है। (We Spent a Billion Dollars Fighting the Houthis…and Lost – The Ron Paul Institute for Peace & Prosperity)
पश्चिमी देशों में इजराइल को समर्थन देने को लेकर हमेशा से मौजूद रही आम-सहमति भी हाल के महीनों में टूट गई है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में जिस बड़े पैमाने पर इजराइल विरोधी छात्र आंदोलन देखने को मिले, वह अभूतपूर्व है। खास यह है कि इजराइल विरोधी मुहिम में बड़ी संख्या में युवा यहूदी भी शामिल हुए हैं। जाहिरा तौर पर, यहूदियों की नई पीढ़ी पूरे परिदृश्य को नए नजरिए से देख रही है। Zionism उनकी सोच का केंद्रीय बिंदु नहीं रह गया है।
इस संदर्भ में यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि Zionism (यहूदीवाद) और Judaism (यहूदी धर्म) दो अलग बातें हैं। Judaism एक महजब है, जबकि Zionism एक राजनीतिक परियोजना रही है। इसलिए यहूदी धर्म और यहूदीवाद को समानार्थी नहीं समझाना चाहिए। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में रहने वाले युवा यहूदी अब इस फर्क को अधिक गहराई से समझ रहे हैं। वे उस परियोजना से खुद को जोड़ने को इच्छुक नहीं हैं, जो नरसंहार का कारण बनी है। बल्कि ऐसे नौजवानों की काफी संख्या है, जो Zionism को अपने धर्म की बदनामी के रूप में देखने लगे हैं। इस परिघटना का दूरगामी असर होगा। अमेरिका में इजराइली लॉबी खास मजबूत रही है। लेकिन अगली पीढ़ी में भी ऐसा रहेगा, इसकी संभावना अब कम मालूम पड़ती है।
और सात अक्टूबर के हुई घटनाओं का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ है कि नई पीढ़ी के फिलस्तीनियों में अब अपने उद्देश्य के प्रति एक नया संकल्प देखने को मिल रहा है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फैले ये फिलस्तीनी पश्चिमी किनारे पर स्थित फिलस्तीनी प्राधिकरण और उसके नेतृत्व के समझौतावादी रुख से घोर असंतुष्ट हैं। वे फिलस्तीन के एक नए भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। उनकी चर्चाओं से संकेत मिलता है कि उनकी नई कल्पना आधुनिकता और लोकतंत्र की भावनाओं से प्रेरित है। वे ऐसा फिलस्तीन चाहते हैं, जहां मुसलमान, यहूदी, ईसाई आदि सभी धर्मों के लोग तमाम तरह के भेदभाव से मुक्त होकर समान मौलिक अधिकारों के साथ रहें। ये सभी लक्षण दीर्घकालिक महत्त्व के हैं।
तात्कालिक तौर पर जो संभावना साफ नजर आ रही है, वह Zionism का ढहना है। अगर यह विचार ढहता है, तो मौजूदा स्वरूप में इजराइल का बने रहना कठिन हो जाएगा। इस रूप में कहा जा सकता है कि वर्तमान युद्ध में भले कुछ मोर्चों पर इजराइल भारी पड़ता दिखा हो, लेकिन उसके युद्ध जीत सकने की संभावना लगातार क्षीण होती जा रही है। यह घटनाक्रम पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों की दुनिया पर कमजोर होती पकड़ का भी एक ठोस संकेत है। इससे यह संकेत मिला है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था एक नई सुबह की ओर स्थिर गति से बढ़ रही है। इजराइल-फिलस्तीन युद्ध ने इस परिघटना को और अधिक बल प्रदान कर दिया है।
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं)