वाराणसी। बनारस की गर्म दोपहर थी। धूप, जैसे आसमान से नहीं, ज़मीन के अंदर से निकल रही हो। उस तपिश के बीच एक अधजली औरत अपनी झोपड़ी की राख को ऐसे घूर रही थी, जैसे अभी भी उसमें कुछ बाकी हो-कोई सपना, कोई याद, कोई उम्मीद। उनका नाम है मीरा बनवासी। उम्र ज़्यादा नहीं, लेकिन चेहरा अब उम्र से कहीं ज़्यादा जला हुआ। उनकी आंखें कुछ कहती हैं, मगर आवाज़ नहीं निकलती। जब वो कहती हैं, “मेरा बेटा दीपक मड़ई में सो रहा था… मैं नहाकर निकली ही थी… जब देखा कि पूरी मड़ई धधक रही है… बचाने दौड़ी तो खुद भी जल गई…”-तो लगता है कि यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि एक पूरे तबके की त्रासदी है।
घटना 31 मार्च 2023 की है। ग्राम खरगूपुर, पोस्ट हाथी, ब्लॉक सेवापुरी, थाना जंसा, जिला वाराणसी। यही वह जगह है जहां मीरा बनवासी और उनके जैसे 10-12 बनवासी परिवार सालों से रहते आए हैं। इनकी बस्ती सड़क किनारे है, ज़मीन सरकारी है, लेकिन जीवन का संघर्ष पूरी तरह निजी और पीड़ादायक है। झोपड़ी में गुजर-बसर करने वाले ये परिवार कहीं से भी गैरकानूनी नहीं लगते-क्योंकि इनमें जीवन है, श्रम है, और ज़मीन से मोहब्बत है। लेकिन शायद यही मोहब्बत कुछ लोगों को खटकती है।
मीरा बताती हैं कि घटना वाले दिन वह अपने बेटे दीपक को मड़ई में सुलाकर नहा रही थीं। उसी समय एक स्थानीय व्यक्ति वहां से गुज़रा और उसके जाते ही मड़ई धधकने लगी। मीरा ने जब आग देखी तो बच्चे को बचाने दौड़ीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे खुद भी जल गईं। उनका आधा चेहरा और शरीर बुरी तरह झुलस गया। बेटे को किसी तरह बाहर निकाला, लेकिन उसकी आंखों में डर स्थायी हो चुका है।
मीरा की झोपड़ी के साथ-साथ सरिता और प्रेमा की मड़इयां भी जल गईं। ये सब उस समय घर में नहीं थीं, लेकिन जब लौटीं तो उनका संसार राख हो चुका था। गेहूं, चावल, कपड़े, राशन, दवाएं, बच्चों की किताबें, मुंडन के लिए रखी गई जमा पूंजी, मोबाइल फोन-हर चीज़ उस आग में समा गई, जो शायद सिर्फ़ लकड़ियों को नहीं, आत्माओं को भी जलाने आई थी।
पुलिस? हां, मीरा और अन्य पीड़ित जंसा थाना पहुंचे। लेकिन वहां उन्हें ‘शिकायतकर्ता’ की बजाय ‘संदिग्ध’ की तरह देखा गया। कहा गया, “खुद ही आग लगाई होगी।” यह वाक्य सिर्फ एक ताना नहीं, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था की तस्वीर है जहां गरीबों की बात पहले शक के दायरे में आती है, और कभी न्याय के पन्नों तक पहुंच ही नहीं पाती।
खरगूपुर बस्ती की गूंगी चीख
मीरा ने बनारस के पांडेयपुर स्थित मानवाधिकार जननिगरानी समिति को एक पत्र लिखा-एक पुकार, एक दस्तावेज़ जो सिर्फ घटना का विवरण नहीं, बल्कि उस दर्द का दस्तावेज़ है जो प्रशासनिक चुप्पी से कहीं अधिक जलाता है। पत्र में मीरा ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि गांव के एक दबंग व्यक्ति की नज़र सड़क किनारे की ज़मीन पर है, जहां ये बनवासी सालों से रह रहे हैं। यही कारण है कि उस बस्ती को जलाने की कोशिश हुई। जब आग लगी, वह व्यक्ति वहां मौजूद लोगों से कहता रहा-“जलने दो…”, लेकिन बस्ती के लोगों ने मिलकर आग बुझाई। चेहरा झुलसा हुआ, शरीर पर फफोले, और मन में एक ही सवाल-“हमने क्या बिगाड़ा था?” वे बार-बार कहती हैं-“वो घर ही तो था हमारा… अब कहां जाएंगे?”
खरगूपुर मुसहर बस्ती के लोगों का कहना है कि घटना जानबूझकर करवाई गई। कारण? वह ज़मीन, जहां ये परिवार बसे हैं, अब कीमती हो गई है। शहर फैल रहा है, सड़क चौड़ी हो रही है, और ऐसे में ‘झोपड़पट्टी’ आंख की किरकिरी बन चुकी है। इसलिए अब इन्हें हटाया जाना है। लेकिन हटाया कैसे जाए? कानूनी तरीका लंबा है, तो क्यों न डर, दहशत और आग से रास्ता साफ़ किया जाए?
इस हादसे में सरिता की मड़ई भी खाक हो गई। वो अकेली महिला हैं। उनके पति पिंटू की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। एक बेटा, एक बेटी और एक उजड़ चुकी गृहस्थी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। उनकी हालत ऐसी नहीं कि इलाज करा सकें। उनके पास न इलाज के पैसे हैं, न रहने की जगह। अनाज, बर्तन, कपड़े-सब राख हो चुके हैं। यहां तक कि घर के बाहर लगे सहजन और जामुन के पेड़ तक इस आग की चपेट में आ गए। गांव के बच्चों के खेलने के झूले अब जल चुके हैं, और उस राख के ढेर पर नंगे पांव चलती मीरा की बेटी अब भी पूछती है-“मम्मी, हमारा घर कब बनेगा?”
चश्मदीद सूरज, भारती और अन्य ग्रामीणों ने साफ़ कहा है कि यह आग ज़रूर जानबूझकर लगाई गई थी। लेकिन पुलिस की भूमिका पहले दिन से ही संदिग्ध रही। एफआईआर दर्ज नहीं हुई। दबंगों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कोई राहत नहीं दी गई। जब पीड़ितों ने थाने में दोबारा रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, तो उन्हें कह दिया गया, “थाना पुलिस की ओर से कह दिया गया कि पारिवारिक मामला है।” इस एक वाक्य ने इंसाफ के सारे दरवाज़े बंद कर दिए।
इस बस्ती की राख अब भी उड़ी नहीं है। हवा में अब भी धुएं की हल्की गंध है। लेकिन सबसे गहरी गंध उस अन्याय की है, जो सिर्फ़ यहां नहीं, देश के हर कोने में महसूस की जा सकती है। यह कहानी बनारस की है, लेकिन इसके किरदार हर शहर, हर गांव में मिल जाएंगे-मीरा की जगह कभी राधा होगी, कभी फातिमा, कभी चंद्रा… लेकिन दर्द एक जैसा होगा।
सवाल यह नहीं है कि मीरा, प्रेमा और सरता को इंसाफ मिला या नहीं? सवाल यह है कि जब कोई मां झुलस जाती है, उसका बच्चा मरते-मरते बचता है, तब भी अगर व्यवस्था कहे “पारिवारिक मामला है”, तो इंसाफ का रास्ता कहां बचेगा? मीरा आज भी अपनी झोपड़ी की राख के पास बैठकर इंतज़ार कर रही हैं-शायद कोई सुने, शायद कोई देखे, शायद कोई लिखे… ताकि दुनिया को पता चले कि झोपड़ी के साथ उनके सपने भी जल गए।
31 मार्च की उस रात जब आग लगी, तो बस झोपड़ियां नहीं जलीं, एक पूरी जिंदगी का सामान भस्म हो गया। लकड़ी, बांस और पत्तों से बनी मड़इयों के साथ किसी मां की गोद जल गई, किसी बच्चे की हंसी, किसी बाप की मेहनत, और किसी बुजुर्ग का आसरा राख हो गया। खरगूपुर की मुसहर बस्ती में जो जला वो सिर्फ घर नहीं थे-वो इंसान की गरिमा, उसका स्वाभिमान, और इंसाफ की उम्मीद थी।
बगल में बैठी प्रेमा, जिसकी उम्र 58 के पार है, आग के बाद की राख में बैठी अपने जल चुके घर को देखती है। उनकी भूरी आंखों में सख्त उदासी है। वो कहती हैं-“सब कुछ चला गया, अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। पड़ोसी जो थोड़ा-बहुत देते हैं, उसी से जी रहे हैं। कई रातों से नींद नहीं आई। जिंदगी कैसे चलेगी, समझ नहीं आता।”

यह सिर्फ एक आग नहीं थी-यह उन आवाज़ों को खामोश करने की साजिश थी जो अब भी जीने की ज़िद में लगी हैं। मीरा, प्रेमा, अर्जुन, और सरिता की कहानी किसी अख़बार की हेडलाइन नहीं बनी, लेकिन इनकी आंखों में तैरती राख, पूरी व्यवस्था पर सवाल है, “गरीब की आंच इतनी धीमी क्यों है कि न थाने तक पहुंचती है, न सरकार तक?”
राख में दबे सपनों की चीख
खरगूपुर मुसहर बस्ती के बग्गी कहते हैं, “महीनों से हमारे पास कोई काम नहीं है। पहले जब काम मिलता था तो आदमी-औरत सब काम करते थे। हर किसी को रोज़ की सौ-दो सौ रुपये दिहाड़ी जरूर मिल जाया करती थी, लेकिन अब कुछ नहीं। बीमारी से हम भले ही नहीं मरे, लेकिन बेरोज़गारी ने जिंदगी पहाड़ बना दी। सरकार सड़कें बनवा रही है और गड्ढे भरे जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई काम नहीं देता। गंगा किनारे आरती की रोशनी हर शाम बनारस को रोशन करती है, लेकिन हमारी बस्तियों में हर रात अंधेरे और भूख के बीच बीतती है। प्रशासन मौन है, सरकार निष्क्रिय, और समाज की संवेदनाएं कहीं खो चुकी हैं।”
खरगूपुर की मुसहर बस्ती में अर्जुन वनवासी जैसे लोगों के लिए चुनावों में किए गए वादे अब झूठ की तरह लगते हैं। “हर बार कोई न कोई नेता आता है, कहता है हालात बदलेंगे। पर आज तक कुछ नहीं बदला। हमारे घर पहली बारिश में डूब जाते हैं, रास्ते दलदल हो जाते हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता।”
कोरोना की मार के बाद इन लोगों की जिंदगी जैसे थम सी गई है। “ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मुसहरों को आज कोई काम नहीं मिलता। स्कूल बंद हैं, मिड डे मील बंद है, बच्चों को खाना नहीं मिलता। हम मजदूरी करके दो वक्त की रोटी जुटाते थे, अब वो भी नहीं है,” अर्जुन कहते हैं। सरिता, जो मिट्टी पर बैठी थी, कहती है, “यहां किसी के पास काम नहीं है। भूख अब स्थायी मेहमान बन गई है। सब्ज़ी खरीदने की हैसियत नहीं है। राशन है, पर वो भी अधूरा।”
इस घटना के बाद एक अप्रैल 20125 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का एक प्रतिनिधिमंडल बनारस में पुलिस कमिश्नर से मिला। नंदलाल पटेल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पुलिस की निष्क्रियता और गरीबों के साथ अन्याय पर चिंता जताई गई। प्रतिनिधिमंडल में शिव शंकर सिंह, शिव शंकर शास्त्री और पीड़िता मीरा भी शामिल थीं। नंदलाल पटेल ने कहा, “हमारे देश में गरीब होना अब अपराध बनता जा रहा है। जिनके पास न ज़मीन है, न पहुंच, उन्हें कोई नहीं सुनता।”

सीपीएम नेता नंदलाल पटेल सवाल उठाते हैं-“मुसहरों के बच्चे जब खाना मांगते हैं तो मार खा जाते हैं। क्या यही समाज है? ये सिर्फ आगजनी की घटना नहीं, ये व्यवस्था की नाकामी की कहानी है। यदि यही हाल रहा तो समाज में खाई ऐसी बढ़ेगी कि हर संवेदनशील इंसान कांप जाएगा। मीरा की आंखों में सिर्फ राख नहीं, सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या उसका बेटा फिर हंसेगा? क्या उसे इंसाफ मिलेगा? क्या कोई उसकी आवाज़ सुनेगा?”
महिलाएं जब अपना दुखड़ा सुना रही थीं तो सीपीएम नेता शिवशंकर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, “इस आग में सिर्फ झोंपड़ी नहीं जली, मीरा की उम्मीद जली है। वो अकेली महिला जो पहले ही ज़िंदगी से लड़ रही थी, अब इंसाफ और जिंदगी दोनों के लिए लड़ रही है।” आज भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। न कोई सरकारी राहत, न प्रशासन की दिलचस्पी।
मुसहर बस्तियों की हकीकत
पूर्वांचल की मुसहर बस्तियों में ज़िंदगी का चेहरा एक-सा है-पिचके गाल, बुझी हुई आंखें और कुपोषण के शिकार बच्चे। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि उनके लिए किताबों से पहले रोटी ज़रूरी है। उनके घरों में सबसे पहले भूख बोलती है, पढ़ाई नहीं। झोपड़ियों में किताबें नहीं, खाली बर्तन और धुएं से भरे कोने होते हैं।
उत्तर प्रदेश में दलितों के भीतर भी सबसे वंचित-महादलित श्रेणी में आने वाला मुसहर समुदाय, लगभग 9.5 लाख की संख्या में अलग-अलग जिलों में बिखरा हुआ है। यह समुदाय सदियों से हाशिए पर है-बिना ज़मीन के, बिना अधिकारों के और बिना बुनियादी सुविधाओं के। शिक्षा, पोषण और एक पक्की छत का सपना इनकी ज़िंदगी में आज भी अधूरा है।
बनारस के कोईरीपुर, दल्लीपुर, रमईपट्टी, औराब, सरैया, कठिरांव, असवारी, हमीरापुर, मारूडीह, नेहिया रौनाबारी, जगदीपुर, थाने रामपुर, बरजी, महिमापुर, सिसवां, परवंदापुर, सजोई, पुआरी खुर्द, मेहंदीगंज, शिवरामपुर और लक्खापुर जैसी दर्जनों बस्तियों में आज भी वनवासी मुसहर समुदाय के हजारों लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका जीवन किसी अंतहीन पहाड़ी रास्ते की तरह है-जिसका कोई आसान मोड़ नहीं, कोई राहत नहीं।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी, चंदौली और कुशीनगर जिलों में मुसहर समुदाय की ज़िंदगी किसी खामोश चीख़ की तरह है, जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। यहां से भूख से मौत की खबरें आना अब जैसे आम बात हो गई है। लेकिन जब ये खबरें आती हैं, तो सरकारें आंखें फेर लेती हैं और मौत की असल वजह को ‘बीमारी’ या ‘संयोग’ बता देती हैं।
मुसहरों की दशा पर वर्षों से काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मंगला राजभर याद करते हैं, “2019 में कुशीनगर में जब पांच मुसहरों ने दम तोड़ा, तो सबने जाना कि वे भूखे थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी मौत का कारण ‘बीमारी’ बताया।” यहां तक कि भाजपा के पूर्व विधायक गंगा सिंह कुशवाहा ने भी माना था कि ये मौतें कुपोषण और दवाओं की कमी की वजह से हुई थीं।
मंगला की बातें यहीं खत्म नहीं होतीं। वे बताते हैं कि 28 दिसंबर 2016 को इसी जिले में सुरेश और गंभा नाम के दो मुसहरों की भूख से मौत हो गई थी। बनारस के पिंडरा क्षेत्र की रायतारा मुसहर बस्ती में रोहित वनवासी की भी कुपोषण से मौत हुई थी। मामला इतना गंभीर था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दखल देना पड़ा और शासन ने रोहित की मां मीना को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया।
राजनीति से परे एक पीड़ा
पूर्वांचल के मुसहरों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में ‘वनमानुष’ कहा जाता है। सरकारी अभिलेखों में दोनों को अलग जातियों में दर्ज किया गया है, जबकि दोनों की जिंदगी एक जैसी है-बदहाली और बहिष्कार से भरी। मुसहरों की बस्तियां बिखरी होती हैं, इसलिए न चुनावों में इनका ज़िक्र होता है, न ही सियासी दल इन्हें अपना मानते हैं।
साल 1952 में किराय मुसहर ने बिहार के मधेपुरा से चुनाव जीतकर एक उम्मीद जगाई थी। बाद में मिसरी सदा, नवल किशोर भारती, जीतन राम मांझी और भगवती देवी जैसे नेता इस समुदाय से उभरे, लेकिन यह विडंबना है कि इनमें से कोई भी अपने समाज के लिए कोई ठोस बदलाव नहीं ला सका।
सोनभद्र के दल्लू वनवासी जब पहली बार बीडीसी चुने गए, तो लगा जैसे कुछ बदलेगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सामाजिक कार्यकर्ता श्रुति नागवंशी कहती हैं, “महादलित समाज में बदलाव की रफ्तार बहुत धीमी है। उनके नेता भी अब केवल खुद तक सीमित हो गए हैं, समाज के लिए नीतियां गढ़ने की सोच तक नहीं पहुंचते।”
अख़बार अचूक रणनीति के संपादक विनय मौर्य यादव कहते हैं, “मुसहर जाति की पीड़ा शायद सबसे उपेक्षित है। ये न केवल भूमिहीन हैं, बल्कि सामाजिक रूप से बहिष्कृत भी हैं। इनके दर्द का कोई मुकम्मल दस्तावेज़ नहीं है, यहां तक कि दलित साहित्य में भी ये हाशिये पर हैं।”
विनय एक मार्मिक घटना का ज़िक्र करते हैं-जौनपुर के गरियाव गांव की। जब मुसहरों की ज़मीन के ऊपर से सड़क निकली, तो ज़मीन की कीमतें बढ़ गईं। बस यहीं से उनकी मुसीबतें शुरू हो गईं। सामंतों ने दलित जातियों को ही मुसहरों के खिलाफ खड़ा कर दिया और तूफानी नामक व्यक्ति की जीभ कटवा दी। पुलिस आई, पर गवाही वही हुई जो दबंग चाहते थे। पीड़ा और उत्पीड़न के बीच भी मुसहरों की कोई बड़ी आवाज़ नहीं बन पाई, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व की कमी हमेशा आड़े आई।
सबसे आसान निशाना-मुसहर
2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र की तीन ताली मुसहर बस्ती में जाकर वादा किया था कि अब इनके दिन बदलेंगे। कुछ वादे ज़मीन पर आए भी-आवास मिले, कुछ योजनाएं पहुंचीं। लेकिन जीवन की दिशा नहीं बदली। सोनभद्र के वरिष्ठ पत्रकार राजीव सिंह बताते हैं कि विकास के साथ-साथ शराब का ठेका भी पहुंच गया। “अब बस्ती के 80 फीसदी लोग नशे की चपेट में हैं,” वे कहते हैं, “सरकारी योजनाएं आईं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक हालात और बिगड़ गए। मशीनीकरण ने परंपरागत काम छीन लिया। दोना-पत्तल, डोली-बहंगी का काम खत्म हो गया। लोग ईंट भट्टों पर मजदूरी करने लगे, लेकिन लॉकडाउन ने वह सहारा भी छीन लिया।”
जनमित्र न्यास ने बनारस और आसपास के मुसहरों के लिए लड़ाई लड़ी है-चाहे शिक्षा, चिकित्सा या न्याय की बात हो। दर्जनों बंधुआ मजदूर छुड़ाए गए, पुलिस द्वारा लादे गए फर्जी मुकदमों का संज्ञान लिया गया। डॉ. लेनिन कहते हैं, “मुसहर समुदाय आज भी घुप्प अंधेरे में जी रहा है। गरीबी के कारण ये पुलिस और दबंगों के लिए सबसे आसान शिकार हैं।”
जब उनसे पूछा गया कि असल समस्या क्या है, तो वे कहते हैं, “स्थिति बदली ज़रूर है, थोड़ी जागरूकता आई है, लेकिन शोषण अब भी जारी है। सरकार ने सीलिंग की ज़मीन का पट्टा तो दिया, लेकिन कब्जा नहीं दिलाया। इसी वजह से ये लोग अब भी ज़ुल्म का शिकार हैं।”
डॉ. लेनिन बताते हैं कि सरकार भले फरमान जारी करती हो कि मुसहरों को ज़मीन दी जाए, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। ज़मीन का आवंटन होते ही दबंग कब्जा कर लेते हैं, अदालतों में केस जाता है, तारीख पर तारीख पड़ती है और अंततः मुसहर टूट जाते हैं-मन से भी और उम्मीद से भी।
मानवाधिकार जन निगरानी समिति की कार्यकर्ता छाया कहती हैं, “मुसहरों के पास न रोजगार है, न इज़्ज़त। योजनाएं आती तो हैं, लेकिन पहुंचती सामंतों के घरों तक हैं। पहले सरकार साइकिल देती थी, पोशाक देती थी, तो लगता था कि पढ़ाई के बाद नौकरी भी मिलेगी, पर अब पढ़ाई का मतलब भी खत्म होता जा रहा है।”
परंपरा से बेबसी तक
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की मान्यता प्राप्त मुसहर समुदाय कभी खेतों में चूहे पकड़ने का काम करता था। चूहों के बिल से निकले अनाज को ही अपनी कमाई मानते थे और बदले में खेत में चूहों को दबाने का काम करते थे। सूखा पड़ता तो यही चूहे इनकी आजीविका बन जाते। आज वही मुसहर परिवार बनारस और आसपास के ईंट भट्टों, कालीन कारखानों और मज़दूरी के धंधों में बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं।
जीवन की जद्दोजहद में जुटे मुसहर समुदाय के पास आज भी न भविष्य की योजना है, न वर्तमान की सुरक्षा। कुछ बस्तियों में पक्के मकान तो आए, पर रोटी, रोजगार और शिक्षा की गारंटी अब भी कोरी कल्पना है। पूर्वांचल की मुसहर बस्तियां आज भी ‘विकास’ के दस्तावेज़ों में पीछे छूट गई हैं-और उनकी ज़िंदगी अब भी एक पहाड़ की तरह सामने खड़ी है-जिसे लांघने की कोई सीढ़ी नहीं, सिर्फ़ संघर्ष की चप्पलें हैं।
उत्तर प्रदेश भारतीय आदिवासी-वनवासी कल्याण समिति के संचालक हरिराम वनवासी बेहद पीड़ा से कहते हैं कि मुसहर समुदाय को सियासी दलों ने बस छलावा दिया है। बस्तियों में स्कूल नहीं हैं। बच्चे अगर पढ़ने लगें, तो ऊंची जातियों के बच्चे और शिक्षक उन्हें हतोत्साहित करते हैं। यह भेदभाव इतना गहरा है कि पढ़ाई छोड़ देना ही उन्हें आसान रास्ता लगता है।
किसी भी मुसहर बस्ती में कदम रखते ही यह साफ़ महसूस होता है कि ज़िंदगी यहां इंसानी गरिमा से कोसों दूर है। वही झोपड़ी जिसमें पूरा परिवार रहता है, वहीं भेड़-बकरियां भी पलती हैं और उसी में खाना भी बनता है। बरसात आती है तो छतें टपकने लगती हैं, और उन्हें ठीक कराने के लिए न पैसे होते हैं, न किसी सरकारी मदद की उम्मीद। यह हताशा सिर्फ अनेई तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल की मुसहर बस्तियों में पसरी हुई है।
(विजय विनीत बनारस के वरिष्ठ पत्रकार हैं)







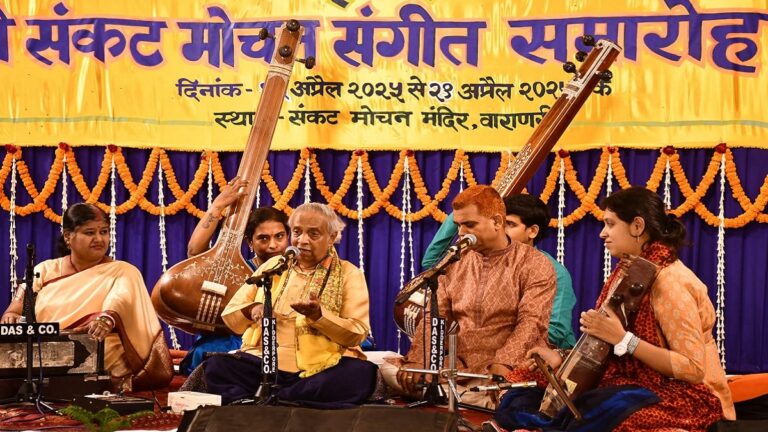



+ There are no comments
Add yours