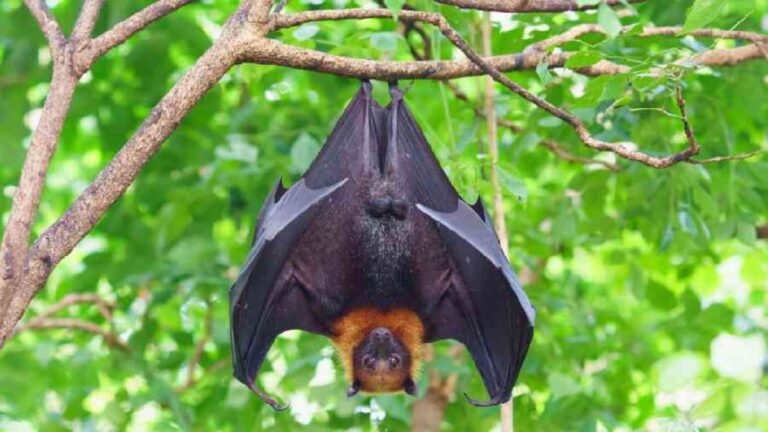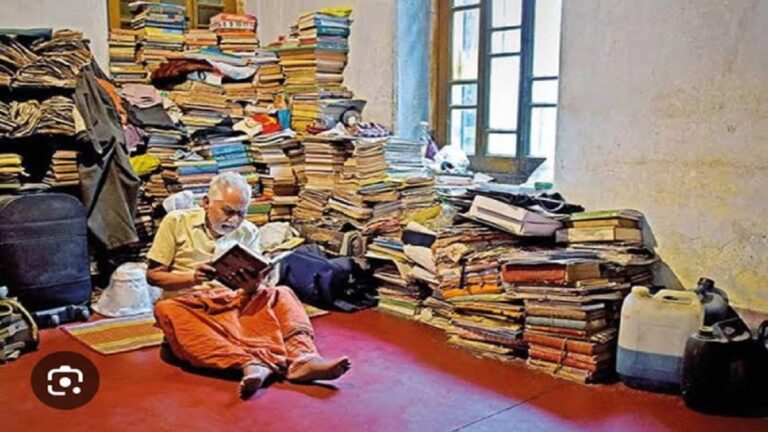अमेरीकी मौसम विज्ञानियों ने अलनीनो के खत्म हो जाने और अलनीना के शुरू होने की घोषणा कर दिया है। अलनीनो मई के तीसरे हफ्ते तक खत्म होने की ओर चला गया था। इस घोषणा से दुनिया के किसी भी मौसम विज्ञानियों का कोई विरोध नहीं था। भारत में मौसम विज्ञान की खबरची, खासकर हिंदी अखबारों में इसे मार्च के महीने में ही खत्म होने और मानसून की बारिश की उम्मीदों को खूब बढ़ा चढ़ाकर छाप रहे थे। उस समय वे आने वाली गर्मियों के बारे में कत्तई नहीं बता रहे थे कि यह कितना लंबा होने वाला है।
भारत के दक्षिण में समुद्री हवाओं का मैदान की ओर दबाव का रुख करना और पश्चिमी विक्षोभ में मई के मध्य से सूखा और गर्म हो जाने से पूरे उत्तर भारत में लू चलने की कोई खबर नहीं थी। इन दो तरह की हवाएं पूरे भारत में एक लंबे गर्मी के मौसम का निर्माण किया है जिसमें रिकार्ड स्तर का तापमान, उसकी चपेट में आने वाले शहर और दिन-रात के तापमान में सामान्य से ऊपर बने रहना एक विशिष्टता बन गई।
पानी की कमी, बिजली की मांग और काम की विकट स्थितियों ने शहरी जीवन को गहरे प्रभावित किया। गर्मियों में सब्जी की खेती पर पर गहरा असर पड़ा है जबकि धान की खेती की तैयारी और उसकी बुवाई लगभग महीने भर आगे की ओर खिसक गया है। यह वर्ष 2023 की ही एक पुनरावृत्ति की तरह है लेकिन पिछले साल से मौसम कहीं अधिक आक्रामक रुख ले रखा है।
अलनीनो से अलनीना में संक्रमण लंबा समय लेता है। प्रशांत महासागर जितना शांत दिखता है, उतना है नहीं। आस्ट्रेलिया, दक्षिण एशिया से उत्तरी और दक्षिणी अमेरीकी के बीच फैले प्रशांत महासागर में चलने वाली हवाओं के दो नाम हैं अलनीना और अलनीनो। ये हवाएं समुद्र के भीतर और समुद्र के ऊपरी सतह, दुनिया के सारे देशों को किसी न किसी तरह से प्रभावित करती हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव निश्चित ही इन दो हवाओं के गिरफ्त में आने वाले देश तो हैं ही, इसका अफ्रीका और एशियाई महाद्वीप पर सीधा असर पड़ता है।
बारिश की कमी और अधिकता, चक्रवाती तुफानों में बढ़ोत्तरी और भूमध्यसागर से चलने वाली समुद्री हवाओं की गुणवत्ता सीधे तौर पर प्रभावित होती हैं। जब भी अलनीनो का असर शुरू होता है, भारत से लेकर मध्य एशिया और अफ्रीका तक में बारिश की कमी और गर्म हवाओं का सीधा प्रकोप आता है। यह जितना ही लंबा होता है उतना ही सूखे और गर्मी के समय को लंबा करता जाता है।
जब मई में अलनीनो को ‘डेड’ घोषित किया गया तब भारत में, खासकर हिंदी अखबारों ने मानसून के सामान्य हो जाने की घोषणा कर डाली। इन अखबारों के रिपोर्टर और संपादक मानो इस बात से बेखबर रहते हैं कि उनके इन खबरों को पढ़ने वाले वे लोग भी होते हैं जो खेती से सीधे और अपरोक्ष तौर पर जुड़े रहते हैं। अलनीनो के ‘डेड’ हो जाने का अर्थ यह नहीं था कि तुरंत ही अलनीना का प्रभाव शुरू हो गया। यह हजारों किमी में फैले एक भूक्षेत्र के मिजाज बदलने की एक प्रक्रिया है। यह एक स्विच से चलने वाली कोई मशीन नहीं है।
अलनीना के प्रभाव में आने का समय जुलाई से सितम्बर तक रखा गया है। इसका भारत के मौसम पर असर कब से पड़ेगा, इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। जिस समय अलनीनो के खत्म होने और अलनीना के शुरू होने का समय बताया जा रहा था, उसी समय अमरीकी देशों के मौसम विज्ञानियों ने दक्षिणी और उत्तरी अमेरीका के बीच, जिसमें समुद्री क्षेत्र भी शामिल है एक विशाल ‘हीट डॉम’ बनने की खबर भी आई। निश्चित ही समुद्री हवाओं के बदलाव पर इंसान द्वारा पैदा किये गये इस ‘हीट डॉम’ का असर पड़ेगा। खासकर, इसके असर का अनुमान अमेरीकी देशों पर पड़ने की उम्मीद है।
मानसून में देरी और कमी को अब साफ देखा जा सकता है। इस बार भी पिछले साल की तरह ही मानसून में न सिर्फ उसकी गति में धीमापन देखा गया, उसकी क्षमता भी कम मापी जा रही है। भारत के मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इस बार मानसून सामान्य से 20 प्रतिशत कम रहेगा। आमतौर पर मानसून जून के दूसरे हफ्ते तक उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करते हुए दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में दस्तक देने लगता है। इस बार जून के अंतिम हफ्तों का समय शुरू होने वाला है और मानसून अभी उत्तर बिहार की तरफ बेहद कमजोर या नहीं के बराबर ही दस्तक दिया है।
इस दौरान उत्तर प्रदेश के जिले, खासकर प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ जैसे शहर सबसे गर्म शहरों में शुमार हो रहे हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र से लेकर नीचे दक्षिणी राज्यों और उत्तर-पूर्वा में मानसून की बारिश जून के मध्य तक देखी गई। लेकिन, उड़िसा, बंगाल और मध्य प्रदेश से लेकर पूरे उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत को बारिश की उम्मीद जून के अंतिम दिनों तक का इंतजार करना पड़ेगा। इस दौरान, पश्चिमी विक्षोभ की सूखी और गर्म हवाएं पश्चिमोत्तर से उतरते हुए नीचे के मैदानी इलाकों में उतरती रही हैं। इससे उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे लंबी गर्मी का मौसम देखने को मिल रहा है।
जून के मध्य तक मानसून से होने वाली बारिश की कमी का सीधा असर धान की खेती पर पड़ता है। भारत की कुल खेती में अभी भी 70 प्रतिशत की हिस्सेदारी मानसून से होने वाली बारिश है। भारत की आधी खेती सीधे मानसून की बारिश पर निर्भर है। भारत में अलग अलग प्रांतों में खेती का पैटर्न अलग अलग होने और पानी की जरूरत को पूरा करने के साधन अलग अलग हैं। दिल्ली जैसी जगह में सामान्य से अधिक तापमान बने रहने की अवधि 40 दिन से अधिक हो चुकी है। राजस्थान और हरियाणा की स्थिति भी यही है।
बिहार और उत्तर प्रदेश में मार्च के अंतिम हफ्तों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर चला गया। अप्रैल और मई में कुछ दिनों में बारिश और तापमान में कमी को देखा गया। लेकिन, आमतौर पर यहां लू का प्रकोप बना रहा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश में, खासकर मिर्जापुर में बड़ी संख्या में मतदाता कर्मचारियों की मौत एक खबर बन गई थी। यह पूरे चुनाव में एक बार में सबसे अधिक मौत की खबर थी। सामान्य तौर पर लू से उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली मौत की खबर छिटपुट आती ही रहीं। इसका कुल असर पानी की उपलब्धता पर पड़ रहा है। जमीन के नीचे के पानी के प्रयोग तेजी से बढ़ा है।
दिल्ली का हाल बेहाल है। इस बार मई-जून के महीने में जब दिल्ली का तापमान 50 डिग्री को छूते हुए ऊपर की ओर उठा तब एकबारगी मौसम विभाग को भी विश्वास नहीं हुआ। मौसम विभाग ने तापमान मापने वाले यंत्र के सेंसर पर नजर रखना शुरू किया और दुरूस्त करना उपयुक्त समझा। लेकिन, जब भारत के इस या उस शहर से तापमान के असामान्य होने की खबर आने लगी तब इस बात को स्वीकार करना भी जरूरी हो गया कि तापमान भी अपने अनुरूप ‘हीट डॉम’ या गर्म द्वीपों का निर्माण करता है। हीटवेव शब्द भारत में 40 डिग्री सेंटिग्रेड से ऊपर तापमान उठने, सूखी गर्म हवा के बने रहने और नीचे और ऊपर दोनों ही तापमान में चार से पांच डीग्री का उठान होने की स्थिति को कहते हैं। मौसम की यह परिस्थिति अन्य कारकों के साथ मिलकर और भी खतरनाक स्थिति में जा सकती है।
दिल्ली और आसपास के इलाकों के आसमान में छोटे-बड़े कणों की विद्यमानता, कार्बन और अन्य गैस उत्सर्जन वे बड़े कारण हैं जो हवा में तापमान को लंबे समय तक गर्म रखते हैं जिससे न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी होती है। इसी तरह, सड़क निर्माण, सघन भवन और उनकी संरचना दिन में सूरज की रोशनी को तेजी से सोखते हैं और बहुत धीमे ठंडे होते हैं। इससे शाम के समय में भी तापमान में बढ़ोत्तरी बनी रहती है। रात में बनी रहने वाली गर्मी जब एक बार फिर दिन की गर्मी के साथ मेल खाती है और सूखी गर्म हवाओं के साथ मिलने लगती है तब गर्म द्वीपों का निर्माण होने लगता है। धरती के कुल बढ़े तापमान का असर भारत के औसत तापमान में वृद्धि में देखा गया है जो ताप की स्थितियों में गुणात्मक असर डालता है।
दिल्ली, जहां सड़क, भवन, रास्ते आदि बनाने में बड़े पैमाने पर सीमेंट, पत्थर, बालू आदि का प्रयोग होता है, ताप को सोखने और उसे बनाये रखने में बहुत उपयुक्त होते हैं। पूरी दिल्ली का परिक्षेत्र देखा जाय तो यहां महज 20 सालों में शहरीकरण में लगभग 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई है। शहरी निर्माण 2003 में 31.4 प्रतिशत था जो 2022 में 38.2 प्रतिशत हो गया है। बड़े पैमाने पर शहरी विकास योजनाएं और मेट्रों और फ्लाईओवर जैसी इंफ्रास्ट्राक्चर का निर्माण सड़के के किनारों की जमीन और पेड़ों को खत्म करते गये हैं और ये फैलते गये हैं। यदि एनसीआर को मिला दिया जाय तो स्थिति और भी भयावह दिखेगी। दिल्ली के गांव अब भारत के सबसे घने बसे हुए मुहल्लों में तब्दील हो चुके हैं।
उद्योग और भवनों के विशाल फैलाव को समेटे हुए दिल्ली, नोएडा, गुरूग्राम, पानीपत मानसून की पहुंच से दूर, पश्चिम की गर्म हवाओं के चपेट में आने के बाद यहां की फैक्टरीयों की भट्टी में बदलने लगता है। यह शहर न सिर्फ एक केंद्रीयकृत एयरकंडीशन्ड मेट्रो का संचालन कर रहा है, यहां के विशाल ऊंचे भवन, मॉल और ऑफिस इसी एयरकंडीशन मशीनों पर निर्भर है। इस सोमवार को दिल्ली में 89 गीगा वॉट बिजली की जरूरत पड़ी थी। एक गीगा वाट में 1000 मेगावॉट बिजली आती है। यहां सिर्फ बिजली की मांग की ही बात नहीं है।
यहां उसकी सप्लाई देने वाली संचार व्यवस्था कायम रखना भी एक बड़ा काम है। ऐसे में, ट्रांसफार्मर का जलना, तारों में आग लगना जैसी बड़ी समस्याएं इस बार देखने को मिल रही हैं। इस बिजली की मांग की आपूर्ती भी एक बड़ी चुनौती है। हाइड्रो और थर्मल दोनों ही बिजली उत्पादन में पानी एक निर्णायक भूमिका में होती है। गर्मी की बढ़त इन दोनों ही उत्पादन पद्धति को प्रभावित करती है। हाल ही में आये एक रिपोर्ट के अनुसार हिमांचल और उत्तराखंड में ग्लेशियरों के पिघलने और पुरानी नदियों और नालों के सूखने का सिलसिला बढ़ रहा है। यह सिर्फ बिजली उत्पादन को ही नहीं, पीने के पानी के संकट को बढ़ाने वाली खबरें हैं।
अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरा जब पानी का शहर माने जाने वाला बंगलुरू शहर पीने के पानी के लिए तरसने लगा। दिल्ली में पीने के पानी को लाने वाली नहर पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया और पानी ‘चुराते हुए’ गिरफ्तारी भी हुई। पानी की आपूर्ती को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया और वहां दिल्ली सरकार को इस संदर्भ में डांट सुननी पड़ी।
दिल्ली एक समय झीलों का शहर था। यहां राजस्थान से आने वाली साहिबी नदी है और यमुना जीवन दायिनी की तरह यहां बहती है। ये दोनों ही नदियां दिल्ली में घुसने के साथ मृत हो जाती हैं। यहां के झीलों के रखरखाव के खूब दावे किये गये, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखता है। इस तरह दिल्ली पानी के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर पूरी तरह निर्भर है। जो निश्चित ही गर्मी के दिनों में, बारिश की कमी से आपूर्ति प्रभावित होने लगती है।
जलाशयों के नये निर्माण की कमी पानी की आपूर्ति में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। दिल्ली में सारा जोर यहां के कचड़ा, पानी की साफ सफाई पर है, जिसके परिणाम आज तक देखने को नहीं मिले। लेकिन, इस सबका फायदा पानी आपूर्ति में लगी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और स्थानीय स्तर पर पानी के ठेकेदारों को हो रहा है। पानी का असमान वितरण भी दिल्ली के गरीब इलाकों को पानी से वंचित रखता है और उन्हें हफ्ते में दो या तीन दिन पानी की आपूर्ती दी जाती है। एक शहर बनाते हुए उनके निवासियों के प्रति यह बेरूखी और भेदभाव शहरी जीवन को और भी दुरूह और जानलेवा बना देता है।
मौसम की सीधी मार मजदूरों की आय और रोजगार पर पड़ता है। मई के दूसरे हफ्ते से जब दिल्ली और एनसीआर में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने लगा तब हरियाणा और दिल्ली राज्य सरकारों की ओर से मजदूरों के संदर्भ में कुछ निर्देश जारी हुए। इन निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ, इस संदर्भ में कम ही रिपोर्ट आई। इन निर्देशों का कोई खास असर देखा नहीं गया। आमतौर पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर काम करना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है।
इससे अधिक तापमान पर काम करने के लिए कुछ सुविधाओं का होना जरूरी है, खासकर काम की अवधि छोटी होनी चाहिए। इससे श्रम करते हुए शरीर की मांसपेशियों के टूटने से पैदा होनी वाली गर्मी और बाहर का तापमान का कुल योग शरीर में खून के प्रवाह, पानी की आपूर्ती, उर्जा के क्षरण और किडनी, दिल और मष्तिष्क के काम करने की क्षमता, पेशियों की क्षमता को सुचारू स्तर पर बनाये रखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होने पर शरीर में थकान, अंगों में काम करने की क्षमता में गिरावट और बेहोशी, मौत जैसी संभावनाएं होती हैं।
भारत के बहुत थोड़े मजदूर ही संगठित क्षेत्र में काम करते हैं जहां काम की स्थितियां अपेक्षाकृत बेहतर हैं। भारत की विशाल आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं जहां सिर्फ काम की स्थितियां ही नहीं, रोजगार और आय की भी स्थिति बुरी है। इस समूह में एक बड़ा वर्ग, नीति आयोग के अनुसार लगभग 77 लाख गिग वर्कर है, जो एक कंपनी के साथ स्वयम्सेवी की तरह काम कर रहा होता है। यह जोमैटो और अमेजन से लेकर ओला, उबर जैसी कंपनियों के लिए काम करते हैं। ये मजदूर मौसम की मार के बीच काम कर कर रहे होते हैं। कंपनियां सेवा आपूर्ति में इन्हीं मजदूरों की आय का एक हिस्सा वसूलते हैं। मौसम की मार एक ओर मजदूरों के काम की क्षमता को प्रभावित करते होते हैं वहीं ये कंपनियां इनसे पैसा वसूलने में लगी रहती हैं।
इसी तरह, भवन और निर्माण क्षेत्र में लगे मजदूरों को इस गर्मी में लगातार काम करने में लगा रहना पड़ा। यहां कुल काम के आधार पर ही मजदूरों की आय निर्भर रहती है। गर्मी ने कुल काम की क्षमता में जितनी गिरावट की ओर ले गई, उतना ही आय में कमी देखी गई। हाल ही में यूनाईटेड नेशन्स इकॉनमिक एण्ड सोशल कमीशन फॉर एशिया एण्ड द पैसिफिक पर जारी रिपोर्ट में बढ़ते तापमापन पर चिंता जताते हुए काम के समयावधि में होने वाली कमी और इसी अनुपात में आय में हो रही कमी की ओर इशारा किया है।
ग्रीनपीस इंडिया और नेशनल हॉकर फेडरेशन ने अपने नये रिपोर्ट में दावा किया है कि दिल्ली में अप्रैल-मई के दौरान सड़कों की रेहड़ी-पट्टी वाले दुकानदारों का 80 फीसदी हिस्सा की आय प्रभावित हुई है। इसमें 50 प्रतिशत की आय बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट ने नमूना सर्वेक्षण के आधार पर बताया है कि गर्मी की वजह से ग्राहकों की संख्या में भारी गिरावट आई। वहीं दुकान चलाते हुए कई स्तर पर प्रभाव झेलना पड़ा। खासकर, चिड़चिड़ाहट, ताम से झुलसन, थकान, पेशियों और सिर में दर्द, पानी की कमी की समस्या आई। उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं उनके काम को अधिक प्रभावित कर रही थीं। यह रिपोर्ट बताती है कि सरकार की ओर से हीटवेव से निपटने के लिए उन्हें कोई दिशा-निर्देश, सहयोग आदि नहीं मिला। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को खुद ही निपटना पड़ा। हीटवेव से आय में होने वाले नुकसान को लेकर सरकार की ओर कोई तैयारी नहीं दिखती है।
एक बड़ा सवाल है मौसम की मार से किधर जाया जाये। हाल ही में एक चार्ट के माध्यम से पूंजीवाद के पैदा होने से लेकर आज तक के बढ़ते तापमान को प्रर्दशित किया गया था। इसे ध्यान से देखें तब साफ दिखता है कि ऑटोमोबाइल के आगमन के साथ ही तापमान में तेज वृद्धि होती है। भारत के संदर्भ में इसी तरह का एक चार्ट सामने आना चाहिए। दुनिया के कुछ बढ़े तापमान का लगभग 66 प्रतिशत असर भारत पर है।
दुनिया के स्तर पर भारत पर्यावरण की बैठकों में साउथ ब्लॉक की लॉबी करता है, जिसमें काबर्न उत्सर्जन के आधार पर और उससे होने वाले नुकसान की भरपाई के दावे वह अन्य देशों के साथ मिलकर विकसित देशों से हर्जाने की मांग करता है। इससे वह अपने यहां होने वाले नुकसान और ग्रीन उर्जा को विकसित कर सके। लेकिन, जब भी पर्यावरण का सूचकांक घोषित होता है भारत की स्थिति बदतर रहती है। यह पिछले कुछ सालों से और भी नीचे के पायदान पर गया है।
येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सूचकांक में भारत पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में से 176वें स्थान पर है। यह ठीक वैसे ही जैसे अडानी एक ओर ग्रीन उर्जा के नेतृत्व का दावा करते हैं लेकिन वह साथ ही भारत के विशाल जंगलों के सफाये में भी एक अग्रणी भूमिका निभा रहे होते हैं। विकास के लिए कार्बन उत्सर्जन की छूट हासिल करने के लिए भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जितना भी दावा किया जा रहा हो, भारत में इसका कुल असर सफलता में परिवर्तित होते हुए नहीं दिख रहा है।
हरित क्रांति बिजली, पानी और रसायनिक खादों के एक ऐसे ट्रैप में किसानों को पहुंचा चुका है जहां आय बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग के सारे दावे भारत के विकास में एक धीमा योगदान ही बना रहा है। धीमी विकास दर पर कई गुना तेजी से बढ़ते शहर न तो रोजगार की तलाश को पूरा कर रहे हैं और न ही एक बेहतर जिंदगी की परिस्थितियां मुहैया करा रहे हैं।
विकास की जो धारा बह रही है, वह निश्चित ही सामान्य जीवन और प्रकृति के अनुकूल नहीं है। वह जीवन और प्रकृति को बेहद बुरी अवस्था की ओर ठेल रहे हैं। जरूरी है भारत में विकास की वैकल्पिक संरचना के बारे में चिंतन करने की और एक ठोस योजना बनाते हुए उस पर काम करने की। समय अब भी है। मौसम अपने बदलते क्रम में निश्चित ही हमारे अनुकूल होगा, यदि हम मौसम को उसके मिजाज से परखें और अपनी जिंदगी को प्रकृति के साथ जोड़ते हुए आगे ले जाएं।
(अंजनी कुमार स्वतंत्र पत्रकार हैं)