बनारस। देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस में संकट मोचन मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि वह स्थल है जहां हर वर्ष सुरों की एक ऐसी अजश्र धारा बहती है, जो जाति, धर्म, संप्रदाय और मतभेदों की सीमाओं को लांघ जाती है। जहां वाद्य गूंजते हैं, स्वर लहरियां उठती हैं, ताल और लय की समवेत अनुभूति होती है, वहां न कोई हिन्दू होता है, न मुसलमान-वहां केवल राग होते हैं, भक्ति होती है, समर्पण होता है और उस संपूर्णता में डूबा हुआ मनुष्य। यह समारोह बनारस का मौन उत्तर है उन तमाम आवाज़ों को, जो बांटना चाहते हैं; यह वह आलाप है, जो हमें याद दिलाता है कि जब तक सुर जीवित हैं, तब तक समरसता भी जीवित है।
बनारस स्थित संकट मोचन मंदिर का संगीत समारोह केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, वह उस बनारस की आत्मा का उत्सव है, जिसमें हनुमान भक्त गोस्वामी तुलसीदास की रामकथा की गूंज है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की वैदिक जड़ों से जुड़ी परंपरा की मिठास भी। यह वह मंच है जहां कंठ से निकली हर तान, हर आलाप-ईश्वर तक पहुंचने की एक अंतःप्रार्थना बन जाती है। यह वह स्थल है जहां संकट में भी संगीत रुका नहीं। जब मंदिर परिसर आतंक की छाया से कांपा, तब भी रियाज़ की लौ बुझी नहीं, बल्कि दीप बनकर उजाला करती रही। जब समाज में सांप्रदायिकता का जहर घुलाने की कोशिशें हुईं, तब यही संगीत, यही सुर-प्रेम, सौहार्द और साझी तहज़ीब के रक्षक बन गए।

संकट मोचन संगीत समारोह का आयोजन न शाही मंच पर होता है, न रोशनी और प्रचार के तमाशे के बीच। यह उस मंदिर के प्रांगण में होता है, जहां मिट्टी में तुलसी की गंध है, जहां हर सुर तुलसीदास की भक्ति को छूता है और हर रसिक, चाहे वह किसी भी पंथ या विचार से हो, एक ही शरण में बैठा होता है-संगीत की। दरअसल, संकट मोचन मंदिर का संगीत समारोह केवल एक सांस्कृति आयोजन नहीं, वह उस बनारस की आत्मा का उत्सव है, जहां संकट में भी संगीत रुका नहीं। जहां मंदिर परिसर में आतंक की छाया पड़ी तो संगीत ने दीप बनकर उजाला किया। जहां सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की कोशिश हुई, वहीं प्रेम, सौहार्द और साझी तहजीब ने उस विष को अमृत में बदल दिया।
संगीत की इस उपासना में अब एक सौ दो साल पूरे होने को हैं। यह बात कितनी अद्भुत और भावविभोर कर देने वाली है कि यह समारोह आज भी बिना टिकट, बिना किसी बाहरी तामझाम के, मंदिर के प्रांगण में, आम जन के बीच, रात भर चलता है। जहां एक रिक्शा चालक और एक बड़े उद्योगपति दोनों एक ही पंक्ति में बैठकर, एक ही सुर में डूब जाते हैं। जहां भीड़ नहीं होती, वहां रसिक होते हैं। जहां श्रोता नहीं, वहां साधक होते हैं।

बीते वर्षों में संकट मोचन संगीत समारोह ने अनगिनत दिलों को छुआ है। इन छह रात्रियों के अनुष्ठान में वे सभी राग जाग उठते हैं, जो रात के अंधकार में खिलते हैं, कौंस, कान्हड़ा, रामकली, भैरव, ललित, जोग। जैसे-जैसे रात गहराती है, संगीत की आत्मा मंदिर के द्वार से निकलकर संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो जाती है। यह वह आयोजन है जहां मंच पर खड़ा कोई कलाकार केवल प्रस्तुतकर्ता नहीं होता, वह मंदिर के आंगन में एक श्रद्धालु की भांति ‘हाजिरी’ देता है। उस ‘हाजिरी’ में उसकी शिक्षा, जाति, धर्म नहीं देखे जाते देखा जाता है उसका समर्पण, उसका स्वर, उसका भाव, और उसकी ‘तपस्या’। संकट मोचन संगीत समारोह ने अनेक रूढ़ियों को तोड़ा है। वह पहला मंच था जहां मंदिर में महिला फनकारों को आमंत्रित किया गया। और फिर एक-एक कर मंदिरों के बंद दरवाजे खुलते गए, सुरों की रोशनी भीतर उतरती गई।
समावेशी सोच ने गिराई आडंबर की दीवार
अस्सी का दशक आते-आते इस समावेशी सोच ने बनारस में एक और दीवार गिराई-आडंबर की दीवार। अब संकट मोचन संगीत समारोह का मंच केवल हिंदू संगीतज्ञों का नहीं रहा, बल्कि इसमें मुस्लिम और अन्य धर्मों के कलाकार भी ससम्मान आमंत्रित किए जाने लगे। जब पाकिस्तान से आए ग़ज़ल सम्राट गुलाम अली ने संकट मोचन के प्रांगण में अपने अशआरों को सुरों की चादर में लपेटकर पेश किया, तो श्रोताओं की आंखें भीग गईं। वे समारोह के सबसे प्रिय कलाकारों में शुमार हो गए। वहीं, शास्त्रीय संगीत के महामनीषी पंडित जसराज हर वर्ष अमेरिका से बनारस आकर संकट मोचन में सुरों की साधना को अपना प्रणाम अर्पित करते रहे।

इस मंच पर हिन्दुस्तान के ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के भी फनकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गुलाम अली ने जब पहली बार संकट मोचन में ग़ज़ल गाई तो बनारस की रात जैसे थम गई। उनकी आवाज़ में जैसे मोहब्बत की सदी भर की दुआएं थीं। वह आवाज़ किसी मुल्क की नहीं थी, वह आवाज़ इंसानियत की थी। गुलाम अली ने कहा था, “हमें मोहब्बत का पैगाम बांटने की जरूरत है… और अगर कोई ताक़त यह नहीं चाहती कि हम मिलकर रहें, तो यह संगीत है जो वह दीवार तोड़ देगा।”
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी संकट मोचन संगीत समारोह में शहनाई बजाना चाहते थे। उनके नाम का ऐलान भी हुआ, लेकिन प्रोग्राम से पहले वो दुनिया से रुखसत कर गए। संगीत अपने समय से बड़ा होता है, यह उस दिन साबित हुआ। बीते सालों में संकट मोचन मंदिर के प्रांगण में जिन सुरों की गूंज सुनाई दी, वे केवल संगीत नहीं थे, वे साधना की साक्षात् अनुभूति थे। उस्ताद शाहिद परवेज खां की सितार की झंकार हो या मशकूर अली खां, गुलाम अब्बास खां, अकरम खां, सलीम अल्लाहवाले, शिराज अली खां, मोइनुद्दीन और मोमिन खां जैसे सारंगी के साधकों की अलक्षित उंगलियों की तरंग इन सुरों ने मंदिर की चुप्पियों को रसविभोर कर दिया।

इस परम सांगीतिक तीर्थ में पंडित जसराज की दिव्य गायन साधना से लेकर विदुषी गिरिजा देवी, गंगोत्री देवी, वाणी जयराम, पंडित राजन-साजन मिश्र, पंडित छन्नूलाल मिश्र, शुभा मुद्गल, उस्ताद राशिद खां, पंडित अजय चक्रवर्ती, डॉ. अश्विनी भिडे देशपांडे, उषा रंजन, और उज्ज्वल जालान जैसे दिग्गजों ने अपने स्वरों से आराधना की है। इन सबके बीच जो एक बात कभी नहीं बदली, वह है-नम्रता की परंपरा। यह गायन नहीं, उपासना है। यह संगीत नहीं, एक अनंत भक्ति की तरंग है।
इनके साथ ही शंभु भट्टाचार्य, पंडित संजय गुप्ता, हृदय नारायण मिश्र, मनोज कुमार मिश्रा, रवि शंकर मिश्रा, नील रंजन, संजय वर्मा, अजय झा, रवि श्रीवास्तव, प्रेमकांत वर्मा, राजेश्वर आचार्य, भरत भूषण गोस्वामी, सुरेश चंद्रवर्ती, लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी, सतेंद्र मोहन भट्ट, ब्रजेश मिश्रा, राकेश पाठक और विपुल कुमार जैसे फनकारों ने भी अपनी स्वरलिपि इस पवित्र भूमि पर अंकित की है। इन कलाकारों का मानना है कि यहां आने वाला हर कलाकार, चाहे वह किसी भी ऊंचाई का क्यों न हो, मंच पर आने से पहले संकट मोचन के चरणों में नतमस्तक होता है, क्योंकि यह मंच नहीं, मंदिर है।
महिला फ़नकारों को मिली नई पहचान
एक समय था जब बनारस के मंदिरों की चौखटें स्त्रियों के स्वर और ताल की दस्तक को नकार देती थीं। संगीत केवल पुरुषों के गले से ही सुनने योग्य समझा जाता था। परंतु सत्तर के दशक में संकट मोचन संगीत समारोह ने रूढ़ियों की इस अंधी दीवार में पहला सुराख किया। जब इस पावन मंच ने पहली बार महिला फ़नकारों को आमंत्रित किया, तो यह सिर्फ़ एक सांस्कृतिक निर्णय नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। इसके बाद पूर्वांचल के अन्य मंदिरों में भी सालाना संगीत समारोहों में स्त्रियों की भागीदारी की राह खुली।
साल 1960 के दशक तक यह मंच केवल पुरुष कलाकारों के लिए आरक्षित था, लेकिन कंकना बनर्जी ने अपने गुरु के साथ प्रस्तुति देकर इस परंपरा को बदला। इसके बाद महिला गायिकाओं और नृत्यांगनाओं की भागीदारी भी बढ़ी और महोत्सव अधिक समावेशी बनता गया। पहले प्रस्तुति स्थल हनुमान जी की प्रतिमा के ठीक सामने होता था, लेकिन भीड़ के कारण अब यह मंदिर के बाईं ओर आयोजित होता है। श्रोताओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर के अंदर और बाहर स्क्रीन लगाई जाती हैं ताकि सभी इस संगीत रस का आनंद ले सकें।

यह आयोजन गर्मियों में होता है, जहां न पंखे होते हैं, न एक समान ऑडियो व्यवस्था। इसके बावजूद कलाकार इस ऐतिहासिक मंच पर प्रस्तुति देने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। आधी रात और सुबह 4:30 बजे के आसपास पूजा और अनुष्ठान चलते हैं, जिस दौरान प्रस्तुतियां रोक दी जाती हैं, इसलिए कलाकारों को अनुकूल समय में प्रस्तुति देनी होती है।
आज यह आयोजन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, सूफी गायन और कर्नाटकी संगीत का सुंदर संगम है। बनारस के जाने-माने फनकार पंडित राजेश्वर के अनुसार यह मंच अब पॉप संगीत तक को स्वीकार कर चुका है। यहां पंजाबी पॉप सिंगर जसवीर जस्सी, तलत अज़ीज़, अनूप जलोटा, जावेद अली और सोनू निगम जैसे कलाकार कई बार प्रस्तुतियां दे चुके हैं। हालांकि कुछ रसिकों को लगता है कि आधुनिक संगीत की मौजूदगी से शास्त्रीय रस में हल्का व्यवधान आता है।
यह आयोजन मात्र एक संगीत कार्यक्रम नहीं, बल्कि संगीत प्रेमियों के लिए एक भावनात्मक और आध्यात्मिक तीर्थ है। जौनपुर की गायिका शालिनी सिंह पिछले कई सालों से संगीत समारोह देखने-सुनने आ रही हैं। वह कहती हैं, “यहां बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो संगीत की बारीकियां नहीं समझते। इस वातावरण में आत्मा संगीत से जुड़ जाती है। यह अविश्वसनीय अनुभव है। यह महोत्सव समय के साथ न केवल बड़ा हुआ है, बल्कि व्यापक भी हुआ है। परंपरा और नवाचार के बीच संतुलन साधते हुए यह आज भी संगीतप्रेमियों के हृदय में बसे एक अनूठे पर्व के रूप में जीवित है।”
अनूठी होती है संगीत की महफिल
संकट मोचन संगीत समारोह कई मायने में अनूठा होता है। यहां संगीत कभी-कभी स्वर नहीं, आत्मा का संवाद बन जाता है। संकट मोचन मंदिर में जब रात्रि के तीसरे पहर कोई राग भैरव फूटता है, तो लगता है जैसे कोई आहिस्ता से मंदिर की सीढ़ियों पर दीप जला रहा हो। यह आयोजन कोई आम संगीत समारोह नहीं, एक लोकपर्व है-भक्ति और संस्कृति की साझी थाली, जहां श्रद्धा सुरों के साथ आराधना करती है। एक सौ दो बरस पहले जो दीपक महंत अमरनाथ मिश्र ने जलाया था, वह आज भी मंद-मंद नहीं, बल्कि तेज़ ज्योति से झिलमिलाता हुआ हमारे सामने है।
संकट मोचन संगीत समारोह की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां कोई मंचीय अभिनय नहीं होता, न कोई औपचारिकता, न कोई अतिथि, न मुख्य अतिथि। न कार्ड छपता है, न न्योता जाता है, न टिकट की जरूरत होती है, न पास की जुगत। केवल सुर होता है, साज होता है और श्रोता होते हैं। बाकी सब कुछ हनुमान जी पर छोड़ दिया जाता है, जो यहां केवल देवता नहीं, श्रोता भी हैं। यही कारण है कि इस समारोह में कोई वीआईपी नहीं होता। संकट मोचन में “तुम रक्षक काहू को डरना” की भावना जीवंत रहती है। हर कोई समान होता है, चाहे वह विदेशी हो या स्थानीय, विद्वान हो या अनपढ़, भक्त हो या संशयवादी। यहां नास्तिक भी आकर श्रद्धा में भीग जाते हैं, क्योंकि संगीत की भाषा सबसे बड़ी होती है-सबसे पुरानी और सबसे विश्वसनीय।
जब पं. छन्नूलाल मिश्र को पहली बार इस समारोह में गाने का अवसर मिला, तो उन्हें एक ही आग्रह रखा गया-आप कुछ भी गाइए, पर बंदिशें केवल रामचरितमानस से हों। और उन्होंने वह किया भी। उनकी तान में तुलसीदास की चौपाइयां घुल गईं और संकट मोचन के प्रांगण में भक्ति की एक और लहर दौड़ पड़ी। वहीं पं. जसराज हर साल मंदिर की फर्श पर बैठते थे, उपवास रखते और फिर रात में गाते थे। उनके लिए यह कोई संगीत प्रदर्शन नहीं था, यह साधना थी। रागों के माध्यम से हनुमान की आराधना थी।
बनारस की वायलिनिस्ट खुशबू निशा कहती हैं, “यही वह जगह है जहां संगीत का हर शिखर कलाकार आकर अपने सुर अर्पित करना चाहता है, बिना पारिश्रमिक, बिना किसी प्रचार-प्रसार के। यह संगीत का सबसे पवित्र मंच है, जहां गाना कोई पेशा नहीं, पूजा है। माना जाता है कि इस मंच पर बिना गाए कोई भी चोटी का कलाकार नहीं कहलाता। जैसे प्राचीन काल में काशी में शास्त्रार्थ करना विद्वता की शर्त होती थी, वैसे ही आज संकट मोचन में प्रस्तुति देना संगीतकार की प्रतिष्ठा का प्रमाण बन चुका है।”
इस समारोह की शुरुआत 1923 में हुई थी। महंत अमरनाथ मिश्र स्वयं पखावज वादक थे और उन्होंने इस आयोजन की नींव डाली। पहले यह आयोजन रामायण सम्मेलन के साथ होता था, फिर संगीत सम्मेलन जुड़ा। बाद में यह तीन दिनों का हुआ, फिर चार दिन का और अब सात रातों तक चलने वाला अनुष्ठान बन चुका है। उनकी परंपरा को महंत वीरभद्र मिश्र ने आगे बढ़ाया, जो बीएचयू के प्रोफेसर थे, पर्यावरणविद थे और स्वच्छ गंगा अभियान के अग्रदूत थे। आज उनके पुत्र प्रो. विशम्भर नाथ मिश्र इस परंपरा को उसी श्रद्धा और सादगी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। वे भी पखावज वादन में सिद्धहस्त हैं।
पहले यह समारोह मंदिर की मुख्य ड्योढ़ी पर होता था। बाद में मंदिर के सामने कुएं के जगत को इसका मंच बनाया गया। तब इसका दायरा स्थानीय कलाकारों तक सीमित था। बनारस के दो मोहल्ले-कबीरचौरा और रामापुरा, जो शास्त्रीय संगीत की आत्मा कहे जाते हैं। वहीं से कलाकार आते थे। समय बदला, मंच बड़ा हुआ, श्रोता बढ़े, लेकिन संकट मोचन संगीत समारोह की आत्मा वैसी की वैसी रही-निर्लिप्त, नि:स्वार्थ, निष्कलंक। आज भी न कोई मंचीय लाउडस्पीकर है, न कैमरे की चकाचौंध। केवल सुर, ताल और लय की वह त्रयी जो मिलकर आराधना बन जाती है। संकट मोचन संगीत समारोह सौ बरस पार कर चुका है, लेकिन उसके सुरों की उम्र अब भी वही है, जैसे अभी-अभी रचा गया हो कोई राग, किसी भक्त की सांसों में।
अनूठे संगीतकार, अनूठी परंपरा
संकट मोचन संगीत समारोह की आत्मा बनारस है, मगर इसकी बाहरी सांसें भी हैं, जिनका पहला स्पंदन उस समय महसूस किया गया जब पंडित मणिराम, पद्मविभूषण पंडित जसराज के बड़े भाई, बनारस से बाहर के पहले ऐसे कलाकार बने जिन्हें संकट मोचन के मंच पर आमंत्रित किया गया। वह कोई साधारण क्षण नहीं था। वह एक युगांतकारी पल था जब बनारस की संगीत परंपरा ने बाहरी सुरों के प्रति अपने द्वार खोले। फिर 1966 में वायलिन के अद्भुत जादूगर पंडित वी. जी. जोग ने जैसे इस दरबार को अपनी तानों से मोहित कर लिया। उस दिन उनकी वायलिन में बनारसी गंगा की धार समा गई थी। उनके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे पंडित राजन-साजन मिश्र के चाचा और गुरु पंडित गोपाल मिश्र। वह शाम न सिर्फ़ संगीत की संगति थी, बल्कि गुरु-शिष्य परंपरा और बनारस की विरासत का भावनात्मक संवाद भी।
उस समय की परंपरा थी कि संकट मोचन का यह समारोह तबले की गूंज से आरंभ होता। पंडित किशन महाराज की उंगलियों से निकलती आवाज़ें जैसे दरबार के पत्थरों पर थिरकती थीं। यह शुरुआत होती थी उस यात्रा की, जो अंत में उनके ही गुरु, पंडित कंठे महाराज के तबले की गंभीरता में डूब जाती थी। तबला एक साधना था, और संकट मोचन उस साधना का साक्षात मंदिर। जब कोविड आया और महामारी ने दरबार को सूना कर दिया, तब एक ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेते हुए जब पंडित जसराज ने यह कहा कि वे संकट मोचन दरबार में उपस्थित नहीं हो सकते, तो उनकी आंखें भर आईं। यह केवल एक कलाकार का भाव नहीं था, वह उस भक्त की करुण पुकार थी जिसे उसके आराध्य से दूर कर दिया गया था।
मेवाती घराने से जुड़े भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया था। इनकी तरह ही सुप्रसिद्ध बासुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया इस साल संगीत समारोह में आए तो अपने भावों को साझा किया। कहा, “हमारा संगीत केवल मंच का अभिनय नहीं रहा, वह तो हमारी आत्मा की पुकार रहा है। हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में, विशेषकर ऋग्वेद में, ध्वनि और स्वर का अस्तित्व स्पष्ट दिखाई देता है। “नेमि नमंति चक्षषां मेषं विप्रा अभिस्वंरा” इस मंत्र में गायक वृत्त बनाकर देवताओं के लिए गायन कर रहे हैं। वेदों के अनुसार, मंदिरों के निर्माण से भी बहुत पहले, वाद्य यंत्र बन चुके थे। ब्रह्मा ने उसे जन्म दिया, शिव ने उसे लय दी और नारद ने उसे लोक में प्रवाहित किया।”
“प्राचीन ग्रंथों में सबसे पुराना शब्द जो वाद्य स्वर के लिए आया, वह ‘स्वराति’ है-“अव स्वरातति गर्गर:।” इससे पता चलता है कि भारतीय संगीत का मूल स्वर में है, लय में है, नाद में है। ऋग्वेद और सामवेद में जहां एक ओर ऋचा गायन की छंदानुशासन की परंपरा रही, वहीं दूसरी ओर सामगायन में पाठ की नादात्मकता और उसकी मुद्रात्मक अभिव्यक्ति जुड़ती गई। जब हस्तमुद्राएं गायन से जुड़ीं, तो वह केवल ध्वनि नहीं रही, वह दर्शन बन गई। गायन का पहला रूप अर्थहीन ध्वनियों का था-एक ऐसी नाद-यात्रा जिसमें कोई भाषा नहीं थी, सिर्फ़ भावना थी। कुछ-कुछ वैसा ही जैसे आज का तराना।”
चौरसिया कहते हैं, “वैदिक ऋषियों का संगीत मंदिरों में नहीं, जंगलों में था-अपने आश्रमों में, यज्ञों के मध्य, ध्यान की लय में। वहां कोई श्रोता नहीं, केवल सृष्टिकर्ता था। धीरे-धीरे यह संगीत मंदिरों में प्रविष्ट हुआ और ईश्वर को प्रसन्न करने का एक गूढ़ माध्यम बन गया। खजुराहो और कोणार्क जैसे मंदिरों की दीवारों पर अंकित गंधर्वों की मूर्तियां इस बात का प्रमाण हैं कि संगीत और भक्ति का यह संगम शाश्वत है, सनातन है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की यह सबसे प्राचीन शैली मंदिरों की देहरी से उपजी। जब मंदिरों में देवता को भोग के साथ राग भी चढ़ाया जाता था, जब पूजा में दीपक के साथ आलाप भी जलते थे। यह गायन शुद्ध, गंभीर, और ध्यान में डूबा हुआ होता था। मंदिरों से होते हुए यह संगीत लोक तक पहुंचा और फिर राजदरबारों में अपने शिखर को छूने लगा।”
ज्ञान, मोक्ष और संगीत त्रिवेणी बहती है
संकट मोचन मंदिर के महंत प्रो. विशंभरनाथ मिश्र कहते हैं, “बनारस जहां ज्ञान, मोक्ष और संगीत त्रिवेणी की तरह बहते हैं, वहीं संकट मोचन का मंदिर इस त्रिवेणी में जैसे एक पावन तीर्थ है। इस तीर्थ में ध्रुपद की साधना, हनुमानजी की उपासना बन जाती है, क्योंकि वे केवल पराक्रमी नहीं, रसिक भी हैं। वे रण के रौद्र भी हैं और राग के रसनिष्ठ भी। कहते हैं जब वे प्रभु श्रीराम के सामने मृदंग बजाते थे, तब गंधर्व लोक भी अभिभूत हो उठता था। संकट मोचन मंदिर में संगीत केवल भक्ति नहीं, उसका विस्तार भी है। यह कोई संयोग नहीं कि इस मंदिर में हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी को जब संकट मोचन संगीत समारोह शुरू होता है, तब उसके पहले स्वर से अंतिम ताल तक पूरे वातावरण में संगीत नहीं, भक्ति बहती है।”
प्रो. मिश्र कहते हैं, “संकट मोचन संगीत समारोह केवल एक आयोजन नहीं, यह भारतीय संगीत की आत्मा का उत्सव है। यह उत्सव बताता है कि संगीत का परम उद्देश्य केवल आनंद नहीं, आत्मा की मुक्ति है। संकट मोचन संगीत समारोह हर वर्ष इस सत्य को साक्षात करता है। यह केवल कलाकारों का नहीं, हमारी संस्कृति का जयघोष है। काशी की यह परंपरा, यह समारोह, यह संगीत-सब मिलकर एक ऐसी नदी बनते हैं, जो केवल स्वर नहीं बहाती, संस्कृति बहाती है, साधना बहाती है। यहां मंच पर बैठा कलाकार एक प्रस्तोता नहीं, एक उपासक होता है। वह प्रस्तुति नहीं देता, वह अर्पित करता है। मंच मंच नहीं, एक आरती की थाली बन जाता है। राग का दीपक जलता है, ताल की लौ थिरकती है, और स्वर, जैसे प्रभु के चरणों में सिर नवाते हैं।”
बनारस के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र दुबे इस सांस्कृतिक विरासत को केवल संगीत का उत्सव नहीं मानते, बल्कि इसे गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल कहते हैं। वे याद करते हैं, “जब संकट मोचन मंदिर में बम विस्फोट हुए, तो प्रशासन ने प्रबंधन पर बंद करने का दबाव बनाया। लेकिन उस वक्त मुफ्ती-ए-बनारस और लाल चर्च के पादरी स्वयं मंदिर पहुंचे, और यह साबित कर दिया कि संगीत और आस्था किसी एक मज़हब की जागीर नहीं हैं।संकट मोचन मंदिर ने समूची दुनिया को सिखाया है कि संगीत का कोई मज़हब, कोई जात, कोई लिंग, और कोई वर्ग नहीं होता। यहां एक रिक्शा चलाने वाला संगीतप्रेमी, करोड़ों का कारोबार करने वाले धनकुबेर के साथ पंक्ति में बैठकर राग-रागिनियों में डूब जाता है।”
राजेंद्र कहते हैं, “आज जब आधुनिकता की दौड़ में हमारे आसपास के उत्सव अपना आत्मा खोते जा रहे हैं, तब संकट मोचन संगीत समारोह एक जीवित विरासत की तरह खड़ा है। एक गवाही की तरह कि कला जब मंदिर की चौखट पर सिर झुकाकर प्रवेश करती है, तब वह केवल सुंदर नहीं रहती, वह पवित्र भी हो जाती है। यह आयोजन संगीत का कुंभ है, जहां एक बार आ जाने वाला लौटकर ज़रूर आता है। और जब लौटता है, तो केवल स्मृतियों में नहीं, बल्कि सुरों की किसी पगडंडी पर जो उसे मंदिर की शांति, बनारस की आत्मा और संगीत के मोक्ष तक ले जाती है।”
“यहां संगीत का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई लिंग नहीं। संकट मोचन ने दुनिया को बताया है कि यदि कहीं सच्चा लोकतंत्र है तो वह इसी संगीत में है।” और यह बात केवल कथन नहीं, अनुभूति है। जिसे केवल संकट मोचन की रात में बैठकर ही समझा जा सकता है।- यदि यही कार्यक्रम कहीं किसी सभागार में होते, तो एक दर्शक को बीस से बाईस हज़ार रुपये तक चुकाने पड़ते। परंतु यहां संगीत की यह गंगा बिना टिकट, बिना भेदभाव, हर साल बहती है।”
दुबे कहते हैं, “संकट मोचन संगीत समारोह की जड़ें गहरी हैं-पंडित अमरनाथ मिश्र (पखावज वादक) और प्रो. वीरभद्र मिश्र (गायक) की परंपरा को अब पंडित विशंभरनाथ मिश्र (पखावज वादक) ने आगे बढ़ाया है। आज इस आयोजन मंडल में वे संगीत साधक शामिल हैं, जिन्हें केवल सुनकर नहीं, आत्मा से अनुभव किया जाता है। वे संगीत की उस गहराई में उतर चुके हैं, जहां छल, भंगिमा और दिखावे का कोई स्थान नहीं होता। यूं कहा जाए, तो वे सब उस जलधारा की मछलियां हैं, जो केवल सच्चे सुरों में सांस लेती हैं।”
छह रातों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में संकट मोचन मंदिर परिसर सुरों की पवित्र गूंज से गूंज रहा है। मंच पर देशभर से आए दिग्गज कलाकारों की प्रस्तुतियां श्रोताओं को भावविभोर कर रही हैं। संगीत प्रेमियों की भीड़ मंत्रमुग्ध होकर हर प्रस्तुति का आनंद ले रही है। तावरण में राग, ताल और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिल रहा है। समारोह में इस बार भी मुस्लिम कलाकारों की भागीदारी ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। तबला वादक उस्ताद अकरम खां, शास्त्रीय गायक समीउल्लाह खां, सितार वादक रईस खां, उस्ताद मेहताब अली नियाजी और अरमान खान अपनी प्रस्तुति से महफिल में चार चांद लगा रहे हैं।
इस साल भी भजन सम्राट अनूप जलोटा की मधुर भक्ति रचनाएं श्रोताओं को भक्ति भाव में सराबोर करेगी। पंडित साजन मिश्र की गायकी, सुरेश तलवलकर की लयकारी, पंडित धर्मनाथ मिश्र और पंडित शिरोमणि की पारंपरिक शास्त्रीय प्रस्तुतियां समारोह को ऊंचाइयों तक ले जाएंगीं। रवि शंकर मिश्रा, सलील भट्ट, नागराज माधवप्पा और अजय चक्रवर्ती जैसे प्रतिष्ठित कलाकारों की प्रस्तुतियां भी श्रोताओं को शास्त्रीय संगीत की गहराइयों में गोता लगवाएंगी। इस भव्य संगीत महाकुंभ में युवा कलाकारों को भी मंच दिया गया है, जो आने वाले समय में भारतीय संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह संगीत महोत्सव केवल एक कार्यक्रम भर नहीं, बल्कि संगीत प्रेमियों के लिए वार्षिक तीर्थयात्रा जैसा है।
बनारस के वरिष्ठ रंगकर्मी और संवेदनशील कवि व्योमेश शुक्ल इस सांस्कृतिक विरासत को केवल संगीत का उत्सव नहीं मानते, बल्कि इसे गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल कहते हैं। संकट मोचन मंदिर परिसर में चल रहे ऐतिहासिक संकट मोचन संगीत समारोह के संचालक एवं देश के प्रतिष्ठित रंगकर्मी, साहित्यकार व्योमेश कहते हैं, “संकट मोचन मंदिर ने समूची दुनिया को सिखाया है कि संगीत का कोई मज़हब, कोई जात, कोई लिंग, और कोई वर्ग नहीं होता। यहां एक रिक्शा चलाने वाला संगीतप्रेमी, करोड़ों का कारोबार करने वाले धनकुबेर के साथ पंक्ति में बैठकर राग-रागिनियों में डूब जाता है। संकट मोचन संगीत समारोह हमें यह सिखाता है कि संगीत में धर्म नहीं होता-उसमें दिशा होती है, वह दिशा जो ईश्वर की ओर, और सबसे पहले इंसान की ओर ले जाती है।”
“संकट मोचन समारोह केवल संगीत का मंच नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा का जीवंत उदाहरण है। यह गरीबों का संगीत समारोह है। बनारस और पूर्वी उत्तर प्रदेश के देहाती नागरिक, जो धूप में तपे हुए, धोती-कुर्ता पहने आते हैं, इस मंच पर संभ्रांतता की परिभाषा बदल देते हैं। विगत 102 वर्षों से यह समारोह हमें याद दिलाता है कि शास्त्रीय संगीत के असली पारखी अब भी शहरों से ज्यादा गांवों में बसते हैं। भारतीय संस्कृति का उच्च अगर कहीं है, तो वह गांवों में है।”
इस अनूठे समारोह की नींव रखने वालों का स्मरण करते हुए व्योमेश पंडित किशन महाराज, पंडित अमरनाथ मिश्र, कविराज आशुतोष भट्टाचार्य और गोपालजी मिश्र को नमन करते हैं और कहते हैं, यह समारोह कलाकारों द्वारा कलाकारों के लिए कल्पित और संचालित एक अनूठा आयोजन है। यह केवल एक संगीत उत्सव नहीं, बल्कि बनारस की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Cultural Heritage) का जीवंत प्रमाण है। यह वह मंच है जिसने उत्तर भारत में पहली बार कंगना बैनर्जी जैसी महिला कलाकार को मंच दिया और अनगिनत मुस्लिम कलाकारों को भी मंदिर प्रांगण में अपनी विद्या दिखाने का अवसर दिया। यह समारोह बताता है कि बनारस अमर है। बनारस का जो वर्तमान है, वही उसका भविष्य भी है।”
समारोह की समावेशिता पर विशेष बल देते हुए व्योमेश कहते हैं कि यह मंच न केवल अमीर-गरीब की खाई को मिटाता है, बल्कि धर्म और जाति के भेदभाव को भी नकारता है। यहां केवल कलाकारिता, भगवत प्रेम और हनुमान जी के दरबार में हाजिरी लगाने का जज़्बा मायने रखता है। अंत में उन्होंने कहा, “अगर किसी कलाकार ने संकट मोचन में परफॉर्म कर लिया, तो मानो उसने एक तीर्थ स्नान कर लिया। यहां कलाकारों के सत्य की परीक्षा होती है। संकट मोचन संगीत समारोह, एक बार फिर बनारस की सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना का प्रतीक बनकर उभरा है, जहां संगीत, श्रद्धा और समरसता एक साथ झंकृत होते हैं।”
(विजय विनीत बनारस के वरिष्ठ पत्रकार हैं)






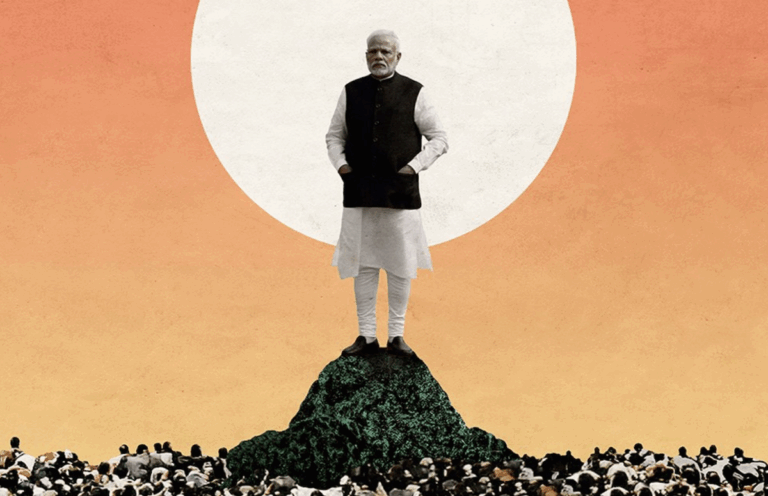


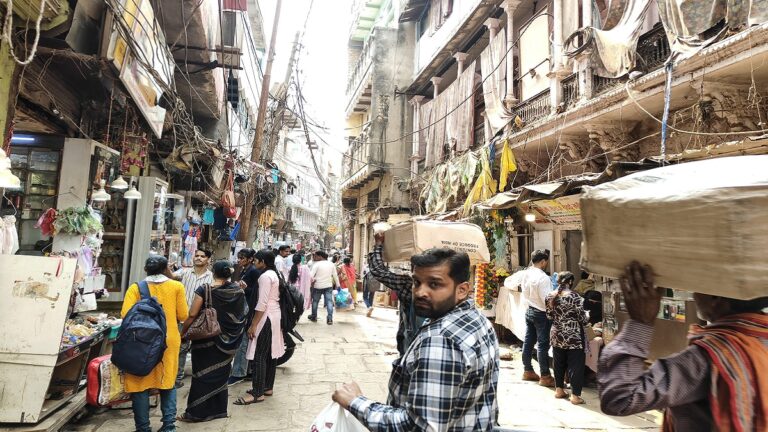

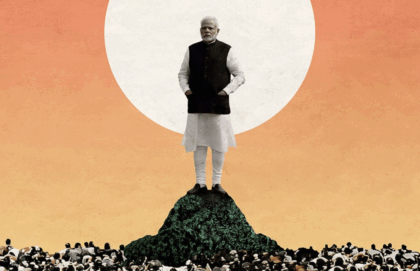
+ There are no comments
Add yours