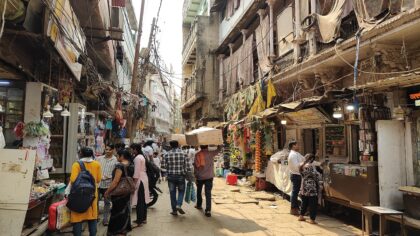पश्चिमी यूरोपीय ताकतों ने अपने उपनिवेशों से आर्थिक सरप्लस को हड़पा, और इसने भौतिक रूप से और बड़े पैमाने पर 18वीं सदी से लेकर बाद तक उनके अपने औद्योगिक संक्रमण के साथ ही साथ नए यूरोपीय settlements के इलाकों तक पूंजीवाद के विस्तार में मदद पहुंचाई। लेकिन आर्थिक विकास के साहित्य में हमें ऐसे दोहन के बारे में नहीं के बराबर जानकारी मिलती है, दोहन की विशाल मात्रा या उसके विशिष्ट, वास्तविक और आर्थिक तरीकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके बारे में अभी बहुत शोध किया जाना बाकी है। हालांकि भारत के संदर्भ में एक सदी से अधिक समय से इस दोहन पर जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया एक बहुत समृद्ध बहस होती रही है जिसे दो महान लेखकों दादा भाई नौरोजी और RC दत्त ने शुरू किया था।
यहां हम अपने को भारत के संदर्भ में होने वाले दोहन तक सीमित रखेंगे। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाय तो 18वीं 19वीं शताब्दी में, पूंजीवाद के केंद्र देशों में औद्योगिक संक्रमण में उपनिवेशों से होने वाले दोहन की उपेक्षा की गई है। मुख्यधारा की व्याख्या में पूंजीवादी औद्योगिकरण के लिए पूरी तरह आंतरिक गतिविज्ञान को श्रेय दिया गया है, कुछ लेखकों का तो यहां तक मानना है कि उपनिवेश पूंजीवादी केंद्रों पर एक तरह से बोझ थे, जो उनके बिना ज्यादा बेहतर स्थिति में होते।
भारत के मामले में दोहन की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है, कि कुल कर राजस्व का एक तिहाई नियमित रूप से खर्च नहीं किया जाता था बल्कि उसका उपयोग सामान खरीदने के लिए किया जाता था जिसे निर्यात कर दुनिया से सोना और विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती थी।
लेकिन यह अर्जित संपत्ति, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, उसका लाभ हमारे देश को नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें शासक सत्ता द्वारा हड़प लिया जाता था। दो अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि उपनिवेशों से विशेषकर भारत से निर्यात सरप्लस के रूप में अर्जित इस सोना और विदेशी मुद्रा ने 19वीं सदी के आखिरी चतुर्थांश में पूंजीवाद के विकास को तेज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अपने उपनिवेशों से अर्जित निर्यात सरप्लस को बड़े पैमाने पर विदेशों को पूंजी निर्यात करके ब्रिटेन ने यूरोपीय देशों के तथा यूरोप की नई सेटलमेंट बस्तियों वाले देशों के औद्योगिकरण को तेज किया।
इसका दूसरा पक्ष यह था कि उपनिवेशों में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता घटती गई और आबादी का दरिद्रीकरण बढ़ता गया। यह दोहन बहुआयामी था। इसका आंतरिक पहलू था उत्पादकों से rent और टैक्स से आर्थिक सरप्लस का दोहन। भारत में राज्य द्वारा नकद वसूली सबसे प्रमुख माध्यम थी, जिसमें भू राजस्व लंबे समय तक प्रमुख अवयव था।
स्वतंत्र उत्पादक सरकार को सीधे टैक्स देते थे। जो tenant खेतिहर थे, वे अपने आर्थिक सरप्लस में से भूस्वामी को rent देते थे जिसे वह सरकार को देता था। अफीम और नमक पर सरकार का एकाधिकार, जिसका बोझ किसानों मजदूरों पर पड़ता था, राजस्व का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत था। हालांकि टैक्स अपने आप में दोहन नहीं था। बल्कि यह जब दूसरे, वाह्य आयाम से जुड़ता था, जैसा नौरोजी और दत्त ने कहा, बजट में कर राजस्व के एक बड़े हिस्से को “विदेशी खर्च” बता दिया जाता था, यानी देश के अंदर नियमित खर्च से अलग कर दिया जाता था, इसे दुनिया के साथ भारत के उत्पादकों के निर्यात सरप्लस की अदायगी माना जाता था और इसे लंदन में रखा जाता था। इस निर्यात सरप्लस से नकद सिक्का और स्टर्लिंग मिलती थी, अकाउंटिंग में हेराफेरी करके इसका पूरा इस्तेमाल औपनिवेशिक देश अपने लिए करता था।
देश के बजट का ऐसा इस्तेमाल, निर्यात सरप्लस के उत्पादकों को उन्हीं के टैक्स योगदान से भुगतान, जबकि माल निर्यात का लाभ कभी भी उस देश के हिस्से नहीं आता, यह किसी संप्रभु देश में संभव नहीं है।
यह औपनिवेशिक व्यवस्था की विशिष्टता है। प्रत्यक्षतः निर्यात सामग्रियों के सभी उत्पादकों को भुगतान किया जाता था।औपनिवेशिक निर्यात का एक हिस्सा ब्रिटिश उत्पादकों से टेक्सटाइल के आयात द्वारा भुगतान किया जाता था।
लेकिन यह आयात औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के व्यापार को उदार बना कर किया जाता था। स्थानीय दस्तकारों, बुनकरों के विस्थापन की कीमत पर माल खपाया जाता था, जबकि ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी केंद्रों में औपनिवेशिक उत्पादकों से संरक्षण की व्यवस्था थी, ऐसा एक सदी से ऊपर तक था।
कुल निर्यात सरप्लस में से आवश्यक लगने वाले आयात को घटाने के बाद जो कुल निर्यात सरप्लस बचता था, वह एक नियमित व्यवस्था के रूप में उत्पादकों को नहीं दिया जाता था। क्योंकि उन्हें देश के अंदर जमा होने वाले टैक्स में से भुगतान किया जाता था। ऐसे टैक्स का बड़ा हिस्सा उन्हीं उत्पादकों से वसूला जाता था, किराया, जमीन की लगान और अप्रत्यक्ष करों के बतौर, विशेष कर नमक पर एकाधिकार से। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्पादकों से वास्तव में टैक्स वसूला जाता था जबकि यह आभास कराया जाता था कि उन्हें भुगतान किया जा रहा है।
उदाहरण के लिए मान लीजिए भारत में एक किसान दस्तकार, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में सरकार को 100रु टैक्स दिया। उसने 50रु में 10गज कपड़ा और दो बोरा चावल एक स्थानीय व्यापारी को बेचा। यह एक सामान्य क्रय विक्रय हुआ और उत्पादक के टैक्स से उसका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि व्यापारी ने उसको पैसा दे दिया इस उम्मीद से कि उसे आगे बेचकर वह कमाएगा। अब मान लीजिए कि कंपनी के किसी एजेंट ने वही सामान उससे अर्जित 100रु टैक्स में से 50रु देकर खरीद लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि इस मामले में उत्पादक को कुछ नहीं मिला। अगर टैक्स वसूलने वाला एजेंट ही उत्पादक से सामान खरीदता तो उससे वह पूछ सकता था। लेकिन ये दोनों एजेंट अलग होते थे, इसलिए उत्पादक उन दोनों को एक साथ जोड़कर नहीं देख पाता था।
कंपनी के एजेंट द्वारा खरीद
उत्पादक को किसी देशी व्यापारी द्वारा खरीद जैसी ही सामान्य प्रतीत होगी। लेकिन यह गुणात्मक रूप से बिल्कुल भिन्न थी क्योंकि उत्पादक ने जो टैक्स दिया था, उसी का एक हिस्सा उसके माल की कीमत के रूप में उसके पास वापस आया। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे उत्पादक समझ नहीं रहा है जबकि उत्पादक से कपड़ा और चावल ले लिया गया। इस लेनदेन में कुल 100 रु का टैक्स 50रु नकद और 50रु के कपड़े और दो बोरी चावल में विभाजित हो गया।
कुल मिलाकर उत्पादक ने यह सामान कंपनी को मुफ्त में निर्यात के लिए दे दिया। कपड़ा और चावल इंग्लैंड को निर्यात कर दिया गया, 5पाउंड का माल कुल मिलाकर 7 पाउंड में।
क्योंकि किसान और दस्तकार कुल टैक्स में मुख्य योगदान कर्ता थे, लेकिन उन्हें वास्तव में कोई भुगतान नहीं हुआ। कुल मिलाकर हुआ यह कि उनके टैक्स का एक हिस्सा नकद से माल में बदल दिया गया निर्यात के लिए।
यह जो राजकोषीय वित्तीय व्यवस्था को सीधे व्यापार से जोड़ दिया गया, यही उपनिवेशों से दोहन का सार है।
जहां उत्पादक गुलाम नहीं थे बल्कि नाम के लिए स्वतंत्र लघु उत्पादक थे, टैक्स दाता किसान और दस्तकार थे। शुरू में स्थानांतरण प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से पारदर्शी थी। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई व्यापार की इजारेदारी 1600 ईस्वी में शुरू हुई। कंपनी को एशिया से अपने आयात सरप्लस के लिए चांदी में भुगतान करना पड़ता था, जिससे शुरुआती दौर में व्यापारियों का उन्हें गुस्सा भी झेलना पड़ा।
कंपनी को 1765 में बंगाल राज्य में कर राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। बड़े पैमाने पर दोहन तभी से शुरू होता है।
कुछ दोहन तो पहले से ही लघु उत्पादकों पर दबाव डालकर उनके सामानों को कम दाम पर खरीदने से शुरू हो गया था। लेकिन यह 1765के बाद होने वाले भारी दोहन की तुलना में कुछ भी नहीं था, जब स्थानीय टैक्स का इस्तेमाल करके निर्यात के सामान मुफ्त में हड़पा जाना शुरू हुआ।
बंगाल की तीन करोड़ आबादी ब्रिटेन की लगभग चार गुना थी। कंपनी की लूट की हवस, जिसके तहत अगले 5 साल में राजस्व वसूली को जबरदस्ती तीन गुना कर दिया गया, उसके फलस्वरूप 1770 के भयानक अकाल में वहां की एक तिहाई आबादी खत्म हो गई। 1792 तक पूरी तरह स्थिति सुधर नहीं पाई थी, फिर भी स्थाई बंदोबस्त के तहत भू-राजस्व की उगाही उस साल ब्रिटेन के भू-राजस्व से अधिक थी।
अगले 80साल में राजस्व संग्रह तीन गुना हो गया, जब बंगाल को आर्थिक आधार बनाते हुए कंपनी ने कई और राज्यों पर राजनीतिक आधिपत्य कायम कर लिया, बॉम्बे , मद्रास, पंजाब और अवध। बर्मा वाले तीन युद्ध लड़े। उपजाऊ निचले बर्मा पर 1856 में और पूरे देश पर 1885 तक कब्जा हो गया।
भू-राजस्व की वसूली सब जगह शुरू हो गई। जिले के सबसे बड़े अधिकारी का नाम ही कलेक्टर पड़ गया। ब्रिटेन बिना कोई मूल्य दिए राजस्व से खरीदे गये चावल, नमक, नील, कच्चा कपास आदि से पट गया। जो उसकी अपनी जरूरतों से ज्यादा था, वह दूसरे देशों को पुनः निर्यात कर दिया जाता था।
इस दोहन में यह निहित था कि ब्रिटेन को व्यापार घाटे के लिए भारत को कुछ भुगतान नहीं करना था, जैसा उसे दूसरे संप्रभु देशों मसलन फ्रांस को करना पड़ता। यही दूसरे संप्रभु देशों या भारत के लिए भी 1765 तक सच था। लेकिन उसके बाद जब से स्थानीय टैक्स संग्रह शुरू हुआ, स्थिति बदल गई। भारत से कपड़े और चावल के निर्यात के बदले इंग्लैंड को कुछ नहीं देना था क्योंकि उत्पादकों को उनके टैक्स में से वह कीमत पहले ही दी जा चुकी थी यानी उन्हें दरअसल कुछ नहीं मिला था। टैक्स के रूप में वसूला जा रहा यह आर्थिक सरप्लस, उससे हासिल किया गया मुफ्त का माल यही भारतीय उपनिवेश से संपदा के दोहन का सार था।
इससे शून्य कीमत पर वसूली गई मालों पर अंधाधुंध मुनाफे से केवल कंपनी को फायदा नहीं हो रहा था, इससे एक देश के बतौर ब्रिटेन को भी फायदा हो रहा था। भारतीय सामानों के आयात सरप्लस के भुगतान की कोई जिम्मेदारी इंग्लैंड पर नहीं थी। ऊपर से दिखने वाला भारत से व्यापार घाटा पर इंग्लैंड के लिए कोई भुगतान की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि वह इंग्लैंड के संसाधनों को बढ़ा रहा था। क्योंकि वह तो भारत में संग्रह किए गए स्थानीय करों से हासिल किया गया आयात था।
1790 की इंग्लैंड की आयात निर्यात रिपोर्ट में कहा गया कि ईस्ट इंडिया के व्यापार में निर्यात से बहुत अधिक जो आयात यानी व्यापार घाटा दिखता है, लेकिन यह कंपनी के भारी राजस्व के फलस्वरूप होने के कारण वह नुकसानदेह होने की बजाय हमारे सरकारी खजाने में जबरदस्त बढ़ोत्तरी दिखाता है।
अगर उपनिवेश एक संप्रभु राष्ट्र होता तो इसका विदेशी व्यापार से होने वाला मुनाफा देश के खजाने में आता। इसकी अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति को बढ़ाता और निर्यात सरप्लस यहां के उत्पादकों को उनकी मुद्रा में लाभ पहुंचता, उस टैक्स से संबद्ध जो भले उन्हें देना पड़ता या न पड़ता। जो टैक्स वे देते, वह सामान्य बजट प्रक्रिया का हिस्सा होता।
औपनिवेशिक ताकत को हमेशा स्थानीय आबादी के ऊपर किसी न किसी रूप में संपत्ति का अधिकार स्थापित करने की जरूरत पड़ती थी। क्योंकि यह आवश्यक शर्त थी सरप्लस वसूलने और उसको अपने देश भेजने की।
भारत में यह टैक्स वसूली का संप्रभु अधिकार था, तो वेस्ट इंडीज में गुलाम प्लांटेशन मजदूरों का श्रम था जिससे सरप्लस निचोड़ा जाता था। आयरलैंड में जाकर बसे अंग्रेज जमींदारों ने स्थानीय किसानों की जमीन ले ली, उनसे भू-राजस्व और टैक्स के बतौर आर्थिक सरप्लस वसूला जाता था।
हर मामले में सामान मुफ्त में लिया जाता था जो हड़पे गए आर्थिक सरप्लस के बराबर माल होता था, चाहे वह slave rent हो, भू राजस्व हो, कर हो या इन तीनों का मिला जुला रूप हो। कंपनी के माध्यम से कर द्वारा वित्त पोषित स्थानांतरण बिल्कुल सीधा और पारदर्शी था।
कुल टैक्स राजस्व के एक चौथाई से लेकर एक तिहाई तक वार्षिक टैक्स राजस्व निर्यात के सामान खरीदने के लिए खर्च होता था, 1840 तक सूती कपड़े जिसका बड़ा हिस्सा थे। इस तरह ब्रिटेन को भारी मात्रा में सामान मिल जाते थे , जो उसकी अपनी जरूरत से बहुत अधिक होते थे। इसका एक हिस्सा वह अपने पास रख लेता था, शेष दूसरों को अन्य सामानों के बदले जिसे उसको जरूरत थी, निर्यात कर देता था।
आयातित सूती कपड़ा तो वह पूरा निर्यात कर देता था क्योंकि 1700 में ब्रिटिश ऊन उद्योगपतियों के दबाव में ब्रिटिश संसद ने भारत और फारस से आयातित शुद्ध सूती कपड़ों के उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। और 1721में उसका उपभोग करने वालों पर भारी आर्थिक दंड भी लगा दिया था। भारत से कंपनी द्वारा आयातित सारे टेक्सटाइल का इंग्लैंड के बंदरगाहों पर भंडारण होता था और वहीं से यूरोप और कैरेबियन देशों को निर्यात कर दिया जाता था।
लगभग 7दशक बाद, 1774 से शुरू करके एक बार जब मशीनों से सूती धागा तैयार होने लगा तब उसके उपभोग पर प्रतिबंध हटा लिया गया। लेकिन चुंगी के रूप में, जिसे 1775 से 1813 तक बहुत बढ़ा दिया गया, ब्रिटिश बाजार में एशियाई सूती कपड़ों
पर प्रतिबंध जारी रहा। जो अंततः 1846 में खत्म हुआ।
एशियाई सूती कपड़ों के खिलाफ ब्रिटेन की कड़ी संरक्षणवादी नीति की जो लगभग 150 साल तक चली उसकी भारत की कैंब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री और अन्य ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति तथा सूती कपड़ा उद्योग में तकनीकी बदलाव के तमाम इतिहासकारों ने पूरी तरह उपेक्षा कर दी है। हाल के लेखक भी भूलने की इसी बीमारी के शिकार लगते हैं।
उष्णकटिबंधीय इलाके के उत्पादकों के खिलाफ ब्रिटेन के व्यापारियों की सही चित्र को समझने के लिए जो उनके उपनिवेश बनने के पहले ही शुरू हो गई थीं, हमें FRIEDRICH List, Dutt, Paul Baran Mantoux, and Paul Baran के शुरुआती लेखों को पढ़ना होगा।
Mantoux का सूती कपड़ों की मशीनरी का विस्तृत विवरण, जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का चालक थी, उससे स्पष्ट है कि एशियाई कपड़ों पर प्रतिबंध ने मांग को पूरा करने के लिए मशीनों के नवीनीकरण और आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित किया। भारतीय टेक्सटाइल के खिलाफ भेदभाव पर लिस्ट की टिप्पणियां भी यही बताती हैं।
शुद्ध कपास के उपभोग पर प्रतिबंध Mantoux के शब्दों में वह चाहे जहां से भी हो, प्रतिबंध लगा रहा। कोई भी संरक्षण इतना पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि इसने कपड़ा उत्पादकों को घरेलू बाजार पर वास्तविक एकाधिकार दे दिया।”
1650 से जारी Navigation Acts के तहत प्रत्येक महत्वपूर्ण समान पहले इंग्लैंड के बंदरगाहों पर आता था, उसके बाद दूसरे जगहों को उसका पुनर्निर्यात किया जाता था। सामानों को ब्रिटिश जहाजों में ब्रिटिश अधिकारियों की देखरेख में ही ले जाया जाता था।
यह एक गलत धारणा है कि उपनिवेशों से सबसे महत्वपूर्ण आयात कच्चे माल का होता था। खाने का सामान पूरी 18वीं सदी में, और मध्य उन्नीसवीं सदी तक सबसे महत्वपूर्ण आयात बना रहा, जब कच्चे कपास का आयात तेजी से बढ़ने लगा।
Phyllis Deane ने 1965 में The First Industrial Revolution में इसकी विस्तार से विवेचना किया कि 18वीं सदी में पुनर्निर्यात कितने महत्वपूर्ण थे, जिससे ब्रिटेन को यूरोप से नेवी से जुड़े रणनीतिक समान खरीदने में मदद मिली।
यह विमर्श 1969 में उनकी कोल के साथ मिलकर प्रकाशित किताब में आया। उन लोगों ने पुनर्निर्यात को आयात व निर्यात दोनों जगह से हटा लिया, जब ब्रिटिश व्यापार की कुल मात्रा की चर्चा किया।
उन्होंने जो आयात देश में रोक लिया गया और देशी निर्यात को जोड़कर गणना किया, यह एक अवधारणा है जिसे विशिष्ट व्यापार कहा जाता है। यह अवधारणा मैक्रो इकोनॉमिक्स की किसी टेक्स्टबुक में नहीं मिलेगी, न तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है (मसलन UN, WB या IMF)।
ये व्यापार की कुल मात्रा की गणना में कुल आयात तथा पुनर्निर्यात समेत कुल निर्यात को जोड़ते हैं। यही सही अवधारणा है। क्योंकि पुनर्नर्यात से आयात किया जाता था, वह उपभोक्ता सामग्री का हो या कच्चे माल का, ठीक वैसे ही जैसे घरेलू निर्यात से किया जाता था।
उत्तर दक्षिण के की उत्पादक क्षमता की विषमता
यूरोप के एक ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित देश का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर कब्जा एक तरह से कभी खत्म न होने वाली सोने की खान पर कब्जा है। यह सोने से भी ज्यादा लाभदायक है। सोने कि सीवन तो अंततः चली जाएगी लेकिन सरप्लस पैदा करने किसान और कारीगर की कर देने की क्षमता तब तक बनी रहेगी जब तक चरम शोषण द्वारा उनका अस्तित्व ही नहीं मिट जाता।
उनसे और अधिक उष्णकटिबंधीय फसलें जैसे गन्ना चावल मसाले काफी चाय तम्बाकू वनस्पति तेल जैसे मूंगफली नारियल का तेल अफीम जूट कपास तरह तरह की लकड़ियां, बागान आदि पैदा करवाए जा सकते हैं जो ठंडी जलवायु वाले इलाकों में नहीं उग सकतीं।
शीत कटिबंधीय यूरोप के उत्तरी क्षेत्र के देश इन उत्पादों के लिए न उस समय इंपोर्ट सब्स्टीट्यूट कर सकते थे, न आज कर सकते हैं। इसके विपरीत उत्तरी क्षेत्र की कोई ऐसी वस्तु नहीं थी, जिसे उष्ण कटिबंधीय इलाके के लोगों को बड़े पैमाने पर आयात करना पड़े, क्योंकि वे अपनी जरूरत की सारी परंपरागत चीजें पैदा कर सकते थे। वे साल में कम से कम दो फसलें पैदा कर लेते थे जबकि ठंडे इलाकों में जलवायु के कारण एक फसल ही पैदा कर सकते थे। दक्षिण के बड़े देश जाड़े के मौसम में ठंडे इलाके की सब फसलें पैदा कर सकते थे, इसके साथ ही मानसून में वे अपनी फसलें तो पैदा करते ही थे। चीनी सम्राट क्यानलॉन्ग ने व्यापार छूट के लिए आए जॉर्ज ।।। के दूत से कहा था कि “हमारे स्वर्गीय साम्राज्य में सारी चीजें बहुतायत में उपलब्ध हैं और हमारी सीमाओं के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है।”
विषम उत्पादन क्षमता की यह जो भौतिक सच्चाई थी, जो यूरोपियन देशों के ऐतिहासिक अभियान और ताकत द्वारा उन्हें पराधीन बनाने तथा व्यापार के लिए मजबूर करने की ओर ले गई , उसकी रेकॉर्डों ने पूरी तरह उपेक्षा कर दी, बल्कि एक तरह से उसके अस्तित्व को ही नकार दिया। रिकॉर्डों ने अपने तुलनात्मक लाभ के मॉडल में मान लिया कि दोनों देश दोनों चीजें पैदा करते हैं।
यानी सारे देश सभी समान पैदा करते हैं। उनकी विशिष्टता और विनिमय से दोनों का लाभ होता है। इस तथ्य को भुला दिया गया कि ठंडे इलाकों में ये सामान पैदा ही नहीं होते। घरेलू स्रोतों से बहुत से सामानों की किसी भी मूल्य पर कीमत शून्य थी और यह स्थिति आज तक बनी हुई है।
रिकॉर्डों के सिद्धांत में एक साधारण सी गलती थी, जहां एक सामान्य सत्य को मान लिया जाता था और उससे एक सामान्य निष्कर्ष निकाल लिया जाता था और उसे सभी स्थितियों पर लागू कर दिया जाता था, जहां वह assumption सही नहीं भी होता था।
क्योंकि रेकॉर्डों की मूल प्रस्थापना ही सही नहीं है। इसलिए दोनों पक्षों को लाभ नहीं हुआ। उल्टे, ऐतिहासिक साक्ष्य दिखाते हैं कि कमजोर देशों को निर्यात की चीजें पैदा करने के लिए मजबूर किया गया जिससे वहां घरेलू खाद्यान्न उत्पादन घट गया। यह भी दिखता है कि इन देशों में घरेलू मैनुफैक्चरिंग उत्पादन भी घट गया और बेरोजगारी बढ़ गई जब इसे अनिवार्यतः विदेश से आयात के लिए खोल दिया गया, क्योंकि बेरोजगार हुए लोगों को खपाने के लिए जमीन भी कम ही बची।
ब्रिटेन के अपने सामानों की मांग की तुलना में उष्णकटिबंधीय सामानों की उत्तरी जनसंख्या में मांग अधिक थी क्योंकि स्थानीय स्रोतों से वे वहां स्थाई तौर पर अनुपलब्ध थीं। आयातित सामग्री के बड़े हिस्से के पुनर्निर्यात से ब्रिटेन के घरेलू निर्यात की क्रयशक्ति 1765 से 1821 के बीच 55% बढ़ गई।
ब्रिटेन द्वारा पुनर्निर्यातित सामान का 80% उष्णकटिबंधीय इलाकों से होता था और निर्यात मुख्य यूरोपीय भूभाग को होता था। 18 वीं सदी में नीदरलैंड का आयातित सामानों का पुनर्निर्यात इसके घरेलू सामानों के निर्यात से अधिक था। इस तरह दोहन और पलायन से दोहरा फायदा था। पूंजीवादी केंद्रों को अपने उपयोग के लिए न सिर्फ मुफ्त में ट्रॉपिकल सामान मिल रहा था
बल्कि वे दूसरे टेंपरेट इलाकों से विनिमय द्वारा अपने जरूरत के सामान लेने के लिए भी स्वतंत्र थे, जिनकी उनके यहां कमी होती थी।
एशिया, वेस्ट इंडीज और आयरलैंड मिलकर 1784 से 1826 के बीच ब्रिटिश आयात का आधा देते थे। ब्रिटेन को अपने एशिया और वेस्ट इंडीज के उपनिवेशों से 1801से 1821 के बीच अपने जीडीपी का 5.3%,से 6.1% आयात सरप्लस हासिल हुआ। आर्थिक गणना से पता लगता है कि आजादी मिलने तक भारत से 369.65 अरब पाउंड संपदा का ब्रिटेन द्वारा दोहन किया गया।
क्रमश: जारी…………..।
(प्रो प्रभात पटनायक और प्रो उत्सा पटनायक के लंबे लेख का संक्षिप्त भावानुवाद है। साभार Monthly Review, अनुवाद लाल बहादुर सिंह )