इक्कीसवीं सदी की आरम्भिक हिन्दी कविता को बीसवीं सदी के अन्त की हिन्दी कविता का ही विस्तार माना जा सकता है। तो प्रश्न यह उठेगा कि बीसवीं शती की कविता क्या है, उसकी प्रवृत्तियां क्या हैं, पहचान क्या है, विशिष्टताएं क्या हैं और तत्समय कौन से कवि सृजनरत रहे हैं। मोटे तौर पर बीसवीं सदी के अन्त की हिन्दी कविता को समकालीन कविता का नाम दिया गया। लेकिन प्रश्न यह भी है कि ऐसा कौन सा समय है जिस दौरान लिखी गई कविता समकालीन नहीं होती। हो सकता है उस कालखंड में कुछ विशेष प्रवृत्तियां अनेकानेक कारणों से कविता में रही हों और उन्हें उस तरह संबोधित और वर्गीकृत किया जाए लेकिन उस समय तो उन्हें समकालीन ही कहा जाएगा।
बहरहाल बीसवीं शती के अंत में लिखी गई कविता क्या थी इस पर बात करना उचित होगा। तो इस संदर्भ में मैं इस कालखंड के कुछेक कवियों की राय साझा करना चाहूंगा। जैसे कि प्रभात त्रिपाठी का मानना है कि- ‘इसमें कोई शक नहीं कि आज की कविता में पर्याप्त विविधता है। रूप और अंतर्वस्तु दोनों में यह विविधता लक्ष्य की जा सकती है, लेकिन इस विविधता के साथ ही कवियों और कवि यश:प्रार्थियों के चलते इसमें एक तरह की एकरसता भी है।’
अब प्रभात जी को यह एकरसता प्रगतिशील-जनवादी कविता के संदर्भ में दिखती है, रूपवादी, श्रंगारी, प्रकृत और शब्दों से खेलने वाली वायवीय कविता में वह एकरसता नहीं देखते हैं, न देखना पसंद करते हैं। अत: उन्हें अशोक वाजपेयी, प्रयाग शुक्ल, जितेन्द्र कुमार, मंगलेश डबराल, सुदीप बैनर्जी और विष्णु खरे अधिक विविधता भरे लगते हैं। पता नहीं क्यों इसमें उन्होंने लीलाधर जगूड़ी और कुंअर नारायण को क्यों छोड़ दिया।
खैर यह उनकी निजी रुचि और पसंद का प्रश्न है। उस पर टिप्पणी करना बाज़िब नहीं। इस कालखंड में विजेन्द्र, चंद्रकांत देवताले, भगवत रावत, मलय, अरुण कमल, राजेश जोशी, नरेन्द्र जैन, केदारनाथ सिंह, आलोक धन्वा, इब्बार रब्बी, उदय प्रकाश, मदन कश्यप, कुमार अंबुज आदि अनेकों कवि भी कविता रच रहे थे जिनपर एकरसता का आरोप कतई नहीं लगाया जा सकता।
अब ध्यान दें समकालीन कविता के, अपने अतीत से संबंध पर केदारनाथ सिंह कहते हैं कि-‘समकालीन कविता का अतीत के साथ रिश्ता कुछ कम हुआ है और उसमें वह प्रेरकता का तत्व लगभग नहीं रहा जो इससे पूर्ववर्ती कविता के संदर्भ में होता था।’ यहाँ यह कहा जा सकता है – निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शील आदि से प्रेरकता न मिलना या लेना कवि का निजी मामला है। कहीं प्रतिबद्धता का प्रश्न है, कहीं अलग दिखने का। पर अब यहाँ अरुण कमल का मानना है कि ‘पीछे की सारी कविता हमारी टेक है। एक कवि में अनेक पूर्वज कवियों के गुणसूत्र मिले होते हैं पर वह सजग होकर एक नई संगति बिठाता है पूर्वज कवियों के बीच जो उसकी परंपरा होती है। हर थोड़े समय पर नई संगति बिठानी पड़ती है।’
साहित्य को आम तौर पर भाव-केंद्रित मानव-क्रिया माना जाता है जहाँ रस और सौंदर्य की प्रधानता रहती है। आजाद भारत में पचास का दशक नयेपन का आग्रही था, शायद वह अपने आंदोलनधर्मी अतीत से पिंड छुड़ाना चाहता था। इसके विपरीत धूमिल, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल जैसे जनकवियों के बाद कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह ने समाज में व्याप्त संघर्ष के हवाले से अपनी काव्यगत मंशा को आकार दिया।
अस्सी के दशक में विश्वव्यापी साम्राज्यवाद का विध्वंसक पैंतरा मुखर हुआ था, और भारत में भी नवउदारवादी उभार की आहटें आने लगी थीं। उन्हें देश में बढ़ते उग्र तनावों के बीच देखा जा सकता था। तब आर्थिक संकट भी मंडराने लगा था और ऐसा विकल्प भारतीय अवाम के पास न बचा था जहाँ सकारात्मक सोच के लिए सुरक्षित जगह होती। इस अनिश्चय की घड़ी में कुमारेंद्र ने लेखकीय रणनीति के तहत निम्न मध्य वर्ग, दलितों और आदिवासियों की तरफ देखना शुरु किया, जहाँ उन्हें श्रम, प्रयोगधर्मिता और साहस के स्रोत नजर आए।
कुमारेन्द्र के यहाँ हो-ची-मिन्ह के वियतनाम, माओ के चीन पर कविताएं तो हैं ही, अमरीकी साम्राज्यवाद के सच को प्रस्तुत करती कविताएँ भी हैं। तो क्रांतिकारी रचनाओं के वे दुर्लभ अनुवाद भी हैं जो ‘युग परिबोध’ पत्रिका के लिए उन्होंने सहर्ष किये थे। अपने समय की विसंगतियों के चलते एक कशमकश कुमारेन्द्र में आकार लेती रही, जिसकी तीखी अभिव्यक्ति उनकी ‘‘लाल तराई का गीत’’ शीर्षक प्रसिद्ध कविता में व्यक्त हुई।
साहित्य और कलाओं में वैचारिक आंदोलनों को सामाजिक सरोकारों और मानवीय मूल्यों को रेखांकित, स्थापित करने के लिए आवश्यक उपादान की तरह देखा जाता रहा है। वैचारिक आंदोलनों ने साहित्य और कलाओं को अनेक बार नई दिशा दी है। मगर पिछले कुछ सालों से न सिर्फ हिंदी, बल्कि दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में कोई साहित्यिक आंदोलन नहीं दिखाई देता। तो क्या इसका अर्थ यह लगाया जाना चाहिए कि साहित्य कहीं ठहर गया है, उसकी कोई दिशा नहीं है, वह सामाजिक सरोकारों, मानवीय मूल्यों से विमुख, स्वच्छंद हो चुका है? या इसके पीछे कोई और कारण हैं?
किसी भी युग की परिस्थितियों को रचनात्मक संगति देने में उस देश के नागरिकों एवं समाज का हाथ निश्चित रूप से होता है। रचनाकार समाज की एक इकाई होने के कारण सृजन में सक्रिय रहता है और अपनी रचनाओं के माध्यम से वह युगीन परिस्थितियों को उजागर करता है अर्थात् उसके काव्य में उसका युग बोलता है। यह बहुप्रचलित मान्यता है कि किसी युग की परिस्थितियों को जानने के लिए उस युग के साहित्य का अध्ययन आवश्यक होता है और साहित्य के अध्ययन के लिए युगीन परिस्थितियों को जानना एक अनिवार्यता हो जाती है। यह युग सत्य साहित्य में अनेकायामी होता है और उनकी अभिव्यक्ति भी अनेकों माध्यमों द्वारा की जाती है।
भारतीय लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हुई हैं, उसमें जन भागीदारी बढ़ी है। लोकतंत्र का नियंत्रण अब पूंजीपतियों और कॉरपोरेट के हाथ में है वह अब कुछ समूह या जातियों के हाथ तक सीमित नहीं है। इसका परिणाम है कि वंचित और सुविधा संपन्न तबके का अंतर भी तेजी से बढ़ा है। इस अंतर को पाटने के लिए जैसा जन-प्रतिरोध होना चाहिए, वैसा नहीं दिखता है। सामूहिक संघर्ष की जगह छोटे-छोटे संघर्ष का यह समय है।
देश और दुनिया के विभिन्न अंचलों में चलने वाले छोटे-छोटे आंदोलनों के जरिए प्रतिरोध की नई जमीन और भाषा अस्तित्व में आई है। बाबा नागार्जुन ने कविता के रूप और शिल्प में कई प्रयोग किए हैं। वे लगातार मुक्त छंद के साथ छंदोबद्ध कविताएं भी लिखते रहें हैं। खासतौर से उनकी आंदोलनधर्मी कविताएं छंदों में ही हैं। ऐसे अवसरों पर उन्होंने सहज और लोक प्रचलित छंदों का उपयोग किया है।स्पष्टत: लय अथवा छन्द कविता का अन्तर्वर्ती तत्व है, जो उसे गद्य से पृथक करता है।
राजस्थान में अन्य हिंदी प्रदेशों की तरह ही गीत और नवगीत सृजन की समृद्ध परंपरा रही है। ये गीत पाठकों को आंदोलित भी करते रहे हैं और संवर्धित भी। इनमें हरीश भादानी और ताराप्रकाश जोशी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। महेन्द्र नेह और बृजेंद्र कौशिक इसी परंपरा की अगली कड़ी हैं।
वरिष्ठ गीतकार ताराप्रकाश जोशी के गीतों में अपने समय का यथार्थ कुछ यूं अभिव्यक्त हुआ है-
लगभग एक थकन दे जातीं
सड़कें कहीं नहीं ले जातीं
पगडंडी खोई जनपथ में
जनपथ, राजपथों में खोया
शाम थका पटरी पर सूरज
बाजू पर सिर धरकर सोया।
बहुत सहज, सौम्य और संप्रेष्य गीत पंक्तियां हैं। उनका एक और गीत है:
बस्ती बस्ती भय के साये
कहाँ मुसाफिर रात बिताए
कुछ हिस्से हैं बटमारों के
कुछ हिस्से हैं अय्यारों के
कुछ नीलामी कुछ ठेके पर
कुछ हिस्से पहरेदारों के..
व्यवस्था और समाज का जो नकारात्मक चरित्र है वह यहाँ स्पष्ट है।
बिडंबना देखें–
न्यायालय में दया मांगने
जब भी कोई कर फैलाये
ऐसा लगे कसाईघर में
बकरे की मां खैर मनाये
मैनेजर पांडेय के अनुसार- ‘नवगीत और जनगीतों में समकालीन समस्याओं से साक्षात्कार की चिंता है। इनमें सामाजिक संवेदनशीलता के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति और जन जीवन के भीतर व्यक्ति मन के अंतर्द्वन्द्वों की पहचान की कोशिश भी है। इसलिए उनमें एक सहृदय कवि की सहज बौद्धिकता की चमक भी है जो पाठकों और श्रोताओं को प्रभावित भी करती है।’
गीत-गजलकार लोकेश कुमार साहिल मानते हैं-
गीत गेयता का मन है
गीत खुशी में गीत रुदन में
गीत लोक की धड़कन है…
विकास की भ्रामक अवधारणा को वह यूं प्रकट करते है-
ये विकास के कुटिल रास्ते
लील रहे जंगल को
कब तक ये देखे योगेश्वर
बढ़ते हुए अमंगल को…
वरिष्ठ कवि बृजेंद्र कौशिक की पंक्तियां हैं-
बन गए जब से सियासी केंद्र सारे अस्तबल
रेंकने वाले भी कर रहे तब से चोला बदल
एक रंग में चाहता रंगना विविधता देश की
सांस्कृतिक स्वातंत्र्य की अभिव्यक्ति में बढ़ता दखल।
लेकिन कवि यहाँ महज व्यवस्था की विसंगतियों और अंतर्विरोधों को रेखांकित करने से ही संतुष्ट नहीं होता वह प्रतिरोध और संघर्ष के लिए तत्पर रहने का आह्वान भी करता है-
बहुत सहा अब रार करेंगे
जुल्मों का प्रतिकार करेंगे..
इसी क्रम में स्पष्टता के साथ जनवादी कवि हंसराज चौधरी उद्घाटित करते हैं-
हर खुशी खा गए अमन खा गए
बेचकर बागबां ही चमन खा गए
यह सिला है शहादत का हद हो गई
बेचकर राजनेता कफन खा गए…
सांप्रदायिकता की आहट वह महसूस करते है और आशंकित हैं कि कहीं यह साजिश सफल न हो जाए-
वो झूठ की बुनियाद पर रचते हैं साजिशें
तुम देख लेना भाइयों में वैर न हो जाय…
इक्कीसवीं सदी में मानवाधिकार साहित्य चिन्तन का प्रमुख विषय है जिसका केन्द्र बिन्दु मानव-मूल्य है। मानवाधिकार से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है, जिसके हक़दार सभी मानव है।
कामेश्वर त्रिपाठी अपने समय के बहुत चेतस और संवेदनशील रचनाकार हैं। वह कहते है-
कुफ्र भी है यहाँ कहर भी है जाम भी है यहाँ जहर भी है
हर कहाँ किसी को मुनासिब ये जिंदगी मुख्तसर भी है
खेत में खेत रह गया जो क्या पता उसका कि सहर भी है
इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वह कहते हैं-
कुछ इधर के बाकी थे उधर के लोग
मरने वालों में सभी थे अपने घर के लोग
सभ्यता के विकास के साथ – साथ व्यक्ति की जीवन – शैली में भी परिवर्तन आता चला जाता है। पिछले कुछ वर्षों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। तीव्र गति से परिस्थितियों एवं पर्यावरण में परिवर्तन लक्षित हुए हैं । गांव की फिजां भी बदली है।
गुरुचरण सिंह मौड कहते हैं-
है दौलत के जिस पहाड़ पे कब्जा कुबेर का
ये लूटी गई है झोंपड़ी मेरे ही गांव से।
———————
खाली पड़े तालाब अब आब को तरस रहे
सारी नदियां खून से हैं अब भरी हुई।
नये आयामों की निर्मिति ने इस सदी को बीती हुई सदी से भिन्न और विशिष्ट बनाया है। वैश्वीकृत पूंजी के नए छलना रूप के प्रभाव के कारण मनुष्यों के मूल्यबोध में आमूलचूल परिवर्तन दृष्टिगत हो रहा है। औद्योगीकरण, निजीकरण , उदारीकरण एवं कॉर्पोरेटीकरण ने एक अद्भुत परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। आदमी इस चकाचौंध में खो गया है। युवावर्ग धूमिल भविष्य से चिंतातुर है। शिक्षित नौजवान रोजगार विहीन, लक्ष्यविहीन और श्रीहीन होता जा रहा है।
आज के समाज में विश्वास का स्थान धोखे और स्वार्थों ने ले लिया है। जिसके कारण लोगों में आपाधापी मची हुई है। हिंसा और अपराध की प्रवृत्ति पनपने लगी है तथा लोगेां का जीवन – मूल्यों के प्रति अविश्वास बढ़ने लगा है।
सलीम खां फरीद लोकतंत्र में चुनावों को राजनेताओं द्वारा जनता को भ्रम रखने का उपक्रम मानते हैं-
जब तक यह मतदान है भाई
तब तक तुझपर ध्यान है भाई
कोई उस तोते को मारे
जिसमें इनकी जान है भाई…
अंधविश्वास, कर्मकांड और धर्म में उसकी आस्था बढ़ी है। अनिश्चितता के बढ़ जाने के कारण मनुष्य को कुंठा और अवसाद ने घेर लिया है। वर्तमान सत्ता उसके स्वप्नों को पूरा कर पाने में अक्षम है अत: अब उसे अंधराष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता कीआग में झोंक दिया है। इक्कीसवीं सदी के कवि इस सत्य और यथार्थ से अनजान नहीं हैं। वे अपनी कविता में इन स्थितियों पर रिएक्ट कर रहे हैं। हां राजनीति के वैश्विक पूंजीवादी चरित्र और मानवद्रोही प्रकृति के बरक्स समाजवादी संरचना को विकल्प मानकर नहीं देख पा रहे हैं।
हमारे समाज में दलित वर्ग , नारी तथा कृषकों व मजदूरों का आदिकाल से ही शोषण होता रहा है तथा यह क्रम आज भी जारी है।
आर पी बौद्ध कहते हैं-
पृथ्वी की पूरी परिधि को घेर लिया है
पुराना खिलाड़ी है
खेल है विशाल
सब जगह बिछा रखा है जाल..
आज के दौर में सूचना क्रान्ति, कम्प्यूटर क्रान्ति, मीडिया आदि के लाभ अवश्य हुए हैं लेकिन इसके कारण सामाजिक चेतना में एक नकारात्मता आई है। एक ओर शिक्षा का प्रसार बढ़ा है तो दूसरी ओर जनसंख्या में अबाध वृद्धि के कारण शैक्षणिक बेरोजगारी भी बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि हुई है तो महंगाई में भी बढ़ोतरी हुई है। जनता यह समझ नहीं रही है और तरह तरह के भ्रमों को सच मान बैठी है।
दिनेश गौड़ आगाह करते है-
बंद करो नफरत की बातें
मत मंदिर मस्जिद की बात करो
आधी जनता भूखी सोती
पहले उस जीवन की बात करो..
मदन मोहन सजल कहते हैं-
धीरे चल जिंदगी, ज्वलंत सवालों के जवाब अभी बाकी हैं
जिसने भी तोड़े दिल ऐसे चेहरों के हिसाब बाकी हैं।
विभिन्न सामाजिक आंदोलनों और आर्थिक निर्भरता कम होने के कारण महिलाओं व दलितों की स्थिति में सुधार हुआ है तो सामाजिक समानता का स्वप्न अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। वैश्वीकरण के कारण सारा विश्व, ग्राम बन रहा है तो वहीं आपसी द्वेष, साम्पद्रायिकता , अलगाव आदि के कारण व्यक्ति और व्यक्ति के बीच दूरी बढ़ गई है।
रामेश्वर बगाड़िया लिखते हैं-
झुलस गए वन उपवन सारे
जहर भरी एक हवा चली है
फूल खिले और बिखर गए
सहमी सहमी हर कली है।
स्त्री शिक्षा ने जहाँ स्त्री की आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त किया है वहीं नई समस्याएं भी उभर कर आ रही हैं। सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है।
कारपोरेट मीडिया ने समाज के स्वरूप को ही बदल दिया है। एक नया विवेकहीन नेरेटिव बना दिया है। सूचना तंत्र के हर क्षण बदलते, विकसित होते औजारों के कारण भी समाज का स्वरूप बदल रहा है। कारपोरेट, पूंजी और अपराध के गठजोड़ के चलते व्यवस्था पंगु हो गई है और राजनीति पतन के गर्त में पहुंच गई है। ऐसी स्थितियों मे जनसंघर्ष ही अंतिम विकल्प है और कविता इसे समझने का एक सहज, सौम्य प्रयास है।
(शैलेन्द्र चौहान वरिष्ठ लेखक है और जयपुर में रहते हैं।)






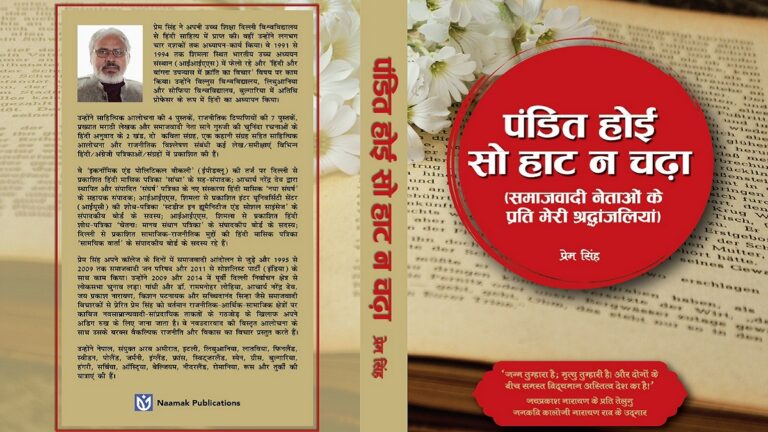





+ There are no comments
Add yours