अरबी मूल के ‘सफ़ारी’ और अफ्रीका की स्वाहिली मूल के ‘मसाफ़ीरी’ शब्द से बना है प्रचलित स्वाहिली का शब्द ‘वासाफ़ीरी’ यानी सफ़री या यायावर। इसी नाम के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश साहित्यिक-सामाजिक तिमाही जर्नल, वासाफ़ीरी के 107वें अंक में (अगस्त 2021) अंग्रेजी लेखक, उत्तर औपनिवेशिक विमर्शकार और फ्रांकफुर्ट की गोएथे यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्राध्यापक पवन कुमार मालरेड्डी ने प्रख्यात लेखिका अरुधंति रॉय का इंटरव्यू किया है। इसमें एक सवाल के जवाब में रॉय ने कहा था कि “बात दूसरी दुनियाओं की संभावना की नहीं हैं, बात ये है कि वे अन्य दुनियाएं तो पहले से बाकायदा मौजूद हैं। उनका दम घोंटा जा रहा है, उन्हें कुचला जा रहा है। उपन्यास आपको वे अन्य दुनियाएं दिखा सकते हैं। लड़ने के, जीने के, हंसने के, अलग अलग चीज़ों के बारे में हंसने के अलग अलग तरीके दिखा सकते हैं। तो उन दुनियाओं का अस्तित्व तो है ही। और वे आपस में जुड़ी हुई भी हैं। अरुंधति के उपन्यास “अपार ख़ुशी का घराना” में अंजुम जंतर मंतर की गहमागहमी के बीच ऐलानिया अंदाज़ मे कहती भी हैः हम दूसरी दुनिया से आए हैं।”
अरुंधति की इस टिप्पणी की रोशनी में, संयोग से इसी पत्रिका में लंबे समय तक संपादकीय दायित्व निभाते रहे गुरनाह के समूचे रचनाकर्म को देखा जा सकता है जो बुनियादी रूप से अन्य दुनियाओं के बारे में ही हैं, उन्हीं के रैबासियों को संबोधित हैं और उन्हीं के दुखों, संघर्षों, यातनाओं, बिछोहों, विस्थापनों, मोहब्बतों, टकरावों, स्वार्थों और जिंदगानियों के बारे में हैं।
साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटिश लेखक अब्दुलरज़ाक गुरनाह 73 साल के हैं और पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया देश के मूलनिवासी हैं। उनको नोबेल मिलने पर ख़ुशी जताते हुए पूर्व नोबेल विजेता और अफ्रीका के दिग्गज लेखक वोले सोयेंका ने कहा कि 35 साल बाद नोबेल घर लौटा है। सोयेंका ने जिसे घर कहा है वो महाद्वीप कई देशों, दिशाओं, राष्ट्रीयताओं और उप-राष्ट्रीयताओं में बंटा हुआ है। पश्चिम अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका के अपने अपने तनाव हैं तो उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका, अरब देश हों या और यूरोपीय सभ्यताओं से स्पर्श के बिंदु- अफ्रीका शायद सभी महाद्वीपों में सबसे जटिल, दर्द भरे और विहंगम इतिहास से भरा रहा है। जानकारों का कहना है कि गुरनाह उत्तर-औपनिवेशिक अफ्रीकी अनुभूति और एक इस्लामी आंतरिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
नोबेल कमेटी ने साहित्य के नोबेल चयन में एक बार फिर सबको हैरान ही किया है। हालांकि गुरनाह आधुनिक अफ्रीकी साहित्य फलक पर लंबे समय से जाने जाते रहे हैं लेकिन दावेदारों की सूचियों और अटकलों में उनका नाम कभी उभर कर नहीं आया था। इसीलिए पुरस्कार की घोषणा के बाद नोबेल कमेटी की ओर से आए फोन में उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए यही कहा कि मैं भी हैरान हूं कि क्योंकि मैं भी औरों की तरह किसे मिलता है के अंदाज़ में उत्सुक ही था। लेखिका, अकादमिक, वारस्कैप्स पत्रिका की संपादक और रेडिकल बुक्स कलेक्टिव की सह-संस्थापक भक्ति ऋंगारपुरे ने स्क्रॉल डॉट इन में अपने लेख में एक अंग्रेजी मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि नोबेल के कमरे में इस बार हाथी दाखिल हो गया है। चर्चा तो केन्या के दिग्गज लेखक न्युगी वा थ्योंगों की थी और पिछले कुछ लंबे अरसे से होती आ रही है लेकिन एक अन्य पूर्व अफ्रीकी लेखक को चिन्हित कर लिया गया। लेखिका का कहना है कि अंग्रेजी भाषी दुनिया में उसी अफ्रीकी साहित्य का बोलबाला है जो दक्षिण अफ्रीका और नाईजीरिया से आता है। दक्षिण अफ्रीका के दो लेखक जेएम कोएट्जी और नादीन गोर्डिमर नोबेल जीत चुके हैं और नाईजीरिया के वोले सोयेंका भी नोबेल विजेता लेखक हैं। अफ्रीकी भाषा और बोलियों के प्रखर पैरोकार और अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व के धुर विरोधी न्युगी वा थ्योंगो को नजरअंदाज कर अंग्रेजी भाषी और अंग्रेजी में लिख रहे गुरनाह को पुरस्कृत करने में क्या नोबेल ने अपना पूर्वाग्रह भी झलकता है, दुनिया के साहित्यिक हल्कों में इस पर भी चर्चाएं और विवाद जारी हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरनाह कमतर लेखक हैं या उनके साहित्य में अपनी संस्कृति और भाषा के स्वर फीके हैं।
अब्दुलरज़ाक गुरनाह केंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर, वहीं अंग्रेजी भाषा और पोस्टोकलोनियल साहित्य के प्रोफेसर के रूप में काम कर चुके हैं। दस उपन्यासों के अलावा उत्तर-औपनिवेशिक विमर्श, हिंद महासागरीय इलाके के साहित्य और कैरेबियाई साहित्य पर अकादमिक महत्त्व के निबंधों के रचियता गुरनाह ने अफ्रीकी साहित्य पर केंद्रित दो खडों में निबंधों की पुस्तक भी संपादित की है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से 2007 में प्रकाशित “अ कम्पैनियन टू सलमान रुश्दी” पुस्तक के भी वो संपादक हैं। साहित्यिक विमर्श के जर्नल “वासाफिरी” में सह-संपादक वो रहे हैं। दो बार बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित हो चुके हैं। परा-सांस्कृतिक अस्मिताओं, पलायन, विस्थापन, स्मृति और संकर अस्मिताएं उनके लेखन के मूल स्वर हैं। यहां तक कि महासागर और समन्दर भी वहां महज एक भूगर्भीय भौगौलिक उपस्थिति नहीं बल्कि अपने अकेलेपन और पलायन को अभिव्यक्त करने वाली अनगिनत लहरे हैं- अपने भीतर जारी एक निरंतर उछाड़-पछाड़। टिप्पणीकार लूका प्रोनो के मुताबिक, “बाहरी होने और अलग होने की स्थितियां भले ही जातीय, धार्मिक, नैतिक अंतरों से आई हों या सामाजिक अंतरों के चलते- ये स्थितियां ही गुरनाह के लेखन की धुरी हैं।”
1957 में अल्बैर कामू, 1986 में वोले सोयेंका, 1988 में नगीब महफ़ूज़, 1991 में नादीन गोर्डीमर, 2003 में जेएम कोएट्ज़ी और 2007 में डोरिथ लेसिंग के बाद, 2021 में, अफ्रीकी महाद्वीप से साहित्य का नोबेल पाने वाले गुरनाह सातवें लेखक हैं। सोयेंका के बाद नोबेल पाने वाले, अफ्रीका के दूसरे काले लेखक हैं। वो तंजानिया के छोटे से, 15 लाख की आबादी वाले ज़ंज़ीबार द्वीप से आते हैं। 1960 के दशक में ये इलाका ब्रिटिश उपनिवेश से आजादी के बाद तंजानिया में विलीन हो गया था। हालांकि वहां स्वायत्त सरकार चल रही है। लेकिन ये विलय गुरनाह जैसे रचनाकर्मियों क लिए अलगाव लेकर आया। ज़ंज़ीबार में अरबों के खिलाफ राज्य के आतंक से बचने के लिए गुरनाह साठ के दशक में ही ब्रिटेन जा बसे। उपनिवेशी दौर को सहने वाले इन छोटी छोटी जगहों के खामोश इतिहास में देखने का अवसर मुहैया कराती हैं। ये जगहें राष्ट्र की विराट छवि के तहत भी दबी-सहमी रहती आती हैं। इन उपराष्ट्रीयताओं की सुनवाई नहीं होती। गुरनाह अपने उपन्यासों में ऐसी दबी हुई भटकती हुई आवाज़ों के लिए जगहें बनाते हैं। जख़्मी स्मृति और दमित सामूहिकता के नायक उनके उपन्यासों में धीरे धीरे सांस लेते हैं, खड़ा होते हैं, भटकते हैं। वे अपने व्यापक अलगावों में जुड़ाव के सूत्रों की एक अंतहीन तलाश में मुब्तिला रहते हैं। निर्वासितों और विस्थापितों के अवसाद और अलगाव और अजनबियत की ऐसी विरल, करुण और विशिष्ट गाथा कहने वाले गुरनाह इस समय अंतरराष्ट्रीय साहित्य में चुनिंदा लेखकों में एक होंगे।
अफ्रीका की निर्वासित, विस्थापित और तड़पती रूहों को पश्चिम के अंधेरो-उजालों में कौनसे अनुभवों से गुज़रना पड़ता है, इसका सबसे तीक्ष्ण और विलक्षण वर्णन हमें गुरमाह के उपन्यासों में मिलता है। वे आसनी से जज्ब हो जाने वाले लेखक नहीं हैं। एक विराट अवसाद वहां पसरा हुआ है जो अपनी कहानी कहता रहता है और किरदार जैसे किसी पत्थर की तरह तरह अपनी अपनी उदासियों और उलझनों मे टस से मस नहीं होते हैं। एक बहुत बड़ा वजन वे लिए चलते हैं। ये वो वजन है जिससे उस जन को मुक्त कराना तो दूर की बात है, उसकी शिनाख्त में भी समकालीन सत्ताएं और कला-राजनीति विफल रही है या जानबूझकर कई कारणों से अनदेखा करती रही है। गुरनाह का अपना जीवन भी अपना दर्द भी उनकी रचनाओं में से झांकता है। वे एक अंधेरे से निकल कर आने में कामयाब तो हुए लेकिन नस्लवाद का एक नया अंधेरा उन्हें निगलने के लिए आतुर रहा था। द गार्जियन डॉट कॉम में डेविड शैरियटमैडारी को दिए एक इंटरव्यू में गुरनाह विस्थापन की ऐतिहासिक तकलीफ को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि “हमारे वक्तों की ये एक बहुत बड़ी दास्तान है।
उन लोगों की कहानी जिन्हें अपने मूल निवास से दूर अपनी जिंदगियों को फिर से निर्मित करना, सहेजना और संवारना पड़ता है। वे क्या याद रखते हैं? और जो वे याद रख पाते हैं उससे निबाह कैसे कर पाते हैं? वे जो तलाश पाते हैं उससे कैसे निबाह कर पाते हैं? और ये भी कि उन्हें कैसे देखा जाता है?” इसी इंटरव्यू के दरमियान गुरनाह ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजरवेटिवों की खबर भी लेना नहीं भूलते और खासतौर पर देश की गृहमंत्री प्रीति पटेल को लेकर तो उनका कहना है कि उनसे वो संवाद में मुब्तिला नहीं होना चाहते हैं। ध्यान रहे कि ब्रिटेन में आने वाले विस्थापितों, शरणार्थियों और शरण मांगने वालों और पलायन को लेकर जो नई नीति बनी है उसकी चौतरफा आलोचना की जा रही है और मानवाधिकार हल्कों में भी सवाल उठे हैं। गुरनाह इस विडंबना की ओर इशारा करते हैं कि ये नियम ऐसे मंत्री के रहते आए है जो खुद यहां आकर बसी होंगी या उनके माता पिता बसे होंगे। और वे ही अब सख्त हैं। गुरनाह के मुताबिक पलायन और माइग्रेशन को लेकर आज के सकारात्मक बदलावों की बात अधिकांशतः भ्रामक ही है।
नोबेल पुरस्कारों के 120 साल के इतिहास में ये सम्मान पाने वाले गुरनाह चौथे काले लेखक हैं और तीन दशकों से भी ज्यादा के वक्फे में नोबेल पाने वाले पहले काले अफ्रीकी हैं। 1987 में, करीब चालीस साल की उम्र में गुरनाह का पहला उपन्यास आया था, “द मेमरी ऑफ डिपार्चर” (रवानगी की याद।) लेकिन उन्हें ख्याति मिली 1994 में आए अपने चौथे उपन्यास “पैराडाइज़” (जन्नत) से जो बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। 2002 में प्रकाशित “बाइ द सी” (समन्दर किनारे) उपन्यास भी बुकर की लॉंग लिस्ट में शामिल था। उनकी सबसे ताजा रचना है- 2017 में आया उपन्यास “ग्रेवल हार्ट” (बजरी भरा दिल।) गुरनाह का पाठ राहतें नहीं देता, और परेशान करता है और असहज बनाता है। वे एक असामान्य जीवन के ब्यौरे हैं, एक असामान्य भूगोल से निकला हुआ एक असामान्य जीवन। एक असामान्य समय का अस्थिर अशांत चित्त जो अपने जुड़ाव के बोध को कभी अपने भीतर तो कभी उस पेचीदे भूगोल में तलाशने की कोशिश करता है। गुरनाह के एक पुराने उपन्यास, “एडमाइरिंग साइलेंस” (ख़ामोशी की सराहना) में बेनाम नैरेटर कहता है, मैं विभेदों में रहना चाहता हूं। गुरनाह का कहना है कि विभेदों में रहने के लिए अंतर करने में भी समर्थ होना चाहिए।
2001 में प्रकाशित छठे उपन्यास बाइ द सी (समन्दर किनारे) में गुरनाह का मुख्य किरदार शाबान नाम का लड़का कहता हैः “मैं शरणार्थी हूं। मैं शरण चाहता हूं। ये साधारण शब्द नहीं हैं भले ही उन्हें सुनने की आदत के चलते वे ऐसे ही लगने लगें। ” ये पंक्ति ही मानो उस समूची तकलीफ़ और विडंबना को एक झटके में उभार देती है जिससे अफ्रीकी और खाड़ी देशों समेत दुनिया के बहुत से हिस्सों के लोग भुगतते आ रहे हैं। गुरनाह की लंबे समय से प्रकाशक-संपादक अलेक्जेंडर प्रिंगल ने मिडलईस्टआई वेब पत्रिका में गुरनाह को मिले सम्मान को देर आये दुरुस्त आए बताते हुए कहा कि गुरनाह ने विस्थापन और पलायन की जो हृदयविदारक तस्वीर ही नहीं बल्कि उन वंचितों के जीवन का जो खाका उतारा है, वो अभिभूत कर देने वाला है। उन्हें उम्मीद है कि जंजीबार और तंजानिया के सांस्कृति परिदृश्य में अभी तक कमोबेश कम पढ़े गए गुरनाह को पढ़ा जाएगा और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी विभिन्न भाषाओं में उनके उपन्यासों के अनुवाद जा पाएंगें।
जड़ों की ओर लौटने की बेकली और अतीत की स्मृतियों के तानेबाने से रचे गुरनाह के नॉवलो में अतीतजीविता या नॉस्टेलजिया नहीं है। वहां अतीत, आज की तरह है। एक खुद्दार लेकिन तकलीफदेह याददिहानी की तरह। आयरलैंड के ख्यात ऑनलाइन जर्नल पोलिटिको डॉट आई के डिजिटल आर्काइव खंड में मैगील पत्रिका की शेन क्रीवी को 2010 में एक इंटरव्यू में गुरनाह बताते हैं कि भारत की अंग्रेजी उपन्यासकार अनीता देसाई के नॉवल, “क्लियर लाइट ऑफ डे” (दिन का साफ़ उजाला) से एक वाक्य उन्होंने अपने उपन्यास, “एडमाइरिंग साइलेंस” में इस्तेमाल किया था। “नथिंग इज़ ओवर, एवर।” (कुछ भी कभी नहीं खत्म होता)। इसी हवाले से गुरनाह कहते हैं कि अतीत भी ऐसा ही है। वो वर्तमान में रहता है, क्योंकि हम अपनी कल्पनाशीलताओं में भी रहते हैं और अपने वास्तविक यथार्थ और जीवन में भी। इस तरह अतीत हमारे कल्पनाशील लैंडस्केप का हिस्सा होता है और हमेशा जिंदा रहता है। कभी भी समाप्त नहीं होता या पूरी तरह बीत नहीं जाता है।
कमोबेश इसी संदर्भ में चीनी उपन्यासकार मो यान सहज ही याद आते हैं। संयोग से वे भी साहित्य का नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं। 2012 में नोबेल पुरस्कार ग्रहण करने के बाद अपने चर्चित नोबेल भाषण में मो यान ने कहा था कि “रचना का स्रोत चाहे स्वप्न हो या असल ज़िंदगी, निजी अनुभव के साथ उसे मिलाने के बाद ही वो विशिष्टता से भरी जा सकती है, तभी उसे जीवंत विस्तार से गुंथे हुए ख़ास पात्रों के जरिए लोकप्रिय बनाया जा सकता है, तभी उसमें एक समृद्ध और यादों को जगाने वाली भाषा आ सकती है और तभी उसका एक सुचिंतित तराशा हुआ ढांचा खड़ा किया जा सकता है।।। मैं जानता हूं कि लोगों के दिलों में और ज़ेहन में एक धुंधला सा इलाक़ा बना हुआ रहता है, एक ऐसा इलाक़ा जिसे गलत और सही या अच्छा और बुरा के सामान्य अर्थों में सही ढंग से नहीं समझा जा सकता। और ये विशाल इलाक़ा वही है जहां एक लेखक अपनी प्रतिभा को खुला छोड़ देता है। जब तक रचना सही परिप्रेक्ष्य में और विशद रूप में इस अस्पष्ट, भारी पैमाने पर विरोधाभास भरे इलाक़े की व्याख्या करती है, तभी वो अवश्यंभावी रूप से राजनीति से आगे रहेगी और साहित्यिक उत्कृष्टता बनाए रखेगी।”
गुरनाह भाषा और उसे बरतने को लेकर चिनुआ अचेबे और न्युगी वा थ्योंगो जैसे दिग्गज लेखकों से न सिर्फ अलग सिरे पर खड़े हैं बल्कि उनका विरोध भी करते हैं। एक साक्षात्कार में अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए गुरनाह का कहना है कि अचेबे की दलील ये है कि उपनिवेश विरोधी संघर्षों और वैचारिक लड़ाइयों में भी अंग्रेजी को अनुकूलित किया जा सकता है। यानी अंग्रेजी का इस्तेमाल मूलनिवासियों के हितार्थ नही बल्कि औपनिवेशिक शक्तियों के स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही किए जाने की आशंका रहती है। उधर न्युगी की मान्यता ये है कि ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि भाषा उस सब पर हमला कर देती है जो आप करते हैं। उसकी घुसपैठ इसमें होती है कि आप उसे कैसे इंटरप्रेट करते है, वो मूल्यों पर झपट्टा मारती है, चीज़ो को नियंत्रित करती है। लेकिन गुरनाह का कहना है कि “इस तरह भाषा न उपकरण या औजार या सबब की तरह काम करती है या दूसरी तरफ़ इस ढंग से जो करीब करीब गैरप्रतिबिम्बित है। मैं नहीं मानता हूं कि इस तरह लेखक और भाषा एक दूसरे से जुड़ते हैं।
इसलिए मैं दोनों कैपो में से कहीं नहीं खुद को पाता हूं।” गुरनाह कह चुके हैं कि अंग्रेजी अब औपनिवेशिक शक्ति की भाषा नहीं है, ये सबकी भाषा है। गुरनाह की मातृभाषा स्वाहिली है और लेखन के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाने के बावजूद उनके गद्य में स्वाहिली के निशान बिखरे हुए रहते हैं। एक भाषा के भीतर दूसरी भाषा रहती है। वो दूसरी भाषा ही दरअसल स्मृति और जन्म की भाषा है। इस तरह वह पहली भाषा भी है जो दूसरी भाषा में अनेक स्वरों और आशयों में प्रतिबिम्बित होती रहती है। भाषाएं आपस में गुंथी हैं जैसे अकेलेपन और अजनबियत के साथ गर्माहट और रिश्ते और नयी जिंदगी घुलीमिली रहती है।
जर्मनी की फ्रांकफुर्ट यूनिवर्सिटी के विभिन्न अनुशासनों से जुड़े शोधार्थियों और विद्वानों की अफ्रीका-एशिया पर केंद्रित शोध परियोजना (2013-2019)- अफ्रीकाज़ एशियन ऑप्शन्स यानी अफ्रासो के लिए 2016 में फाबिएन रॉथ, मारा होलजेन्थाल और लीसा जिंगेल के साथ एक बातचीत में अपनी लेखन शैली पर प्रभावों के बारे में गुरनाह ने कहा कि सीधे तौर पर तो किसी प्रभाव को रेखांकित करना कठिन है लेकिन “इंग्लैड में अजनबी के तौर पर रहते हुए, अपना रास्ता खोजने की कठिनाइयों के बीच, एक छूटा हुआ घर- इन तमाम चीज़ों ने मुझ पर असर डाला। मैं चीजों को लिखता ही जा रहा था, नोट करता जाता था और कुछ बनता जाता था जब एक दिन ऐसा मोड़ आया कि मैंने सोचा ये क्या है। मै इसका क्या करूंगा। एक ऐसा बिंदु आता है जब आपको चीज़ों को लिख कर रख लेने और लेखन के अंतर को समझना होता है। ये अपनी देह की पुकार की तरह है।”
एक बिंदु पर ये लेखन उपन्यास की शक्ल लेने लगता है और फिर आप सुधार करते जाते हैं एक बार इस चक्कर में फंस जाओ तो फिर छुटकारा मुमकिन नहीं। बेहतरी की तलाश करते करते एक प्रकाशक की तलाश करते हैं और फिर लेखक हो जाते हैं। उपन्यास की जगह यहां पर कुछ देर के लिए कविता को भी रखकर देखें तो पिछले साल दिसंबर में दिवंगत हुए, भारतीय कवि मंगलेश डबराल की 1991-92 की एक चर्चित छंदबद्ध कविता ‘छूट गया है’ की याद सहज ही आ जाती है जो न सिर्फ लेखकीय विस्थापन और प्रवासी नागरिक की विडंबना की अनिवार्य सी तक़लीफ़ की ओर इशारा करती है बल्कि एक तरह से यहां गुरनाह के लेखन को ही मानो उद्घाटित करती दिखती हैः
“भारी मन से चले गए हम/ तजकर पुरखों का घरबार/ पीछे मिट्टी धसक रही है/ गिरती पत्थर की बौछार/ थोड़ा मुड़कर देखो भाई/ कैसे बन्द हो रहे द्वार/ उनके भीतर छूट गया है/ एक एक कोठार।”
उत्तर-औपनिवेशिक विमर्श के अध्येताओं अनुपमा मोहन और श्रेया दत्ता ने 2019 में पोस्टरकलोनियल टेक्स्ट्स वेबसाइट के लिए गुरनाह से ईमेल के जरिए एक लंबा संवाद किया था। उस बातचीत के दौरान श्रेया ने लेखक से पूछा कि उनके उपन्यासों में एक दिल्लगी, एक हल्की सी उमग भी नहीं दिखती, ‘कॉमिक रिलीफ’ नदारद है। एक वेदना, बेकली और छटपटाहट वहां रहती है और एक अकेलापन मंडराता रहता है। तो अवसाद का एक वातावरण क्या एक औपन्यासिक रणनीति है? इस पर गुरनाह का कहना था कि उनके उपन्यासों में विनोद न होने की बात को वो नही मानते। “विनोद के आशय सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन कॉमेडी तो है- घटनाओं में भी और भाषा में भी। और रही बात दर्द और अकेलेपन के साए की तो मैं मानता हूं कि वो तो मानव अस्तित्व की एक शर्त है।” गुरनाह का कहना है कि उनके लेखन के केंद्र में तीन स्थितियां प्रमुख रूप से हैं: जुड़ाव, अलगाव और विस्थापन। इन तीनों बिंदुओं के साथ और भी बहुत सार मुद्दे हैं जो नुकसान और दर्द और उससे निजात पाने के तरीकों से जुड़े हैं। “मैं उस साधन-संपन्नता के बारे में लिखता हूं जिनकी मदद से लोग ऐसे अनुभवों को हासिल करते हैं उनसे जूझते हैं।”
उपन्यासअंश
गुरनाह जिस उपन्यास से पूरी दुनिया में चर्चा में गए थे वो उनका चौथा उपन्यास ‘पैराडाइज़’ था। 258 पेज के अंग्रेजी में प्रकाशित इस उपन्यास के सबसे पहले और सबसे आख़िरी पैरा का हिंदी रूपांतर यहां पेश है। गुरनाह के लेखक व्यक्तित्व की एक झलक इसमें देखी जा सकती हैः
सबसे पहले लड़के की बात। उसका नाम युसूफ़ था और उसने अचानक अपने 12वें साल में अपना घर छोड़ दिया था। उसे याद आया कि वो सूखे का मौसम था। जब हर नया दिन बीते हुए दिन जैसा होता था। अनपेक्षित फूल खिलते थे और मर जाते थे। विचित्र कीड़े चट्टानों के नीचे से मंडराते हुए आते और जलते उजाले में जान गंवा देते। सूरज ने दूरस्थ पेडों को हवा में कांपने पर मजबूर कर दिया था, मकान थरथरा उठे थे और उसांस भरने लगे थे। रौंदते क़दमों को धूल के बादलों ने और फुला दिया था और दिन के उजाले पर एक सख़्त, निर्विकार शांति पसर गई थी। ठीक यही पल मौसम में लौट आते थे।
उसने चांदनी में अपनी बुज़दिली को उसकी गर्भ झिल्ली में फिर से जगमगाते हुए देखा और याद किया कि उसने कैसे उसे सांस लेता हुए देखा था। वो उसके परित्याग के पहले आतंक का जन्म था। अब जबकि वो कुत्तों की स्वाभाविक पतित भूख का नज़ारा देखता था, उसने सोचा कि वो जानता था कि ये किस चीज़ मे तब्दील होगी। मार्च करते फौजियों की टुकड़ी अब भी दिख रही थी जब उसने अपने पीछे बागीचे में दरवाजा बंद करने जैसा शोर सुना। उसने फौरन इधर उधर नज़रे घुमायीं और फिर आंखों में टीस के साथ टुकड़ी के पीछे दौड़ पड़ा।
(लेखक और पत्रकार शिवप्रसाद जोशी का ये आलेख समयांतर पत्रिका के नवम्बर 2021 अंक में प्रकाशित है)








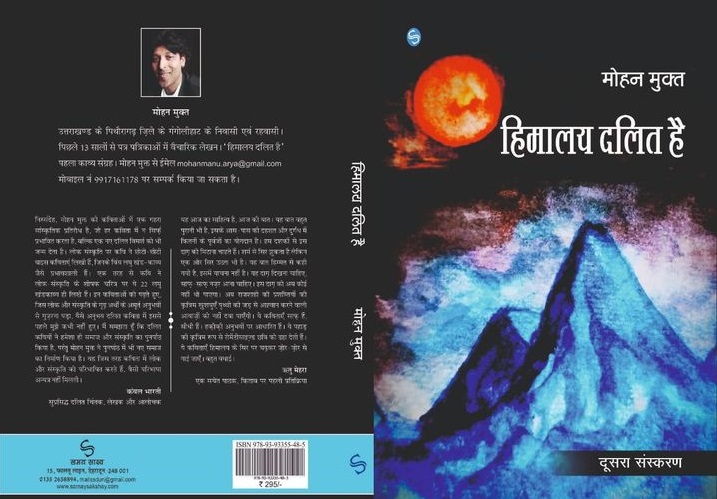



+ There are no comments
Add yours