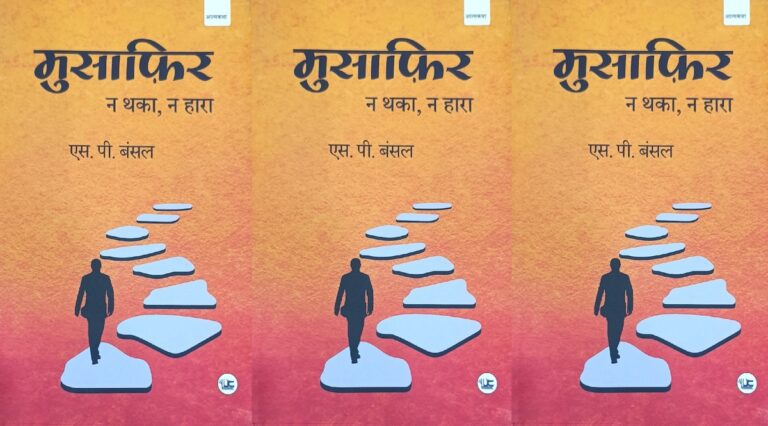कल मंटो फिल्म देखी । पता नहीं किनके लिये इस फिल्म की पटकथा लिखी गई है । जिन्होंने मंटो की कहानियों को नहीं पढ़ा है और मंटो के साहित्य की चर्चा से परिचित नहीं हैं, हम नहीं जानते वे इस फिल्म का एक शब्द भी समझ पायेंगे या नहीं । सचमुच इस जगत के अंदर कितने-कितने जगत समाहित हैं। शास्त्रों की भाषा में भुवन । छोटे, बड़े, विशाल, सर्व-व्यापी । एक अकेले आदमी के खुद के भुवन से शुरू करके विश्व और पूरे ब्रह्मांड के भुवन तक । सबकी अपनी-अपनी भाषाएं हैं, इतनी अपनी कि आप उन्हें उनकी कूट भाषा भी कह सकते हैं । खग ही जाने खग की भाषा । उसकी दुनिया में अन्य का प्रवेश निषिद्ध होता है ।
वैसे ही साहित्य और अदब का भी अपना एक जगत है और उसके अंदर की चर्चाओं की अपनी भाषा भी । कुछ मायनों में वह इतनी सीमित होती है कि इस जगत के बाहर के आदमी के लिये बिल्कुल अबूझ हुआ करती है । नंदिता दास की बनाई यह ‘मंटो’ फिल्म लगभग वैसी ही भाषा की एक फिल्म है । इसे सिनेमाघरों में दिखाना सचमुच हमारी साहित्यिक बिरादरी का अपने दायरे के बारे में एक चरम आत्म-विश्वास का ही परिचय देती है ।
बहरहाल, हमें तो इस फिल्म से एक तृप्ति मिली कि किसी जमाने के तरक्कीपसंद लेखकों की साक्षात उपस्थिति में हम अपने मकबूल कथाकार मंटो को चलता-फिरता, एक पारिवारिक जीवन के सुखों और तनावों को जीता और अपने समय की फिल्मी चकाचौंध में भी अपनी खास शख्शियत में खोया हुआ जिंदा देख पा रहे थे । इसमें हमारे दिलों में बसी ‘ठंडा गोश्त’, ‘टोबाटेक सिंह’ से लेकर उनकी कई कहानियों के परिवेश की झाकियां दिखाई दी थीं । हम उन पर चर्चा करके खुश थे । लेकिन अंत में हम यही सोचते हुए निकले कि एक कथाकार की हर कहानी खुद में एक पूरा जीवन लिये होती है । उसकी इतनी कहानियों के इतने सारे जीवन को उस एक कथाकार के अपने छोटे से जीवन के डब्बे में डाल कर दबा कर सिकुड़ा देने के इस उपक्रम को हम कौन सा हाइपर टेक्स्ट कहेंगे ?
ऐसे डब्बे ही शायद जीवन संबंधी विचारों को समग्र रूप में समेटने वाली विचारधाराओं के डब्बे होते हैं, जिनके एक इंच ऊपर उठे ‘लिहाफ’ के अंदर के सत्य को दिखाने के कौतुहल से भी न जाने कितनी और नई कहानियां बनती जाती हैं ! खैर, इस मंटो फिल्म का हम जैसे चंद लोगों के लिये तो कुछ या बहुत ज्यादा मायने हो सकता है, लेकिन सिनेमा के साधारण दर्शक के लिये यह एक शराबी और सनकी लेखक के पारिवारिक जीवन और बिखरे हुए सामाजिक परिवेश के कुछ अबूझ से ‘चलचित्रों’ का एक बेतरतीब सा गुच्छा भर लगती है ।
शायद लेखक की जिंदगी को हमेशा उसके चरित्रों से जोड़ कर देखने की मासूम ललक का भी यह एक फल है । मंटो को जानने के लिये यह कत्तई यथेष्ट नहीं है । तथापि, मंटो पर मूलत: उनकी कहानियों के मंचन के जरिये नाटक तो कइयों ने किये हैं, वैसी ही एक कोशिश फिल्म के माध्यम पर करने के लिये नंदिता दास साधुवाद की हकदार हो सकती हैं । लेकिन फिर भी कहेंगे, फिल्म सिर्फ नाटक, अर्थात जीवन के सत्यों का संवादमूलक निचोड़ नहीं है ।
(अरुण माहेश्वरी वरिष्ठ लेखक और स्तंभकार हैं। उनकी कई किबातें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप आजकल कोलकाता में रहते हैं।)