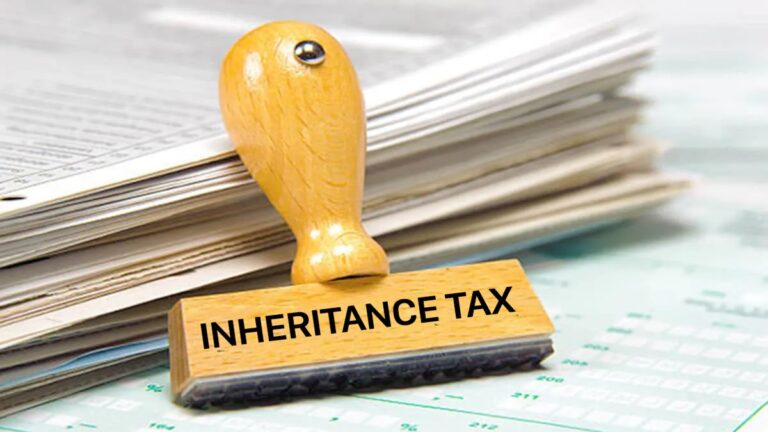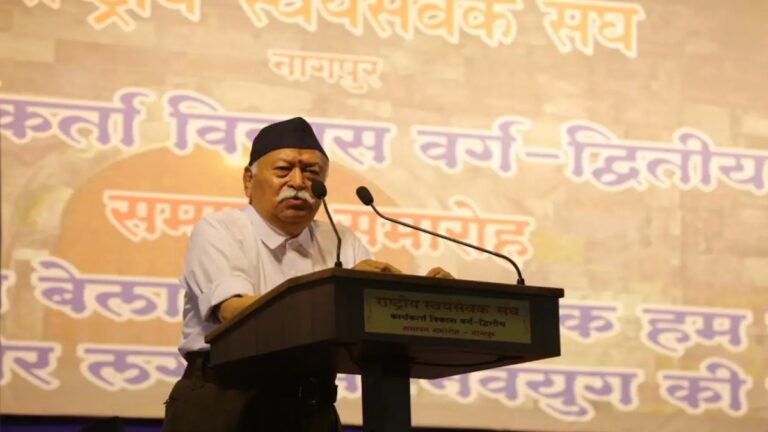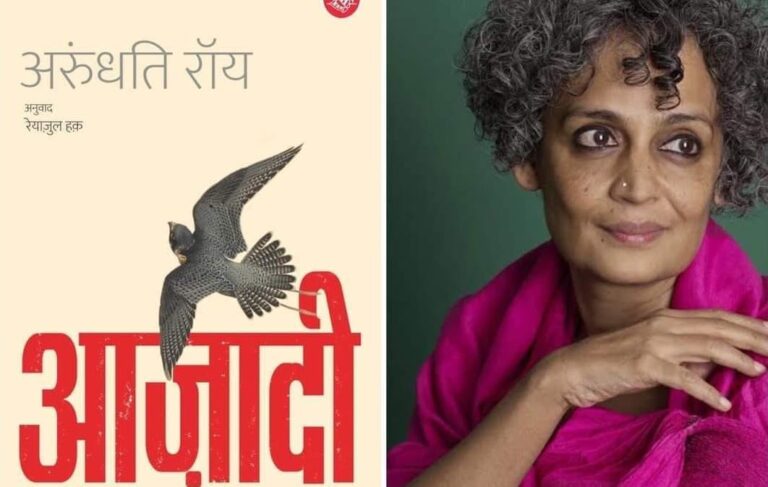एक चलते हुए आंदोलन के बारे में लिखना बहुत कठिन होता है, विशेष रूप से नक्सलवादी किसान विद्रोह के बारे में। इसके सटीक मूल्यांकन में बड़ी समस्या यह है कि या तो इसके समर्थक बहुत भावुक होकर इसका मूल्यांकन करते हैं या फ़िर विरोधी बहुत नफ़रत से। ये बातें किसी भी परिघटना के समग्र मूल्यांकन में बाधा उत्पन्न करती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज यह आंदोलन खण्ड-खण्ड होकर सैकड़ों टुकड़ों में बंट गया है तथा इन सभी गुटों की इस आंदोलन के बारे में अपनी अलग-अलग राय है।
इस आंदोलन पर अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गईं, जिसमें विप्लवदास गुप्त की ‘नक्सलवादी आंदोलन’, अभय कुमार दुबे की ‘क्राति का आत्मसंघर्ष’ और शिव कुमार मिश्र की ‘पलासी से नक्सलबाड़ी तक’ इसके अलावा प्रोफेसर मंनोरंजन मोहंती की भी पुस्तक महत्वपूर्ण है। आंदोलन के पचास वर्ष पूरे होने पर अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने इस पर विशेष अंक प्रकाशित किए तथा इस पर महत्वपूर्ण लेख भी लिखे गए,लेकिन इन सभी में लेखकों ने अपनी सांगठनिक वैचारिक प्रतिबद्धता से ही इसका मूल्यांकन किया है।
बावज़ूद इसके इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता,कि आज से 57 वर्ष पहले पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी प्रखण्ड में जो घटना घटित हुई थी, वह न केवल अपने देश में बल्कि समूचे दक्षिण पूर्व एशिया में महत्वपूर्ण घटना थी। इसने न केवल भारत में बल्कि उसके पड़ोसी देशों नेपाल, पूर्वी पाकिस्तान (बंगला देश), पाकिस्तान के बलूचिस्तान तथा श्रीलंका के भी वामपंथी आंदोलन पर जबरदस्त प्रभाव डाला। इन सभी जगहों पर कम्युनिस्ट पार्टियां ‘क्रांतिकारी बनाम संशोधनवादी’ के आधारों पर बंट गई थीं। इस आंदोलन पर वैश्विक हालातों का भी बड़ा प्रभाव था।
अमेरिका में अमेरिका की वियतनाम में जारी बर्बरता के ख़िलाफ़ व्यापक आंदोलन चल रहे थे, इसके साथ ही वहां पर नारीमुक्ति के आंदोलन के साथ ही साथ काले अमेरिकी लोगों के ख़िलाफ़ नस्लभेद के विरोध में ‘दलित पैंथर’ जैसे आंदोलन चल रहे थे, इसके अलावा श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में हथियारबंद वामपंथी आंदोलन चल रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात थी, कि चीन और सोवियत संघ में संशोधनवाद बनाम क्रांतिकारी दिशा पर महत्वपूर्ण बहस चल रही थी।
चीन में कम्युनिस्ट पार्टी में कथित रूप से घुसे पूंजीवादी तत्वों के ख़िलाफ़ सांस्कृतिक क्रान्ति चल रही थी, इन सबका भी व्यापक प्रभाव इस आंदोलन पर पड़ा। 25 मई 1967 को बंगाल के नक्सलबाड़ी अंचल में जमींदारों और सूदखोरों के ख़िलाफ़ किसानों के सशस्त्र आंदोलन की शुरूआत के तुरन्त बाद चीन की पेकिंग रेडियो ने इस आंदोलन पर एक कार्यक्रम ‘भारत में बसंत का बज्रनाद’ पेश करके चारु मजूमदार, जंगल संथाल, कानू सान्याल और सौरेन बसु जैसे नक्सलबाड़ी प्रखण्ड में मामूली कम्युनिस्ट नेताओं को रातों-रात वैश्विक नेताओं में बदल दिया था।
इस आंदोलन का महत्व इस बात में है, कि इसने कम्युनिस्ट आंदोलन में क्रांतिकारी बनाम संशोधनवाद के बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींच दी, लेकिन बहुत जल्दी ही यह आंदोलन हिंसावाद का मोह न छोड़ पाने तथा जन कार्यवाहियां विकसित न कर पाने के कारण आंदोलन को व्यापक पराजय का सामना करना पड़ा। केवल कोलकाता में ही सड़कों पर हज़ारों नौजवानों को घसीटकर मार दिया गया, इसमें सरोज दत्त, और द्रोणाचार्य घोष जैसे बड़े कवि-लेखक भी थे, इस कारण से बंगाल के बौद्धिक समाज में जो शून्यता पैदा हुई वो आज तक भरी न जा सकी। आज भी हम बंगाल में जो हिंसा की संस्कृति देखते हैं, वह उस समय की उपज है। बाद के दौर में इस आंदोलन के सबसे वरिष्ठ नेता तथा नवगठित सीपीआई मार्क्सवादी-लेनिनवादी के महासचिव ‘चारु मजूमदार’ गिरफ़्तार कर लिए गए तथा पुलिसथाने के लॉकअप में विवादास्पद हालातों में उनकी मौत हो गई।
नक्सलवादी आंदोलन में चारु मजूमदार की भूमिका का सटीक विश्लेषण करने में आज भी आंदोलन से निकले अधिकांश ग्रुप बचते हैं, लेकिन इसका कारण वैज्ञानिक या वैचारिक न होकर भावनात्मक अधिक है। उनके ढेरों प्रशंसक मानते हैं, कि अगर चारु मजूमदार न होते, तो नक्सलबाड़ी भी नहीं होता, यह बात काफ़ी हद तक सही भी है। संशोधनवाद से निर्णायक विच्छेद करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका से कोई इंकार नहीं कर सकता, परन्तु यह भी सत्य है कि विचारधारा की लड़ाई भावनाओं से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तय होती है। नक्सलबाड़ी या चारु मजूमदार का मूल्यांकन भावनाओं से ऊपर उठकर इन्हीं कसौटियों पर ही हो सकता है।
नक्सलवादी आंदोलन के प्रारंभिक समय में वे एक क्रांतिकारी थे, लेकिन हिंसावादी कार्य दिशा पर एक जनवादी क्रांतिकारी लाइन लागू न कर पाने के कारण जल्दी ही वे एक मध्यवर्गीय हिंसक लाइन के प्रवक्ता मात्र बन गए। बाद में उनकी कार्यशैली से यह बात और स्पष्ट हो जाती है। आंध्र प्रदेश में ‘नागी रेड्डी’ जैसे वरिष्ठ नेता वहां पर हिंसावादी लाइन की जगह जनआंदोलन की लाइन लागू करना चाहते थे, लेकिन चारु मजूमदार ने कमेटी में अपनी लाइन लागू करवाई, जो बाद में व्यापक पुलिस दमन और पार्टी के व्यापक विनाश का कारण बनी।
इसके अलावा बंगाल में उनकी लाइन के अनुसार बंगाली पुनर्जागरण के नायकों जैसे:-‘विवेकानन्द, ईश्वरचंद विद्यासागर या रवीन्द्रनाथ ठाकुर’ को प्रतिक्रियावादी घोषित करके बंगला में विशेष रूप से कोलकाता में उनकी मूर्तियों को तोड़ने का जो अभियान चलाया गया, उससे बंगाल के मध्यवर्ग में नक्सलवादियों के प्रति नफ़रत पैदा हुई। पार्टी में एक समय में चारु मजूमदार के प्रशंसक रहे ‘असीम चटर्जी’ तक ने इसका विरोध किया, परन्तु चारु मजूमदार ने किसी की बात नहीं मानी तथा विरोध करने वालों को ही अलगाव में डाल दिया, इसका व्यापक प्रभाव संगठन पर पड़ा और ढेरों लोग उससे अलग भी हो गए।
इसी घटनाक्रम में सौरेन बसु के नेतृत्व में नक्सलवादियों का एक प्रतिनिधिमंडल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिलने चीन गया, वहां वे चाऊ एन लाई और लिन पिआओ से मिले थे। उन सबने चारु मजूमदार की हिंसावादी लाइन की आलोचना की और कहा कि “आप लोग हिंसावादी कार्य दिशा को छोड़कर मज़दूर किसानों में काम करते हुए जन आंदोलनों को विकसित करें।” चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की यह राय एक दस्तावेज़ के रूप में सामने आई, जिसे चीनी पार्टी के दस्तावेज़ के नाम से जाना जाता है। सौरेन बसु इसके बारे में बतलाते हैं, “चारु मजूमदार ने जब इस दस्तावेज़ को पढ़ा, तो वे बेहोश हो गए, उन्होंने तुरन्त उसे नष्ट करने को कहा।” लेकिन उन्होंने नष्ट करने से पहले उसकी एक और कॉपी बना ली थी, जो बाद में चारु मजूमदार की गिरफ़्तारी के बाद सामने आई। दस्तावेज़ को नष्ट करना एक अक्षम्य अपराध था, जिसने क़रीब-क़रीब सारी पार्टी को नष्ट कर दिया।
आज क़रीब-क़रीब सारे ग्रुपों ने चारु मजूमदार की हिंसावादी कार्य दिशा से नाता तोड़ लिया है, केवल भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को छोड़कर। उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। जिन ग्रुपों ने इस लाइन को छोड़ा, उन्होंने इसे मजबूरी में ही छोड़ा, क्योंकि अब ऐसे हालात बन गए थे कि हथियारबंद संघर्ष चलाना संभव नहीं रह गया था। इन ग्रुपों ने कभी अपने दस्तावेज़ों में चारु मजूमदार के हिंसावादी लाइन की समग्र राजनीतिक आलोचना नहीं की, कुछ लोगों ने की भी तो बहुत धीमी जुबान से।
इसी तरह का एक ग्रुप में ‘सीपीआई-एमएल (लिबरेशन)’ भी था, जिसे आजकल लोकप्रिय भाषा में माले भी कहते हैं। इसने 90 के दशक तक मध्य बिहार में सामंतों की हथियारबंद सेनाओं के ख़िलाफ़ लम्बे समय तक हथियारबंद संघर्ष चलाया, जिसमें उनके ‘महासचिव जौहर’ पुलिस मुठभेड़ में मारे भी गए। भारी नुकसान के बाद उन्हें महसूस हुआ, कि बिहार के मैदानी इलाक़ों में वे हथियारबंद संघर्ष नहीं चला सकते, इसलिए चुपचाप उन्होंने अपनी अवस्थिति बदल ली, तथा सीपीआई-सीपीएम की तरह सीपीआई-एमएल भी विधानसभा-लोकसभा का चुनाव लड़ने लगी। अब तीनों पार्टियों में मूलतः कोई अंतर नहीं रह गया है।
हिंसावादी राजनीतिक लाइन के अलावा एक सांगठनिक लाइन भी होती है, इस लाइन को लागू करने वाले लोगों को नेतृत्व में अपनी बातों को लागू करने की बहुत जल्दी पड़ी रहती है, इसलिए वे जोड़-तोड़ तिकड़म करते हैं। विरोधी विचारों के लोगों को अलगाव में डालने के लिए वे उनका चरित्र हनन और विभिन्न तरीकों से कुत्साप्रचार भी करते हैं। 90 के दशक के बाद विभिन्न नक्सलवादी ग्रुपों में जो टूट-फूट हुई, उसके पीछे कमोबेश यही कारण थे, हालांकि इसके पीछे वैचारिक कारणों की तलाश की जाती रही है,जो बिलकुल ग़लत है।
अब थोड़ी सी बात भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के बारे में:-यह आज भी चारु मजूमदार की हिंसावादी कार्यदिशा से दृढ़ता से जुड़ा है। वह न तो चारु मजूमदार को हिंसावादी मानता है और न अपने संगठन को। भारत में इतना ज़्यादा पूंजीवादी विकास हो जाने के बावज़ूद यह संगठन अभी भी देश को अर्द्धसामंती-अर्द्धऔपनिवेशिक समाज मानता है। इनका कार्यक्षेत्र मूलतः देश के अत्यंत दुर्गम तथा जंगली इलाक़ों जैसे-छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा मध्यप्रदेश के इलाक़ों में आदिवासियों के बीच है। इन इलाक़ों में भारतीय पूंजीपति तथा कॉरपोरेट-जिसमें टाटा-बिड़ला,अडानी-अंबानी और जिंदल जैसे घराने विदेशी कॉरपोरेट के साथ मिलकर यहां पर पाई जाने वाली अमूल्य खनिज सम्पदा की लूट कर रहे हैं।
इन कॉर्पोरेटों का भारतीय शासकवर्ग के साथ गहरा सम्बन्ध है। ये लोग शुद्ध साम्राज्यवादी कॉरपोरेट हैं, कोई सामंत नहीं। वास्तव में भारत में जिस सामंती समाज की चर्चा माओवादी अपने साहित्य में करते हैं वह कब का समाप्त हो चुका है। माओवादी वहां पर आदिवासियों के कॉर्पोरेट शोषण के ख़िलाफ़ उन इलाक़ों में कुछ छिटपुट हथियारबंद संघर्ष चला रहे हैं, परन्तु समाजवाद की लम्बी यात्रा के लिए उनमें समग्र दृष्टिकोण का भारी अभाव है। उनका साहित्य बुर्जुआ मानवतावादी बातों से भरा है। देश में क़रीब 80% आबादी मज़दूरों और किसानों की है, उनको देश की मुख्य भूमि पर संगठित किए बिना आप समाजवाद के लिए संघर्ष कर ही नहीं सकते हैं।
माओवादियों ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली तथा देश के दक्षिणी इलाक़ों में कुछ छात्र संगठन,दलित संगठन, मज़दूर संगठन तथा सांस्कृतिक संगठन बनाकर कुछ जन कार्यवाइयों की शुरूआत ज़रूर की है, लेकिन हथियारबंद संघर्ष के ग्लैमर के कारण वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो लेखक, राजनीतिक या संस्कृति कर्मी ईमानदारी से जन कार्यवाइयों में लगे उनका भी दमन माओवादियों के नाम पर किया जा रहा है। माओवादियों के निजी त्याग-बलिदान से कोई इंकार नहीं कर सकता, परन्तु अगर आपकी लाइन ही दिवालिया है, तो आपके महान बलिदान की कोई क़ीमत नहीं है।
आज सम्पूर्ण नक्सलवादी आंदोलन या कहें तो भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन उग्रवामपंथी तथा उग्रदक्षिणपंथी दोनों तरह की अतियों का शिकार है। एक ओर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या माले जैसे संगठन शुद्ध संसदवादी हो गए हैं, हालांकि वहां भी ये बुरी तरह से असफल हैं। दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जैसा संगठन है, जो छुटपुट हथियारबंद संघर्ष के द्वारा बड़ा सामाजिक परिवर्तन करना चाहता है।
निस्संदेह नक्सलवादी आंदोलन ने भारतीय समाज, राजनीति यहां तक की साहित्य पर भी गहरा प्रभाव डाला है तथा देश में परिवर्तन की एक नयी चाहत भी पैदा की है, लेकिन आज बदलती हुई दुनिया में साम्राज्यवाद-पूंजीवाद ने अपने में बहुत बदलाव किए हैं तथा शोषण के नये-नये विविध सूक्ष्म रूप विकसित किए हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन को भी बदलती हुई नयी दुनिया के अनुसार अपने को परिवर्तित करना होगा, तभी हम भारत में भी नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह की विरासत के असली हक़दार होंगे।
(स्वदेश कुमार सिन्हा स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)