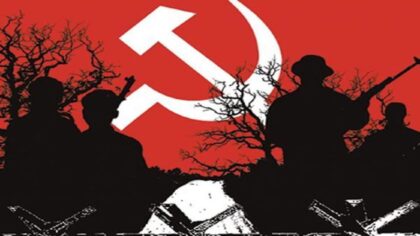भारत में तानाशाही के ठोस रूप को आमतौर पर इंदिरा गांधी द्वारा 1975-77 के बीच लगाये गये आपातकाल के तौर पर देखा जाता है। लेकिन, जब भी कोई सरकार दमनकारी रूख अख्तियार किया, उसके उस कृत्य को तानाशाही, फासीवादी आदि नाम दिया गया। कई बार इसे पुलिसिया राज भी कहा गया। हालांकि, अपने देश के इतिहास में ऐसा किसी पुलिसिया राज का जिक्र नहीं आता है। यह शब्द भारतीय संदर्भ में अमूमन कानून का मनमाने और दमनकारी उपयोग का अर्थ देता है, न कि सैनिक तानाशाही का। लेकिन, पिछले कुछ सालों से एक नये शब्द का प्रयोग शुरू हुआ है, वह है संवैधानिक तानाशाही। इसे बहुसंख्यावादी तानाशाही का नाम भी दिया गया। राजनीतिक सिद्धांतकारों का एक बड़ा हिस्सा अब भी इसे हिंदुत्व फासीवाद या हिंदुत्व की तानाशाही का नाम देने से कतरा रहा है, जबकि इसका प्रयोग बेहद धड़ल्ले के साथ हो रहा है।
इस लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसी राजनीतिक प्रवृत्तियां उभरकर आई हैं, जो भारत के संसदीय राजनीति की कुछ ऐतिहासिक प्रवृत्तियों की निरंतरता को दिखाता है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो नई हैं और आगामी राजनीति में ठोस रूप लेने का रुख भी दिखा रही हैं। इसमें पहला जिक्र विपक्ष के प्रति भाजपा के रुख का करना जरूरी हैः अमूमन शासन में रहने वाली पार्टी जब चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सेदार होती है, तब उसमें खुद को वैध शासक के तौर पर पेश करती है और विपक्ष के दावे को नकारती है।
पिछले लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा के बड़े नेता और खुद प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भारत की शासन व्यवस्था के लिए एक खतरा घोषित करना शुरू किया। उन पर ऐतिहासिक तौर पर भ्रष्ट होने, देश के हितों का नुकसान पहुंचाने और गलत नीतियों से विकास को बाधित करने का आरोप लगाना शुरू किया। इस बार के लोकसभा चुनाव में यह प्रवृत्ति और भी मजबूत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कई सारे भाषणों में कांग्रेस की नीतियों को संपत्ति के मौलिक अधिकार के लिए एक चुनौती की तरह पेश किया और उसे ‘घुसपैठियों’ का समर्थन देने से जोड़ दिया।
भाजपा और खुद मोदी द्वारा ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ उछाले गये नारे का यह चरम रूप था, जो लोकसभा चुनाव के आरम्भिक तीन चरणों तक बना रहा। चुनाव प्रचार में पार्टी के घोषणापत्र और उसकी नीतियों को आपराधिक कृत्य की श्रेणी में पहुंचा देने की कोशिशें कुछ और नहीं है, यह उस पार्टी के सामाजिक और राजनीतिक आधार पर सीधा हमला भी होता है। ये आधार समाज के नागरिक और पहचान आधारित नागरिकों का समूह होते हैं। मोदी अपने भाषणों में पहले भी इन पहचानों को त्यौहारों और कपड़ों से पहचानने का आग्रह कर चुके हैं। इस बार वह इसे सीधा कांग्रेस से जोड़कर पेश कर रहे थे।
दूसरी प्रवृत्ति भाजपा द्वारा मोदी को एकमात्र नेता के तौर पर पेश करना था। पिछले दस सालों से मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर विराजमान हैं। लेकिन, यदि उन्हें भाजपा द्वारा एकमात्र नेता की तरह पेश करने की रणनीति के तौर पर देखा जाय, तब यह समयावधि 12 साल से अधिक की हो जाती है। संसदीय राजनीति में पार्टी संरचना में एक नेतृत्व का उभरना और सत्ता हासिल करने के दौरान प्रधानमंत्री पद का चुनाव एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रिया होती है। इस दौरान कैबिनेट और पार्टी की संरचना में नये नेतृत्व का उभरना जारी रहता है।
इस बार लोकसभा चुनाव में, और कैबिनेट के लंबे चौड़े दायरे में किसी भी नये नेतृत्व का उभार नहीं दिखता है। भाजपा नेतृत्व में लगातार इस तीसरे लोकसभा चुनाव में नेतृत्व के उभरते चेहरों को सामने लाने की बजाय एकमात्र मोदी का चेहरा ही पोस्टरों, होर्डिंग्स और अन्य प्रचार सामग्रियों से भर दिया गया। एकमात्र नेतृत्व राजनीति में सिर्फ विकल्पहीनता को पेश करने की ही रणनीति नहीं है, यह संसदीय राजनीति में विविध राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक समूहों, उनके आर्थिक हितों के लिए निरंतर बनने वाली उन गोलबंदियों का नकार भी है, जिसके बल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया खुद का नवीनीकरण करती है।
दरअसल, भाजपा ऐसे समूहों को राजनीति के एकीकरण के लिए खतरा मानती है और उन्हें कथित तौर पर अपनी समाहितीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की ओर ले जाती है, या उन्हें सामाजिक समरसता के लिए खतरा बना देती है। उसने इसी प्रक्रिया को पार्टी के भीतर भी लागू करती हुई लगती है, जिसका सीधा परिणाम एकमात्र नेता के तौर पर मोदी की पेशगी में दिखी है।
तीसरी प्रवृत्ति चुनाव प्रचार में परमात्मा का अवतरण और मसीहा के उत्थान के रूप में दिखा है। मोदी की भक्ति अब धीरे धीरे एक धर्म में बदलती हुई दिख रही है। यह काम उनके भक्त नहीं खुद मोदी मीडिया के माध्यम से करने में लग गये। यह भी इस लोकसभा चुनाव का ही एक हिस्सा है। वह तीसरे चरण में ही खुद को परमात्मा से जोड़ने लगे थे। चौथे चरण के दौरान मीडिया को दिये गये व्यापक साक्षात्कारों में खुद को जिस तरह दैवीय आभा के साथ पेश करने लगे उसका कुल जमा अर्थ एक मसीहा के अवतरण का था, जो वह खुद थे।
इस संदर्भ में इंदिरा गांधी को 1971 में बांग्लादेश बनाने का जो श्रेय दिया गया और पाकिस्तान के ऊपर भारत की जीत का जो सेहरा उन्हें प्रदान किया गया, उसका अंतिम परिणाम उनकी ‘दुर्गा’ की उपाधि थी। इस दुर्गा ने जब आपातकाल लगाकर ‘संहारक’ की भूमिका में आई तब उनके सामने दंडवत होने वालों की कतार लग गई। मोदी के हिस्से में ऐसी कोई जीत नहीं है। लेकिन, पिछले कई सालों से उन्हें विश्वपटल का एक सर्वमान्य नेता की तरह पेश करने की कोशिशें जारी हैं। उन्हें एक तरफ युद्ध रुकवा देने का श्रेय दिया जाता है, वहीं पड़ोसी देशों को सबक सिखा देने वाले व्यक्तित्व की तरह भी पेश किया जाता है। हालांकि इसका कोई ठोस आधार नहीं है। उन्हें जिस बात का श्रेय दिया जा सकता है वह है विपक्ष की पार्टियों को तोड़ना, उनकी सरकारों को गिराना और उनके खिलाफ आपराधिक मुकद्मों के सहारे जेल में डालना, …।
भाजपा और खुद मोदी ने मसीहा के आगमन के लिए जिस चेहरे को चुना, वह खुद मोदी हैं। उन्हें भारत के मान्य देवताओं से बड़ा बताने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया। मोदी में किसी भी मानदंड से मसीहा के गुण भले ही न दिखते हों, उन्हें मसीहा की तौर पर पेश करना और खुद उनके द्वारा ही अपने को मसीहा की तरह बताना एक दूरगामी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा दिखता है। ऐसी रणनीति सिर्फ मनमाने निर्णय लेने की क्षमता को हासिल करने का ही नहीं है, यह हिंसा के प्रयोगों को एक पवित्र कार्य बना देने की क्षमता से लैस होने का दावा भी है। मोदी और भाजपा ने अपने प्रति बनाए और पैदा हुए भक्ति भाव और बुद्धिजीवियों द्वारा ‘मोदी मसीहा?’ जैसे शीर्षकों का प्रयोग इस लोकसभा में इसे गुणात्मक तौर पर बदल देने की रणनीति को अख्तियार किया है।
चौथी प्रवृत्ति शासकीय संस्थानों की भूमिका में आये बदलाव में दिखा है। खासकर, चुनाव आयोग की भूमिका एक गहरे संदेह से भर गया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संसदीय लोकतंत्र को बनाये रखने में इसकी निर्णायक भूमिका है। जो पार्टी सत्ता में होती है, आने वाले या होने वाले चुनावों में निश्चित ही सरकारी संस्थानों का उपयोग अपने हितों में कर लेना चाहती है। लेकिन, निश्चित ही यह उपयोग उन दायरों के भीतर होता है जहां तक किसी पार्टी की सत्ता का दखल जा सकता है। जब यह दखल नियंत्रण में बदल जाए तब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाये रखना संभव नहीं रह जाता। पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग में भाजपा का दखल नियंत्रण में बदलता गया है। यह नियंत्रण सिर्फ चुनाव आयोग की संरचना में ही नहीं आया, यह कार्यप्रणाली में भी अभिव्यक्त होना शुरू हो गया है।
लोकसभा चुनाव के पहले जितने बड़े पैमाने पर विपक्ष की पार्टियों, नेताओं और उनकी सरकारों के खिलाफ जिस तरह से विभिन्न शासकीय संस्थानों का प्रयोग किया गया उससे संसदीय लोकतंत्र की पार्टी कार्यप्रणाली टूटने के कगार पर पहुंच गई। इसी तरह सामाजिक आंदोलन बनाने के लिए विपक्ष की पार्टियों की पहलकदमी पर जिस तरह के मुकद्मे दर्ज हुए वह भी काफी खतरनाक किस्म के थे।
सत्ता संस्थान, सत्तासीन पार्टी और विपक्ष के त्रिकोण में चुनाव आयोग एक नियामक की भूमिका में आने की जगह इस बार वह खुद इसी त्रिकोण में एक सत्ता संस्थान की तरह ही काम करता हुआ दिखा। और, वह संवैधानिक संस्था होने के अधिकार से वंचित होता दिखा है। खासकर, जब हम उस पर लग रहे ठोस आरोपों और पेश किये गये तथ्यों की नजर से देखें तब यह स्थिति और भी भयावह दिखती है। कांग्रेस द्वारा पेश किये गये 111 सीटों पर वोट की गिरावट का विश्लेषण जब वह लोगों के वोट से वंचित कर दिये जाने से जोड़ता है, तब यह सिर्फ आरोप भर नहीं है। इसी तरह से, वोट के प्रतिशत में बदलाव और कुल वोटों की संख्या को न बतलाना भी चुनाव की मूलभूत प्रक्रिया को अपारदर्शी बना देने के करीब जाता हुआ लग रहा है।
लेकिन, सबसे अधिक चिंतनीय बात वोट डालने के दौरान मुस्लिम समुदाय के साथ हुए भेदभाव के आरोप और उनके खिलाफ पुलिस द्वारा हिंसा के प्रयोग, चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप की वे खबरें हैं, जिससे चुनाव की मूलभूत प्रक्रिया ही नष्ट होती दिखी है। देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें, वीडियों प्रचारित और प्रसारित हुए जिसमें मुस्लिम समुदाय के वोट के अधिकार प्रभावित होते हुए दिखते हैं। चुनाव आयोग ने कुछ मामलों में निश्चित ही संज्ञान लिया है, लेकिन यह मसला छिटपुट हुई घटना का हिस्सा नहीं है।
यह एक खास तरह की राजनीति से जाकर जुड़ता है जिसकी मानसिकता में वह दोयम दर्जे का नागरिक भी नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया से किसी भी समुदाय को बाहर रखना, किया जाना या उसे बाहर होने के अहसास से भरते जाना, … एक नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन ही नहीं है, उसे संसदीय लोकतंत्र से बाहर कर देना भी है। चुनाव आयोग द्वारा इस पर चुप्पी संसदीय लोकतंत्र को उस दिशा की ओर ले जा सकती है, जहां चुनाव का अर्थ किसी सत्ताशीन पार्टी के शासन को ही आगे बढ़ाना भर जाएगा। इस तरह के प्रयोग भारत के विभिन्न राज्यों में पहले भी देखा गया है, और वहां ऐसी प्रक्रियाओं का नतीजा आमजनों की हत्याओं में ही बदलता हुआ दिखा है।
पांचवी प्रवृत्ति हम बाजार अर्थव्यवस्था, खासकर शेयर बाजार में हुए उठापटक में देख सकते हैं। अमूमन शेयर बाजार लोकसभा चुनावों में अपनी प्रवृत्ति को जाहिर करता है। जब भी सत्तासीन पार्टी चुनाव में उतरती है, सबसे पहले वह बाजार को आश्वस्त करती है कि वह उसके हितों का ख्याल करेगी। लेकिन, बाजार सत्ता के चुनाव में उतरी पार्टियों से अधिक की चाह रखती हैं। 2014 में जब कांग्रेस सरकार खत्म हुई और मोदी के नेतृत्व में भाजपा का आगमन हुआ तब उसने ऐतिहासिक उछाल मारा था। तबसे बाजार मोदी पर भरोसा कर रहा है।
इस बार जब चुनावों में वोट कम पड़ने शुरू हुए और मोदी की हवा कमजोर साबित होनी शुरू हुई, तब शेयर बाजार में उठापटक शुरू हुई। शेयर बाजार के खिलाड़ी इस बात से आश्वस्त थे कि मोदी इस लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं। उनकी चिंता यह थी कि इस बार उनका बहुमत सीट कम हो रहा है। इस बात को आश्वस्त करने के लिए बकायदा प्रशांत किशोर जैसे चुनाव विश्लेषकों का प्रयोग किया गया। लेकिन, इस बाजार की प्रवृति में जो बात छिपी हुई है वह भीषण बहुमत की चाह है। उसे एक ऐसा नेता चाहिए जो बाजार के लिए निर्णय लेते समय किसी अड़चन और रुकावट से परे हो। उसे दरअसल एक तानाशाह चाहिए जो बाजार के हितों के लिए अन्य दबावों को दरकिनार करने की क्षमता रखता हो और जनता को अपनी लोकप्रियता में बांधे रखकर उनके खिलाफ किसी भी तरह की गोलबंदी का रद्द या खत्म कर देने की क्षमता रखता है।
उसे भी एक मसीहा की जरूरत है। निश्चित ही, यदि हम अडानी के कारनामों को देखें, तब हम उसके उत्थान में हर तरह की बाधा को खत्म होता हुआ देखते हैं। चाहे वह वित्तीय अनियमितता हो, कोयला घोटाला या पर्यावरण को बर्बाद करने का आरोप हो। भारत की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय संस्थानों की पकड़ और उद्यमों में मनमाने आवंटन, अधिग्रहण और श्रमिक कानूनों की बढ़ती अप्रासंगिकता एक ऐसी आर्थिक संरचना का निर्माण करती है, जिसका अंतिम बोझ किसानों, युवाओं और महिलाओं पर पड़ रहा है। इस लोकसभा चुनाव में बाजार पिछली बार की तरह ही लेकिन उससे और अधिक मजबूत नेता का इंतजार कर रहा है।
उपरोक्त प्रवृत्तियां भारत की संसदीय राजनीति में एक ध्रुवीकरण की ओर ले जाती हुई दिख रही हैं। भाजपा के नेतृत्व में आरएसस और विश्व हिंदू परिषद की भूमिका आधारभूत और निर्णायक रही है। इन तीनों में हिंदू महासभा और अन्य इसी तरह के संगठन अपनी निर्णायक और बड़ी भूमिका का निर्वाह करते रहे हैं। ये संगठन भारत की आर्थिक संरचना और उसकी राजनीतिक का भी निर्वाह करते रहे हैं। भारत के निर्माण में जिन आर्थिक समूहों और उद्योगपतियों ने भूमिका निभाई है, उसमें जमींदारों, छोटे और बड़े रजवाड़ों ने भी बड़ी भूमिका निभाई है।
ये वही समूह हैं जिनसे भारत का शासक वर्ग बनता है। आरएसएस और इससे जुड़ी पार्टी और संगठनों का उत्थान और पतन उतनी सीधी नहीं है, जितनी दिखाई जाती है। भारतीय संस्कृति के नाम पर हिंदुत्व की चाह रखने वाला भारत के पूंजीपति और जमींदार वर्ग को कभी भी अन्य धर्मों या समुदायों या किसान-मजदूरों के कत्लेआम से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे निश्चित ही गांधीजी की हत्या से फर्क पड़ा। वे हिंदुत्व को इस हद तक की संकीर्णता में नहीं देखना चाहते थे। लेकिन, उनका चुनाव निश्चित ही भारत की महान हिंदू संस्कृति के साथ जाकर जुड़ता है।
इसमें बहुसंख्या का चुनाव तो है ही, इसमें जाति आधारित समाज में जो कार्य विभाजन है उससे न सिर्फ सस्ते श्रम की खेत और उद्योग में उपलब्धता आसान हो जाती है, साथ ही इससे पैदा हुई विविधता स्थानीय राजनीति को वह जगह प्रदान करती है जिससे केंद्रीयकृत राजनीति मजबूत और नियंत्रित बनी रहे। आज आरएसएस और उसकी पार्टी भाजपा और उसके विभिन्न संगठन सत्ता में सीधी भागीदारी कर रहे हैं।
यह हिंदुत्व की चरम राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। यह रास्ता उतना आसान नहीं है जितना पहले विश्वयुद्ध के बाद यूरोपीय देशों में बन गया। भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति के शीर्ष पर जो पूरी तरह से पतित जमींदारों, भूस्वामियों, सूदखोरों और दलाल पूंजीपतियों और नैतिक तौर पर पतित सट्टेबाज नेताओं का हुजूम बैठा है उसके नीचे एक विशाल छोटे उद्यमियों, मध्य उद्योगपतियों, किसानों, मजदूरों, मेहनतकशों का संसार सरगर्मियों में डूबा हुआ है। युवा एक नये रास्ते की तलाश कर रहा है।
इस बार जब राहुल गांधी ने संविधान की किताब लेकर इसे बचाने के बारे में नारा दिया तब वह निश्चित ही उन लोगों तक पहुंचना चाहते थे जो इस दायरे से भी बाहर कर दिये गये हैं। विपक्ष के नेताओं ने जिस तरह छोटे-छोटे कस्बों तक जाने का अभियान चलाया, उससे साफ दिखता है कि उनका दायरा ऊपर की ओर कम हुआ है, वे नीचे विशाल जन के बीच ही उम्मीद देख रहे हैं। यह अनायास ही नहीं है जब एक टीवी एंकर एक आदिवासी नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जंगल भेज देने की बात करता है। जंगल में भेजकर वहां ‘माओवादी’ के तमगे के साथ मार देना आज बेहद आसान सा हो गया है।
इस संसदीय लोकतंत्र में चुनाव के परिणाम जो भी हैं, भारत की राजनीति अर्थव्यवस्था एक तानाशाह पार्टी व्यवस्था की चाह में डूबी हुई है। यदि उसे मनमुताबिक परिणाम हासिल होता है तब यह तानाशाही खतरनाक तरीके से आगे जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है, तब नई सत्तासीन पार्टी के लिए उतना ही चुनौतीभरा रास्ता होगा। संभव है, वह धीमे ही सही, उसी तानाशाही वाले रास्ते पर आगे जाए, जैसा कि चुनावी इतिहास की एक परम्परा रही है। इस चुनाव में साफ है, सत्ता के बदलाव की चाभी जनता के पास ही है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव के अभियानों ने इतना तो जरूर ही स्पष्ट किया है। वैसे, एक आम राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए यह सबक एक आम सी ही बात है, हालांकि यह रास्ता उतना आसान नहीं है जितना यह सिद्धांतों में दिखता है।
(अंजनी कुमार स्वतंत्र पत्रकार हैं)