शिक्षा पर रबीन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध उक्ति हैः ‘सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है।’ ऐसी उक्तियां भारत के अन्य महापुरूषों के उद्गारों में आसानी से मिल जाएगी। किसी दर्शन, विचार को पेश करने के लिए यदि हम आदर्श स्थिति का चुनाव करें, और उस दिशा में प्रयास करें तब अक्सर ही ऐसे आदर्श सिद्धांतों का चुनाव जरूरी हो जाता है। लेकिन, ऐसे चुनाव और सिद्धांतों की प्रस्तुति को जब ठोस राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हालातों से गुजरना होता है, तब इस तरह के सूत्रीकरण का दम फूलने लगता है।
भारत में शिक्षा दर्शन और शिक्षा की अवस्था में सुधार को लेकर अक्सर आयोगों का गठन और उस पर रिपोर्ट आते रहे हैं। यह काम केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पर होता रहा है। इसमें विदेशी संस्थानों ने अलग से भूमिका निभाई है। खूब सारे दावे और खूब सारी योजनाओं का अंतिम परिणाम कभी भी न तो शिक्षा के व्यापक हो जाने में दिखाई दिया और न ही यह समाज का उच्च आदर्शों के साथ लैस कर पाया। धर्म, भाषा, जाति, समुदाय, …यहां तक कि व्यवहार के मानदंड, जिसे सामाजिक एटिकेट कहा जा सकता है, के आधार पर भेदभाव की गहरी छाया न सिर्फ शिक्षा की पूरी संरचना में व्याप्त दिखाई देती है बल्कि शिक्षा पूरी करने के बावजूद भी पूर्वाग्रहों का ढांचा खत्म ही नहीं हो पाता है और फिर यह अगली पीढ़ी में चलता चला जाता है।
‘प्रोफेसर की डायरी’ एक ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था से रूबरू कराता है जिसकी राजनीति एक ओर समाज की उन जड़ों के साथ जाकर जुड़ती है जिसे आप नृविज्ञानिक ढांचा कह सकते हैं। इसके जड़ का अध्ययन आपको सिर्फ जाति, धर्म, समुदाय आदि सारणियों के तहत ही नहीं, उसके विकास की अवस्थाओं के साथ भी जोड़कर करनी होगी। और इसका दूसरा हिस्सा, जो आधुनिक शिक्षा संस्थानों की विविध सोपनों से भरी व्यवस्था है, जिसमें आधुनिकता का दावा है और वर्चस्व की सक्रिय व्यवस्था है, जिसकी स्वतंत्रता के विशाल गुब्बारे के भीतर सांस लेने की एक सीमित कंडीशनिंग है जिससे बाहर आने का अर्थ है, कि आप अब कहीं नहीं हैं।
इस पुस्तक के अंतिम अध्याय से इसे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। डॉ. लक्ष्मण यादव ‘शजर छीन लिया, परिंदा उड़ चला’ में लिखते हैं: ‘‘चौदह साल जिस कॉलेज को दिया, उसे मुझसे छीन लिया गया। साढ़े इक्कीस साल के एक अनगढ़ शख्स को जिस कॉलेज ने गढ़कर तैयार किया, उसी से मुझे निकाल दिया गया। वजह बताने का न तो कोई नियम है और न कोई जरूरत। उन्हें भी सब पता है और मुझे भी। बस अफसोस यही कि कॉलेज के कई अपनों ने उतना साथ नहीं दिया, जितने की दरकार थी।/अम्मा और बड़े चाचा को लेकर ही चिंतित था कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अम्मा बोलीं- ‘हम त पहिलें से ही कहत रहलीं, गौं से रहा। ढेर मत बोला। लेकिन न तोहार बाप कब्भों हमार बात मनलें और न तूं मनला। अब देखा कुल निकार दहलें न। चला कऊनो बात ना, परसान मत होइहा। कुछ ना होई घरे चल अइहा, चिंता मत करिहा। सब अच्छा होई।’’
इन पक्तिंयों को पढ़ते हुए यही लगता है कि शिक्षा व्यवस्था सिर्फ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। एक पूरी राज्य व्यवस्था है जिसकी सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपने नहीं हैं। मां के लिए भी वे ‘अन्य’ की तरह आते हैं। उनसे उनका बेटा एक भिड़ंत की स्थिति में हैं। मां इस व्यवस्था को जानती हैं और अपने अनुभव को बेटे के साथ साझा करती हैं, लड़ने का तरीका बताती है। जबकि हम यह भी जानते हैं कि मां कभी भी इस शिक्षा व्यवस्था में बेटे के बराबर तक पढ़ने नहीं आई, वह कैंपस में नहीं आई, …। वह इस कैंपस को अपने गांव-गिराव में लड़ी लड़ाईयों के अनुभव से देखती हैं।
ऐसा नहीं है कि डॉ. लक्ष्मण यादव गांव के अनुभवों से मरहूम थे। वह वहां के यथार्थ और हासिल किये अनुभवों को एक नई दुनिया का हिस्सा बना लेने, चाह और सपनों से भरे हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में आये। जब वह यहां के एक कॉलेज में एक प्रोफेसर (एड्हॉक) चुन लिए जाते हैं, तब भी वह उस यथार्थ की खुरदुरी जमीन से अलग नहीं होते हैं: ‘पता है, कलम-किताब ने मेरे लिए आज जिंदगी का नया अध्याय लिख दिया। आज का दिन मेरे लिए ऐसा रहा गोया भूमिहीन मजदूर के हिस्से जमीन का टुकड़ा आ गया हो। आज उस खेत को मनभर निहार कर फसलों की अपार संभावनाएं संजोकर घर लौटा हूं। मेरी उम्र के हर नौजवान को ऐसे मौके नहीं मिल पाते। मेरे जैसे अनगिनत युवाओं को मौजूदा व्यवस्था के अनगिनत इम्तिहान रौंद कर घर लौटने को मजबूर कर देते हैं। मुझे प्रोफेसर बनने का मौका मिल गया। राकेश, संगीता, मनोज, अभिनव, रेनू और फूलबदन मेरे बैचमेट थे जो अब गांव लौटकर खेती, मजदूरी, दिहाड़ी या चौका बर्तन कर रहे होंगे। और आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कालेज में पढ़ा कर लौट रहा हूं। उनकी बहुत याद आ रही है।(आईन में प्रोफेसर)।’
जिस दुनिया में वह प्रवेश कर रहे थे, उसमें औपचारिक तौर पर आधुनिकता, सेक्युलर माहौल, संविधान और न्याय की अवधारणा पर स्थापित संस्थाओं और शिक्षा का लोकतांत्रिक दर्शन का भास हो रहा था, लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरा और अनभै साचा की टकराहटें सामने आईं, समाज की वही गहरी खाईयां, भेदभाव और वर्चस्व की राजनीति की संरचनाएं खुलती गईं। कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षक, छात्र, कक्षा, नियुक्तियां और यहां तक कि छात्रों की भर्ती से लेकर पाठ्यक्रमों की नीतियां तक ताकतवरों के हाथों में फंसी हुई दिख रही थीं। यहां भी वही जाति व्यवस्था, भेदभाव, मनमानापन, पूर्वाग्रह और गिरोहबाजी का माहौल उभरकर सामने आता दिखने लगा।
डॉ. लक्ष्मण यादव शिक्षकों के नैतिक पतन से लेकर कुलपति के हाथी पर सवार होने का जो दृश्य गढ़ते हैं, वे कोई अनजानी बातें नहीं हैं लेकिन इस पुस्तक के कलेवर में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सामंतवाद की सवारी और विश्व बैंक जैसे संस्थानों की जी हुजूरी का पूरा ढांचा खुलकर सामने आ जाता है। डॉ. लक्ष्मण यादव से जब शजर छीन लिया जाता है तब इस विश्वविद्यालय की दहलीज से सवाल करने का निर्णय लेते हैं: ‘मैंने तय किया कि मैं इस अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा। सवाल ये उठाया कि मुझे निकाले जाने की वजह बताई जाए। इसे निजी लड़ाई बनाने की बजाय बर्बाद होती उच्च शिक्षा से जोड़कर देखा।’
लड़ाई को आगे ले जाने का निर्णय डॉ. लक्ष्मण यादव को संघर्षां के स्तरों से जोड़ देती है। वह अपने परिवार से हासिल अनुभवों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में हासिल किये अनुभवों के साथ जोड़ते हुए चलते हैं और इस दुनिया की सच्चाई से टकराने के अपने तौर तरीके खोजते हैं। वह रोहित वेमुला को याद करते हुए एक महिला शोधार्थी के वाक्यों को उद्धृत करते हैं: ‘‘सब मिलकर हर रोज थोड़ी-थोड़ी हमारी हत्या करते हैं उसे नाम देते हैं सुसाइड का। सही ही लिखा रोहित ने अपने आखिरी खत में कि मेरा जन्म ही एक दुर्घटना थी। इन कैंपसों में आकर हमें भी यही लगता है कि हमारा दलित, आदिवासी, पिछड़े घरों में जन्म लेना ही दुर्घटना है। मैं इतना बोल रही हूं कि इसलिए क्योंकि मैंने सोच लिया है, इन द्रोणाचारियों के सामने कभी गिड़गिड़ाने नहीं जाऊंगी। ये द्रोणाचारी कभी भी न्याय नहीं करेंगे।’’
इतिहास, मिथक, धर्म, संस्कृति और जाति की संरचना में पगी हुई जिस नैतिकता और व्यवहार का जन्म होता है उसकी मूल धुरी सत्ता का वर्चस्व होता है। भारत में शिक्षा को जिस तरह से जकड़कर रखा गया है और उस पर परम्परा, धर्म, मूल्य और नैतिकताओं का जिस तरह का बोझ लाद दिया गया है उससे सिर्फ शिक्षा ही तबाह नहीं हो रही है, इसकी संस्थाएं चरम पतन की ओर बढ़ चली हैं। ये पुलिसिया डंडों से भी बदतर हो चुकी हैं। एड्हॉक शिक्षकों की नियमित नियुक्ति न होना और उनका आत्महत्या कर लेना, एक भयावह तस्वीर का एक छोटा सा दिखने वाला हिस्सा ही है। इसके भीतर की संरचना में कितने शिक्षक और छात्र भी घुटनभरे हालात में जी रहे हैं, उसकी तस्वीरें, फिलहाल अभी आना बाकी है।
‘एक प्रोफसर की डायरी’ एक रोजनामचे की तरह दर्ज की हुई इबारत की तरह दिखती है। इसकी परतों में गांव का समाज, शिक्षा से उम्मीदें और नाउम्मीदी भी की इबारते हैं। इसमें खेत की मेड़ों के हाइवे में बदलने की नीतियों के खुलासे हैं, जिससे विकास के चलकर आने की बातें कहीं गईं। लेकिन, यह सड़क पर चलती हुई गाड़ियों के सरल समीकरणों की तरह नहीं हैं। इस पर पूंजी के मालिकों का ही नहीं, सामंतों का भी वर्चस्व है। ये सामंत और उनकी संरचनाएं विकास के साथ चलते हुए शहर की संस्थाओं में भी आये और काबिज हुए।
साम्राज्यवाद अपनी पूंजी के साथ सिर्फ नीतियां लेकर नहीं आया, वह शहर से गांव की ओर काबिज होते हुए गया। अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत क्षमता और प्रतियोगिता का मसला नहीं है। यह पुस्तक उसकी नृवैज्ञानिक पहचान, उसकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता, उसकी राजनीतिक समझदारी और संस्थानों की संरचना में संविधान और न्याय जैसी शब्दावलियों का कानूनी प्रक्रिया के माध्यमों को हासिल में बदल देने की क्षमता और अक्षम होने के कारणों को सामने लेकर आता है।
यह पुस्तक आंकड़ों और व्याख्याओं का सहारा लेने की बजाय एक डायरी की शैली में बदलता है, यह आत्मकथा का रूप अख्तियार करते हुए राजनीति की उस पेचिदा गलियों में लेकर चला जाता है जिसमें हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं है वह इतिहास से निकल कर आते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय की आधुनिकता को रौंदते हुए एक नये पतनभरे युग की औपचारिक शुरूआत करता है।
( समीक्षक अंजनी कुमार स्वतंत्र पत्रकार हैं)


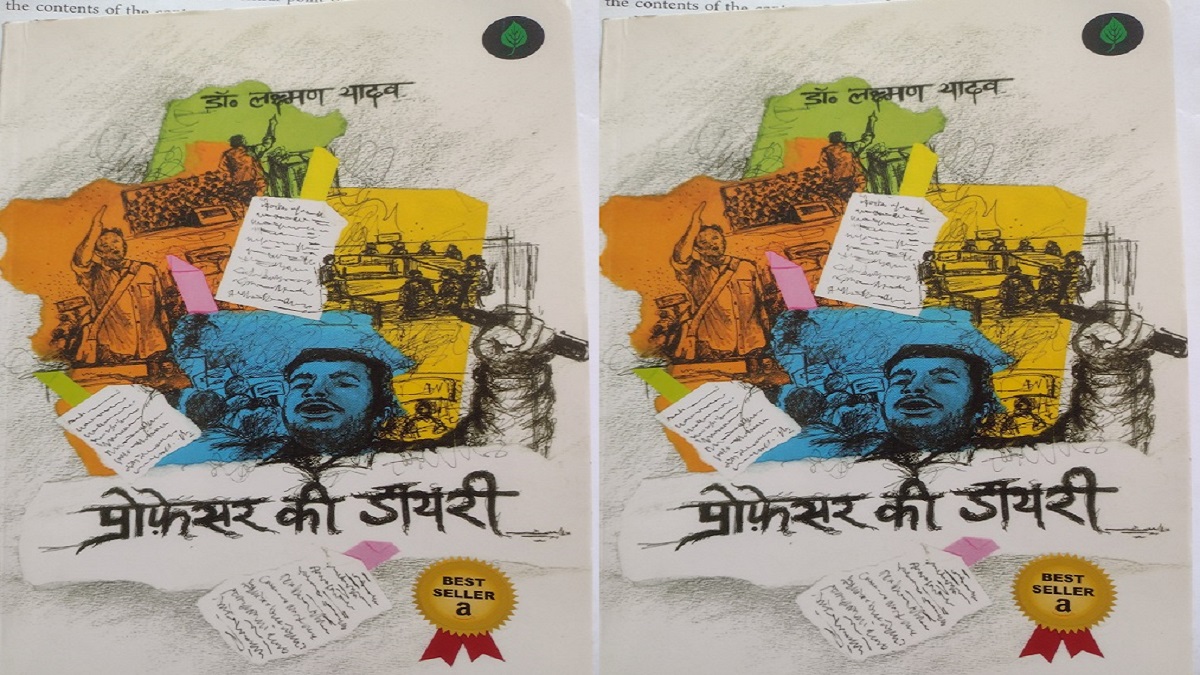

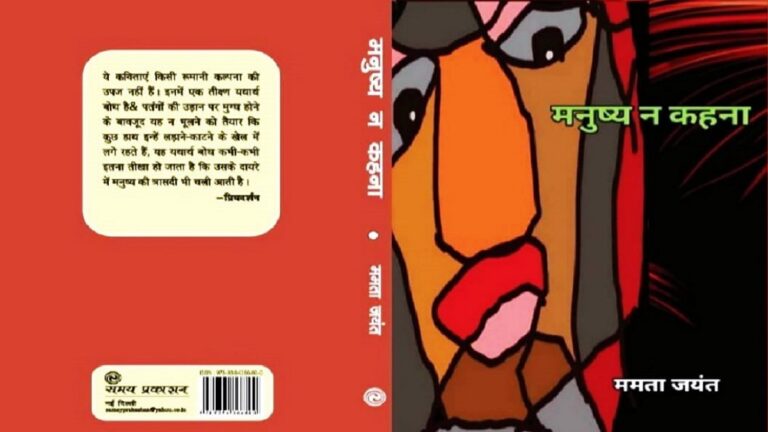

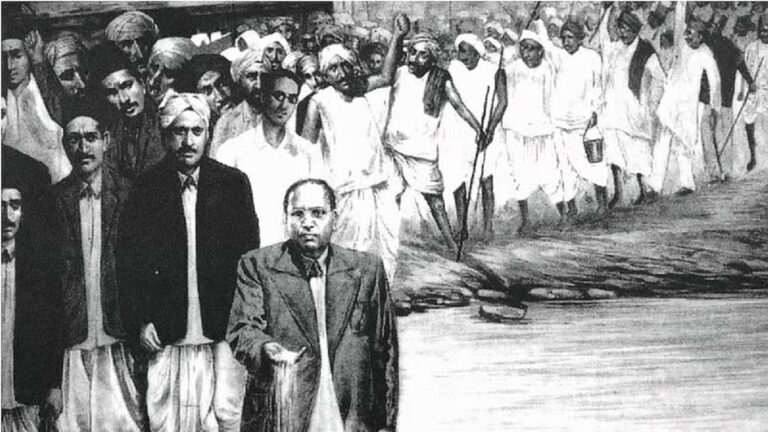





Ye book mere bhi college ke dino ko yad dilata hai ki kaise mere sath bhed bhaw kiya jata tha