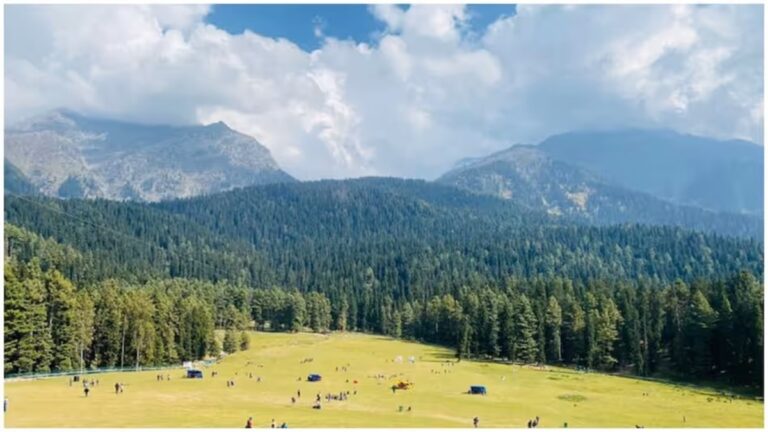झारखंड। पेसा अधिनियम को लेकर पिछले 28 अक्टूबर 2024 को “आदिवासी स्वशासन अधिकार मंच” के द्वारा झारखंड के रांची जिला अंतर्गत नामकुम स्थित बगईचा के सभागार में एक कार्यशाला आयोजित की गयी। जिसमें इस बात पर चर्चा की गयी कि पेसा के तहत पारम्परिक मॉडल ग्रामसभा का ढांचा कैसा हो?
पेसा अधिनियम के उद्देश्यों की हम चर्चा करें तो इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना है।
यह कानूनी रूप से आदिवासी समुदायों, अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के अधिकार को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को शासित करने के अधिकार को मान्यता देता है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करता है।
वहीं पेसा अधिनियम ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंज़ूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है।
PESA एक्ट यानी “पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट”। यह एक भारतीय कानून है जो 1996 में पारित किया गया था और 1997 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना है।
यह देश के 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, और राजस्थान में पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में नामित किया गया है।
कार्यशाला में कहा गया कि PESA नियमावली को लागू कराने के उद्देश्य से हर गांव स्तर पर मॉडल ग्रामसभा गठन करने की जरूरत आन पड़ी है। जो पत्राचार के माध्यम से दबाव बनाने का काम करेगा।
इसी उद्देश्य के तहत झारखण्ड के अनुसूचित जिलों संताल परगना, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, प.सिंहभूम, पू.सिंहभूम व सरायकेला खरसावां जिले के करीब 24 गांवों के पारम्परिक ग्राम प्रमुखों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में ग्रामसभा गठन की प्रक्रिया में मुख्य बिन्दुओं पर पूरे दिन की कार्यवाही के दौरान चर्चा हुई।
नियंत्रण का मॉडल कैसा हो? विभिन्न मदों का प्रबंधन का मॉडल कैसा हो? भूमि, संस्कृति तथा ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का मॉडल कैसा हो? ग्रामसभा में गांव के विकास का मॉडल, प्लानिंग और कार्य-निष्पादन कैसे हो?
बाहरी अवांछित तथा असमाजिक तत्वों से ग्राम की सुरक्षा और पारम्परिक न्याय प्रणाली को सिस्टेमेटिक बनाना और कोल्हान के “न्याय पंच” के तर्ज पर पूरे राज्य के आदिवासी पारम्परिक स्वशासन को इलाके में लागू करने को लेकर लंबी बहस हुई।
कार्यशाला में वाल्टर कंडुलना ने कहा कि आदिवासी परम्परागत स्वशासन प्रणाली में तीन स्तरीय व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अभी तक केवल बुनियादी ग्राम स्तरीय व्यवस्था को ही मान्यता दी गई है। उन्होंने परम्परागत प्रणाली की संपूर्ण संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे शासन प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता है।

वहीं, घनश्याम बिरुली ने कहा कि ग्राम सभा के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में अपने संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण लेना बहुत महत्वपूर्ण है। पेसा में दिए गए अन्य सभी अधिकारों पर भी जोर दिया जाना चाहिए, ताकि गांव के सदस्य उनका प्रयोग कर सकें।
प्रो. राम चंद्र ओरोन ने स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायत प्रणाली की उत्पत्ति के बारे में बात करते हुए कहा कि अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्रों के लिए अपवाद बनाए गए थे, क्योंकि ये सामान्य/राजसी सम्पदाओं से अलग पहले से मौजूद विशेष सामाजिक शासन प्रणाली थीं।
एलिना होरो ने कहा कि यह बैठक विशेष थी, क्योंकि स्वशासन प्रक्रिया में पहले से शामिल प्रतिभागी पेसा के ढांचे में अपने लिए एक रोडमैप फिर से तैयार करने में सक्षम हैं, जबकि वे अपने संबंधित समुदायों में स्वशासन की पारंपरिक प्रथाओं में गहराई से निहित हैं।
टॉम कावला (जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉ. बी.डी. शर्मा के साथ थे) जो तत्कालीन दक्षिण बिहार के 800 लोगों के साथ अपने पारंपरिक स्वशासन प्रणाली को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
अन्य राज्यों के आदिवासी समुदाय के नेताओं के साथ दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 1996 में पेसा कानून बना। कवाला ने कहा, संघर्ष आज भी जारी रहना चाहिए जब तक कि ग्राम सभाएं और आदिवासी स्वशासन प्रणाली अपने पूर्ण रूप में कार्यात्मक नहीं हो जाती।
इस अवसर पर विनीत मुंडू ने कहा कि झारखंड में पेसा और इसके नियम के लिए संघर्ष लंबा रहा है, लेकिन राज्य के लिए पेसा नियम नहीं बनने के कारण बहुत कुछ खो गया है, पेसा का आह्वान भी आदिवासी स्वशासन की दिशा में संघर्ष का एक हिस्सा है।
उन्होंने आगे कहा, पेसा के अनुसार ग्राम सभाओं के रूप में इसे शुरू करने से ग्रामीण और अनुसूचित क्षेत्रों के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के लिए दरवाजे खुलेंगे।
सुषमा बिरूली ने कहा कि कोल्हान में ‘न्याय पंच’ पेसा का सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां समुदाय के सदस्यों के बीच सामाजिक और भूमि विवादों के मामले में न्याय प्रदान करने के लिए प्रथागत स्वशासन की कानूनी मान्यता है।
इस कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों का सक्रिय योगदान रहा। सभी ने अपने अनुभव और बहुमूल्य सुझाव दिये।
कार्यक्रम को सफल बनाने में वाल्टर कुंडलना, घनश्याम बिरुली, रामचंद्र उरांव, सुषमा बुरुली, रोज खाखा, विनीत मुंडू, कृष्णा समड, प्रकाश कोनगाड़ी, सुदर्शन भेंगरा, मनमसीह गुड़िया, जागरण मुर्मू, सोमाय मार्डी, गणेश मुर्मू सहित कई लोगों का सहयोग रहा।
(प्रेस विज्ञप्ति।)