पृष्ठभूमि ऐसी है कि उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयानों को अक्सर केंद्र में सत्ताधारी पार्टी की राय से जोड़ कर देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट पर धनखड़ का ताजा हमला भी इस संदर्भ से अलग नहीं है। धनखड़ ने ताजा टिप्पणी तमिलनाडु विधान सभा से पारित विधेयकों की मंजूरी रोके रखने के राज्यपाल एन.आर. रवि के रवैये के खिलाफ आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर की है।
सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 से मिले विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए लंबित रखे गए दस विधेयकों को मंजूर हो गया घोषित कर दिया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 200 में मौजूद अस्पष्टता को खत्म करते हुए व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति/ राज्यपाल को विधायिका से दो बार पारित विधेयक को 90 दिन के अंदर मंजूरी देनी होगी।
अब धनखड़ की टिप्पणियों पर गौर कीजिएः
- सुप्रीम कोर्ट यह कैसे तय कर सकता है कि राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए?
- अनुच्छेद 142 को लोकतंत्र के खिलाफ परमाणु मिसाइल बना दिया गया है।
- न्यायपालिका तेजी से लोगों का भरोसा खो रही है।
- (दिल्ली हाई कोर्ट के) एक जज के यहां नकदी बरामद हुई और उस मामले में कुछ नहीं किया गया। जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई?
(https://x.com/MrSinha_/status/1912808572544495909)
उप-राष्ट्रपति की बातों को अगर सत्ताधारी जमात की सोच के रूप में देखा जाए, तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि संविधान में निहित संघवाद (फेडरलिज्म) और विभिन्न संस्थाओं के बीच अवरोध एवं संतुलन (check and balance) की व्यवस्था के खिलाफ उसके भीतर बेसब्री किस हद तक पहुंच गई है। इसका संकेत सत्ताधारी जमात की ये मंशा है कि चूंकि उसने चुनाव जीता है, इसलिए उसकी जो भी मर्जी हो, उसमें किसी को अड़चन नहीं डालनी चाहिए।
मगर केंद्र में सत्ताधारी समूह यही सुविधा राज्यों में जनादेश पाए दलों और उनकी सरकारों को नहीं देना चाहता। ध्यान दीजिए यहां मुद्दा क्या है?
तमिलनाडु की निर्वाचित सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था के तहत विधान सभा से विधेयक पारित कराए। राज्यपाल ने पुनर्विचार से लिए लौटाने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, तो कुछ विधेयकों को विधान सभा ने दोबारा मंजूरी दी। संविधान के अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि राज्यपाल ऐसे विधेयक को “यथाशीघ्र” मंजूरी देंगे। अब अगर वर्षों- वर्षों तक वह “यथाशीघ्र” आए ही नहीं, और संबंधित राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की पनाह में जाए, तो कोर्ट का क्या दायित्व होगा?
यहां ये भी गौरतलब है कि किसी अन्य राज्य से संबंधित ठीक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया हो, और किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल उसकी अनदेखी कर रहे हों, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कैसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा उचित होगी? याद करना चाहिए कि पंजाब के ठीक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट राज्य के व्यवहार को अनुचित ठहरा दिया था। लेकिन इससे तमिलनाडु के राज्यपाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि परंपरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सारे देश पर लागू होता है।
तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय का यही संदर्भ है। वैसे इसका दायरा तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। लगभग हर गैर-भाजपा शासित राज्य में राज्यपालों की भूमिका वहां के प्रशासन में रुकावट डालने और टकराव खड़ा वाली एजेंसी की हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के ऐसे व्यवहार पर अपनी नापसंदगी जताई है। अनुमान लगाया जा सकता है कि उससे केंद्र में सत्ताधारी जमात तिलमिला-सा गया है, जिसकी अभिव्यक्ति उप-राष्ट्रपति के आक्रामक रुख में हुई है।
लेकिन गैर-भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों का व्यवहार शिकायत का एकमात्र मुद्दा नहीं है। बल्कि जो बड़े मसले हैं, उनकी तुलना में यह एक सामान्य बात मालूम पड़ेगी। बड़े मसले आम और वित्तीय स्वायत्तता से जुड़े हुए हैं।
यह सर्वविदित है कि आरएसएस की विचारधारा में भारतीय राज्य-व्यवस्था की कल्पना एकात्मक शासन के रूप में रही है। इस विचारधारा में बहुलता के सम्मान के बजाय समरसता की बात की जाती रही है। इसलिए फेडरलिज्म और बहु-सांस्कृतिक पहचानों को मान्यता उनकी सहज सोच का हिस्सा नहीं हैं। भारत में भाषाई राज्यों का गठन बहु-सांस्कृतिक मान्यता और बहुलता के सम्मान के सिद्धांत पर हुआ था। जबकि आरएसएस/ भाजपा की सोच उसके ठीक उलट है। ऐसे में संविधान में निहित राज्यों की स्वायत्तता के प्रावधानों से उसका टकराव स्वाभाविक परिघटना है।
मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ऐसे टकराव कई बिंदुओं पर उभरे हैं। राजनीतिक कारणों से ये गैर-भाजपा शासित- खास कर दक्षिणी राज्यों के साथ ज्यादा जाहिर हुए हैं। मगर महाराष्ट्र जैसे राज्य में भी हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य करने के सवाल पर शुरू हुआ विवाद संकेत है कि टकराव का दायरा कहीं बड़ा है। हिंदी भाषी राज्यों के मामले में सांस्कृतिक-भाषाई टकराव की गुंजाइश कम है। मगर वित्तीय स्वायत्तता के हरण का मुद्दा देर-सबेर वहां भी सुलगेगा, ये आशंका मौजूद है।
यह फौरी विडंबना भर है कि दक्षिणी राज्यों ने भी अभी वित्तीय स्वायत्तता का सवाल नहीं उठाया है। मगर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था ने राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को बेहद संकुचित कर दिया है। इसकी वजह से वे स्वतंत्र रूप से कोई विकास या कल्याण कार्य शुरू करने की स्थिति में नहीं रह गए हैँ। अब इसकी चुभन राज्यों को महसूस होने लगी है। फिलहाल, नव-उदारवादी विचारधारा का प्रभाव पूरे राजनीतिक दायरे में इतना गहरा है कि ऐसे सवाल किसी पार्टी की प्राथमिकता नहीं हैं। मगर यह स्थिति हमेशा रहेगी, यह सोचना यथार्थवादी नहीं होगा।
फिलहाल, दक्षिणी राज्यों ने कई शिकायतें जताई हैं। उनमें ये मुद्दे उभर कर सामने आए हैः
- 2026 में लोकसभा सीटों का संभावित परिसीमन
- नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूले को अनिवार्य करना (यानी हिंदी को पढ़ाई को हर राज्य में अनिवार्य करना।)
- भाषा का मसला फिलहाल तमिलनाडु में गरमाया हुआ है
- नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट)
- और, राज्यपालों का व्यवहार
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन के सवाल पर जो बैठक बुलाई, उसमें चार दक्षिणी राज्यों में सत्ताधारी दलों (डीएमके, कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट) के अलावा पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, ओड़िसा में प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने भी भाग लिया।
उसके बाद एक अन्य महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्टालिन ने राज्यों की स्वायत्तता के क्षरण का आकलन करने और उन्हें वापस पाने के उपाय सुझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में समिति बनाने का एलान किया है। समिति को वैसे तो 2028 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट देनी है, लेकिन उससे जनवरी 2026 तक अंतरिम रिपोर्ट देने को कहा गया है। उसकी कार्यसूची में 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने का मुद्दा भी है। तमिलनाडु सरकार चाहती है कि शिक्षा को फिर से राज्य सूची में लाया जाए।
अंतरिम रिपोर्ट के लिए दिया गया वक्त महत्त्वपूर्ण है। अप्रैल-मई में तमिलनाडु में विधान सभा चुनाव होंगे। पिछले कुछ महीनों की सक्रियता से साफ है कि डीएमके अगले विधान सभा चुनाव में राज्य की स्वायत्तता को प्रमुख मुद्दा बनाएगी। संभावना है कि जोसेफ समिति की अंतरिम रिपोर्ट उसमें उसका सहायक बनेगी।
तमिलनाडु की पहल के साथ कम-से-कम दक्षिणी राज्यों की पूरी सहानुभूति है। इस रूप में स्टालिन की पहल का संदर्भ बड़ा है। यह उचित ही होगा कि इसे देश में बहुलता एवं विभिन्न सांस्कृतिक पहचानों के अनादर और राज्यों की स्वायत्तता के कथित हनन के खिलाफ मोर्चाबंदी के रूप में देखा जाए। राज्यपाल के व्यवहार संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इस मोर्चाबंदी को आगे बढ़ा रहे दलों ने अपनी नैतिक जीत के रूप में देखा। उप-राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया की एक पृष्ठभूमि यह भी है।
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं)






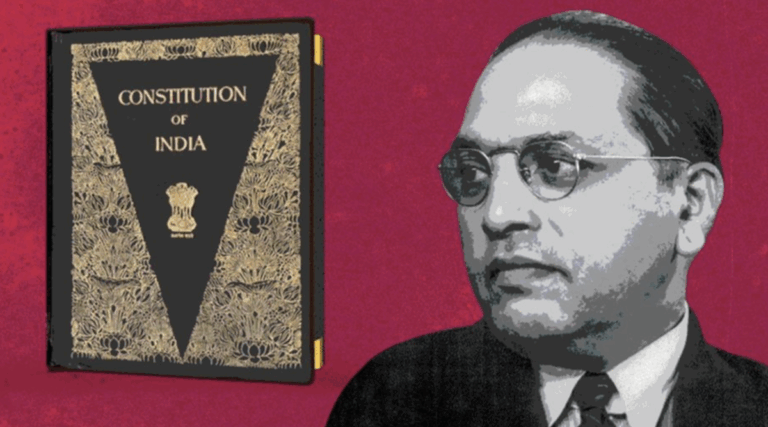





+ There are no comments
Add yours