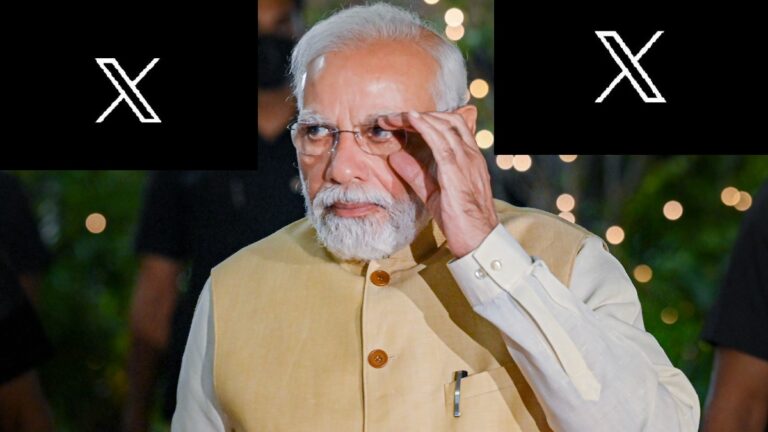भारत में लोकतंत्र का चुनाव परिणाम बताता है कि चुनाव के माध्यम से ‘चुनावी तानाशाही’ को पराजित किया जा सकता है। ‘चुनावी लोकतंत्र’ की दृष्टि से यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं होती है और न है। इसका जितना बखान किया जाये कम ही है। बखान करते समय यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव के माध्यम से ‘चुनावी तानाशाही’ को निर्णायक रूप से पराजित किया जा सकता है। ‘कारण’ के रहते ‘कार्य’ यानी परिणाम के फिर से उपस्थित हो जाने की संभावना या आशंका के घटित होने की संभावना या आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।
‘चुनावी तानाशाही’ का कारण चुनाव है। तो क्या ‘चुनावी तानाशाही’ के डर से चुनाव को ही ना-मंजूर कर दिया जाना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र की समस्त संभावना चुनाव के माध्यम से ही सुनिश्चित होती है। इसलिए चुनाव महत्त्वपूर्ण है। मुश्किल यह है कि चुनाव के रहते ‘चुनावी तानाशाही’ की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है! तो फिर रास्ता क्या बचता है? रास्ता बचता है चुनाव प्रक्रिया को दुरुस्त करना। चुनाव प्रक्रिया दुरुस्त रहे तो ‘चुनावी तानाशाही’ की आशंका समाप्त नहीं भी तो बहुत कम जरूर हो जाती है।
भारत में चुनाव सुधार की मांग लंबे समय से की जा रही है। चुनाव की प्रक्रिया को दुरुस्त किये जाने के लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की स्थापना 1999 में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद के अध्यापकों के एक समूह ने की। इसकी पहल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उम्मीदवारों के लिए अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि का हलफनामा के माध्यम से जरूरी हो गया है। चुनावी फंड (Electoral Bonds) के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में एक पक्ष एडीआर भी था।
गैर-चुनावी संस्थाओं, कम्युनिष्ट पार्टी और अदालत चुनाव सुधार के प्रावधानों के लिए कोशिश करती रहती है। बड़ी कही जानेवाली राजनीतिक पार्टी की इस प्रक्रिया में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखती है। सहकारिता का जज्बा लोकतंत्र के लिए बहुत मूल्यवान होता है। सहकारिता के जज्बा के अभाव में लोकतंत्र निर्जीव हो जाता है। सहकारिता के जज्बा का मतलब होता है अपनी भलाई सुनिश्चित करने के लिए दूसरों की भलाई करना, भलाई के लिए तत्पर रहना।
चुनाव सुधार के कानूनी पहल के लिए एडीआर जैसे संगठन अपना काम करते रहते हैं। हर संगठन की अपनी सीमा होती है, अपना कार्य-क्षेत्र और कौशल होता है। सामान्य लक्ष्य को हासिल करने के लिए बाकी काम अन्य संगठन की सक्रियता जरूरी होती है। एक संदर्भ पर उदाहरण के लिए विचार किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों के हलफनामा में आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक पृष्ठभूमि का उल्लेख होता है। मुख्य धारा की मीडिया में उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की विशिष्ट चर्चा शायद ही कभी होती है। सामान्य परिचर्चा में अधिक-से-अधिक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, प्रतिशत आदि का सामान्य विश्लेषण होता है। उम्मीदवार भी प्रतिपक्षी उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि की चर्चा नहीं करते हैं, अधिक-से-अधिक भ्रष्टाचार के मुद्दों की चर्चा करके आगे बढ़ जाते हैं। एक तरह की मनोवैज्ञानिक मिलीभगत बन गई लगती है।
भारत के लोकतंत्र की संवैधानिक संरचना में व्यापक सुधार की जरूरत की गंभीरता को अविलंब विमर्श के केंद्र में लाया जाना चाहिए। यह दलीय-निष्ठा पर आघात किये बिना भी मानना चाहिए कि दल की अंदरूनी राजनीतिक गतिविधि, खासकर दल के भीतर चुनाव के मामले में तानाशाही का रुख और रवैया रखनेवाला दल या नेता, अपने संवैधानिक आचरण में कभी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है। जिस किसी दल की अंदरूनी राजनीतिक गतिविधि में तानाशाही का रुख और रवैया दिखे, लोकतंत्र को पसंद करनेवालों को उससे अपनी दूरी अविलंब तय कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं करने का मतलब लोकतंत्र को ‘चुनावी तानाशाही’ खतरे की चपेट में पड़ने से रोकने में लापरवाही बरतना है।
ईवीएम (Electronic Voting Machines) को लेकर बार-बार विवाद उठता रहता है। बार-बार संदेह व्यक्त किया जाता है। चुनाव नतीजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े व्यंग्यात्मक लहजा में पूछा, ‘ईवीएम मर गया कि जिंदा है!’ कभी चाल-चरित्र-चेहरा पर इतरानेवाली भारतीय जनता पार्टी में चिढ़ाने-चिल्लाने-चौंकाने की प्रवृत्ति घर कर गई है। यह दुखद है। अभी दुनिया के जाने-माने व्यक्ति एलन मस्क ने भी अमेरिकी चुनाव के प्रसंग में ईवीएम (EVM) पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने भी इसे ‘ब्लैक-बॉक्स कहा है।
अखिलेश यादव समेत विपक्षी गठबंधन (इंडिया अलायंस) के सभी नेता अपना संदेह व्यक्त कर चुके हैं। एक मात्र पार्टी भाजपा है जिसे ईवीएम पर आज कोई संदेह नहीं है। हालांकि पहले तो इतना संदेह था कि चुनाव विशेषज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के नेता जेवीएल (Guntupalli Venkata Lakshmi Narasimha Rao) Democracy at Risk लिखकर अपना संदेह व्यक्त किया था। लेकिन वह सब गये जमाने की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम पर अपने से भी ज्यादा विश्वास है। ईवीएम को लेकर नागरिक समाज पहले से ही सवाल उठाता रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। लेकिन संदेह का वातावरण समाप्त नहीं हो सका है। अभी सही वक्त है, इस संदेह को दूर किया जाना चाहिए।
जीवन में इसलिए, लोकतंत्र में भी विश्वास का बहुत महत्व होता है। चुनाव प्रक्रिया पर बार-बार संदेह होना लोकतंत्र के हित में नहीं है। कारण यह कि लोकतंत्र जीवन की बुनियाद रचता है। सहयोग, सहमेल, सहकार, सह-अस्तित्व जितने भी मानव-मूल्य हैं, सकारात्मक भाव हैं उनकी बुनियाद में विश्वास ही प्राण का संचार करता है। लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसके मूल में विश्वास विन्यस्त रहता है। लोकतंत्र ही वह व्यवस्था है जहां विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति होती है। इसलिए स्वतंत्रता का सर्वाधिक बोध लोकतंत्र में होता है। विश्वास का अभाव या कहें संदेह का प्रभाव, जीवन को इसलिए, लोकतंत्र को भी तहस-नहस कर देता है।
रक्तपातहीन परिवर्तन की सर्वाधिक संभावना से संपन्न रहने के कारण लोकतंत्र महत्त्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया में विश्वासहीनता कितनी घातक हो सकती है, इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं है। जिस तरह से शहर के लोगों में समाज के सक्रिय रहने पर संदेह होता है, उसी तरह से कुछ संपन्न लोगों के मन में लोकतंत्र की उपादेयता के प्रति भी कोई खास आग्रह नहीं रहता है। बल्कि कहा जाये तो हिकारत का ही भाव रहता है। प्रासंगिक रूप से पहले की तुलना में इस प्रवृत्ति में सुधार हुआ है। जिन्हें लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार से ‘कल्याण’ की उम्मीद रहती है, वे गरीब लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जी-जान लगा देते हैं। हिंसा को कभी वैध नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान दिया जा सकता है कि कुछ खास इलाकों में लोग कई बार जायज तो कई बार नाजायज कारणों से भी जी-जान लगा देते हैं। क्योंकि उन्हें लोकतंत्र से ‘कल्याण’ की उम्मीद रहती है।
जीवनयापन की जरूरतों के तहत लोक के मन में बसी ‘कल्याण योजना’ की आकांक्षा को ‘लाभार्थी योजना’ के लालच में बदलने की कोशिश की कामयाबी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा में भारतीय जनता पार्टी कहां से कहां पहुंच गई! बहुत भरोसा था, ‘पचकेजिया मोटरी’ के बदले वोट देकर मतदाताओं के ‘पुण्य बटोर’ में लग जाने पर, ‘श्रीमान’ को! सामान्य नेता होता तो लोकतांत्रिक वोटर से ‘पचकेजिया मोटरी’ के बदले वोट मांगने के पहले उसकी आत्मा कांप जाती। लेकिन ‘श्रीमान’ तो ‘परमात्मा के अवतार’ और अ-जैविक व्यक्तित्व हैं, उनके मामले में नैतिकता का कोई प्रसंग नहीं होता है। परमात्मा के अवतार की आत्मा नैतिकता के किसी सवाल पर कभी नहीं कांपी, वे तो दूसरे की आत्मा को ‘प्रवर्तनास्त्र’ से प्रकंपित करते रहे हैं! नतीजा सामने है।
भारत के मतदाताओं ने साबित कर दिया है कि वह लोकतंत्र का सौदा नहीं कर सकता है। रखो अपनी ‘पचकेजिया मोटरी’ अपने पास! हजारों साल से पूजित हमारे भगवान को हमारे विरुद्ध नहीं खड़ा किया जा सकता है, चाहे बना लो जितना भी भव्य-दिव्य-विराट मंदिर। सामान्य जन का जीवन अतिरेकी विराटता के पूजन से नहीं, लघुता के समवाय से चलता है। पता नहीं सौ-साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस संस्कृति की बात कर रहा था! सबसे भयानक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत के लोगों की मौलिक वृत्तियों के साथ छल करने का कोई प्रकरण नहीं छोड़ा गया। चुनाव परिणाम देखने के बाद, भारतीय जनता पार्टी का अपने पक्ष में ‘स्थाई बहुमत’ का जुगाड़ कर लेने का भ्रम और संभावना में कुछ-न-कुछ टूट तो जरूर हुई होगी। राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ उपचार में लगा है, यह जरूरी भी है और स्वाभाविक भी।
भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत सारे लोगों ने आहूति दी है। याद किया जा सकता है किसान आंदोलन पर हुए अत्याचार की घटनाओं को। किसानों की मांगों पर कोई सकारात्मक रुख और रवैया सरकार ने नहीं अपनाया। बहुत सारे किसानों ने आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई। अभी एक तरफ परेशान किसान अपनी मांग को लेकर फिर से कमर कस रहे हैं तो दूसरी तरफ अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए 16 जून 2022 को घोषित अग्निपथ योजना, जिसके तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को ‘अग्निवीर’ नाम दिया गया है।
कहना न होगा कि सामान्य रूप से सेना के अधिकारियों के पद पर नियुक्त होनेवालों और ‘अग्निवीर’ बननेवालों की समाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में अंतर होता है। क्या अंतर! यह कहने की जरूरत है क्या? तूफान तो यहां भी खड़ा होगा। अभी ‘राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा’(NEET) के पेपरलीक को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वह अपनी जगह, पेपरलीक का पहले से चला आ रहा मामला अपनी जगह। किस मामले में कौन सी सकारात्मक कार्रवाई हुई है?
देश के युवाओं की हालत के बारे में अलग से कुछ कहने कि जरूरत है क्या? पिछले दिनों तो नागरिक जीवन के संदर्भ में किये गये हर सवाल को सरकार टेढ़ी नजर से देखती थी, हर आवाज देश-द्रोही करार दी जाती रही है। अभी चुनाव के बाद आई सरकार का रुख और रवैया क्या होता है, देखना होगा। बहुत मुश्किल से ‘चुनावी तानाशाही’ के दौर से भारत का लोकतंत्र बच निकला है। इस वक्त नागरिक जमात के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र की रक्षा में दी गई आहूतियों को याद करे और भविष्य में ‘चुनावी तानाशाही’ के खतरे से बचाव के लिए चुनाव सुधार के विभिन्न जरूरी पक्षों पर विचार करे और उसे व्यापक प्रचार-प्रसार में लाया जाये। 2024 के आम चुनाव में ‘चुनावी तानाशाही’ को आघात तो लगा है, लेकिन संजीवनी बूटी की तलाश जारी है। कब ‘चुनावी तानाशाही’ का खतरा इस या उस ओर से उठ खड़ा हो जाये, कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए कहने की जरूरत नहीं है कि ‘चुनावी तानाशाही’ से बचाव के लिए जो भी किया जाना जरूरी हो, अविलंब किया जाना चाहिए।
दलबदल कानून को अधिक सार्थक और प्रभावी बनाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। ‘आया राम, गया राम’ की राजनीतिक खुराफात को रोकने के दलबदल संबंधी कानून के परिप्रेक्ष्य को समझते हुए इसकी व्यापक समीक्षा की जरूरत है। सरकार की स्थिरता के लिए दलबदल संबंधी कानून की अहमियत है। लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता है कि दलबदल कानून से राजनीतिक दल के सदस्यों की आंतरिक स्वतंत्रता कम हुई है और राजनीतिक दलों में अंदरूनी तानाशाही को बढ़ावा भी मिला है। एक सामान्य और स्वस्थ लोकतांत्रिक परिवेश में माना जा सकता है कि दलबदल विरोधी कानून स्वतंत्रता को बाधित नहीं करता है, यह जरूरी भी है। लेकिन इसके अन्य असर की समीक्षा की ही जानी चाहिए।
यह ठीक है कि स्वतंत्रता के नाम पर मनमानेपन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मनमानेपन के डर से स्वतंत्रता की बलि भी नहीं ली जा सकती है। चुनाव के माध्यम से मतदाताओं की संप्रभुता जन-प्रतिनिधियों को शर्त के साथ अंतरित होती हैं। शर्तें संविधान से तय होती हैं। जन-प्रतिनिधियों के पास मतदाता से प्राप्त संप्रभुता को अपनी ‘अन्य प्रेरित इच्छा’ के अनुसार किसी को भी अंतरित करने का अधिकार जन-प्रतिनिधियों को नहीं होना चाहिए। इसे कानूनी तरीके से रोके जाने का उपाय किया जाना चाहिए। ध्यान रहे, उन उपायों में राजनीतिक दलों की अंदरूनी राजनीति में दलीय तानाशाही को बढ़ावा देनेवाला तत्व नहीं होना चाहिए।
दलबदल कानून दलों के विभाजन को नहीं, दलों के विलय को मान्यता देता है। दलबदल के पहले सदस्यों या समूह को अपने दलबदल संबंधी निर्णय के कारणों का उल्लेख अपने निर्वाचित होने का प्रमाण-पत्र जारी करनेवाले प्राधिकार के पास हलफनामा के रूप में जमा करने को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस हलफनामा को चुनाव आयोग के वेबसाइट पर मतदाताओं की जानकारी और टिप्पणी के लिए समय-सीमा के उल्लेख के साथ डालना चाहिए। आनन-फानन में किये जानेवाले दलबदल को रोकने पर विचार किया जाना चाहिए।
चुनाव आयोग किसी चुनाव में उम्मीदवारी के लिए दायर किये जानेवाले नामांकन पत्र में शिक्षा, वित्तीय स्थिति, आपराधिक मामलों के साथ-साथ उनके दलबदल का ‘संपूर्ण विवरण’ देना भी जरूरी किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए कई उपाय किये जा सकते हैं। उसी सदन की सदस्यता के निरर्हता के सवाल को उसी सदन के बहुमत से निर्वाचित कोई प्राधिकरण निरपेक्ष और स्वतंत्र रूप से हल कर सकता है या नहीं; इस पर गहरे संदेह का वातावरण बन गया है, खासकर महाराष्ट्र प्रकरण के बाद।
राजनीति विनियमन अधिनियम (Politics Regulation Act) जैसी किसी संवैधानिक व्यवस्था की मांग पर भी नागरिक समाज सोच सकता है। दोहराव की चिंता किये बिना बार-बार कहने की जरूरत है कि अंदरूनी राजनीतिक गतिविधि, खासकर दल के भीतर के चुनाव के मामले में तानाशाही का रुख और रवैया रखनेवाला दल या नेता अपने संवैधानिक आचरण में कभी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है। चाहे जैसे भी ‘चुनावी तानाशाही’ के खतरे को रोकने और ‘चुनावी लोकतंत्र’ को स्वस्थ बनाये रखने के लिए जो उपाय किया जा सकता है, अवश्य किया जाना चाहिए। यह ठीक है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है, जो कभी फेल न करे! व्यवस्था के फेल होने के डर के कारण सभ्यता और सभ्य समाज ने नई-नई व्यवस्था बनाने का काम छोड़ा तो नहीं है न!
विश्वास किया जाना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र के लिये दी गई आहुतियों को याद रखने से 2024 के आम चुनाव के परिणाम से लोकतंत्र के लिए वैचारिक संघर्ष के विभिन्न आयाम स्वतः सामने आयेंगे।
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)