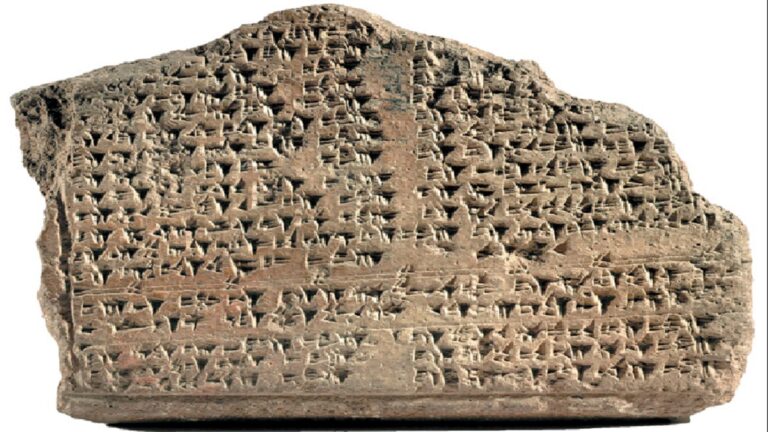इस बात से आज कौन इनकार कर सकता है कि इससे पहले भारत इतना धार्मिक नहीं हुआ था। इतनी असमानता भी कभी नहीं थी। समाज में इतना विभाजन भी कभी नहीं था। संसदीय राजनीति में इस कदर बहुमत का राज नहीं था। और, संसदीय राजनीति से बाहर रहने वाले संगठन और संस्थानों का देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर, चुनाव की प्रक्रिया और छोटी से छोटी नीतियों के निर्माण पर इतनी पकड़ कभी नहीं थी।
इतना बड़ा प्रधानमंत्री का पद नहीं था जिसकी कार्रवाई, व्यवहार से लेकर निर्णय की क्षमता इस कदर अभिव्यक्त हुआ हो जिसमें संविधानिक व्यवस्था अपना अर्थ खो दिया है।
शोर इतना बढ़ चुका है कि जिसमें आप सिर्फ शोर करने वाले को तो सुन सकते हैं लेकिन आप इसके शिकार लोगों की आवाज का नहीं सुन सकते। यह निश्चित ही क्लासिकी संदर्भों में ईश्वर की आवाज नहीं है। यह ईश्वर के पद पर बैठे लोगों की वे चीखें हैं जो मंदिरों से लेकर बाजारों तक काबिज हैं। बाजार की हर पहुंच के साथ इनका धर्म आपके घरों में पहुंच रहा है और घरों का एक कोना ही सही, कब्जा जरूर करता गया है।
जैसे ही आप धर्म का मुद्दा सामने रखिये, बौद्धिक समाज इसका एक एक रेशा खोल कर रखना शुरू करेगा और यह भी बतायेगा कि यह निहायत ही निजी आस्था का हिस्सा है। वह संविधान खोलकर दिखाएगा जिसमें इस निजी आस्था के आधार पर भारत की सेक्युलर व्यवस्था को पेश करेगा। बहस को और आगे बढ़ाने पर यह धर्म के अफीम होने और न होने की ओर पहुंच जाएगा।
एक दूसरी धारा इसे भारतीय संस्कृति की परम्परा से जोड़ते हुए धर्म को यूरोपीय आस्था से खुद को अलग करने की ओर ले जाएगा। धर्म के इस उभार के पीछे की राजनीति और उसके संदर्भ को इतिहास के उस सुदूर हिस्से की ओर ले जाएंगे जिसमें जनता पलते-बढ़ते आ रही है। लेकिन, उस मुख्य और आधुनिक संदर्भों के बारे में बात करने से लगातार कतराता रहेगा जिससे यह पालित और पोषित हो रहा है।
इन संदर्भों का आधुनिक परिप्रेक्ष्य इस उभार को फासीवाद की उस परिभाषा तक ले जाएगा जो यूरोप के आधुनिक राष्ट्र-राज्यों के चरित्र में समाहित होता गया। भाजपा के नेतृत्व में धर्म का जो उभार हुआ है, उसका फासीवाद के चरित्र के साथ मेल बैठता है, इसे नकारने, मुंह मोड़ने से बचने का सबसे आसान रास्ता है, धर्म को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ दिया जाये और इसके अतिवाद के बारे में चिंता व्यक्त कर दिया जाए।
जब रेडिकल कम्युनिस्ट आंदोलन की ओर से पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहे मंदिरों और अन्य धार्मिक संस्थानों की संख्या के बारे रिपोर्ट पेश किया गया था, तब इस तरह के सामान्यीकरण को अतिवाद कहा गया था। वह की वाम गठबंधन की सरकार मध्यवर्ग से लेकर गावों तक इस तरह के धर्म के बढ़ते प्रभाव को नजरअंदाज करने में ही नहीं, कई जगहों और कार्यक्रमों में इसे बढ़ावा भी दे रही थी।
पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन बर्गा के बाद खेती और उद्योग को लेकर उन्हीं नीतियों की ओर बढ़ा गया जो केंद्र में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को लेकर अपनाया गया था।
वामपंथी सरकार की हिस्सेदार पार्टियां आर्थिक नीतियों की चुनौतियों और बढ़ते सामाजिक संकट को लेकर अपने बौद्धिक समुदाय का सहयोग हासिल कर भारत में ‘विकास’ की समस्या को हल करने के एक नये रास्ते का विकल्प दे सकती थी। जल्द ही वाम सरकार का पतन हो गया और राजकीय दमन से रेडिकल कम्युनिस्ट आंदोलन को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद पश्चिम बंगाल धर्म एक ताकत बनकर उभरा और संकटग्रस्त समाज में एक संगठनकर्ता बनने की दिशा में बढ़ गया।
इस संदर्भ में एजाज अहमद, जो वैश्वीकरण को साम्राज्यवादी पूंजीवाद के संदर्भ में देख रहे थे और उसके आक्रामक और कब्जाकारी रुख, धर्म के प्रयोग को एक साथ रख रहे थे। उन्होंने भारतीय संदर्भ को भाजपा के उभार में देखा।
प्रो. मीरा नन्दा ने धार्मिक पुनरूत्थान को बाजार से जोड़ते हुए इसकी तीखी आलोचना को रखा और प्रतिरोध के लिए सांस्कृतिक पक्ष डा. आंबेडकर की नजर से रखा। इनकी व्याख्याओं की निश्चित ही सीमाएं थीं। लेकिन, बौद्धिक समुदाय ने जिस पक्ष को नजरअंदाज किया वह धार्मिक उत्थान को भारतीय राजनीतिक-अर्थशास्त्र से काटकर देखना। दूसरा, धर्म को निरपेक्ष ढंग से देखना भी एक बड़ी समस्या रही। धर्म के उभार को साम्प्रदायिकता की नजर से देखना भी वास्तविक समस्या से मुंह मोड़ लेना था।
गोलबंदी और हिंसा का प्रयोग प्रतिरोध और वर्चस्व के बीच की लड़ाई के रूप में ही अभिव्यक्त होता है। जिस गोलबंदी और हिंसा में राज्य इस या उस तरीके से, या सीधे तौर पर हिस्सेदार होता है, वह निश्चय ही वर्चस्वशाली पक्ष है और दूसरा पक्ष प्रतिरोध की स्थिति में ही होता है। इसमें धर्म का प्रयोग वर्चस्व और प्रतिरोध दोनों ही कारक के रूप में हो सकता है। यदि राज्य की ओर से इसका प्रयोग होता है, तब इसे फासीवाद कहना ही उपयुक्त होता है।
पिछले 30 सालों में अपने देश में राजकीय कोष से धर्म के हिस्से में सीधे धर्म या संस्कृति या परम्परा के नाम पर जिस तरह से खर्च बढ़ता गया है, उसी गति से राज्य की धर्म की तरफदारी की गति भी बढ़ती गई है। सिर्फ सरकारी खर्चे पर ही विशाल मंदिरों का निर्माण नहीं हो रहा है, सरकार के बाहर बैठी संस्थाएं बड़े पैमाने पर इस दिशा में काम कर रही हैं।
यह एतिहासिक तथ्य है कि राजनीतिक-अर्थशास्त्र का संकट हमेशा ही तीर्थ यात्राओं को न सिर्फ बढ़ा देता है, नये नये तीर्थों का निर्माण भी करता है। इसे हम ईस्वी पूर्व की अंतिम सदी के समय में बौद्ध केंद्रों के विकास में देख सकते हैं और फिर ईस्वी बाद के दूसरी से पांचवीं सदी के समय को देख सकते हैं।
यह एक बार फिर 10वीं और 11वीं सदी में उभरकर आया। इसने 1857 के बाद एक आधुनिक बोध के साथ नया रूप लिया और इन्हीं से अपनी ऊर्जा ग्रहण कर भारत में धर्म की ध्वजाएं दंगा, विभाजन और पतन की कई गाथाएं लिखी गईं और जो आज भी जारी हैं।
भारत में विश्व बाजार आज धर्म के बाजार में बदल गया है। संस्कृति और इतिहास के नाम पर राष्ट्रवाद की जिस इबारत को लिखा गया है, उसे सिर्फ भाजपा ने नहीं लिखा है। लेकिन, आज उसका नियंत्रण भाजपा के हाथ में है। धर्म की पुराने कथानक पर आधारित मठों, केंद्रों, संस्थानों आदि का अर्थ अब खो रहा है। अब भाजपा और संघ इन्हें नया अर्थ प्रदान कर रहे हैं।
यह राज्य का वह रूप है जिसके प्रधानमंत्री को धार्मिक अनुष्ठान करने में गर्व अनुभव होता है और मंदिर में देवता के प्राण प्रतिष्ठा को एक ऐतिहासिक राजनीतिक कार्य मानता है। यह एक ऐसी इबारत है जिसे आप धर्म की व्याख्या से नहीं पढ़ सकते।
आज हम जिस भारत में रहे रहे हैं वहां तेजी से हिंदू होने के दावों में तेज बढ़ोत्तरी हुई है। इस दावे में सिर्फ धर्म नहीं है। इसके लिए आधुनिक राष्ट्र-राज्यों के फासीवादी उभार की सैद्धांतिकी के पन्नों को पढ़ना होगा और इससे भी अधिक भारत के राज्य को सारे पूर्वाग्रहों से निकल कर समझना होगा।
(अंजनी कुमार पत्रकार हैं।)