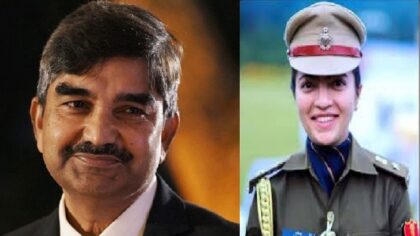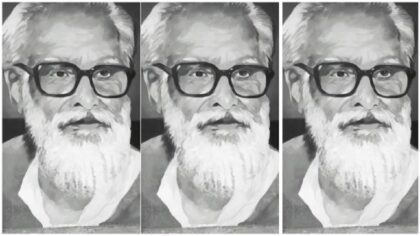भारतीय लोकतंत्र में चुनाव को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। हर लोकतांत्रिक देश में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए विभिन्न प्रकार की चुनाव प्रक्रिया होती है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक वोट-एक मूल्य प्रणाली और कानून निर्माण के लिए संसदीय प्रतिनिधि लोकतांत्रिक तंत्र को चुना।
हाल ही में, परिसीमन प्रक्रिया और इसे लागू करने के उपयुक्त तरीके को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। परिसीमन से जुड़े कई मुद्दे जैसे संघीय ढांचा, समूहों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय असंतुलन आदि इस बड़े प्रश्न से जुड़े हुए हैं।
परिसीमन को समझना
परिसीमन का अर्थ है प्रत्येक राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण। इस प्रक्रिया में चुनावों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी शामिल है।
अंतिम परिसीमन 1976 में हुआ था जब इसे 2026 तक के लिए 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत स्थिर कर दिया गया था।
संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या और उनके क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। यह परिसीमन प्रक्रिया ‘परिसीमन आयोग’ द्वारा की जाती है, जिसे परिसीमन अधिनियम के तहत गठित किया जाता है।
हाल ही में, आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के मुखपत्र ऑर्गनाइजर ने परिसीमन प्रक्रिया और इसके व्यावहारिक प्रभावों, विशेष रूप से देश के दक्षिणी हिस्से में, पर एक लेख प्रकाशित किया। संघ परिवार से जुड़े इस साप्ताहिक ने दक्षिण भारत के विपक्षी दलों की चिंताओं को प्रतिध्वनित किया।
उनका कहना है कि दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में कम जन्म दर के कारण परिसीमन प्रक्रिया लागू होने पर उनके लिए नुकसान की संभावना है।
प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया जनसंख्या के आधार को बदल सकती है और अंततः उन दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटों की संख्या को प्रभावित कर सकती है जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत की।
उन्होंने अपने लेख में इस मुद्दे पर ईस्ट तिमोर, साउथ सूडान और कोसोवो के उदाहरण दिए, जो बढ़ती जनसंख्या के कारण बने देशों की ओर इशारा करते हैं।
विपक्षी दलों ने परिसीमन के विचार का समर्थन करते हुए कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों के कड़े विरोध के कारण पिछले 50 वर्षों से परिसीमन प्रक्रिया स्थिर है। दूसरी ओर, तमिलनाडु विधानसभा ने परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया।
उनका तर्क है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है, इसलिए उन्हें उन राज्यों के कारण परिणाम नहीं भुगतने चाहिए जिन्होंने इसमें सफलता नहीं पाई।
जनसंख्या और वोट के विचार से बहस का विस्तार
लोकतंत्र का प्रश्न केवल एक व्यक्ति-एक वोट तक सीमित नहीं है। यह प्रतिनिधित्व के साधारण सवाल से भी बड़ा है। राजनीतिक विचारकों का मानना है कि परिसीमन अंततः संघवाद के मूल विचार को प्रभावित करेगा, जो राज्य और केंद्र के बीच समान शक्ति के विभाजन का आश्वासन देता है।
हमें इस पूरी प्रक्रिया को संविधान की आकांक्षाओं के अनुरूप समझने की आवश्यकता है, जो पूरी तरह संघीय नहीं है। हमारा संविधान अमेरिकी संविधान के समान नहीं है, जहां राज्यों को केंद्र के साथ समान शक्ति प्राप्त है और शेष शक्तियां राज्यों के हाथों में होती हैं। इसके विपरीत, हमारे संविधान में विविधता की रक्षा के लिए श्रेष्ठ शक्ति केंद्र के हाथों में है।
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम सेल (2024) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। संघवाद संघ के इकाइयों, अर्थात् संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को समाहित करता है। भारतीय संघवाद को विषम के रूप में परिभाषित किया गया है क्योंकि यह केंद्र की ओर झुका हुआ है, जिससे एक मजबूत केंद्रीय सरकार उत्पन्न होती है।”
भारतीय संघवाद की सही व्याख्या यही है। कोर्ट ने आगे कहा, “फिर भी, इसका परिणाम कमजोर राज्य सरकारों के रूप में नहीं निकला है। भारतीय राज्यों को उनके सौंपे गए विधायी अधिकार क्षेत्र में संप्रभुता प्राप्त है।”
इन दो वाक्यों का भारतीय विधायिका की व्यवहारिकता के संदर्भ में कोई बड़ा अर्थ नहीं है क्योंकि किसी भी समय, केंद्र सरकार संशोधनों के माध्यम से राज्यों के कानून बनाने की शक्ति को बदल सकती है और उस विषय को समवर्ती सूची में डाल सकती है।
इसलिए, यह बहस का सही विषय नहीं है कि परिसीमन प्रक्रिया भारतीय राज्य की संघीय संरचना को बाधित करेगी, बल्कि यह वास्तव में ‘केंद्र-केन्द्रित प्रणाली को और उजागर करती है।’
लेकिन कई बार ऐसा पाया गया है कि राज्य अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभाते हैं, जिससे राज्यों के हितों को नुकसान होता है। यदि हम 1947 से भारत के इतिहास पर नजर डालें, तो हम उत्तर भारतीय ब्राह्मणवादी पक्षपाती प्रणाली को पहचान सकते हैं।
हाल ही में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर बहस में, कई आलोचकों ने जोरदार तरीके से अपने तर्क रखे और कहा कि यूसीसी पूरे सामान्य कानून प्रणाली को उत्तर भारतीय ब्राह्मणवादी-पुरुषप्रधान प्रणाली के हित में तय करने का प्रयास करता है, जो कमोबेश सही है।
संभावित समाधान
अमेरिका जैसे संघ में, जहां 1913 के बाद से, विधायिका द्वारा कोई नई सीट नहीं बनाई गई है और जनसंख्या पिछली गिनती के साल से चार गुना बढ़ गई है। उन्होंने आनुपातिकता के तरीके को चुना है, जिसमें सीटों का आवंटन राज्यों के अनुपात के अनुसार किया जाता है। इससे किसी भी राज्य को कोई विशेष लाभ या हानि नहीं होती है।
उदाहरण के लिए, 2020 की जनगणना के आधार पर पुनर्वितरण में 37 राज्यों के लिए सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। टेक्सास ने दो सीटें प्राप्त कीं, पांच अन्य राज्यों ने एक-एक सीट प्राप्त की और सात राज्यों ने एक-एक सीट खो दी (स्रोत: द हिंदू)।
कुछ राजनीतिक वैज्ञानिकों ने स्थानीय शासन आधारित समाधान का सुझाव दिया है, जिसमें उन्होंने स्थानीय पंचायत स्तर की कमजोर शासन प्रणाली की ओर इशारा किया है। विश्लेषण के अनुसार, स्थानीय निकाय सीधे लोगों से जुड़े होते हैं, और इसलिए उन्हें वित्त और जिम्मेदारियों के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए।
स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी, हम अभी भी जनसंख्या की बहस के घेरे में हैं, जिसे प्रणाली में लोगों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, यदि वे वर्तमान स्वरूप में बने रहने के इच्छुक हैं।
(निशांत आनंद कानून के छात्र हैं)