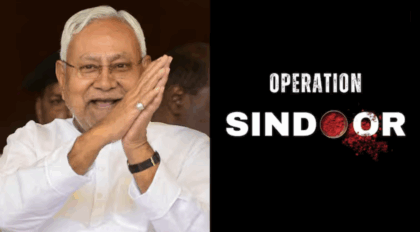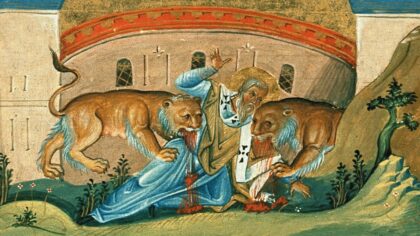एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। अदालत ने अनुच्छेद 201 के तहत समय पर कार्रवाई पर जोर देते हुए विधायी प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी के प्रति चेतावनी दी। इसके साथ ही, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति को उन विधेयकों पर, जिन्हें राज्यपाल असंवैधानिक मानकर उनके विचारार्थ भेजते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेनी चाहिए। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने से अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित विधेयकों के प्रति केंद्र सरकार के दृष्टिकोण में पक्षपात या दुर्भावना की आशंकाओं को कम किया जा सकता है।
राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों की कार्रवाई के लिए समयसीमा तय करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निर्देश दिया कि राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों पर, जो राज्यपालों द्वारा उनके विचारार्थ भेजे जाते हैं, प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर फैसला लेना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि इस अवधि से अधिक देरी होती है, तो उचित कारण दर्ज करना और संबंधित राज्य को सूचित करना आवश्यक होगा।
कोर्ट ने अपने 8 अप्रैल के फैसले को शुक्रवार को सार्वजनिक किया। इसमें तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की कार्रवाई को अवैध और त्रुटिपूर्ण ठहराया गया, क्योंकि ये विधेयक पहले ही राज्य विधानसभा द्वारा पुनर्विचारित किए जा चुके थे।
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई संवैधानिक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन उचित समय के भीतर नहीं करता, तो न्यायालय हस्तक्षेप करने से नहीं हिचकेंगे।”
जहाँ राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करते हैं और राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देते, तो राज्य सरकार को ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध इस न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार होगा। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने पीठ की ओर से लिखते हुए कहा कि अनुच्छेद 201 के तहत, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प हैं—स्वीकृति देना या अस्वीकृति करना।
पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि “अनुच्छेद 201 की एक विशेषता, जिसने वर्षों से केंद्र-राज्य संबंधों में मतभेद उत्पन्न किए हैं, यह है कि इसमें राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति घोषित करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है।”
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि सरकारिया आयोग ने इस मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया था और सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 201 के तहत संदर्भों के शीघ्र निस्तारण के लिए निश्चित समयसीमा अपनाई जानी चाहिए। पुंछी आयोग ने भी अनुच्छेद 201 में समयसीमा जोड़ने का सुझाव दिया था।
सरकारिया आयोग, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर.एस. सरकारिया ने की थी, का गठन 1983 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था। पुंछी आयोग, जिसका नेतृत्व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम.एम. पुंछी ने किया था, 2007 में केंद्र-राज्य संबंधों पर विचार के लिए स्थापित किया गया था।
अनुच्छेद 201 के तहत शक्तियों की व्याख्या करते हुए, पीठ ने कहा, “यद्यपि अनुच्छेद 201 की भाषा राष्ट्रपति के लिए किसी निश्चित समयसीमा का उल्लेख नहीं करती, लेकिन समयसीमा की अनुपस्थिति का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि राष्ट्रपति इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन अनिश्चितकाल तक टाल सकते हैं।”
कोई भी विधेयक, जब तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, कानून नहीं बन सकता। इसलिए, राष्ट्रपति द्वारा संदर्भों का निस्तारण लंबे समय तक न करना जनभावनाओं के विरुद्ध होगा, जो राज्य विधानसभाओं द्वारा विधेयकों के रूप में प्रकट होती हैं।
फैसले में कहा गया, “हम समझते हैं कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत विधेयकों पर विचार करना होता है, और यह कार्य समयबद्धता में बाधित हो सकता है, लेकिन यह तथ्य राष्ट्रपति की निष्क्रियता को उचित नहीं ठहराता।” पीठ ने कहा कि “बिना किसी वैध कारण या आवश्यकता के राष्ट्रपति द्वारा निर्णय में देरी करना संविधान के उस मूल सिद्धांत के विरुद्ध होगा, जिसके अनुसार किसी भी शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता।”
इस संदर्भ में, कोर्ट ने गृह मंत्रालय द्वारा 4 फरवरी 2016 को सभी मंत्रालयों और विभागों को जारी दो कार्यालय ज्ञापनों (OM) का भी उल्लेख किया, जिनमें “राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों के शीघ्र निपटान” के निर्देश थे।
पहले कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा, “यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयकों पर निर्णय के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की गई है, और अत्यावश्यक अध्यादेशों के निपटान के लिए तीन सप्ताह की समयसीमा निर्धारित की गई है।”
फैसले में कहा गया, “इन निर्देशों से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 201 की तात्कालिकता और महत्व को स्वीकारते हुए केंद्र सरकार ने समयसीमा और प्रक्रिया स्पष्ट की है। इन कार्यालय ज्ञापनों का अस्तित्व और स्वीकृति यह दर्शाते हैं कि शीघ्र और समयबद्ध निर्णय लेना अनुच्छेद 201 की भावना और उद्देश्य के अनुरूप है।”
सरकारिया और पुंछी आयोगों की सिफारिशें तथा केंद्र सरकार के दिशानिर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि अनुच्छेद 201 के तहत संदर्भों के निपटान की प्रक्रिया में शीघ्रता आवश्यक है। इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा, “यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि न्यायालय उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जहाँ कोई संवैधानिक प्राधिकारी अपनी जिम्मेदारी को उचित समय में पूरा नहीं कर रहा।”
पीठ ने कहा, “हम उचित समझते हैं कि गृह मंत्रालय द्वारा तय समयसीमा को अपनाया जाए, और राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचारार्थ भेजे गए विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। यदि इस अवधि के बाद विलंब होता है, तो उपयुक्त कारण दर्ज करना और संबंधित राज्य को सूचित करना आवश्यक होगा।”
अदालत ने यह भी कहा कि राज्यों को सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना और उनके सुझावों पर शीघ्र विचार करना चाहिए।
राज्यपाल की तरह, राष्ट्रपति के पास भी पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है, और इसलिए राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी रोकने का फैसला भी स्पष्ट और ठोस कारणों के साथ होना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को किसी भी विधेयक पर पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है, वैसे ही यही मानक राष्ट्रपति पर भी लागू होता है। संविधान में यह नियम स्पष्ट है कि ऐसी असीमित शक्तियाँ किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं हो सकतीं।”
फैसले में कहा गया कि इस अवधि से अधिक देरी होने पर, उचित कारण दर्ज किए जाने चाहिए और संबंधित राज्य को सूचित किया जाना चाहिए। इसके बदले में, राज्यों को विधेयकों पर केंद्र की ओर से उठाए गए किसी भी प्रश्न या सुझाव के प्रति सहयोग करना चाहिए।
न्यायमूर्ति पारदीवाला द्वारा लिखित 414 पृष्ठों के फैसले में कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों से भेजे गए विधेयकों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करना आवश्यक है, क्योंकि राज्य स्तर पर राज्यपालों के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है, जिसके तहत वे विधेयकों को संवैधानिक न्यायालयों के पास उनकी सलाह या राय के लिए भेज सकें।
फैसले में कहा गया, “हमारा मानना है कि यद्यपि अनुच्छेद 143 के तहत किसी विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय को भेजना अनिवार्य नहीं हो सकता, फिर भी राष्ट्रपति को विवेक के उपाय के रूप में, कथित असंवैधानिकता के आधार पर उनके विचारार्थ आरक्षित विधेयकों के संबंध में राय लेनी चाहिए। यह और भी आवश्यक है, क्योंकि राज्य स्तर पर राज्यपालों के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है, जिसके माध्यम से वे विधेयकों को संवैधानिक न्यायालयों को सलाह या राय के लिए भेज सकें।”
यह फैसला तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ दायर एक रिट याचिका पर आधारित था। अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों पर महीनों तक विचार करने के बाद उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने के फैसले को कानूनी रूप से गलत माना।
इस संदर्भ में, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने पड़ोसी द्वीप राष्ट्र श्रीलंका का उदाहरण दिया, जहाँ राष्ट्रपति ने विधेयकों को राय के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजा था। उन्होंने विस्तार से बताया, “यदि राज्यपाल की राय है कि प्रांतीय परिषद द्वारा अधिनियमित कोई कानून असंवैधानिक है, तो वह विधेयक को राष्ट्रपति को भेज सकता है, जो बदले में ऐसे विधेयक की संवैधानिक वैधता पर निर्णय प्राप्त करने के लिए श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करने के लिए बाध्य है। यदि सर्वोच्च न्यायालय कानून को संवैधानिक मानता है, तो राज्यपाल को स्वीकृति देने के लिए बाध्य किया जाता है।”
संवैधानिक न्यायालयों को किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी संवैधानिक वैधता के बारे में सुझाव देने या राय देने से नहीं रोका जा सकता। प्रस्तावित कानून के लिए न्यायिक सोच का उपयोग करने से समय और सार्वजनिक संसाधनों की बचत होती है, क्योंकि इससे महंगी मुकदमेबाजी और देरी से बचा जा सकता है, जो तब होती है जब कोई दोषपूर्ण विधेयक कानून बन जाता है। इसके अलावा, विधायिका को उचित सुधारात्मक उपाय करने के लिए विधेयक की समीक्षा करने का दूसरा अवसर प्राप्त होता है।
हालाँकि, पीठ ने चेतावनी दी कि “उपचार से पहले रोकथाम” के दृष्टिकोण को इस हद तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित करने की प्रक्रिया स्वयं राज्यों की विधायी शक्तियों को विफल करने का साधन बन जाए।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं)