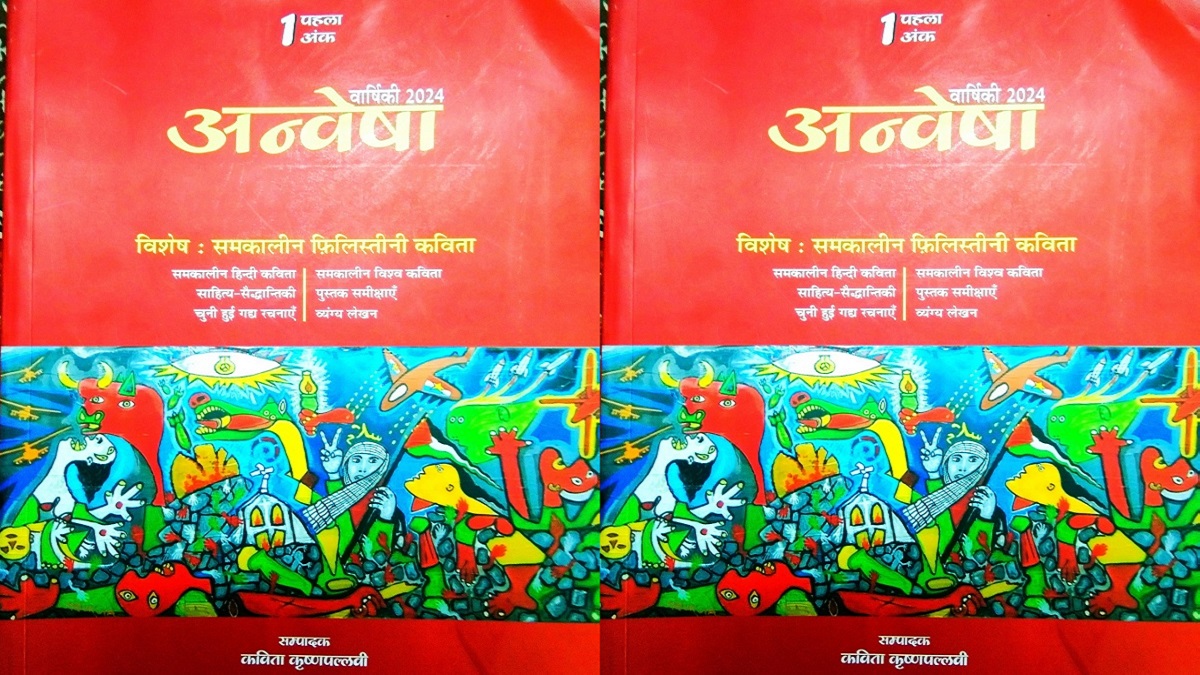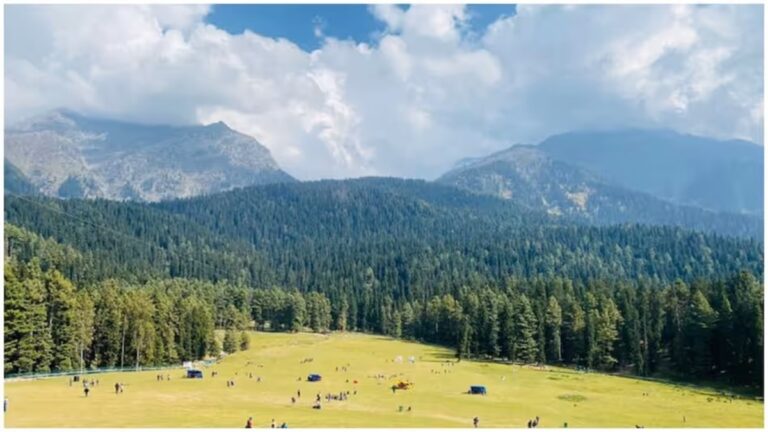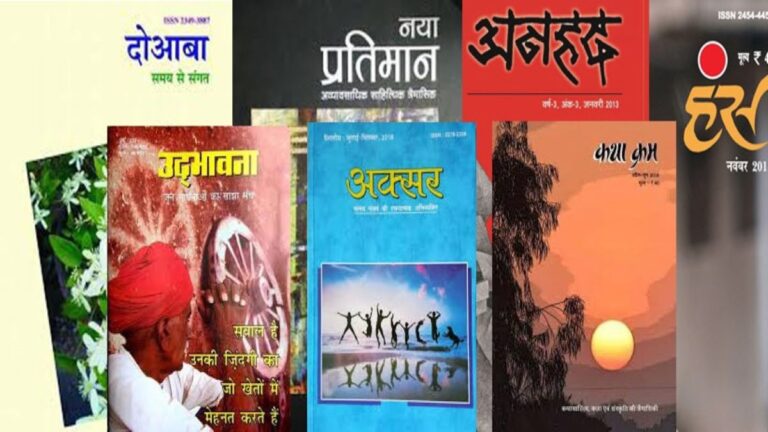अन्वेषा का वार्षिकांक आए हुए कई दिन हो गए। यह प्रवेशांक बहुत भारी-भरकम अंक है। 544 पृष्ठ, आकार भी पुराने जमाने की धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसा। कोई पत्रिका इतने विशाल आकार की हो सकती है, मेरे लिए यह सोचना भी सहज नहीं था। शुरू में उलट-पलट कर दो-चार बार देखा। कुछ पढ़ा, ज्यादा छोड़ा। पहले ही दिन संपादकीय पढ़कर मन बना था कि एक छोटी टिप्पणी लिखूं, लेकिन मामला टलता गया। कुछ अपना दर्द और बाकी दुनिया का दर्द। दर्द बयान करूं या कुछ काम की बात कहूं?
जब मैंने धरती निकाली थी, तो पहला अंक मात्र 48 पृष्ठ का था, यानी इसका एक-बटा-ग्यारह। संकलित सामग्री भी कच्ची-पक्की थी। संपादन का अनुभव और परिपक्वता नहीं थी। अतः इसकी उससे कोई तुलना नहीं हो सकती। वह साढ़े चार दशक पुरानी बात है। यह 2025 का काम है, इसलिए और महत्वपूर्ण है। क्योंकि वह समय संघर्ष, उत्साह और प्रतिबद्धता का समय था। यूं तो वह भी बहुत अच्छा समय नहीं था, लेकिन इस तरह का कॉरपोरेट और आवारा पूंजी का दौर नहीं था। पूंजीवाद का प्रभाव था, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं दिखता था। सांप्रदायिकता और फासीवाद का इतना नंगा नाच नहीं था।
सत्ताएं प्रतिरोध को सिर्फ दबाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं दिखती थीं। विरोध का आंशिक स्वीकरण भी था। हर विरोध को देशद्रोह से नहीं नवाजा जाता था। उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अंग स्वीकार किया जाता था। आज स्थितियां प्रतिकूल हैं। आज ऐसा कोई काम करना आसान नहीं है। फिर भी यह काम हुआ है, अतः सराहनीय और स्वागतयोग्य है।
यह प्रतिकूल समय में एक जरूरी रचनात्मक हस्तक्षेप है।
प्रस्तुत अंक में चौदह खंड हैं। पहला खंड समकालीन फिलीस्तीनी कविताओं पर केंद्रित है। यह बेहद सामयिक, सार्थक और महत्वपूर्ण कर्म है। पत्रिका में संपादकीय की पहली पंक्ति है: “फिलीस्तीन अजेय प्रतिरोध का दूसरा नाम है।” इस खंड में चौबीस कवियों की कविताएं संकलित हैं। ज्यादातर युवा हैं और युद्ध की अमानवीय, भयावह स्थितियों में कविताएं लिखकर अपनी भावनाओं और प्रतिरोध का इजहार कर रहे हैं।
पत्रिका: अन्वेषा
संपादक: कविता कृष्णपल्लवी
संपर्क: दून बास्केट, लोअर नेहरू ग्राम, सिद्ध विहार, रायपुर, देहरादून – 248001
मूल्य: रुपये 500/-
इतना बड़ा काम है। पूरे काम पर बात करना कठिन है। तो समकालीन हिंदी कविता खंड पर की गई संपादकीय टिप्पणी को लेकर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं। इसमें जो बात सर्वाधिक प्रभावित करती है, वह है समकालीन वाम-जनवादी कविताओं के चयन को लेकर जिस साफगोई और ईमानदारी से यह स्वीकार किया गया है कि “सामान्य तौर पर हमने जनवादी, प्रगतिशील और वाम धारा की कविताओं का एक चयन प्रस्तुत करने की कोशिश की है, हालांकि हम इस तथ्य से वाकिफ हैं कि कुछ कवियों की कुछ कविताओं में समग्रता में जनपक्षधरता के बावजूद ‘आइडेंटिटी पॉलिटिक्स’, सबाल्टर्न इतिहास दृष्टि और लोकवाद (पॉपुलिज्म) जैसे विचारधारात्मक विचलनों की छाप या छाया मौजूद है। इसका मूल कारण यह है कि हिंदी के जनपक्षधर कवियों की प्रतिबद्धता भी ज्यादातर मामलों में भावनात्मक और अनुभवप्रसूत हुआ करती है। दर्शन, विचारधारा और राजनीति का गहन-गंभीर अध्ययन बहुत कम कवि करते हैं।”
यह बेहद महत्वपूर्ण अवलोकन है। निष्कर्षात्मक रूप से यह भी बता दिया गया कि “प्रगतिशील हिंदी कविता के वैचारिक पक्ष की दुर्बलता अपने आप में एक गंभीर समस्या है और यह अक्सर सौंदर्यात्मक-रूपगत दुर्बलता को भी जन्म देती है।”
समकालीन वाम हिंदी कविता का पूरा परिदृश्य यहां स्वाभाविक रूप से स्पष्ट हो जाता है। उसकी कमजोरी हमारी समझ में आ जाती है। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि इन बातों की कसौटी पर इन कवियों और कविताओं को कसा जाए। प्रत्येक कवि और उसकी कविताओं पर इस दृष्टि से सहज, सकारात्मक, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक बात की जाए ताकि कवि स्वयं भी यह जान सके कि वह किस खांचे में फिट है, कितने पानी में है। अपनी सृजनात्मकता को और अधिक निखारने के लिए वह क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए। यह रचनात्मक दृष्टिकोण है।
विडंबना यह है कि हिंदी का कवि अपनी आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं करता। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और लोकवाद तथा विचलन (अवसरवाद) उसे बेहद लुभाते हैं। वह अपने आप पर मुग्ध रहता है। अपवाद जरूर होंगे। तो ऐसे में क्या इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होने वाले हर युवा, प्रौढ़, वरिष्ठ कवि का यह दायित्व नहीं बनता कि वह स्वयं अपनी कविताओं और अपने व्यक्तित्व को उक्त संपादकीय कसौटी पर कसे? (वरिष्ठों का रोग अधिक संक्रामक होता है।) तभी इस संकलन में शामिल होने की वास्तविक सार्थकता है, बजाय यह बताने के कि मैं इसमें शामिल हूं और मेरी इतनी कविताएं शामिल हैं। आत्मालोचना बहुत महत्वपूर्ण है। असल परिष्कार इसी तरह घटित होता है।
इस अंक में भारतीय उपमहाद्वीप की अन्य भाषाओं-उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, असमिया, मिया, रोहिंग्या, डोगरी, नेपाली, श्रीलंकाई-की कविताएं शामिल की गई हैं। एशिया महाद्वीप के अन्य देशों-चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, इंडोनेशिया-के कवियों को भी शामिल किया गया है। तुर्की, अफगानिस्तान, ईरान एवं कुछ अन्य अरब देशों के कवियों की कविताएं भी हैं। अमेरिकी और अफ्रीकी कविताएं भी शामिल हैं।
कविताओं के अतिरिक्त वैचारिक आलेख, कहानियां, व्यंग्य और समीक्षाएं भी ली गई हैं। यह सब संकलित, संयोजित और संपादित करने में जो समय और श्रम लगा होगा, वह अवश्य ही इस महाग्रंथ को सार्थकता प्रदान करता है। यह एक व्यक्ति के साथ संगठन का काम है, टीम वर्क भी है। काम बड़ा है, महत्वपूर्ण है, सार्थक है। कमियां हर काम में होती हैं, लेकिन मेरा अभीष्ट उद्देश्य की स्पष्टता और पूर्ति तक ही सीमित है, जिस पर यह कार्य निश्चित तौर पर खरा उतरता है।
फिलहाल इतना ही।
(शैलेन्द्र चौहान लेखक-साहित्यकार हैं और जयपुर में रहते हैं)