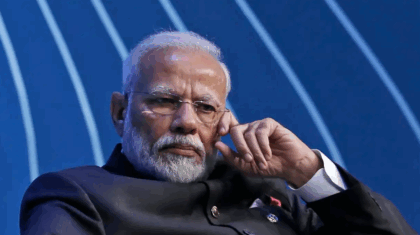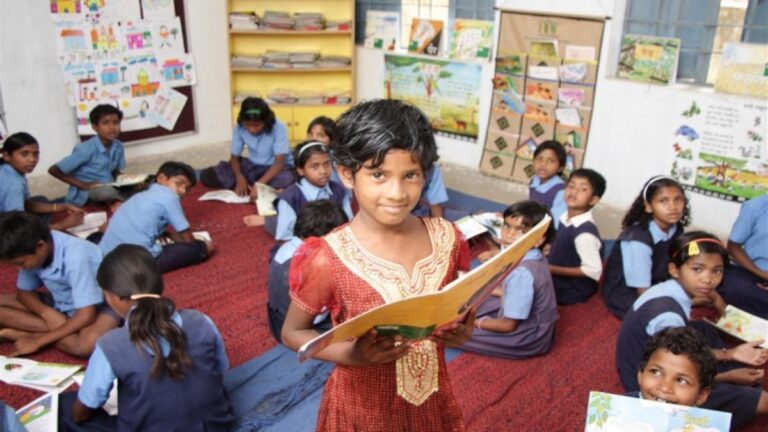(दक्षिण कोरिया के ‘राष्ट्रीय चैंपियन्स’ के विपरीत, अडानी ग्रुप उन क्षेत्रों में मौजूद है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं। नई दिल्ली की मदद के बिना वह दुनिया के बाजार में बहुत कम बेच सकता है।)
अहम सवाल यह है कि पूंजीवाद के विकास में सरकार-व्यापार गठजोड़ के बारे में हम क्या जानते हैं? समकालीन भारत किस तरह से उसकी तरह या उससे भिन्न है?
जब कोई उन्नत पूंजीवाद के बारे में सोचता है, तो यह माना जाता है कि कंपनियां उत्पाद नवाचार (product innovation) और/या लागत में कमी के आधार पर बढ़ती या गिरती हैं।
क्या विभिन्न फर्म ऐसा कोई उत्पाद लेकर आए हैं जो लाखों उपभोक्ताओं की कल्पना पर खरा उतरता हो जैसे एक एप्पल ( Apple) कंप्यूटर या फिर एक आईफोन, या फिर क्या उन्होंने एक नए उत्पादन तकनीक या बेहतर मशीनों (उदाहरण के लिए, एक नया रोबोटीकृत परिवहन उपकरण या औद्योगिक मशीनरी बनाने वाली उत्पादन प्रणाली) के माध्यम से हजारों अन्य फर्मों को आकर्षित किया है?
इसे एक विशिष्ट पाठ्यपुस्तक विवरण कहा जा सकता है, उन्नत पूंजीवाद की यथार्थवादी तस्वीर नहीं। और वह आंशिक रूप से ही सच होगा। उन्नत पूंजीवाद पूरी तरह से, जिसे एडम स्मिथ ने बाजार का अदृश्य हाथ कहा है, द्वारा संचालित नहीं है। व्यापार-सरकार संबंध या लिंक मौजूद हैं – चर्चित रूप से, रक्षा उद्योगों में – लेकिन औद्योगिक नीति द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में भी।
पिछले साल, जो बाईडेन ने यूएस के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए सब्सिडी की घोषणा की और उन फर्मों के लिए भी जो पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर उत्पाद, जैसे इलेक्ट्रिक कार, आदि बनाती हैं। लेकिन सरकार-व्यापार की मिलीभगत, भले ही वह उन्नत पूंजीवाद में मौजूद हो, व्यापक या अनियंत्रित नहीं होती है। वह अक्सर पकड़ में आ जाती है, और दंडित भी की जाती है। इसके अलावा, नीतियां उद्योग-विशिष्ट होती हैं, न कि फर्म- या परिवार-विशिष्ट।
इसके विपरीत, प्रारंभिक पूंजीवाद एक बहुत ही अलग किस्म का ‘पशु’ है। पूंजीवाद के उदय के साथ भ्रष्टाचार ऐतिहासिक रूप से मौजूद रहा है। 1865-1900 के दौर पर विचार करें, जब एक मुख्य रूप से ग्रामीण अमेरिका अपने पहले बड़े पूंजीवादी परिवर्तन से गुजरा था।
अपनी साहित्यिक दृष्टि और बौद्धिक दूरदर्शिता से, मार्क ट्वेन ने सबसे पहले नए आर्थिक मोड़ के सार का पता लगाया था। 1873 में, उन्होंने इसे “गिल्डेड एज” कहा। विभिन्न स्तरों पर सरकारों के साथ तरह-तरह के सौदे करके, अमेरिका के पहले अरबपति- द कार्नेगीज, रॉकफेलर्स, वेंडरबिल्ट्स, मॉर्गन्स – दृश्य पर उभरे।अपनी रेलवे लाइनें बिछाने के लिए, रेल बैरन जे गोल्ड ने घोषणा की, “मैं चार राज्यों की विधानसभाएं चाहता था… इसलिए मैंने उन्हें अपने पैसे से बनाया’। बस ऐसे कथित लुटेरों के बैरन ने सरकारों और विधायिकाओं को “खरीदा”।
राष्ट्रपति थिओडोर रूजवेल्ट (1901-09) के समय में एक सफाई अभियान (cleaning up) शुरू हुआ और आंशिक रूप से परिणाम दिखने लगा। 1860 में, पश्चिमी यूरोप की तुलना में, अमेरिका सुस्त था। 1910 तक अमेरिका, एक सदी से अधिक समय से औद्योगिक नेता- ब्रिटेन- को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया था।
सड़ांध और गतिशीलता की एक साथ उपस्थिति मतलब ट्वेन का “गिल्डेड एज” एक मुहावरे के रूप में प्रचलित हो गया है, और तब से इसका उपयोग होता रहा है। नवीनतम संस्करण चीन का ‘गिल्डेड एज’ (2021) यूएन यूएन आंग (मिशिगन विश्वविद्यालय, ऐनअबोर) द्वारा लिखित, व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तक है।
वह चार प्रकार के भ्रष्टाचार चिन्हित करती हैं: (1) “छोटी-मोटी चोरी” (सड़क छाप नौकरशाहों द्वारा जबरन वसूली और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग); (2) “भव्य चोरी” (राजनीतिक अभिजात वर्ग द्वारा भारी मात्रा में सार्वजनिक धन का गबन); (3) “गतिशील धन”(नौकरशाही बाधाओं से बचने के लिए छोटी रिश्वत); (4) “प्रवेश धन” या “एक्सेस मनी”(व्यापारियों द्वारा राजनेताओं और नौकरशाहों को अनुबंधों और परियोजनाओं के लिए प्रदान किए जाने वाले लाभ और मुआवजा, जो समग्र निवेश दर बढ़ाते हैं और जिससे आर्थिक विकास होता है)।
उनका तर्क है कि भ्रष्टाचार के पहले तीन रूपों ने राष्ट्रीय आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन चीन तेजी से चौथे प्रकार के भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहा है, जो निवेश-बढ़ाता है और विकास-संवर्धन भी, इस प्रक्रिया में वह राजनीति के सभी स्तरों पर कम्युनिस्ट पार्टी के अभिजात वर्ग को लाभ पहुँचाता है। 1995-2015 के दौरान, चीन का निवेश/जीडीपी अनुपात कभी भी 40 प्रतिशत से नीचे नहीं गिरा, और वार्षिक विकास दर विरले ही 9 प्रतिशत से कम रही।
यह तर्क देना आकर्षक लग सकता है कि अडानी-बीजेपी सरकार के संबंध चौथी श्रेणी में आते हैं। उन्होंने जो कुछ भी विशेष रूप से भाजपा के लिए किया हो/ योगदान दिया हो, आखिरकार अडानी का निवेश बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, अनाज भंडारण, सीमेंट में भारी मात्रा में है। सिद्धांत रूप में इन्हें विकास वर्धक कहा जा सकता है।
लेकिन यह तुलना बहुत सरलीकृत होगी। मोदी के भारत के लिए सबसे दिलचस्प समानांतर मॉडल चीन नहीं, बल्कि दक्षिण कोरिया है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पहले चार “एशियन टाइगर्स” में से एक है। 1960 के दशक की शुरआत में, दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति आय मोटे तौर पर भारत के समान थी।
विश्व बैंक के अनुसार दिसंबर 2021 में दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति आय $34,758 थी, जबकि भारत की केवल $2,100 थी।(संयोग से, प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में, चीन, $10,262 पर, अभी भी उच्च आय देश नहीं है।)
दक्षिण कोरिया के साथ तुलना अधिक उपयुक्त है, इसकी ‘गिल्डेड एज’, जो 1960 के दशक के मध्य में शुरू हुई, की एक खास विशेषता थी। चीन के विपरीत, यह एक सुनहरा युग था जिसमें सैमसंग, हुंडई, एलजी, हंजिन जैसे “राष्ट्रीय चैंपियन” थे। तथाकथित “शेबोल्स”, जो मूल रूप से रूप से परिवार-वर्चस्व वाले बहु-क्षेत्रीय (muti-sector) व्यवसाय समूह होते हैं।वे दक्षिण कोरियाई अर्थव्यवस्था की भांति सरकारी संरक्षण में फले-फूले।
लेकिन उनके उदय के साथ भ्रष्टाचार पैदा हुआ। क्रोनी कैपिटलिज्म (2002) में, डेविड कांग(दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय), दक्षिण कोरियाई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख विद्वान लिखते हैं: “घोटाले कोरियाई राजनीतिक इतिहास का एक आवर्ती विषय हैं, और राजनीतिक प्रभाव के लिए धन का आदान-प्रदान … एक खुला रहस्य … रहा है।
जो लोग जेल में समय बिता चुके हैं या निर्वासित हो चुके हैं, उनमें पूर्व राष्ट्रपति हैं …राष्ट्रपति के स्टाफ सदस्य, … सैन्य अधिकारी, राजनेता, नौकरशाह, बैंकर, व्यवसायी और कर संग्रहकर्ता… विकास इतना शानदार था कि इसकी वास्तविकता, भ्रष्टाचार को छुपा लिया जा सका …”
कोरियाई ‘शेबोल्स’ और अडाणी समूह के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि ‘शेबोल्स’ अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार-उन्मुख थे। सरकारी संरक्षण के बावजूद, सैमसंग, हुंडई, एलजी सभी व्यापार योग्य क्षेत्रों में रहे हैं। वे सेल फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमिकंडक्टर्स और ऑटो का उत्पादन करते है, और उन्होंने विश्व उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा ने उनके व्यवसायों पर एक अनुशासनात्मक निगरानी रखी है, जिससे बड़ी क्षमताएँ उत्पन्न हुईं हैं।
अडाणी समूह ज्यादातर गैर-व्यापार योग्य क्षेत्रों में है। बंदरगाहों, हवाई अड्डों, अनाजगोदामों, बिजली उत्पादन जिनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारोबार नहीं है। वे सरकार-संरक्षित और घरेलू रूप से केंद्रित, दोनों हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जो दक्षता लाभ आता है यहां नहीं हैं।
अडानी समूह सैमसंग नहीं है; दिल्ली की मदद के बिना यह दुनिया के बाजार में बहुत कम बेच सकता है। न ही वह भारत की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के साथ तुलना कर सकता है। दक्षिण कोरिया की तुलना में अडाणी-सरकार का गठजोड़ बहुत अलग किस्म की राष्ट्रीय चैंपियंस रणनीति है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बिना बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए इसका निहितार्थ उतना फायदेमंद नहीं हो सकता।
दरअसल, यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय उपकरण के माध्यम से अन्ततोगत्वा संभव हुआ कि अडाणी समूह पर पहली अनुशासनात्मक निगरानी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार अडाणी समूह के कारोबार प्रथाओं को दंडित कर रहे हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है।
(आशुतोष वार्ष्णेय ब्राउन विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के सोल गोल्डमैन प्रोफेसर हैं। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कुमुदनिपति , साभार- द इंडियन एक्सप्रेस, 13 फरवरी )