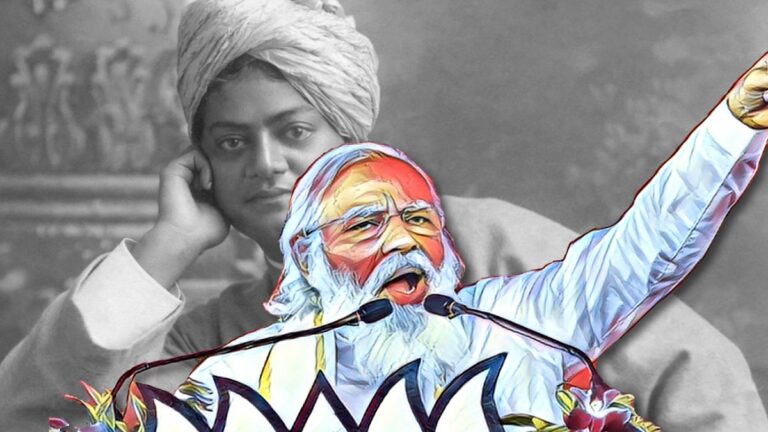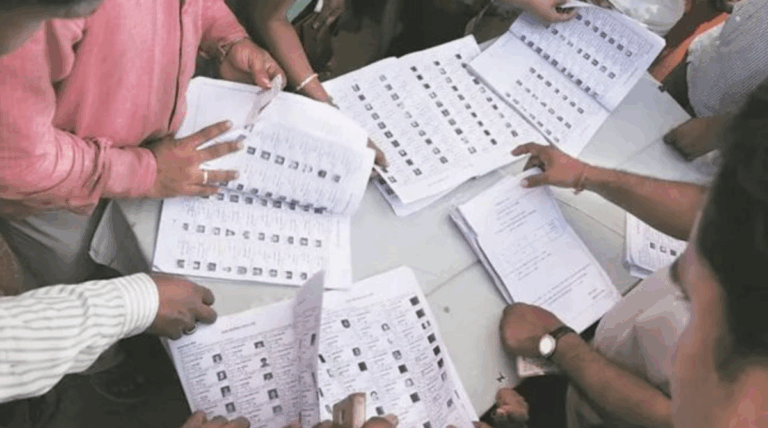प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा से लौटते ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उसके बहुचर्चित आईटी सेल को कुछ ऐसे अभियान में जुटना पड़ा हैः
• भाजपा की समर्थक जमातों में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को कामयाब बताने के लिए प्रचार सामग्रियां सर्कुलेट करने की जोरदार मुहिम छेड़ी गई है।
• इसी के तहत एक फोटोशॉप्ड स्टिकर तैयार कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश हुई है, जिसमें अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मास्ट हेड के नीचे मोटे अक्षरों में छपी हेडलाइन में मोदी को धरती की आखिरी उम्मीद बताया गया है। उसी स्टिकर पर एक दूसरी लाइन में यह कहा गया कि ये महान नेता अमेरिका को अनुग्रहीत करने वहां आया।
• एक वीडियो वायरल किया गया, जिसमें कई धनी देशों का नाम लेते हुए यह कहा गया है कि भले हमारे पास उनके जैसी ताकत या संपत्ति ना हो, लेकिन “हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री है।”
• संभवतः भाजपा नेतृत्व को यह महसूस हुआ कि आईटी सेल के ऐसे अभियानों से बहुत से तर्क क्षमता से शून्य लोगों को तो अपेक्षित संदेश पहुंच जाएगा, लेकिन मीडिया के दायरे में रहने वाले बहुत से लोग शायद ऐसे संदेशों की हकीकत जल्द समझ जाएंगे। इसलिए पार्टी ने विदेश यात्रा से वापसी पर प्रधानमंत्री के स्वागत में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया।
• इस रंगारंग कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री को ‘विश्व प्रिय नरेंद्र मोदी’ के रूप में पेश किया गया। यह संदेश भेजने की कोशिश की गई कि मोदी ने विश्व मंचों पर भारत की ऐसी मजबूत भूमिका बना दी है, जैसा उसके पहले कभी नहीं हुई।
अब गौर करने की बात यह है कि सत्ताधारी जमात को आखिर ऐसे तौर-तरीके अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उसकी वजह का अनुमान लगाया जा सकता है। अतीत में बतौर प्रधानमंत्री जब कभी नरेंद्र मोदी अमेरिका या दूसरे विकसित देशों में गए, वहीं की जमीन से सत्ताधारी जमात ने यह प्रभाव पैदा करने की कोशिश की कि कैसे वहां मोदी की तूती बोल रही है। सत्ताधारी पार्टी होने के नाते अपने धन-बल, मेनस्ट्रीम मीडिया पर लगभग अपने पूरे नियंत्रण, और एनआरआई समुदाय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए तब ऐसा करना उसके लिए आसान था। मगर अब एक तो अमेरिका में बदल चुकी राजनीतिक सूरत और दूसरे कोरोना महामारी के जारी कहर के कारण वहां से यह करना संभव नहीं हुआ।
उलटे जिस मीडिया ने अपनी पहचान सत्ताधारी दल और प्रधानमंत्री के ‘भक्त’ के रूप में बनाई हुई है, खुद उसकी कई रिपोर्टों से वो सच्चाई भारतीय जनता तक पहुंच गई, जो गढ़े गए नैरेटिव की ताकत पर टिकी सत्ता को अपने लिए हानिकारक महसूस हुई होगी। मसलन, इन वीडियो क्लिप्स को याद करें:
• हिंदी के सर्वाधिक देखे जाने वाली टीवी चैनल की एंकर-रिपोर्टर ने ना जाने क्यूं और किस समझ के तहत कैमरे के सामने अखबार के पन्नों को पलटते हुए ये बता दिया कि मोदी की अमेरिका यात्रा की खबर वहां के अखबारों में नहीं छापी गई है।
• उसी चैनल पर मोदी के स्वागत में आए लोगों के बीच संभवतः धार्मिक संगीत में एक साज बजा रहे व्यक्ति से जब पूछा गया कि वो वहां क्यों आए, तो उन्होंने साफ कह दिया कि वे पेशेवर म्यूजिशियन हैं, जिसे वहां “लाया गया” है।
• उसी रिपोर्टर ने वॉक्स पॉप लेने की कोशिश में सड़क पर कहीं जा रहे एक ब्लैक अमेरिकी नागरिक से यह पूछ लिया कि वे मोदी के बारे में क्या सोचते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के शासनकाल में भारत में गरीबी बढ़ी है।
• इसके अलावा प्रधानमंत्री का स्वागत उनकी कथित विश्व छवि हैसियत के अनुरूप ना होना और यात्रा के दौरान जो बाइडेन प्रशासन का बढ़-चढ़ कर उत्साह ना दिखाना हर पल जाहिर होता रहा।
• जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री के साथ साझा प्रेस कांफ्रेंस नहीं की।
• साझा प्रेस कांफ्रेंस उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने की, जिन्होंने लोकतंत्र को लेकर कुछ ऐसी बातें कह दीं, जिनकी व्याख्या विपक्ष और भारतीय मीडिया के एक हिस्से ने मोदी राज की आलोचना के रूप में की।
• जो बाइडेन ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान महात्मा गांधी और धार्मिक सहनशीलता के बारे में उनके संदेश का जिक्र किया। इसकी व्याख्या भी यह कहते हुए की गई कि बाइडेन प्रशासन ने भारत के मौजूदा हाल पर टिप्पणी करते हुए उसके प्रति अपनी नापसंदगी जताई है।
• संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान खाली कुर्सियों और उस दौरान एक बार भी करतल ध्वनि ना होने की बात को लेकर कांग्रेस के नेताओं तक ने ट्वीट किए।
तो कहा जा सकता है कि मोदी की ताजा अमेरिका यात्रा ने उनके विरोधियों को इस बात की पर्याप्त सामग्रियां उपलब्ध कराई हैं, जिनके आधार पर वो कह सकें कि मोदी का जो तिलिस्म बीते वर्षों के दौरान बनाया गया था, वह अब तार-तार हो गया है। तो इस नैरेटिव को संभालने की चुनौती भाजपा और उसके प्रचार तंत्र ने स्वीकार की है, जिसका प्रमाण ‘विश्व प्रिय नरेंद्र मोदी’ की कथा है, जिसे फैलाने में पूरी ताकत झोंक दी गई है।
बहरहाल, प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा की उपलब्धियां क्या कहीं, इस सवाल पर दोनों तरफ की कहानियों से अलग तथ्यों के आधार पर गौर करने की जरूरत है। इसलिए कि भारत की दुनिया में कैसी छवि बन रही है और उसकी वजह क्या है, इसका संबंध सिर्फ मोदी या भाजपा सरकार से नहीं है। बल्कि उसका संबंध भारत के असली सूरत-ए-हाल और भविष्य से है। विदेश जाने वाले प्रधानमंत्री असल में वहां भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहां उन्हें जैसी भी प्रतिक्रिया मिलती है, उसका संबंध असल में वहां भारत को लेकर कायम धारणा से होता है।
बेशक इस बार नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का केंद्रीय पहलू क्वैड्रैंगुलर सिक्योरिटी डायलॉग (क्वैड) की आमने-आमने हुई पहली शिखर बैठक थी। दरअसल, अगर इस बैठक का कार्यक्रम ना होता, तो शायद मोदी के अभी अमेरिका जाने का कार्यक्रम नहीं बनता। क्वैड अमेरिकी भू-राजनीतिक रणनीति में इस समय इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि चीन से “प्रतिस्पर्धा” इस समय उसकी मुख्य चिंता है। कूटनीतिक भाषा में जिसे अमेरिका “प्रतिस्पर्धा” कहता है, उसका असल मतलब चीन को घेरना और उसकी बढ़ती ताकत को नियंत्रित करना है। उसकी राय में इस काम में भारत की भूमिका दो कारणों से महत्त्वपूर्ण है। पहली वजह तो यह है कि भारत में चीन के प्रति दशकों से शत्रुता या होड़ की भावना मौजूद है। इसलिए वह इस काम में स्वाभाविक सहयोगी है। दूसरी वजह यह है कि भारत इस क्षेत्र में चीन के बाद बेशक सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। इसलिए भारत में चाहे जो सरकार हो, या दूसरे क्षेत्रों में भारत की जैसी भी स्थिति हो, अमेरिका की निगाह में क्वैड जैसी गोलबंदी में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका होनी है।
लेकिन चीन से कथित प्रतिस्पर्धा के मामले में बाइडेन प्रशासन की खुद अपनी नीति अस्थिरता और अस्पष्टता की शिकार है। वरना, वह जिस समय क्वैड शिखर सम्मेलन की तैयारी चल रही थी, उसी समय वह (क्वैड में शामिल) ऑस्ट्रेलिया, और ब्रिटेन को लेकर एक अलग त्रिपक्षीय रक्षा करार नहीं करता। ऑकुस (ऑस्ट्रेलिया- यूनाइटेड किंगडम- यूनाइटेड स्टेट्स) नाम से चर्चित इस नए त्रिगुट का भी वही मकसद है, जिसके लिए क्वैड बनाया गया है। त्रिगुट के गठन से अमेरिका के परंपरागत सहयोगी यूरोपीय देशों में जो नाराजगी पैदा हुई, वह सबको मालूम है। बहरहाल, क्वैड के अतिरिक्त त्रिगुट की क्या जरूरत पड़ी, ये सवाल क्वैड में शामिल भारत और जापान को पूछना चाहिए था। जापान चूंकि अमेरिका का क्लाइंट (अधीनस्थ) देश है, इसलिए उससे इसकी उम्मीद रखना व्यर्थ था।
मगर भारत, अगर अभी अपने दावे के मुताबिक स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रश्न जो बाइडेन के सामने रखना चाहिए था। साथ ही अमेरिका में दूसरे मंचों पर भी इसे उठाना चाहिए था। लेकिन ऐसा उन्होंने किया, इसका कोई संकेत नहीं है। उलटे अमेरिका को खुश करने की अत्यधिक बेसब्री में उनकी सरकार ने उनके अमेरिका रवाना होने से ठीक पहले भारत में उत्पादित कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर लगी रोक हटा दी। अमेरिकी मीडिया में उसके पहले ये खबर आ चुकी थी कि इसके लिए अमेरिका दबाव डाल रहा है। अमेरिकी नजरिए में कोरोना वैक्सीन को तीसरी दुनिया के देशों तक पहुंचना निर्यात चीन की कथित वैक्सीन कूटनीति का मुकाबला करने के लिए जरूरी है। जब अमेरिका ने अपने देशवासियों को बूस्टर के रूप में वैक्सीन का तीसरा डोज लगाने का फैसला कर लिया है, तब उसके लिए अधिक संख्या में वैक्सीन बाहर भेजना संभव नहीं है। ऐसे में भारत से ऐसा करने को कहा गया, जहां खुद कोरोना टीकाकरण की दर अभी भी काफी नीचे है।
बहरहाल, भारत का मेनस्ट्रीम मीडिया ऐसी खबरों को सिरे से दबा देता है। इसके बावजूद आज के इंटरनेट के दौर में देश के जागरूक तबकों तक ऐसी खबरें पहुंच ही जाती हैं। तो मोदी की ताजा अमेरिका यात्रा से यह सवाल उठा है कि आखिर क्वैड में शामिल होने की भारत क्या कीमत चुका रहा है? और क्या जो कीमत चुकाई जा रही है, उससे अधिक या कम-से-कम उसके बराबर उसे लाभ होने की संभावना है? आलोचकों ने यह प्रश्न भी उठाया है कि कहीं भारत इस क्रम में अपने लिए नुकसान तो मोल नहीं ले रहा है, क्योंकि चीन हमारा निकट पड़ोसी है, जबकि अमेरिका का सीधा चीन से युद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। बल्कि तमाम संकेत इस बात के हैं कि बाइडेन प्रशासन की प्राथमिकता चीन से अपने टकराव को एक हद से ज्यादा ना बढ़ाने की है, ताकि किसी अनहोनी घटना से बात हाथ से ना निकल जाए।
जाहिर है, तमाम फ्रेंडली मीडिया के बावजूद भारतीय जनमत के एक बड़े हिस्से में ऐसे सवाल अभी मंडरा रहे हैं। जहां तक द्विपक्षीय संबंधों में ज्यादा अहमियत ना मिलने या संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के दौरान फीके माहौल की मिलने की बात है, तो उसकी वजहों को समझने की जरूरत है। कुछ वर्ष पहले जब मोदी विदेश यात्रा पर जाते थे, तो उन्हें वहां उस भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लिया जाता था, जिसकी अर्थव्यवस्था में अपार संभावनाएं देखी जाती थीं। तब मोदी अगर वहां कोई प्रगतिशील या अपनी विचारधारा से हटकर बात कहते थे, तो संदेश यह जाता था कि वैश्विक तकाजों के कारण उनके नजरिए में उदारता आ रही है, जो आर्थिक शक्ति के रूप में भारत के उदय के लिए आवश्यक है। इसलिए जब वे डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी (जनसंख्या) और डेवलपमेंट का जुमला बोलते थे, तो उसे गंभीरता से लिया जाता था।
लेकिन आज भारत को किस निगाह से देखा जा रहा है, ये बात बहुचर्चित वॉक्स पॉप में उस ब्लैक अमेरिकी नागरिक ने आजतक चैनल के सामने दो टूक कह दी। एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में भारत की कहानी (जो इंडिया स्टोरी के रूप में मशहूर हुई थी) बनने की शुरुआत 1991 में अपनाई गई आर्थिक नीतियों के साथ हुई थी। साल 2000 आते-आते पश्चिम के कॉरपोरेट मीडिया ने ये धारणा दुनिया में बना दी कि 21वीं सदी में विश्व अर्थव्यवस्था का इंजन जो देश बनेंगे, उनमें भारत प्रमुख है। जब इस सदी के आरंभिक वर्षों में भारत ने जीडीपी की उच्च वृद्धि दर हासिल की, तो ये धारणा और पक्की हो गई। तब भारत पश्चिमी पूंजीवाद को निवेश और बड़े बाजार की संभावनाओं से परिपूर्ण नजर आता था। उस स्थिति में चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, या मनमोहन सिंह, या नरेंद्र मोदी, उन्हें अपने ‘गुड बुक’ में रखना तमाम विश्व शक्तियों की प्राथमिकता बन गई थी। 2014 में मोदी जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्हें विदेशों में जो उत्साह भरी प्रतिक्रिया मिली, उसके पीछे भारत की ये संभावनाएं ही थीं। यह अकारण नहीं था कि 2015 में उनके आमंत्रण पर सीधे बराक ओबामा 26 जनवरी की परेड में मुख्य अथिति बनने को तैयार हो गए।
लेकिन आज भारत की छवि क्या है? गिर चुकी अर्थव्यवस्था, बढ़ती गरीबी, सिकुड़ता मध्य वर्ग (यानी उपभोक्ता वर्ग) आदि भारत की ऐसी पहचान बन रही है कि अमेरिका की सड़कों पर घूमते एक व्यक्ति को मोदी के नाम से यही बात याद आती है। आज भारत की चर्चा होने पर कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन और अस्पताल सुविधाओं के अभाव में सड़कों पर दम तोड़ते लोगों की कहानियां सुनाई जाने लगती हैं। भारत की चर्चा आने पर दुनिया के कारोबारियों को एक ऐसी सरकार की याद आती है, जिसने खुद अपने कदमों से अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाई है, जिसकी नीतियों में अस्थिरता है, और जिसने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जैसी नीति से अपने को मुक्त व्यापार की संस्कृति से काट लिया है। ऐसा भारत आखिर खुद में कैसे दूसरों की पहले जैसी दिलचस्पी कायम रख सकता है?
विश्व मंचों और कूटनीति में कई देश उस स्थिति में अपनी हैसियत से अधिक महत्त्व प्राप्त किए होते हैं, अगर वे दुनिया में किसी उदात्त विचार या वैचारिक आंदोलन का नेतृत्व/ प्रतिनिधित्व कर रहे हों। मसलन, अपनी आजादी के बाद भारत भले आर्थिक या सैनिक रूप से कोई ताकत नहीं था, लेकिन उपनिवेशवाद विरोधी अपने तेवर के कारण उसे बड़ी ताकतें भी नजरअंदाज नहीं कर पाती थीं। जवाहर लाल नेहरू को उनके वामपंथी रूझान के बावजूद अमेरिका जैसे देश में भी अत्यधिक महत्त्व मिलता था, तो उसकी वजह थी कि वे उन विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिन पर तब एक नई दुनिया बनने का सपना देखा जा रहा था। वे अथवा मार्शल टीटो या गमाल अब्देल नासिर या सुकार्णो एशिया और अफ्रीका के नए आजाद हुए देशों की नव-कल्पना के प्रतिनिधि रूप में विश्व मंच पर उपस्थित होते थे। बेशक एक अप्रतिम विचारक राजनेता की उनकी अपनी छवि का भी इसमें योगदान होता था।
आखिर मोदी किस विचार के प्रतिनिधि के रूप में विश्व मंच पर उपस्थिति होते हैं? उनकी सरकार ने विदेश नीति में टकराव और एक धुरी से जुड़ने को प्राथमिकता दी है। फिर स्थिति यह है कि जो उनके अपने मूलभूत विचार हैं और जिन पर देश में निर्बाध अमल किया जा रहा है, विश्व मंचों पर वे उसे काटती हुई बातें कहते सुने जाते हैं। मसलन, इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने विवेकशीलता और प्रगतिशील विचारों की वकालत की। मगर खाली कुर्सियां संभवतः यह संदेश दे रही थीं कि भारतीय लोकतंत्र ने 2014 से जो मोड़ लिया है, और 2019 से कश्मीर, एंटी-सीएए प्रोटेस्ट, और किसान आंदोलन के सिलसिले में सरकार का जो रुख रहा है, वह दुनिया की निगाहों से छिपा नहीं है। आखिर जिन गांधी की चर्चा उनकी इस यात्रा के दौरान हुई, उनका संभवतः सबसे बड़ा संदेश कथनी और करनी में समानता की तलाश का ही था। गांधी ने कहा था कि उनका जीवन ही दुनिया को उनका संदेश है। उस गांधी की रोशनी में आज के भारत की छवि दुनिया जब देखती है, तो उसे क्या अहसास होता है, इसकी झलक इस बार की अमेरिका यात्रा में हमें देखने को मिली है।
तो यह उचित ही है कि भाजपा-संघ ने उस तिलिस्म को बचाने की मुहिम छेड़ी है, जिसकी बदौलत वे सत्ता में हैं। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि देश के अंदर ये तिलिस्म टूट गया है। बल्कि हकीकत यह है कि प्रचार अभियान से इसकी चमक अभी कायम रखी जा सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा ने उनके और सत्ताधारी पार्टी को इस बात की झलक जरूर दिखा दी है कि खोखले नैरैटिव का करिश्मा वहीं तक कारगर रहता है, जहां कैप्टिव (कैद) दर्शक वर्ग हो। जहां के लोगों को कई कोणों से चीजों को देखने की सुविधा हो, उन्हें शब्दजाल से भरमाए रखना एक सीमित समय तक ही संभव होता है।
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल दिल्ली में रहते हैं।)