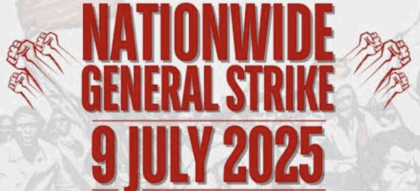मेरे बचपन में नाथपंथी जोगियों का जत्था गांव में आकर हमारे दालान के पास बड़े अब्बा के नीम के पेड़ के नीचे डेरा डाल देता था और हमारी धर्मपरायण अम्मा सोचती थी कि उनके आमद से घर गिरस्ती महफूज रहेगी और शैतानी ताकतें घर से दूर। वे आसपास के गांव में सारंगी की धुन पर गाते हुए रोजी-रोटी इकट्ठा करते थे।
उसका संगीत मधुर तो था ही पर बोल दुनिया के किसी भी तहज़ीब के लिए चुनौती भरा था। मेरी अम्मा इनसे हम बच्चों के लिए दुआ करने के लिए कहती तो जोगियों का दुआ और स्नेह भरा हाथ हमारे सर पर होता था और अम्मा ये मान लेती कि भविष्य में आने वाली बलाओं से उनके बच्चों को निजात मिल गयी।

कैसा अनोखा विश्वास था। हर शाम हमें उनके पास जाकर पूछना पड़ता था कि सबके पास खाना है कि नहीं, इसके बाद ही हमारे घर में रसोईं बनती थी। कभी-कभी हम अगर इनके पास जाने में न नुकुर करते तो अम्मा कहती ना बेटा ना…
‘आह गरीबा कहर खुदाया’ और हम दौड़ पड़ते इनके पास।
कितना बड़ा दिल था अम्मा का कि इतने बड़े जमात से खाना पूछती थी और इसके लिए उन्हें किसी की इजाजत की जरूरत नही पड़ती थी क्योंकि भीतरी अलंग की वो मालकिन थी, जहां अनाज और अन्य खाने-पीने का सामान भरा रहता था। आज हममें इतनी भी संवेदना नहीं बची है कि अपने परिवार या पड़ोसी से भी इस तरह का प्रेम भरा व्यवहार कर सकें।
ज्यादातर जोगी/फकीर बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया समेत पूर्वांचल आसपास के होते थे। अम्मा का घर यानी मेरा ननिहाल कुशीनगर है। अम्मा उन जोगियों से जो लगभग हर साल आते थे, आत्मीय रिश्ता कायम कर चुकी थी और कभी- कभी सदर दरवाजे की ओट से उनसे उनके क्षेत्रों की खेती किसानी और मंहगाई के बारे में पूछती।
उनके चेहरे पर उभरती दुख-सुख की लकीरें साफ-साफ एहसास करा देतीं कि वहां के हालात कैसे हैं।
शायद उन्हें इन जोगियों में नैहर से आने वाले भाई-बाप का अक्स भी दिखता होगा और उनका दुख किसी अपने का दुख। एक और बात कि अम्मा बात करते-करते उनको खाना-पीना बड़े सलीके से पूछती थीं, क्या मजाल की इस दौरान आंचल सर से हट जाए जैसे अम्मा पूरा स्नेह उन पर लुटा देना चाहती हो और उनके सामने उनके नैहर का कोई सदस्य हो।
मेरे वालिद (अब्बा) कभी मोहब्बत से तंज करते कि दुल्हन तुमने इतने प्यार से तो कभी हमें नहीं खिलाया तो अम्मा के चेहरे पर ऐसी विजयी मुस्कुराहट तारी होती जैसे सारे जमाने की दौलत उन्हें मिल गयी हो।
(अम्मा को वालिद साहब सहित सारा परिवार यहां तक कि हमारे रिश्तेदार नातेदार भी दुल्हन से ही सम्बोधित करते थे। ये नाम हमारे दादा हुजूर ने शादी के बाद पहले दिन घर पर आते ही इस्तेमाल किया था सो मृत्यु तक बना रहा। एक बार तो वोटर लिस्ट में भी यही नाम दर्ज हो गया था।)
मांगे सबकी खैर और दुआ फकीरा रहमल्ला की तर्ज़ पर साझी संस्कृति की विरासत का सबसे बड़ा अलमबरदार था ये जत्था और भारत को विश्वगुरु का दर्जा दिलाने की राह का हमराही भी। इनमें जाति और धर्म को लेकर कोई तकरार नहीं था। इनमें बड़ी संख्या मुस्लिम जोगियों की भी थी।
खास बात ये की कई जोगी तो ऐसे थे जो सारंगी की धुन पर राम, राजा भरथरी, मछेन्द्रनाथ और बाबा गोरखनाथ वगैरह पर भजन गाकर भिक्षाटन करते रहते और जहां नमाज़ का वक़्त आया मुसल्ला बिछा कर अल्लाह को याद कर लिया।
अजीब लोग थे और अजीब दौर था। न धर्म बाधक था न जाति और इनमें जो कामन चीज थी वो थी इंसानियत, जिसका आज नितांत अभाव होता जा रहा है। यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ियों को यकीन करना मुश्किल होगा कि कभी हमारे पुरखे इस तरह जिया करते थे।

जाति न पूछो साधु की पूछ सको जो ज्ञान
बदलते वक्त और फिरकापरस्ती की मार से इस संस्कृति पर ग्रहण लगता जा रहा है। आज तो जोगियों का ये जत्था भी नहीं आता है और अब तो अम्मा सरीखे लोग ही बहुत कम होते जा रहे हैं।
आज हम सियासी संकट के ऐसे दौर से गुजर रहे है, जहां ऐसी तमाम विरासतों पर खतरा पैदा हो गया है जिन पर सफर करते हुए भारत आधुनिक हुआ और विविधता और सह-अस्तित्व वाले समाज का निर्माण कर सका। ऐसा साझा समाज दुनिया मे कहीं अन्यत्र सम्भव नहीं हो पाया।
अम्मा अब नहीं रही। वो पढ़ी लिखी सिर्फ नाम भर की थी लेकिन आज सोचता हूं, तो महसूस होता है कि वे आज के ज्ञानियों से कितना समझदार थी जिन्होंने ये मूलतत्व समझ लिया था कि दुखी दिलों पर मरहम लगाना ही इंसान का पावन कर्तव्य है और प्रेम ही शाश्वत सत्य।
धर्म के झमेले सियासतदानों ने गढ़े हैं। आम इंसान तो रोजी-रोटी और प्यार का तलबगार है, नफरत का तो कतई नहीं। अम्मा जैसे लोग अब कहां मिलेंगे जिन्होंने जोगियों के इस मंत्र को गांठ बांध लिया था..
“दुनियां एक झमेला रे बंदे ,न कुछ तेरा न कुछ मेरा”
आइये हम आप सब मिलकर अपनी इस साझी विरासत के पक्ष में खड़े हों और अम्मा की राह पर चलें—–
(डॉ मोहम्मद आरिफ़ इतिहासकार और सामाजिक चिंतक हैं। और आजकल वाराणसी में रहते हैं।)