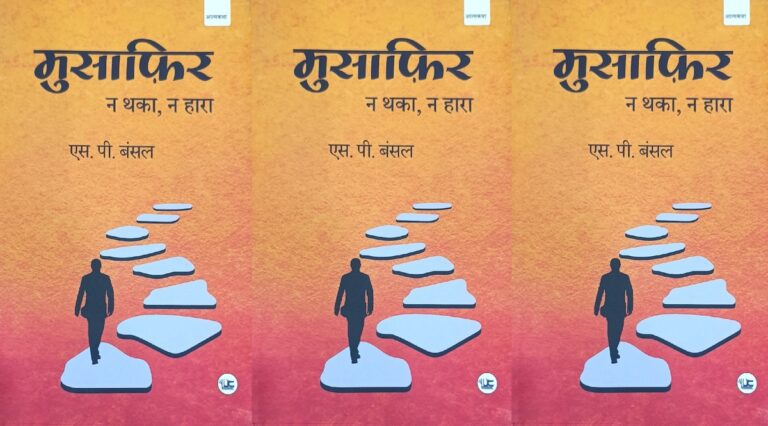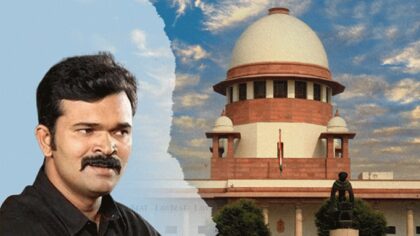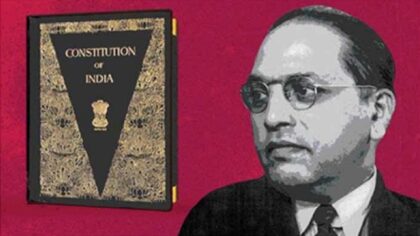पूंजीवाद ने मार्क्सवाद को दफनाने का ऐलान काफी पहले कर दिया था। मार्क्स का दैहिक अंत हुए करीब एक सौ चालीस वर्ष हो चुके हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स की दैहिक विश्राम स्थली पर आज़ भी पर्यटक और प्रतिबद्ध यात्री मिल जाएंगे, पूंजीवाद के महंतों को चिढ़ाते हुए। एक प्रकार से समतावादियों और परिवर्तनवादियों के लिए यह स्थान तीर्थस्थल -सा बन गया है। विश्व के विभिन्न कोनों से लोग मार्क्स को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने आते हैं।
भारत सहित, यूनान, कनाडा, इटली जैसे देशों के यात्री मार्क्स को श्रद्धांजलि देने हाई गेट कब्रिस्तान पहुंचे थे। इंग्लैंडवासी तो आते ही रहते हैं। कुछ चित्रकार मार्क्स की स्मारक वक्ष मूर्ति के रेखाचित्र बना रहे थे। पहले यह ऐसा आकर्षक स्मारक नहीं था। 1956 में समाजवादी शिल्पकार लॉरेंस ब्रेडशॉ ने इस मूर्ति को तराशा और यहां स्थापित किया। मैं 1983 में पहली दफा अकेला इस अंतिम विश्राम स्थली पर आया था। दोपहर का समय था। मेट्रो से आया था। स्टेशन से पूछते पूछते यहां तक पहुंचा था। कुछ रिमझिम का समां था। लोग मार्क्स को नमन करके आ-जा रहे थे। तब मुझे विचित्र ख़ुशी की अनुभूति हुई थी।
आज चालीस बरस बाद अगस्त 2023 में मैं और मधु जोशी यहां पहुंचे हुए हैं, और साथ में हैं लंदन में बसे पाकिस्तानी मूल के लेखक और एक्टिविस्ट अली जाफर ज़ैदी। चार घंटे की मशक्कत के बाद हम इस जगह तक पहुंचे सके थे। हालांकि, जहां से यात्रा शुरू की थी वहां से इसका फासला करीब पैंतालीस मिनट का है। लेकिन, कुछ गूगल की घुमावदार मेहरबानी और बेशुमार कारों के काफ़िले को चीरते हुए पहुंचना पर्वत को जीतने के समान था। तभी तो ज़ैदी जी के होंठ अनायास खुल पड़े “जोशी जी, मार्क्स तक पहुंचना इतना आसान नहीं है।” इस वाक्य को विस्तार देते हुए मैने कहा, “मार्क्स को जीना तो और भी दुश्वार है।” “आप वजा फरमाते हैं”, वे बोले। लंदन में ज़ैदी निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं। तानाशाह जियाउल हक़ के ज़माने में अपने वतन को छोड़ना पड़ा था। ज़ैदी की प्रसिद्ध आत्मकथा: ’ बाहर जंगल और अंदर आग’ में पाकिस्तान की सियासत की कहानी दर्ज़ है। इसका भारत में हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है।

सो, हम तीनों कब्रिस्तान के बंद होते होते पहुंच सके। फिर भी लोग वहां थे, चित्र बना रहे थे, फोटो ले रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे। शांत मुद्रा में मौन रख रहे थे। लोग आते ही जा रहे थे। कनाडा का युवक तो लाल टीशर्ट में था जिस पर हसिया हथौड़ा का प्रतीक बना हुआ था। उसके साथ केरल का युवक भी था। दोनों बंद मुट्ठी को तान कर मार्क्स की प्रतिमा का अभिनंदन भी कर रहे थे यानी ’कॉमरेड मार्क्स, लाल सलाम’। कुछ लोग मार्क्स के वक्ष मूर्ति स्तंभ पर अंकित वाक्य को बार बार पढ़ते जा रहे थे: workers of all lands unite, The philosophers have only interpreted the world in various ways। The point however is to change it। इसके साथ ही पुष्प गुच्छ चढ़ाते। सभी आयु के दर्शक, श्रद्धालु थे वहां। उनकी मुख मुद्राओं पर मार्क्स से आशा की किरण झलक रही थी। मूर्ति शांत और दृढ थी, लेकिन परिवर्तन का आहवान भी उससे विस्फोटित होता प्रतीत हो रहा था। ‘ सब कुछ खोया नहीं है। मनुष्य शेष है। आशा भी।’ ऐसे भाव, शास्वत सन्देश की प्रतीक मूर्ति से अभिव्यक्त हो रहे थे।
मुझे ऐसा लग रहा था। जब हम बाहर लौट रहे थे तब भी एक दर्शक गेट पर चौकीदार से मार्क्स की समाधि तक जाने की विनती कर रहा था। पांच बज चुके थे। चौकीदार विवश था। पर मार्क्स का क्रेज़ थम नहीं रहा था।थमता भी क्यों और कैसे? जब आते समय कॉफी पीने के लिए रास्ते में रुके थे तब एक महिला ज़ैदी जी के पास आई और एक पाउंड देने की गुज़ारिश करने लगी। फिर एक सिगरेट। सेंट्रल लंदन पहुंचे तो वहां भी भिखारी दिखाई दिये। वह कुछ कुपोषण की शिकार भी लगी। वस्त्र, फटे-पुराने थे। बेघर भी रही होगी। किसी श्वेत देश की थी। ज़ैदी जी ने अनुमान से कहा।
मार्च, 1883 में उत्तरी लंदन लंदन के मामूली घर में विश्व सर्वहारा की शोषण-उत्पीड़न से मुक्ति के बहुआयामी दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। उस समय उनकी अर्थी में सिर्फ 13 व्यक्ति शामिल थे। अख़बारों को निधन की जानकारी नहीं दी गया थी। दो रोज़ बाद प्रेस को इसकी जानकारी हुई। इसके बाद तो तांता लग गया। याद आया, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु के साथ भी ऐसा ही हुआ था। प्रेस को खबर नहीं थी। एक दिन बाद संसार को उनकी अंतिम विदाई का समाचार मिला।

मार्क्स की मृत्यु को 2023 में 140 वर्ष हो चुके हैं। बावजूद इसके मार्क्स स्मारक कब्र के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ है। लेकिन, इसे विकृत करने की कोशिशें भी हुई हैं। स्वास्तिक या हिटलर भक्तों ने 1960 में इस कब्र पर स्वास्तिक का निशान बना दिया था। जर्मन में नारे लिखे गए। 1970 के दशक में भी दो दफे बमों के धमाके किये गये। 2011 में इस पर नीला रंग पोत दिया गया था। इतना ही नहीं, 2019 में पता चला कि इसकी संगमरमर की पट्टिका को हथौड़े से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस घटना के कुछ दिन बाद इस स्मारक पर दंगाइयों ने लाल रंग में लिख दिया “घृणा का दर्शन” और “नरसंहार का सूत्रधार” ।
क्या हिटलर भक्त यहूदियों के नरसंहार को भूल गए? इतिहास कैसे भूल सकता है कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैंबर में ठूंस कर मौत का महा तांडव किया था। लेकिन विडम्बना देखिए, आज यहूदियों का आरोपित राष्ट्र इसराइल गजा में फिलिस्तीनियों के साथ हिटलर जैसा व्यवहार कर रहा है। हमास-इसराइल जंग में हजारों मुस्लिम बच्चे, औरतें, वृद्ध मारे जा चुके है। इस किस्त को लिखते समय तक 30 हजार से ज्यादा मानवता का जनसहांर हो चुका था। करीब 80 हजार लोग हताहत हो चुके है।
भारत छोड़ विश्वभर में जन प्रतिरोध किया जा रहा है। यहां तक कि वॉशिंगटन स्थित इजरायल के दूतावास के सामने एक ईसाई युवक ने आत्मदाह करके प्रतिरोध किया। इससे कहीं अधिक घायल हुए। ऐसा लगता है, इस सदी में हिटलर ने यहूदी शासक बन कर अवतार ले लिया है। खैर! इतिहास में ऐसी विभीषिकाओं का सिलसिला चलता रहता है। शासक अपने ही अपराधों से सबक नहीं लेते हैं। वे इंसानों को तबाह करते हैं, और खुद भी तबाह होते रहते हैं।
इसके बाद ही कब्रिस्तान के संरक्षकों ने तय किया कि इस स्मारक स्थल या कब्र पर वीडियो द्वारा 24 घंटे निगरानी रखी जाए। तब से अब तक यह स्मारक सुरक्षित है। इसे कोई क्षति नहीं पहुंची है। इस स्मारक कब्र के पास ही मार्क्स की पत्नी जेनी की भी कब्र है जिनका निधन पति से 18 महीने पहले हो गया था। मार्क्स परिवार के अन्य सदस्यों की कब्रें भी आस-पास हैं। क्या स्मारक स्थल को क्षतिग्रस्त करने से विचार की हत्या हो सकती है? क्या नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की 30 जनवरी, 1948 को नृशंस हत्या करने से उनकी वैचारिक हत्या की जा सकी ? अहिंसा और शांति, आज भी प्रतिरोध के अचूक शस्त्र माने जाते हैं। मार्क्स और महात्मा, दोनों ही प्रतिरोध के योद्धा थे, अपने अपने तरीके से। मैं यही सोचता हुआ वापस कार में बैठ जाता हूं।
मैं या हम युग नायकों की समाधियों की ओर क्यों खिंचे चले आते हैं? मार्क्स को लाल सलाम कहते हुए यह सवाल पैदा हुआ और कार में भी मेरे साथ सफर करने लगा। जब मैं नई दिल्ली में 30 जनवरी मार्ग के सामने से जाता हूँ और गाँधी की समाधि राजघाट पर कभी जाना होता है, एक अव्यक्त -अपरिभाषित सिरहन मस्तिष्क में दौड़ने लगती है। उनके होठों से निकले अंतिम बोल ‘ हे राम’ मुझे हिलाकर रख देते हैं।
ऐसी ही अनुभूति वाशिंगटन डी. सी. स्थित फोर्ड थिएटर में हुई थी, जहां काले गुलामों की दशकों से चली आ रही दासता का खात्मा करनेवाले श्वेत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को गोली मारी गयी थी। वे उस थिएटर की बॉलकनी में बैठ कर ‘आवर अमेरिकन कजिन’ नाटक देख रहे थे। तभी अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र के एक दासता समर्थक श्वेत ने उन्हें गोली मारी थी। यह त्रासदी घटी थी 14 अप्रैल 1865 को। करीब डेढ़ सदी के बाद भी यह जगह श्वेतों और अश्वेतों, दोनों के लिए ‘ तीर्थस्थान’ बना हुआ है। विदेशी पर्यटक तो देखने आते ही हैं।
1985 में मैंने देखा था कि मॉस्को के लाल चौक स्थित लेनिन की समाधि पर लोग कतारबद्ध खड़े हुए थे। 1990 में मैंने देखा था कि बीजिंग में माओ – समाधि के दर्शन करने वाले कम नहीं थे। भगत सिंह और उनके दोनों साथियों का अंतिम संस्कार किस जगह पर किया गया था, यह जिज्ञासा भारत और पाकिस्तान में समान रूप से बनी हुई है। फिर भी पंजाब के फ़िरोज़पुर में तीनों शहीदों की समाधि को देखने लोग आते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधियों के समक्ष आपका शीश स्वतः झुक जाता है। आखें नम हो जाती हैं। आपका अस्तित्व मौनता में डूब जाता है। ऐसी अनुभूति मुझे दो दफे हुई थी। मार्क्स की समाधि यात्रा के समय भगत सिंह की याद आई, यह स्वाभाविक था। दुनिया को अलविदा करने से पहले अपनी काल कोठरी में भगत सिंह लेनिन की जीवनी ही तो पढ़ रहे थे। याद आया। मार्क्स + लेनिन से दोस्ती के बाद ही भगत सिंह कहा करते थे कि भारत को विदेशी गोरे शासकों से ही नहीं, देसी काले शासकों से भी आजादी दिलानी है।
वास्तव में ऐसी विभूतियां मानवता की सार्विक चेतना और स्मृति का अभिन्न भाग बन जाती हैं। स्थानीयता से मुक्त हो कर उनकी कर्म -यात्रा मानव जाती की विरासत का रूप ले लेती हैं। इस रूप में मिल रहा था अपने सवाल का उत्तर।
(रामशरण जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं)