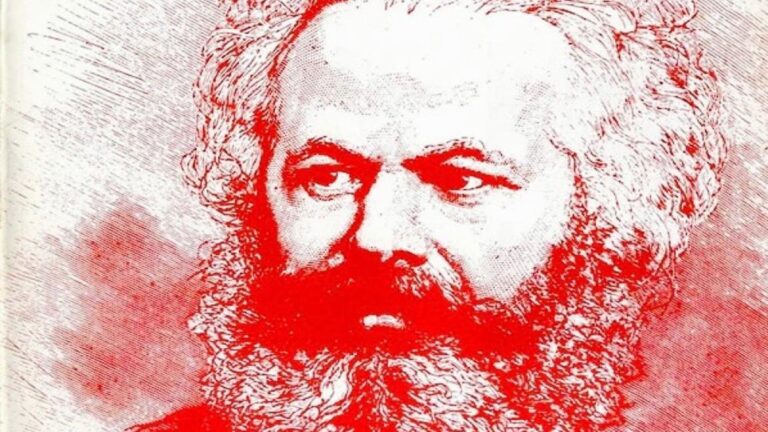भारत की संसद इस समय हंगामे के बीच से गुजर रही है। एक ऐसे संकट से गुजर रही है जिसे हल किये बिना आगे जाने का रास्ता संसदीय लोकतंत्र की उन संभावनाओं को खत्म करेगा, जिसकी दावेदारी की जाती है। इस हंगामे के बीच कुछ ऐसे सन्नाटे भी संसद में उपलब्ध हो रहे हैं जिनके बीच से कई संशोधन अधिनियम, बिल आदि पास हो रहे हैं। इनका असर अब संसद से निकलकर कानून के रूप में हमारे बीच आयेगा और हमारी जिंदगी को प्रभावित करेगा। इस बीच दो ऐसे संशोधन के साथ बिल पास हुए हैं जिस पर संक्षिप्त नजर डाल लेना ठीक होगा। पहला हैः वन संरक्षण संशोधन बिल-2023 और दूसरा हैः जैव विविधता संशोधन बिल- 2023।
वन संरक्षण संशोधन बिल 2023 के तहत वनों का औद्योगिक उपयोग संभव हो जायेगा। यह अपने पूर्ववर्ती 1980 के प्रावधान और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन की परिभाषा में संशोधन कर यह दावा करता है कि इससे वन रोपण की दर बढ़ेगी और वन की उपयोग क्षमता में वृद्धि होगी। यह विधेयक संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में भारत द्वारा कार्बन उत्सर्जन को लेकर दी गई प्रतिबद्धता का हवाला देता है। और, प्रतिपूरक वनीकरण यानी उपयोग आधारित वन का क्षेत्र बढ़ाने पर जोर देता है, जिसमें इसका मालिकाना रखने वाला अपनी जरूरत के अनुसार वन की कटाई कर सकता है; इसके लिए किसी खास अनुमति की जरूरत नहीं रहेगी।
1996 में वन संरक्षण के मसले पर यह निर्णय दिया गया था कि वन में वे सभी क्षेत्र आयेंगे जो वन की तरह आरक्षित हैं या उससे मिलते-जुलते हैं। इस निर्णय के पीछे की मंशा यह थी कि पेड़ों की जो तेजी से कटाई चल रही है उस पर रोक लग जाए और पर्यावरण का संरक्षण बढ़े। इस निर्णय और इससे जुड़े अधिनियम में कई सारी दिक्कतें थीं, जिसकी वजह से वनों पर आधारित जीवन जीने वाले लोगों- जिसमें सबसे अधिक आदिवासी समुदाय था और दूसरे स्तर पर वनों के साथ खेती करने वाले किसान समूह थे- वन अधिकारियों और पुलिस बल के हाथों प्रताड़ित होते थे।
यह समुदाय अपने ही परिस्थिति से वंचित हो गया था। यह संशोधन इसका फिलहाल समाधान नहीं करता है। वह इसके बाहर नये जंगल लगाने और उसके उपयोग की छूट देता है और जिन ‘अपराध’ की श्रेणियों को उपरोक्त समुदाय झेलता है उससे इसे मुक्त कर दिया है। ऐसे लोगों को वन लगाने की अनुमति केंद्र सरकार दे सकती है। यह प्रावधान अब संरक्षित क्षेत्रों के अलावा भी अन्य वन क्षेत्रों में सरकार या किसी प्राधिकरण के स्वामित्व वाले चिड़ियाघर तथा सफारी पर्यटन सुविधा हासिल कर सकती है।
इस संदर्भ में वन भूमि प्रयोग की सीमा रेखा दिसम्बर, 1996 तक की अधिसूचना से बाहर वाली भूमि होगी। यह अंश पेचीदा है, जो आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय वनों को उस दायरे तक ले गया था जिन्हें वन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। यह बिल इस निर्णय में अवर्गीकृत क्षेत्र को परिभाषित करने और उसके उपयोग पर जोर दे रहा है।
यहां यह जान लेना ठीक रहेगा कि जैव विविधता और संरक्षण जंगलों पर ही आधारित होता जा रहा है। जंगल का दायरा कुल क्षेत्रफल के हिसाब से पिछले बीस सालों में स्थिर दिखाई दे रहा है लेकिन उसकी विविधता में तेजी से गिरावट आ रही है। इसका एक बड़ा कारण उसका दोहन है। दूसरी ओर देश के कई हिस्सों में विकास के लिए पेड़ की कटाई तेजी से जारी है और खदानों में जंगल नष्ट हो रहे हैं। यदि हम 2001-2021 के बीच के आंकड़ों को देखें तो 40 प्रतिशत से अधिक घनत्व वाले वन क्षेत्रफल में गिरावट दिखाई देगी जबकि 10 से 40 प्रतिशत घनत्व वाले वनों में एक वृद्धि दिखाई देगी।
इसका दो अर्थ निकल सकता है- बागवानी आदि बढ़ रहा है और जंगलों के नष्ट होने के बाद पेड़ लगाने की अनिवार्यता से इस तरह का दायरा बढ़ रहा है। लेकिन, इतना साफ है कि इससे उच्च घनत्व वाले जंगलों का दायरा नहीं बढ़ रहा है। सरकार इस दूसरे वाले हिस्से से निष्कर्ष निकालकर यह जो विधेयक ला रही है वह जंगल की परिस्थितिकी को महज कार्बन स्टाॅक की तरह देखने का एक रास्ता खोजते हुए लग रही है।
हम जानते हैं कि पहाड़ के क्षेत्रों में सड़क, सुरंग और बिजली-बांध परियोजनाओं ने वहां की परिस्थितिकी पर गहरा असर डाला है और उसके परिक्षेत्र को सीमित किया है। अधिसूचित जंगलों का क्षेत्र आदिवासी समुदाय के रिहाइशी इलाकों में बढ़ता जा रहा है जबकि हाइवे और स्मार्ट सिटी की संकल्पना मैदानी क्षेत्रों के वनों और जैव विविधताओं को खत्म करती जा रही है। ऐसे में, औद्योगिक और व्यवसायिक नजरिये से होने वाले वानिकी का विकास वनों का संरक्षण कम और वनों के विनाश की ओर ले जायेगा। बागवानी या उद्योग आधारित वनीकरण जैवविविधता के खयाल से नहीं बनता है और इसे सिर्फ कार्बन स्टाॅक के रूप में देखना एक संकीर्ण नजरिये को दिखाता है।
सरकार के प्रेस ब्यूरो द्वारा जारी वक्तव्य बताता है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण सीमा और वामपंथी-चरमपंथी क्षेत्रों में विकास और संरचनागत निर्माण में आने वाली बाधाएं हल होंगी। इसमें सीमा क्षेत्र के भीतर की ओर 100 किमी का दायरा रखा गया है। जाहिर है इसमें सर्वाधिक उत्तर-पूर्व के राज्य, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर, राजस्थान जैसे हिस्से आयेंगे और इसके प्रावधानों से प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य और सभी सरकार की संस्थाओं को वन भूमि का पट्टा देने के पहले केंद्र से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
कुल मिलाकर, एक सरसरी निगाह से देखने पर यह विधेयक वन के निजी और औद्योगिक उपयोग को इस उम्मीद के साथ बढ़ावा दे रहा है कि इससे वानिकी को बढ़ावा मिलेगा। सच्चाई यही है कि इसके प्रावधान इस ठोस सच्चाई से मुकर रहे हैं जिसमें खेती के लिए गैर-खेतिहर जमीनों का उपयोग तेजी से बढ़ा है और इसी समयावधि में औद्योगिक और रियल एस्टेट, सड़क परियोजनाओं के लिए तेजी से जमीनों का अधिग्रहण किया है। ऐसा लगता है कि कॉरपोरेट समूह अब जंगल सफारी जैसे पर्यटन पर गहरी नजर रखे हुए हैं, उनके लिए रास्ता खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विधेयक निश्चय ही पर्यावरण के नाम पर है, लेकिन यह इस दुनिया के उपयोग के लिए उद्योगों को रास्ता देता हुआ लग रहा है।
जैव विविधता संशोधन बिल-2023
ऐसा लगता है कि जैव विविधता संशोधन बिल वन संशोधन बिल का एक अनुपूरक हिस्सा है। यह विधेयक संसद में इस उद्देश्य से पास किया है कि इससे भारतीय चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा मिले और इस क्षेत्र में विदेशी निवेश हो। इसके उपयोग में जो बाधाएं हैं, उसे हटा दिया जाये जिससे आयुष चिकित्सकों को लाभ मिल सके।
यह बिल अपने उद्देश्यों में जंगलों और उसके आसपास रहने वाले समुदायों द्वारा औषधीय पौधों और बीजों के उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देने और किसानों द्वारा औषधीय पौधों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात करता है। लेकिन, इसका मूल मकसद इस क्षेत्र में उतरे औषधीय औद्योगिक खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाना है। इन दोनों क्षेत्रों में कोई विदेशी कंपनियां आना चाहती हैं तो उसे भारत की कंपनी के साथ गठजोड़ करके आना होगा।
इसमें एक ऐसा प्रावधान है जिसमें उन लोगों को भी छूट दी गई है जिन्हें संहिताबद्ध पारम्परिक ज्ञान है या उस तक पहुंच सकते हैं। यह छूट आयुष चिकित्सकों के अलावा दी गई छूट है। उपरोक्त की श्रेणी कैसे निर्धारित होगी, इसे तय नहीं किया गया है।
भारत लंबे समय तक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एण्ड टैरिफ और पेटेंट से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों के खिलाफ लड़ता रहा है और अपनी जैव विविधता पर दावा करता रहा है। भारत की भू-परिस्थितिकी एक जटिल और बहुविध क्षेत्र है। इसमें दुनिया के सबसे प्राचीन पठार से लेकर सबसे नूतन पहाड़ निर्माण शामिल हैं। नदियों के बेसिन से लेकर समुद्र का विशाल किनारा है। एक तरफ शांत अरब सागर है और दूसरी ओर हलचल से भरी हुई बंगाल की खाड़ी। नीचे हिंद महासागर का विशाल क्षेत्र जहां से मानसून की यात्रा शुरू होती है और एकदम पश्चिम में राजस्थान के पिछले हिस्सों तक जाती है। इन सबने एक खास तरह की जैव-विविधता को निर्मित किया है।
औपनिवेशिक दौर में जंगलों की भयावह कटाई और जानवरों के अंधाधुंध शिकार से इस परिवेश को काफी नुकसान पहुंच चुका था। 1970 तक विशाल परियोजनाओं ने इसे नुकसान पहुंचाया। लेकिन, पिछले 20 सालों में इन नुकसानों के साथ साथ पर्यावरण में होने वाले बदलावों ने इसे गुणात्मक गति दे दी है। परिस्थितिकी का नुकसान का असर सीधे हमारे जीवन पर पड़ रहा है। एक खास तरह के अनाजों, सब्जियों आदि की मांग ने खेती की व्यवस्था पर गहरा असर डाला है।
भोजन, पर्यावरण और जीवन के बीच एक गहरा रिश्ता है। इसमें आ रहे बदलाव की विभीषिका को हम देख रहे हैं। यह औषधियों और रसायनों का ही प्रयोग- जिसमें गिद्ध से लेकर कई जीव प्रजातियां खत्म हो गईं। ऐसे में जैव विविधता के उपयोग में औद्योगिक छूट न सिर्फ देश की संपदा, बौद्धिक संपदा, जैव संरक्षण और आम जीवन को प्रभावित करेगा; यह अंततः उस जंगल को प्रभावित करेगा जिसकी वजह से उसे यह नाम दिया गया है।
निजीकरण, औद्योगीकरण, वैश्वीकरण आदि शब्दावलियां अब विकास के नाम में समेट दी गई हैं और इनके विनाशक प्रभाव की जगह इसके मुनाफे के प्रभाव को दिखाकर एक चमक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इनका विरोध अब निजीकरण, औद्योगीकरण, वैश्वीकरण का नहीं, अब विकास विरोधी होने में बदल गया है। ऐसा लग रहा है मानो पूंजीवादी साम्राज्यवाद नाम का कोई तथ्य नहीं रह गया है।
ऐसा लग रहा है मानो हर कोई को मुनाफे के लिए लालायित है और इन संशोधित कानूनों, विधेयकों के लागू होते ही सभी खुशहाल हो जायेंगे। जबकि ये प्रावधान हमारे जीवन, संप्रभुता पर गहरा असर डालेंगे और हमारे सामने एक जटिल स्थितियों को पैदा करेंगे। एक कहावत है कि जिस मुंडेर पर काक नहीं/उसमें कोई आस नहीं। यह आस बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि काक भी बना रहे।
(अंजनी कुमार पत्रकार हैं।)