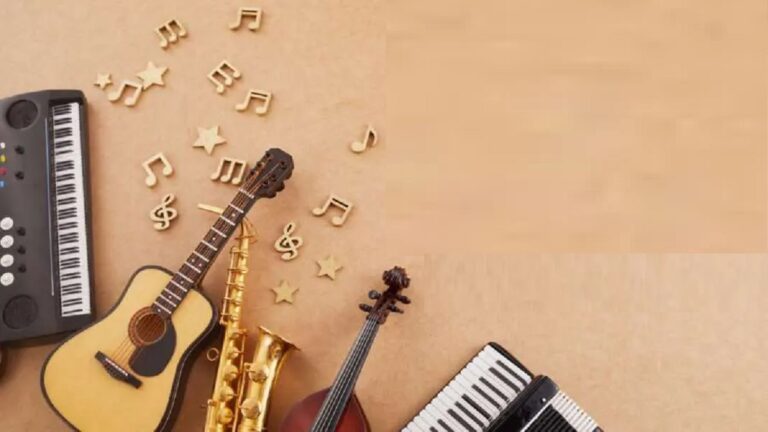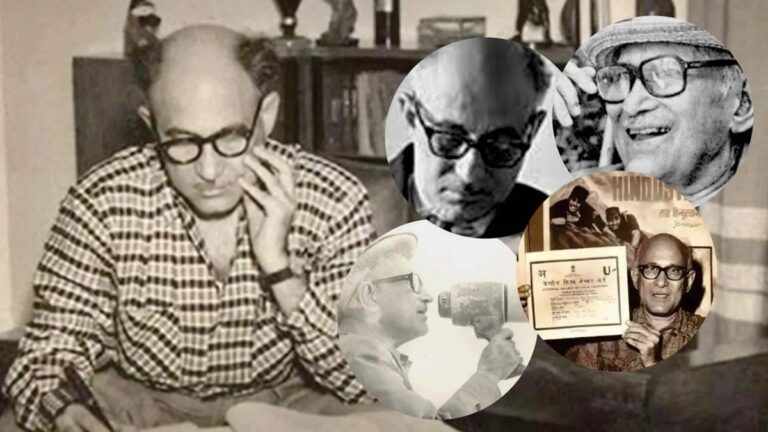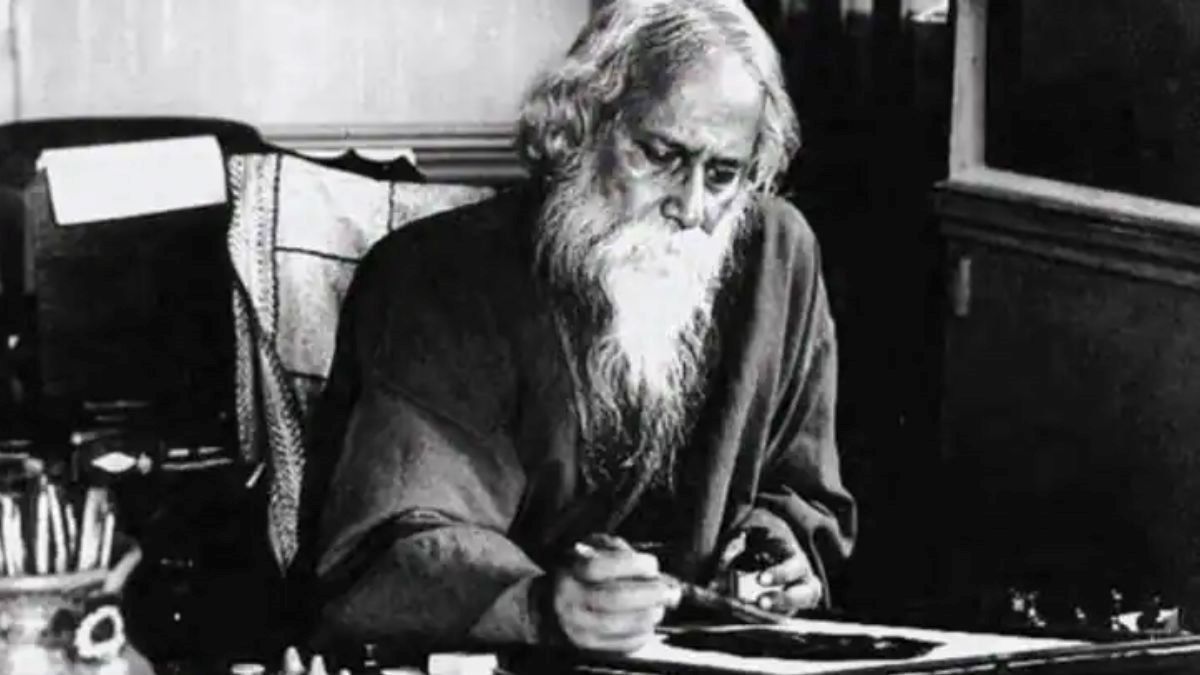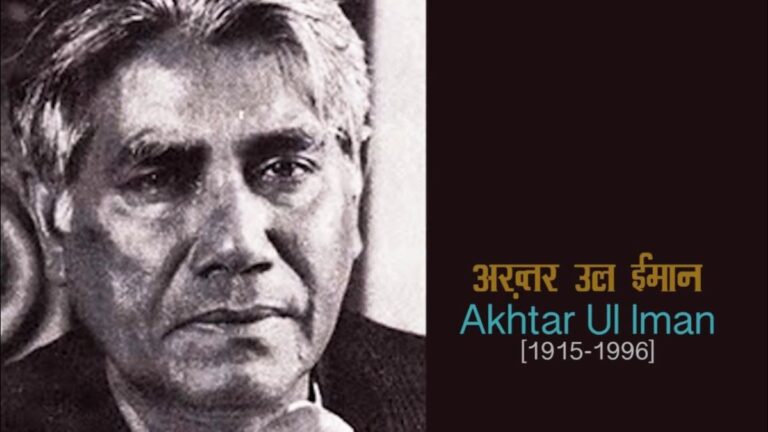मुग़लों के इतिहास को हम अक्सर मुग़ल बादशाहों के नाम और कारनामों से जानते हैं। तक़रीबन तीन सदी तक उन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया। इस इतिहास में मुग़ल औरतों का बहुत कम ज़िक्र मिलता है। इसकी वजह भी है। क्योंकि यह इतिहास ज़्यादातर पुरुषों ने लिखा है। पुरुषवादी नज़रिये से ही वे सब स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं। उनकी नज़र में औरत की कोई अहमियत नहीं। जबकि औरत के बिना इस पूरी काइनात का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता।
नूरजहाँ, मुमताज़ महल, चाँद बीबी, हज़रत महल, हरका बाई, गुलबदन बेगम और जोधाबाई कुछ नाम ऐसे हैं, जिनसे हर कोई वाक़िफ़ है। इन पर बहुत कुछ लिखा भी गया है, लेकिन मुग़ल औरतों की एक बड़ी तादाद मसलन हाज़ी बेगम, सरहिन्दी बेगम, दिलरस बेगम, जहाँजे़ब बानो वगैरह हैं, जिन पर कभी कोई बात-चर्चा नहीं होती। ये औरतें इतिहास में बिल्कुल भुला दी गई हैं। जबकि इन औरतों के मार्फ़त भी हम मुग़ल इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान-समझ सकते हैं।
हालाँकि यह काम बड़ा मुश्किल है, मगर एक छोटी-सी कोशिश कवि पवन करण ने अपनी नई किताब ‘स्त्रीमुग़ल’ के ज़रिए की है। यह कोई शोध प्रबंध या इतिहास नहीं, महज़ कविताओं की एक किताब है। जिसमें लेखक ने सौ कविताओं या यूँ कहिए सौ मुग़ल औरतों के किरदार के बहाने मुग़ल इतिहास पर रौशनी डाली है। उन विस्मृत पन्नों को फिर पलटा है, जिन पर धूल की एक मोटी परत पड़ी हुई थी। ज़ाहिर है कि कविताओं के केन्द्र में औरत ही है। मुग़ल औरतों के दुःख-दर्द, ख़्वाहिशें, अधूरी हसरतें, आरजूएँ और अरमान। फ़िराक़ और वस्ल की बातें।
किताब की कोई भी कविता पढ़ें, यह सिर्फ़ कविता भर नहीं। हर कविता एक इतिहास है। कवि पवन करण ने मुग़ल औरतों से जुड़े छोटे-छोटे प्रसंगों से जैसे उस दौर को ज़िंदा कर दिया है। इन कविताओं से उस वक़्त की राजनीतिक, सामरिक, सामाजिक स्थितियाँ सभी कुछ बयाँ होती हैं। यही नहीं कविता उससे आगे भी चलती है, वह कहीं-कहीं वर्तमान पर भी टिप्पणी करती चलती है। क्योंकि कई मामलों में दुनिया भर के अंदर औरतों के हालात आज भी वैसे ही हैं।
‘लखम बाई’ गुजरात के सुल्तान मुजफ़्फ़र सानी की राजपूत रानी थी। सुल्तान बहादुरशाह की माँ। मुग़ल बादशाह हुमायूँ ने माँडू में बहादुरशाह के साथ दगा किया। मुग़ल औरतें सत्ता के आगे, तो कभी अपना मुँह नहीं खोल पायीं। मगर कवि अपनी कल्पनाशक्ति से इन बेजुबान औरतों को अपनी आवाज़ देता हुआ, इसी कविता में लिखता है, ‘‘धोखेबाज़ बादशाह की जय-जयकार/मुल्क की अवाम कभी दिल से नहीं करती/उसे लगता है तख़्त पर बैठा बादशाह/हमारे साथ भी धोखा कर सकता है/अपने नाम के साथ-साथ वह/मुल्क के नाम को भी डुबा सकता है।’’ (पेज-50)
हमारे देश में स्त्रीधन और दहेज देने की परंपरा कितनी पुरानी है, संग्रह की ‘लाडमलिका’ कविता से पता चलता है। राजपूत राजाओं की तरह मुग़लों में भी यह आम था। शादी में ख़ूब दान-दहेज देने का चलन था। शेरशाह सूरी ने तो दौलत की ख़ातिर कई विधवाओं से निकाह किए, तो उन विधवाओं ने अपनी ज़िंदगी को बचाने की ख़ातिर। अलबत्ता यह बात अलग है कि शादी के बाद भी इन औरतों की ज़िंदगी में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया। उनकी क़िस्मत ज्यों की त्यों बनी रही। वह बादशाह के हरम में उसकी बाँदी बनकर रह गई। ‘‘औरत के पास दौलत हो, तो वह भी/उसे जब चाहे अपने लिए तलवार/या फिर ढाल में बदल सकती है, जैसे मुझ पर/घात लगाए बैठीं शमशीरों के आगे/शेरशाह की सूरत में ढाल बन गई वह/उसे दौलत चाहिए थी और मुझे ज़िंदगी/…..मगर बदले में मुझे और तुम्हें बस ज़िंदगी मिली/एक और बादशाह के हरम की ज़िंदगी/हम जैसी कई औरतों के बीच जहाँ/हमारी दौलत और ख़ासियत खोकर रह गई।’’ (पेज-55)
किताब समीक्षा : ‘स्त्रीमुग़ल’ (कविता-संग्रह),
लेखक : पवन करण,
पेज : 214, मूल्य : 299,
प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, जी-17, जगतपुरी, नई दिल्ली-110051
इतिहास के विद्यार्थियों को यदि छोड़ दें, तो कितने लोग जानते हैं कि मुग़ल बादशाह हुमायूँ की मौत क़िले से गिरकर हुई थी। और आज हम जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में उनका विशाल मक़बरा देखते हैं, वह उनकी दूसरी बीवी हाज़ी बेगम ने अपने ख़र्च से बनवाया था। ‘‘हुमायूँ के इस तरह दुनिया छोड़कर चल देने को/क़ुबूल नहीं कर सकी वह/पुराने क़िले की उस हैसियत से जिससे गिरकर/दम तोड़ा बादशाह ने उससे दुश्मनी बाँध ली उसने।’’ (‘हाज़ी बेगम’, पेज-64)
इस कविता को पढ़कर यह एहसास होता है कि मुग़ल बेगमें हरम में महज़ बाँदी बनकर ही नहीं रहीं, बल्कि उनमें फै़सले लेने की ताक़त भी थी। उनके इरादे आसमान से भी ऊँचे थे। अपनी इच्छाशक्ति से उन्होंने कई मर्तबा नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गईं। एक-दूसरे धर्म के प्रति बढ़ते अविश्वास, असहिष्णुता और नफ़रतों के इस दौर में कितने लोग जानते हैं कि गुलबदन बेगम भी एक मुग़ल औरत थी, जिसने ‘हुमायूँनामा’ लिखा।
इस कविता के मार्फ़त भी कवि ने अपनी कल्पनाशक्ति का ख़ूब इस्तेमाल किया है। स्त्रीवादी नज़रिये से वे इस पूरे वाक़िआत को देखते हैं, ‘‘तलवार का मज़हब आँख मूँदकर चलना होता है/तो क़लम का धर्म आँख खोलकर लिखना/फिर मेरी क़लम मुग़लिया मर्दों की/ख़्वाबगाहों के पर्दे कैसे नहीं उठा सकी।…..काश मैं मुग़ल बेगमों और शहज़ादियों के/जीवन में पसरे अँधेरे और बादशाह और शहज़ादों के/हाथों में लगे ख़ून के धब्बों पर भी लिखती।’’ (पेज-68)
कविता यहीं नहीं रुक जाती, इसकी दो पंक्तियों में जैसे आज का यथार्थ और एक संदेश व्यक्त होता है, ‘‘अपने रंग में सब रंग देने की इच्छा में ख़ूबसूरती नहीं/सबको अपने-अपने रंग में रँगे रहने देना ही ख़ास होता है।’’(पेज-69)
मुग़ल घरानों के अंदर मर्दों के सामने औरत की क्या हैसियत या क़िस्मत है ? किताब में कई मर्तबा सामने आया है। अलग-अलग कविताओं में अलहदा संदर्भों में इसका ज़िक्र है। इंतज़ार और घुट-घुटकर मर जाना बेगमों, राजकुमारियों और शहज़ादियों की नियति है। हरम या ख़्वाबगाह में सभी के एक जैसे हालात हैं। हिन्दू, मुस्लिम न होकर वहाँ वह सिर्फ़ एक औरत है, जो मर्दों के आसरे है। उसकी इच्छाएँ, आशाएँ और उसके सपनों का वहाँ कोई मान नहीं। ‘‘मुग़लिया सल्तनत में यदि औरत एक ज़ुबान है/तो उसका तर्जुमा कोख और उससे/पैदा होने वाली औलादों में ही होता है/मुग़लिया होने से कोई औरत/अपने औरत होने की हद नहीं लाँघ जाती/रहना उसे औरत होकर ही होता है/राजपूतानियाँ हों या मुग़लानियाँ/बेगमें हों या शहज़ादियाँ वे सब मेरी/और तुम्हारी तरह औरते हैं/सबका इंतज़ार और प्यास एक सी है।’’ (‘रोक़य्या बेगम’, पेज-75)
एक दूसरी कविता ‘सलीमा बेगम’ में भी यही बात एक अलग अंदाज़ में दोहराई गई है, ‘‘वो ही क्या हम सभी ईरानी, इस्फ़हानी, हिन्दुस्तानी/बेगमों का आपके हरम और बादशाहत में यही हाल है/मुझ सरीखी अनेक औरतों से जिनमें से कइयों की/ख़ूबसूरती अब सड़ने लगी है आपका हरम भरा पड़ा है।’’ (पेज-79)
इतिहास में मुग़ल हरम के कई क़िस्से प्रचलित हैं। अलग-अलग इतिहासकारों ने इसे अपने तरीके़ से लिखा है। ख़ास तौर पर अंग्रेज़ इतिहासकारों ने अपनी किताबों में इसे ख़ूब बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। मुगल बादशाहों को हरम तक ही महदूद कर दिया है। जैसे अय्याशियों के सिवाए उनके पास कोई काम ही नहीं था। जब वे अपना सारा वक़्त हरम में ही बिताते थे, तो हुकूमत के काम कब करते होंगे। जंग लड़ने और अपनी सत्ता को संभाले रखने का मुश्किल काम किस तरह अंजाम देते होंगे। जबकि मध्यकाल वह दौर था, जब दरबार में ही नहीं, घर के अंदर भी सत्ता के लिए संघर्ष और साज़िशें मुसलसल चलती रहती थीं। ज़रा-सी लापरवाही किसी के लिए भी मौत का पैग़ाम होती थी।
बहरहाल, बात हरम की। मध्यकाल में बादशाह और राजा एक से ज़्यादा शादियाँ करते थे, यह तथ्य है। इसके अलावा औरतों को बराबरी का दर्जा न था, इससे भी भला कौन इंकार कर सकता है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का भी प्रचलन था। यहॉं तक कि औरत ख़ुद अपना फ़ैसला नहीं ले सकती थी। कमोबेश ग़ुलामों की सी ज़िंदगी थी उसकी। यही वजह है कि कवि जब भी किसी मुग़ल औरत के किरदार पर बात करता है, तो हरम के बहाने जैसे उस दौर में औरत की स्थिति को ही बयाँ करता है। ‘‘बादशाह का हरम जितना ब्याह कर लाई/औरतों से रौशन होता है, उससे ज़्यादा/वह लूट और छीन कर लाई औरतों से जगमगाता है।’’ (‘अफ़रोज़ बेगम’, पेज-77)
इन कविताओं में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी बदतर स्थितियों के प्रति औरत का एक प्रतिरोध भी है। वह एक चुभने वाला कटाक्ष करती है। यह औरतें बार-बार अपने बदतर हालात के जानिब हमारा ध्यान खींचती हैं। और बतलाती हैं कि एक औरत सिर्फ़ बादशाह की बेगम या शहज़ादी बनकर ही ख़ुश नहीं रहती, दौलत, ऐश-ओ-आराम ही उसकी मंज़िल नहीं, बल्कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में उससे भी कहीं ज़्यादा चाहिए। इज़्ज़त, फ़ैसलों में भागीदारी, बराबरी का बर्ताव और उससे भी कहीं ज़्यादा बादशाह के दिल में उसके जज़्बात की क़द्र हो।
‘स्त्रीमुग़ल’ की हर कविता इतिहास का एक भुला दिया जाने वाला अध्याय बताती है, जिस पर बहुत कम बात होती है। मिसाल के तौर पर चंदेरी और रायसीन के राजा भूपतशाह के नाबालिग बेटे प्रतापशाह के वजीर पूरनमल की बेटी ‘पद्मावती’ को लोग कितना जानते हैं ? पूरनमल की रायसीन पर हुकूमत थी। शेरशाह ने जब रायसीन के क़िले पर क़ब्ज़ा कर लिया, तो पूरनमल ने उस शेरशाह से जो युद्ध में जीत के बाद कभी अपने दुश्मन के हरम में क़दम नहीं रखता था, अपनी रानी, बेगमों और शहज़ादियों को बचाने के लिए मौत के घाट उतार दिया। ‘पद्मावती’ इस युद्ध के बाद बची, तो बादशाह के हुक्म पर उसे सड़कों पर नचाया गया।
‘पद्मावती’ कविता इसी पूरे दर्दनाक वाक़िये को बयान करती है, ‘‘मालिक-ए-मुल्क हिन्दुस्तान की सड़कों पर/मुझे नहीं मेरी शक्ल में तुम्हारे न्याय को/नचाया जा रहा है, तुम्हारी दी सज़ा को लोग/अपने बीच थिरकता और न थिरकने पर/भीड़ के बीच पिटता देख रहे हैं।’’ (पेज-49) कविता ‘पद्मावती’ औरतों की व्यथा ज़रूर बताती है, लेकिन इस कविता का किताब के शीर्षक से कोई वास्ता नहीं। वह इसलिए कि ‘पद्मावती’ मुग़ल स्त्री नहीं थी। इसी तरह ‘तारा’ जोधपुर के महाराजा गजसिंह के बेटे अमर सिंह की बेटी थी। कवि ‘तारा’ कविता के मार्फ़त मुग़लों और राजपूतों के रिश्तों पर बात करते हुए लिखते हैं, ‘‘बादशाह जहाँगीर और शाहजहाँ दोनों ने/राजपूत रानियों की कोख से जन्म लिया/और मालिक हुए इस मुल्क के/…….राजघरानों की बराबरी यह कि हमें/ब्याहा गया मुग़लों से, इस पर भी/राजपूतों की समझदारी ये/कि धर्म की दीवारें गिराते/और मुग़लों से रोटी-बेटी का/रिश्ता जोड़ते देर नहीं लगी उन्हें, अफ़सोस इसमें मुग़ल रह गए पीछे/वे भी आगे बढ़े होते/तो मुग़ल शहज़ादियों के भाग्य में/कुँआरा रह जाना लिखा न रह जाता/राजपूतानियों की तरह उनकी भी/डोलियों के उठने का सिलसिला/शुरू हो जाता मुग़ल महलों से/अपनी तरह हम भी/उन्हें राजपूत महलों में देखतीं/ये सिलसिला राजाओं और बादशाहों के/बीच ही थमकर नहीं रुक जाता/बढ़ता हुआ पहुँचता अवाम तक/तब मुल्क की तस्वीर देखने लायक़ होती।’’ (पेज-138, 139)
यह ऐसी कड़वी सच्चाई है, जो इतिहास में दर्ज है। मुग़लिया आन, बान और शान पर आँच न पहुँचे, इसलिए मुग़ल शहज़ादियाँ अनब्याही रहीं। मुग़लों ने ख़ुद तो कई अंतरधार्मिक शादियाँ कीं, मगर उन्हें यह न मंजूर था कि उनकी बहनें, बेटियों दूसरे मज़हब में ब्याही जाएं। चाहे उनकी ज़िंदगी बरबाद हो जाए। मुग़लकाल में यह सख़्त क़ानून था कि अगर कोई हिन्दू किसी मुस्लिम महिला से शादी करता है, तो उसे इस्लाम स्वीकार करना होगा। तभी उसका विवाह मुमकिन होगा। तानसेन ने अपनी मुस्लिम महबूबा ‘तानी’ को पाने की ख़ातिर अपना मज़हब तक बदल लिया था। ‘‘मुझे यक़ीन दिलाने के आप मुझसे कितनी/मुहब्बत करते हैं, आपने अपना ख़ुदा बदल लिया।’’ (‘तानी’, पेज-82)
‘स्त्रीमुग़ल’ की कविताओं में औरत की सिर्फ़ बेबसी, बेचारगी ही ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि कहीं-कहीं वह अपने हालात से बग़ावत करने पर भी आमादा दिखती है। ऐश-ओ-इशरत, बादशाह का हरम और उसकी नज़दीकता को ठोकर मारकर वह आवाज़ देती है, ‘‘अम्मीजान, बेगमों और शहज़ादियों के लिए/तो अच्छा ये है कि वे सल्तनत से मिले/अपने ख़िताबों की गठरी बाँधे और जमुना में बहा दें/वे सब इकट्ठी होकर क़िले पर चढ़ जाएँ/और वहाँ से चिल्ला-चिल्लाकर/दुनिया की औरतों को बता दें कि हम/मुग़लिया औरतों की हालत आप से भी ज़्यादा ख़राब है/इन मुग़लिया महलों में हमारी शक्ल में/तुमसे भी गई-बीती औरतें रहती हैं/जो भले ही अच्छा पहनती और खाती हैं/बेगमें और शहज़ादियाँ कहलाती हैं/अस्ल वे वहाँ घुट-घुटकर मर जाती हैं।’’ (‘अकबराबादी बेगम’, पेज-122)
कुछ कविताओं में तो यह लहजा और भी ज़्यादा तल्ख़ हो जाता है। वे अपने अधिकारों के लिए इस हद तक आगे आ जाती हैं, ‘‘तुम जहाँ भर की औरतों की तरफ़ से/ये बात वहाँ भी कह सकती थीं, मर्दो/दुनिया के सभी मज़हबों में औरतों की हालत/ख़राब है, आपको चाहिए कि आप सब/दीन-ए-इलाही की जगह दीन-ए-औरत/ मज़हब शुरू करें और उसे चलाने की/ज़िम्मेदारी भी वे औरतों को ही सौंपें/अपने बारे में वे क्या कहती हैं उसे सुनें/वे अपने लिए कैसा मज़हब चाहती हैं, ये जानें/वे अपने लिए कोई मज़हब चाहती भी हैं या नहीं/इसका इल्म भी होना चाहिए आपको।’’ (‘ख़ानम सुल्तान बेगम’, पेज-86)
यह एक यूटोपिया हो सकता है, लेकिन कवि इसकी तरफ़ अपनी ओर से इसी कविता में आगे एक इशारा करता है, ‘‘आरामबानू, क्या कोई औरत दीन-ए-औरत/नहीं चला सकती, क्या ज़रूरी है/कि वो इसके लिए मर्दों का ही मुँह ताके/मगर….हम बादशाह अकबर की तीनों बेटियाँ/अपने जे़हन से इस बात को न निकलने दें/कि हम न सही कभी हम जैसी ही/कोई औरत मर्दों के इस मज़हब से आकर बाहर/दीन-ए-औरत या उससे भी बढ़कर/आइन-ए-औरत की नींव रखेगी।’’ (पेज-87)
‘स्त्रीमुग़ल’ की कमियों, लेखक की कुछ चूकों और प्रकाशन की त्रुटियों की अगर बात करें, तो सबसे पहले किताब का शीर्षक ही कुछ अटपटा लगता है। ‘स्त्रीमुग़ल’ के बजाए अगर इसका शीर्षक ‘मुग़ल औरतें’ होता, तो कहीं ज़्यादा आकर्षक लगता। ख़ुद लेखक ने किताब में हर जगह ‘स्त्री’ की जगह ‘औरत’ लफ़्ज़ का ही इस्तेमाल किया है। ‘स्त्री मेरे भीतर’ और ‘स्त्रीशतक’ (दो खंड) पवन करण की वे किताबें हैं, जिन्हें ख़ूब मक़बूलियत हासिल हुई। ख़ास तौर पर ‘स्त्री मेरे भीतर’ का तो कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। शायद यही वजह है कि लेखक ने सायास ही इस किताब का शीर्षक ‘स्त्रीमुग़ल’ रखा है। ताकि इस किताब को भी उसी तारतम्य में देखा जाए। किताब का कवरपेज भी कोई ख़ास असरदार नहीं। जबकि इसको बनाते वक़्त और भी अधिक कल्पनाशीलता का परिचय दिया जा सकता था।
कहने को किताब पैपरबैक्स में है, लेकिन इसका दाम 299 रुपए हार्डबाउंड की मानिंद है। ‘स्त्रीमुग़ल’ का शिल्प और भाषा की यदि बात करें, तो इसमें कुछ कविताओं का शिल्प ऐसा है, जिसे आम पाठक आसानी से नहीं समझ सकते। यही नहीं कहीं-कहीं कुछ कविताओं में जो परस्पर संवाद हैं, वे कई मर्तबा आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सामान्य पाठकों को कविता समझने में परेशानी पेश आ सकती है।
जहाँ तक किताब की भाषा का सवाल है, लेखक ने इसमें हिंदुस्तानी ज़बान का इस्तेमाल किया है। नुक़्तों का भी ख़ास तौर पर ख़याल रखा गया है। लेकिन कहीं-कहीं संस्कृतनिष्ट हिन्दी चुभती है। मसलन षडयंत्र, निर्णय, संदेह, इच्छा, अधिकार, सुंदर, सुंदरता, विवश, अनुमान वगैरह। जबकि इन शब्दों के स्थानापन्न हिंदुस्तानी लफ़्ज़ क्रमशः साज़िश, फ़ैसला, शक, आरज़ू, ख़ूबसूरत, ख़ूबसूरती, मजबूर, अंदाज़ा आदि हमारे रोज़मर्रा में ख़ूब प्रचलन में हैं।
एक अहम-तरीन बात और, लेखक ने हर कविता के साथ फुटनोट में संबंधित किरदार का मुख़्तसर-सा तआरुफ़ दिया है। लेकिन अगर इसमें समय-काल का भी ज़िक्र होता, तो और भी बेहतर होता। बावजूद इसके ‘स्त्रीमुग़ल’ एक ख़ास और ज़रूरी किताब है, जिसमें लेखक ने काफ़ी शोध कर मुग़ल औरतों को एक जगह इकट्ठा किया है। उन पर ऐतिहासिक संदर्भों के साथ बात की है।
मध्यकाल में औरतों की स्थिति घर और बाहर क्या थी ? इस पर से पर्दा उठाया है। कहीं-कहीं वे अपनी ओर से इन परिस्थितियों के ख़िलाफ़ ज़रूरी टिप्पणियाँ भी करते हैं। सच बात तो यह है कि ‘स्त्रीमुग़ल’ की कविताओं को सतही पाठ से नहीं समझा जा सकता, बल्कि इन कविताओं के कई पाठ हैं। कविताएँ बहुअर्थी हैं। जितनी बार भी हम इन्हें पढ़ेंगे, हमारे सामने इनके कई अर्थों का ख़ुलासा होगा।
यह आम कविताएँ नहीं, बल्कि बहुस्तरीय कविताएँ हैं। जिन्हें लेखक ने बड़े मनोयोग से पाठकों के लिए गढ़ा है। अलबत्ता आम पाठकों के लिए यह कविताएँ दुरूह हैं, लेकिन इनकी अहमियत से इंकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि आहिस्ता-आहिस्ता ही सही ‘स्त्रीमुग़ल’ की कविताओं पर अब खुलकर बात हो रही है। अलग-अलग नज़रियों से इन कविताओं को परखा जा रहा है। किसी भी किताब और लेखक के लिए इससे बड़ी कामयाबी की बात और क्या होगी।
(ज़ाहिद ख़ान रंगकर्मी और स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)