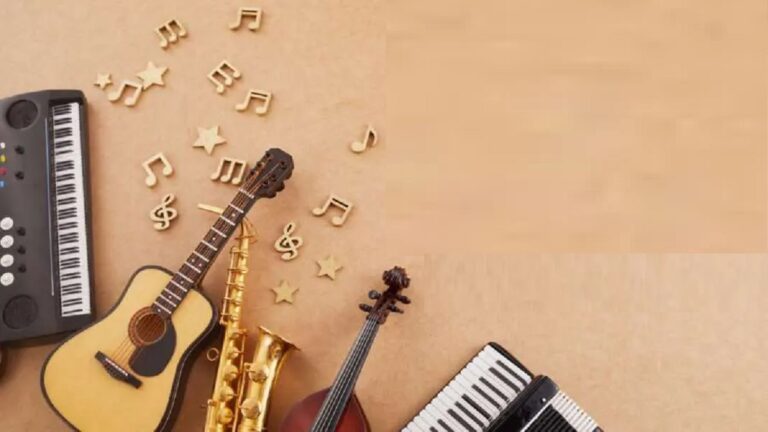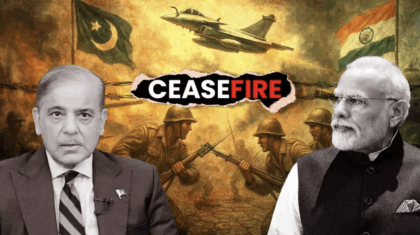प्रयागराज के दारागंज इलाके की एक पुरानी गली में स्थित है ‘धनराज वृद्धाश्रम’। बाहर से देखने पर यह एक साधारण-सा मकान लगता है। फर्श पर फैली दोपहर की धूप और एक खामोशी जो दीवारों के आर-पार तक जाती है। लेकिन जैसे ही इसके भीतर कदम रखते हैं, ऐसा लगता है मानो इस मकान की हर ईंट ने कभी न कभी किसी टूटे हुए दिल की सिसकी सुनी हो।
यहां रहने वाली अधिकतर महिलाएं वे हैं जिनके अपनों ने उन्हें उस मोड़ पर छोड़ दिया, जब उम्र, शरीर और मन तीनों को सहारे की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। वृद्धाश्रम उनके लिए सिर्फ एक छत नहीं, बल्कि ज़िंदगी की आखिरी पनाहगाह है। वृद्धाश्रम के दरवाज़े पर कोई तख्ती नहीं, बस अंदर जाने पर अहसास होता है कि यह सिर्फ दीवारों से घिरा कोई भवन नहीं, बल्कि टूटी उम्मीदों, छूटे रिश्तों और बेसहारा ज़िंदगी के टुकड़ों को समेटे एक अलग दुनिया है।
सुबह की पहली चाय के साथ कुछ बुज़ुर्ग महिलाएं आंगन में चुपचाप बैठी थीं। किसी के हाथ में तस्वीर थी, किसी के मन में यादें। न कोई उत्साह, न कोई शिकायत… बस एक अजीब-सी स्वीकार्यता। जैसे ज़िंदगी से अब कोई सवाल नहीं बाकी है।
इन्हीं में एक चेहरा था 65 वर्षीय पुष्पा देवी का। आंगन के कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठी पुष्पा की सूनी आंखें किसी गहरी तलाश में थीं। वो बार-बार सामने लगे नीबू के पेड़ की ओर देखती जैसे उस पेड़ से उनका कोई पुराना रिश्ता हो, जो अब भी निभा रहा हो।
पुष्पा देवी ने अपने जीवन के कई साल एक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में बिताए। बच्चों की तोतली भाषा, मासूम सवाल और कच्ची स्लेटों पर लिखी पहली अक्षर यही उनकी दुनिया थी। लेकिन जब वक्त आया कि कोई उनके माथे पर हाथ रखकर पूछे, “थक गई हो?”, तो कोई नहीं था। न बच्चा, न पति, न घर।

पुष्पा बताती हैं, “पति हरिद्वार में रहते हैं, हमारे रास्ते अलग हो गए। वजह पूछिए तो शायद जवाब भी न दे पाऊं। बस कुछ ऐसा था जो टूट गया और फिर कभी जुड़ नहीं पाया।” पुष्पा के पास बस एक पुरानी तस्वीर है पति की, जिसे वह हर समय अपने तकिए के नीचे रखती हैं। वो आज भी सिंदूर लगाती हैं, बिंदी पहनती हैं और तस्वीर को देखकर हर सुबह अपने दिन की शुरुआत करती हैं।
“जब पहली बार यहां आई थी, तो दो हफ्ते तक ठीक से खा भी नहीं पाई। हर कोने से पराया-पन झांकता था। फिर एक दिन अहसास हुआ, जब अपनापन न मिले तो परायेपन से ही रिश्ता बना लेना चाहिए। अब यही घर है, यही लोग अपने हैं,” कहते-कहते उनकी आवाज़ भर्रा जाती है।
हर कमरा, एक अधूरी किताब
इस वृद्धाश्रम का हर कमरा एक अधूरी किताब की तरह है। कोई कहानी अधूरी रही, क्योंकि बेटे के आत्मनिर्भर होने के बाद मां की ज़रूरत नहीं रही, कोई इसलिए छूटी क्योंकि बहू को सास की बीमारी बोझ लगने लगी और कुछ कहानियां तो ऐसी हैं जो अब भी किसी के गले से नहीं निकलतीं-वे सिर्फ आंखों से बह जाती हैं।
इस वृद्धाश्रम का हर चेहरा एक अधूरी कहानी है। एक ऐसा पन्ना जो कभी पलटा ही नहीं गया। इन्हीं चेहरों के बीच एक चेहरा था सफेद बाल, झुकी कमर और कांपती पलकों वाली रामकुमारी देवी का। रायबरेली की रहने वाली करीब 68 वर्ष की इस बुज़ुर्ग महिला की आंखों में ठहराव नहीं था, बस एक बहता हुआ सैलाब था जो बोलने से पहले ही बह निकलता था। बातचीत की शुरुआत होते ही उनके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। सिसकियों के बीच जो शब्द निकलते हैं, वे किसी भी इंसान को भीतर तक तोड़ देने के लिए काफी हैं। धीमी आवाज़ में वह कहती हैं, “हमारा इकलौता बेटा ही हमारा दुश्मन बन गया। फिर हमारी दुनिया ही बदल गई।”
रामकुमारी के पास 12 बीघे ज़मीन है इतनी कि उसका सहारा बन सकती थी, लेकिन वही संपत्ति ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा बन गई। बेटा और बेटी दोनों ने मिलकर उन्हें घर से निकाल दिया। मारपीट, गाली-गलौज और तिरस्कार के बाद जब एक दिन उन्होंने दरवाज़े से धक्का दे दिया, तो रामकुमारी के पास सिर्फ एक थैला और उसमें कुछ कपड़े ही रह गए।
बिलकुल अकेली, बेसहारा, वो ट्रेन में बैठ गईं। चित्रकूट जा रही थीं। कोई मंदिर तलाशने जहां बैठकर भीख मांग सकें। लेकिन ट्रेन में एक अजनबी मुसाफिर ने उनके आंसुओं की भाषा पढ़ ली। उन्होंने बात की, सुना और फिर उन्हें प्रयागराज लाकर इस वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। वो कहती हैं, “जब आश्रम आई तो कई रातें बस रोते हुए गुजरीं। लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया है। पर फिर यहां की बहनों ने, स्टाफ ने हमें सहारा दिया। अब यही घर है।”
रामकुमारी आज भी हर सुबह पूजा करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने बेटे-बेटी के लिए भी नहीं। वो प्रार्थना करती हैं कि किसी और मां को वह दिन न देखना पड़े जो उन्होंने देखा। यह सिर्फ रामकुमारी की कहानी नहीं है, तमाम औरतों और बूढ़ों की है।
एक उम्र जो तिरस्कृत हो गई
धनराज वृद्धाश्रम की हर दीवार, हर कोना ऐसी ही कहानियों से गूंजता है, जहां बेटे अपने मां-बाप को त्याग चुके हैं, बेटियां मुंह मोड़ चुकी हैं और रिश्तों की बुनियाद लालच के आगे बिखर चुकी है। यहां की हर सुबह एक नया संघर्ष है खुद को समझाने का, बीते कल को भुलाने का और नए सिरे से जीने का। इन चेहरों पर कोई शिकवा नहीं, बस एक खामोश सवाल है, “क्या मां-बाप होने की यही कीमत है?”
धनराज वृद्धाश्रम के एक शांत कमरे में जहां अक्सर खामोशी चीखती है, वहीं एक चेहरा है जो किसी से कुछ नहीं कहता। सिर्फ दीवारों को देखता है और बीते समय की गूंज में खोया रहता है। यह चेहरा है डॉ. सुमनलता श्रीवास्तव का, जो कभी एक कुशल डॉक्टर थीं, मरीजों का इलाज करती थीं, लोगों की तकलीफें समझती थीं, उनका सहारा बनती थीं। लेकिन आज वही सुमनलता खुद एक सहारे की मोहताज हैं- अकेली, टूटी और भीतर से बिल्कुल खामोश।

एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉ. सुमनलता ने प्रयागराज के कुछ अस्पतालों में सेवाएं दी। उनकी पहचान एक गंभीर और समर्पित चिकित्सक के रूप में थी। लेकिन निजी जीवन में वो जितनी मजबूत दिखती थीं, भीतर से उतनी ही संवेदनशील और अकेली थीं। शादी के दिन जब हर लड़की अपने भविष्य के सपनों में खोई होती है, उस दिन उनके सिर से वह छत भी छिन गई, जिस पर वह भरोसा करना चाहती थीं। विवाह के दिन ही उनके पति का निधन हो गया-यह त्रासदी उन्हें अंदर से हिला गई।
माता-पिता पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। भाई ही थे जो उनके जीवन में सहारा बने रहे। दोनों भाई-बहन एक-दूसरे का ध्यान रखते थे। लेकिन वक्त को शायद यह रिश्ता भी मंजूर नहीं था। एक दिन भाई भी दुनिया से चला गया अचानक। उस दिन के बाद डा. सुमनलता की जिंदगी जैसे ठहर गई। उनकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा।

अकेलापन, दुख और सदमे ने मिलकर उनके ज़ेहन को जकड़ लिया। वो खुद को भूलने लगीं, बोलने लगीं कुछ और, करने लगीं कुछ और। प्रयागराज के एक मानसिक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज तो हुआ, लेकिन जो टूट चुका था, वह जुड़ नहीं सका यानी मानसिक अवसाद जस का तस बना रहा।
वहां से निकलकर वह एक अन्य आश्रम में रहीं, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए बाद में उन्हें धनराज वृद्धाश्रम लाया गया। यहां उन्हें एक अलग कमरे में रखा गया है, ताकि अन्य वृद्ध महिलाओं पर उनकी मानसिक अस्थिरता का असर न हो। वो अक्सर अकेले बैठी रहती हैं, कभी एक ही बात को बार-बार दोहराती हैं, कभी चुपचाप छत को निहारती रहती हैं जैसे किसी की प्रतीक्षा में हों। जब कोई उनसे बात करने की कोशिश करता है तो उनकी जुबान ऐसी बातें कहती है जो किसी को समझ नहीं आतीं कोई टुकड़े-टुकड़े में नाम सुनता है, कोई तारीखें, कोई भूली-बिसरी बातें।
आश्रम की महिलाएं उन्हें बहुत स्नेह से देखती हैं। स्टाफ उनके खाने-पीने, दवाओं और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखता है। लेकिन यह देखभाल उस खालीपन को नहीं भर सकती जो एक भरे-पूरे परिवार के अभाव से उपजा है। डॉ. सुमनलता का कमरा अब अस्पताल की बजाय एक स्मृति कक्ष बन गया है जहां न दवाएं काम करती हैं, न तसल्ली के शब्द। वहां सिर्फ एक स्त्री बैठी है, जो कभी दूसरों की ज़िंदगी बचाया करती थी, लेकिन जब खुद टूट गई, तो कोई उसका हाथ पकड़ने नहीं आया।
उनकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं एक पूरी उम्र का दर्द, एक अकेलेपन की चीख और एक दुनिया से छिन गए भरोसे की गूंज। वृद्धाश्रम अब उनका घर है और यह कमरा उनकी टूटती स्मृतियों की अंतिम पनाहगाह। क्या कोई सुन रहा है इस खामोश डॉक्टर की वेदना? या फिर समाज ने अपनी आदत के मुताबिक उन्हें भी उस कोने में डाल दिया है जहां ‘पागल’ कहकर सब चुप हो जाते हैं?
जब अपने हो गए पराए
बगल के कमरे में बैठी 70 वर्षीय गीता देवी (बदला हुआ नाम) भी कुछ वैसा ही दर्द साझा करती हैं। वृद्धाश्रम में आने के बाद से वह स्वयं को अपेक्षाकृत संतुष्ट और सुरक्षित अनुभव करती हैं। उनके चार संतानें हैं, एक बेटा और तीन बेटियां। परंतु उनकी नातिन को छोड़कर कोई उनका हालचाल लेने नहीं आता। जैसे ही बेटे का नाम लिया जाता है, उनके चेहरे पर रोष की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं।
वह कहती हैं, “ऐसे बेटे के होने या न होने का कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। जिसे अपना पेट काटकर पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, उसी ने आज बुढ़ापे में मुंह मोड़ लिया।” गीता देवी अब वृद्धाश्रम को ही अपना घर मान चुकी हैं। उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ये आश्रम की दीवारें ही अब उनका संसार हैं और यहां रहने वाले लोग ही उनके अपने।
प्रयागराज की 68 वर्षीय लता (बदला हुआ नाम) की कहानी थोड़ी भिन्न अवश्य है, परंतु पीड़ा कम नहीं है। वह बताती हैं, “पच्चीस साल पहले पति का देहांत हो गया। बाद में बेटा भी एक दुर्घटना में चल बसा। उसकी शादी तक नहीं हुई थी। बेटे की मौत के बाद मैं भीतर से पूरी तरह टूट गई।” परिवार ने जब साथ नहीं दिया, तब वृद्धाश्रम ने उन्हें अपनाया। वह बताती हैं कि बेटे के एक मित्र ने उस कठिन समय में उनका साथ दिया, अपने पास कई महीनों तक उन्हें शरण दी। वह अब भी उनसे मिलने आते हैं और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं।”
धनराज वृद्धाश्रम में 71 वर्षीय मोहन राय की जीवनकथा भी कम दर्दनाक नहीं है। वह अपनों की उपेक्षा और छल का शिकार हुए हैं। उनका बेटा उन्हें यह कहकर घर से बाहर लाया कि उसे कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदना है। फिर उन्हें सड़क पर छोड़कर चुपचाप चला गया। मोहन राय घंटों अपने बेटे का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वह लौटकर नहीं आया। अंततः किसी भले व्यक्ति ने उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचाया।

धनराज वृद्धाश्रम में इस समय आठ महिलाएं और पांच पुरुष रहते हैं, जिनकी देखभाल बिना किसी सरकारी सहायता के की जा रही है। कुछ वृद्धों को साझा कमरों में रहना पड़ता है, जबकि कुछ को उनकी आवश्यकता और मानसिक स्थिति के अनुसार अलग कमरे दिए गए हैं। यहां दिन की शुरुआत प्रार्थना और पूजा से होती है। इसके बाद हल्का नाश्ता दिया जाता है और दोपहर व रात्रि में सादा भोजन। संध्या के समय महिलाएं एकत्र होकर बातें करती हैं। कुछ पुरानी यादें बांटती हैं, कुछ चुपचाप समय का बहाव देखती रहती हैं।
आश्रम की संरक्षक डॉ. सुजाता पांडेय बताती हैं कि यह समूची व्यवस्था जनसहयोग, दान और कुछ निजी संसाधनों के माध्यम से संचालित की जा रही है। वह कहती हैं, “सरकार से बहुत अधिक अपेक्षा नहीं है, किंतु पीड़ा इस बात की है कि अब समाज भी बुज़ुर्गों को बोझ समझने लगा है। इस आश्रम में रहने वाली कई महिलाएं महीनों तक अपने बच्चों की राह देखती हैं, लेकिन कोई नहीं लौटता। हर नया आगमन एक नया आंसू लेकर आता है। कुछ महिलाएं तो पहले कई सप्ताह तक किसी से बात भी नहीं करतीं। फिर धीरे-धीरे यहीं को अपना घर मानने लगती हैं।”
सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सुजाता आगे कहती हैं, “हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इन बुज़ुर्ग माताओं के चेहरों पर कुछ पल के लिए मुस्कान ला सकें और उनके दुख कुछ हल्के कर सकें। एक मां ही होती है जो कभी प्यार से गले लगाती है तो कभी डांटती है, पर इस आश्रम में कई मांएं ऐसी हैं जो कुछ भी कहती नहीं। यहां वे स्त्रियां भी रहती हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। कई ऐसे लोग भी यहां आते हैं जिनकी ज़िंदगी में अब कोई बड़ा-बूढ़ा नहीं है। वे यहां इन माताओं में अपने स्नेह और अपनापन की तलाश करते हैं, ताकि दोनों ओर की खाली जगहें थोड़ी-सी भर सकें।”

यह केवल एक वृद्धाश्रम की कथा नहीं, बल्कि उस सामाजिक सच्चाई की एक मर्मांतक झलक है, जिसे हम जाने-अनजाने नज़रअंदाज़ कर देते हैं। रिश्तों की ऊष्मा अब स्वार्थ की तराजू पर तौली जाती है। जिन माता-पिता के चरणों में कभी स्वर्ग देखा जाता था, आज वही मां-बाप अपने ही बनाये संसार से बेगाने होकर एकाकी जीवन जीने को विवश हैं-आश्रित होकर उस दुनिया पर, जिसे उन्होंने अपने श्रम, स्नेह और सपनों से रचा था।
वृद्धाश्रम में महिलाओं की देखरेख कर रहे शुभम पांडेय कहते हैं, “जब कोई समाज अपने बुज़ुर्गों के प्रति संवेदनशीलता खो देता है, तब वृद्धाश्रम केवल एक सुविधा नहीं रह जाते, वे रिश्तों को बचाने की आखिरी कोशिश बन जाते हैं। भारत वह देश है जहां एक समय कहा जाता था-‘मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः।’ पर आधुनिकता की होड़ में हमने वह आंगन ही खो दिया, जहां बुज़ुर्गों की कहानियों की छांव में बचपन सोता था। धनराज वृद्धाश्रम के हर कोने में ‘घर’ शब्द की गर्माहट छिपी है। भले ही अपने उन्हें छोड़ गए हों, लेकिन हम उन्हें एक परिवार की तरह अपनाते हैं।”
धनराज वृद्धाश्रम की दीवारों के भीतर कई अनकही कहानियां दबे स्वर में कुछ पूछती हैं और कुछ बस मौन रहकर सब कह जाती हैं। वृद्धाश्रम की काउंसलर पूजा अस्थाना कहती हैं, “यहां रह रहे बुज़ुर्गों की ज़िंदगी समाज के उस आईने की तरह है, जो दिखाता है कि बुज़ुर्गों को सबसे अधिक जिस चीज़ की आवश्यकता है-वह है सहारा, न कि सिर्फ सम्मान। और जब वह सहारा भी छिन जाए, तो एक छोटा-सा कमरा ही उनका संपूर्ण संसार बन जाता है। शायद अब समय आ गया है कि हम गंभीरता से सोचें, क्या हम आने वाली पीढ़ियों को ऐसा समाज सौंपने जा रहे हैं, जहां बुढ़ापा एक बोझ माना जाएगा, या एक गरिमा से भरी अवस्था मानी जाएगी? “
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में बुज़ुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में बुज़ुर्गों की संख्या 7.7 करोड़ थी, जो कुल आबादी का लगभग 7.5 प्रतिशत थी। यह संख्या समय के साथ और भी बढ़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के वार्षिक कार्य योजना (2022-23) के अनुसार, वर्ष 2021 में बुज़ुर्गों की संख्या लगभग 14 करोड़ तक पहुंच चुकी थी यानि अब वे कुल जनसंख्या का 10 प्रतिशत से अधिक हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इतने बड़े वर्ग को केवल आंकड़ों में गिनते रहेंगे या उनके जीवन में कुछ उजाले भी भरेंगे?
समाज की आत्मा पर एक प्रश्नचिन्ह
जाने-माने शिक्षाविद एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के प्रो. आदेश कुमार मौर्य कहते हैं, “वृद्धाश्रम का अस्तित्व हमारे समाज के लिए बेहद शर्मनाक है। यह हमारे पारिवारिक और सांस्कृतिक संस्कारों में आई चूक का परिणाम है, लेकिन अब इसकी सच्चाई से मुंह मोड़ना भी संभव नहीं। यह हमारी सामाजिक विवशता बन चुकी है। आज तिरस्कार, घृणा, बैर और लालच जीवन के केंद्र में हैं। जिन्होंने कभी हमारी ऊंगलियां पकड़कर हमें चलना सिखाया, वही बुज़ुर्ग आज उपेक्षा और तिरस्कार का सामना कर रहे हैं। यह कटु यथार्थ है कि जिन बुज़ुर्गों ने हमारे लिए अपने जीवन की सबसे कीमती पूंजी समय, प्रेम और परिश्रम न्योछावर किया, आज वे ही अकेलेपन की सज़ा काट रहे हैं।”
प्रो.आदेश मौर्य यह भी कहते हैं कि, “बुज़ुर्गों के गरिमापूर्ण जीवन के लिए कई कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। परंतु कभी लोकलाज का भय और कभी जागरूकता की कमी उन्हें अपनी ही संतान की प्रताड़ना सहने के लिए मजबूर कर देती है। यह बात केवल किसी एक व्यक्ति या परिवार की नहीं, बल्कि उस पूरे समाज की है जो आधुनिकता की चमक में अपने जड़ों से कटता जा रहा है। वह मानते हैं कि आज का सामाजिक परिवर्तन शहरीकरण, आत्मकेंद्रित जीवनशैली और पारिवारिक मूल्यों में गिरावट का सीधा परिणाम है।”
वह कहते हैं, “अब ‘करियर’ और ‘स्पेस’ जैसे शब्द रिश्तों से भी बड़े हो गए हैं। जहां कभी मां-बाप घर की नींव माने जाते थे, वहीं आज वे एक जिम्मेदारी या बोझ समझे जाने लगे हैं। ‘माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007’ जैसे कानून का अस्तित्व होने के बावजूद, जागरूकता की कमी और सामाजिक शर्म के कारण बुज़ुर्गों को न्याय तक नहीं मिल पाता। अगर कोई बुज़ुर्ग अपने ही बच्चों द्वारा उपेक्षित हो रहा है, तो उसे कानून का सहारा अवश्य लेना चाहिए। अगर समाज में कोई देख रहा है कि किसी बुज़ुर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, तो वह भी उसे कानूनी सहायता दिलाकर उसकी गरिमा की रक्षा कर सकता है।”
प्रो.आदेश यह भी कहते हैं कि, “बुजुर्गों की उपेक्षा केवल एक सामाजिक प्रश्न नहीं है, यह आत्मा की पुकार है कि क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं, जहां बुढ़ापा बोझ बन चुका है? क्या हम अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि जब माता-पिता वृद्ध हो जाएं, तो उन्हें एक कोने में छोड़ देना ही समाधान है? यह समय है सोचने का और बदलने का। यह समय है उस बचपन की स्मृतियों को फिर से जीने का, जब मां की थपकी और पिता की सलाह जीवन का सबसे कीमती सहारा होती थी। अगर आज हमने अपने बुज़ुर्गों की अनदेखी की, तो कल हमारी कहानी भी किसी वृद्धाश्रम की दीवारों में दब जाएगी, बिना किसी नाम के और बिना किसी पहचान के।”
बुज़ुर्गों की उपेक्षा पर सज़ा
“मैंटिनेंस एंड वेल्फेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटिजंस एक्ट” एक ऐसा कानूनी प्रावधान है, जो हमारे समाज के उन मौन पीड़ितों की आवाज़ बनता है, जिनके बालों की सफेदी ने हमें कभी जीवन जीने का तरीका सिखाया था। यह कानून साफ कहता है कि संतान या रिश्तेदार बुज़ुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए बाध्य हैं। उनकी सेहत, इलाज, भोजन और निवास जैसी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करना उनका नैतिक ही नहीं, कानूनी दायित्व भी है। अगर कोई इस ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़ता है, तो उसे सज़ा भुगतनी होगी। दोषी को तीन महीने तक की जेल या पांच हज़ार रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
कड़वी सच्चाई यह है कि अक्सर संपत्ति हस्तांतरित होते ही बच्चों और रिश्तेदारों का व्यवहार बदल जाता है। जिन हाथों ने कभी सिर पर स्नेह का आशीर्वाद रखा था, उन्हीं हाथों को झुकाकर बुज़ुर्गों को बेइज़्ज़ती का सामना करना पड़ता है। पर राहत की बात यह है कि अगर कोई बुज़ुर्ग अपनी संपत्ति किसी संतान या रिश्तेदार को सौंप चुका है और वे अब उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो यह संपत्ति का ट्रांसफर रद्द किया जा सकता है। यानी संपत्ति फिर से उसी बुज़ुर्ग के नाम हो सकती है। इसके बाद बुज़ुर्ग चाहें तो ऐसे नालायक बेटा-बेटियों को संपत्ति से बेदखल भी कर सकते हैं।
इस कानून की सबसे बड़ी ताक़त यह है कि यह केवल कागज़ों तक सीमित नहीं है। यह बुज़ुर्गों की गरिमा की रक्षा करता है। यदि कोई बुज़ुर्ग माता-पिता आर्थिक रूप से असमर्थ हैं और उनकी संतान या निकट संबंधी उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो वे ट्राइब्यूनल में जाकर भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं।
बीएचयू के लॉ फैकल्टी के शिक्षक प्रो. मयंक प्रताप सिंह बताते हैं, “मैंटिनेंस एंड वेल्फेयर ऑफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटिजंस एक्ट” के तहत यदि ट्राइब्यूनल किसी संतान को भरण-पोषण का आदेश देता है, तो उस आदेश का पालन एक महीने के भीतर अनिवार्य है। यहां तक कि वे बुज़ुर्ग जिनकी कोई संतान नहीं है, वे भी अपनी संपत्ति के उत्तराधिकारी से भरण-पोषण की मांग कर सकते हैं। देश के अधिकतर जिलों में “मैंटिनेंस ट्राइब्यूनल” और “अपील ट्राइब्यूनल” जैसे तंत्र स्थापित किए गए हैं, जहां बुज़ुर्गों की शिकायतों पर 90 दिनों के भीतर फैसला दिया जाना अनिवार्य है। अगर वे ट्राइब्यूनल के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो वे अपील भी कर सकते हैं।”

“कानून केवल बेटे-बेटियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बालिग पोते-पोतियों की भी यह नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने दादा-दादी या नाना-नानी की देखभाल करें। चाहे संतान जैविक हो, सौतेली हो या गोद ली हुई, कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। हर किसी का कर्तव्य है कि माता-पिता के लिए पर्याप्त भोजन, वस्त्र, रहने की व्यवस्था और इलाज जैसी आवश्यकताएं पूरी की जाएं।”
प्रो.मयंक यह भी कहते हैं, “यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि “माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक देखभाल एवं कल्याण अधिनियम, 2007” के अलावा, भारतीय दंड संहिता यानी सीआरपीसी में भी बुज़ुर्गों के अधिकारों की रक्षा की गई है। सीआरपीसी की धारा 125 (1)(D) और “हिंदू एडॉप्शन एंड मैंटिनेंस एक्ट, 1956” की धारा 20 (1 और 3) के तहत भी माता-पिता अपने बच्चों से भरण-पोषण पाने के हक़दार हैं। यदि कोई संतान अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती, तो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट उसे भरण-पोषण देने का आदेश दे सकता है।”
“यह केवल कानून नहीं, बल्कि उन बूढ़े कांपते हाथों की ढाल है, जिन्होंने एक समय हमारी ऊंगलियां पकड़कर हमें जीवन चलाना सिखाया था। यह व्यवस्था उन्हें फिर से जीने की हिम्मत देती है, सिर्फ कानूनी सुरक्षा नहीं, आत्मसम्मान लौटाने का माध्यम बनती है। अब यह हम पर है कि हम इस सुरक्षा कवच का उपयोग अपने बुज़ुर्गों की गरिमा को बचाने में करें या समाज को उन वृद्धाश्रमों की ओर धकेलते रहें, जिनके हर कोने में उपेक्षा की टीस छिपी होती है।”
(आराधना पांडेय स्वतंत्र पत्रकार हैं और प्रयागराज में रहती हैं)