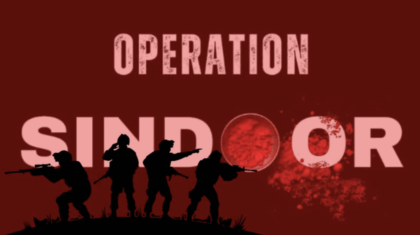भारत में पिछले कई सालों से साधारण बातचीत से लेकर गंभीर चर्चा और ज्ञान-विमर्श यानी समाज में लगभग सर्वत्र विचित्र किस्म के वितंडा का इस्तेमाल होने लगा है। इससे सामने बैठा आदमी लाजवाब नहीं होता है। लाजवाब इसलिए नहीं होता है कि सामनेवाले को कोई जवाब देना ही नहीं होता है, सच पूछा जाये तो वितंडा का कोई प्रयोजनीय जवाब होता भी नहीं है। वितंडा मूल रूप से अपने मूल और जरूरी संदर्भ से काटकर और दूसरे किसी भी मिलते-जुलते गैर-जरूरी संदर्भ से जोड़कर पैदा किया जाता है। इस तरह से मीडिया की सांध्यकालीन सार्वजनिक बातचीत शायद ही कभी साफ-साफ निष्कर्ष पर पहुंच पाती है। अफवाह और शंका का कोई तार्किक समाधान शायद ही कभी निकलता है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य के स्वतंत्र होने का महत्त्वपूर्ण लक्षण होती है। अभिव्यक्ति की योग्यता मनुष्य की मौलिक योग्यता और अभिव्यक्ति की शक्ति मनुष्य की मौलिक शक्तियों में प्रमुख है। अभिव्यक्ति के कई साधन होते हैं। इनमें से भाषा एक प्रमुख साधन है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई सार्थकता ही नहीं बन सकती है यदि श्रुति, यानी सुनने की मनःस्थिति समाज में न बचे या बहुत कम हो जाये! अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने-आप से श्रुति की बाध्यता नहीं बना सकती है। आज समाज और व्यवस्था में एकदम-से गरीब लोगों की ही नहीं, सम्मानजनक ढंग से ‘खाते-पीते’ लोगों की भी, संवेदनशील ढंग से, सुननेवाला कभी-कभी ही मिलता है। ‘खाते-पीते’ लोग व्यवस्था के व्यवहार से मिली पीड़ा को अधिक महसूस करते हैं। लेकिन दुखद और असहाय-सी कर देनेवाली स्थिति यह है कि ‘खाते-पीते’ जीने का जुगाड़ खो चुके लोगों के साथ ‘खाते-पीते’ लोगों का संवाद, संबंध और सरोकार ही जैसे खो गया है! अहंकार सिर्फ सत्ता से पैदा नहीं होता। ‘खाते-पीते’ हुए जीने के जुगाड़ से भी पैदा होता है। कमजोर नागरिक संबंध लोकतंत्र का सब से कमजोर पक्ष होता है।
मनुष्य के मनुष्य बनने में भाषा की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण रही है। अब, भाषा का इस्तेमाल कहने से अधिक छिपाने के लिए हो रहा है। जीवन के खुरदुरे यथार्थ का दर्द दहाड़ती भाषा के सामने हकलाने लगता है! आदमी जो कहता है, उसका मतलब उस के कहे के अलावा भी कुछ होता है। यह जो ‘अलावा कुछ’ होता है, कई बार वही अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराने का एक उदाहरण जरूरी लग रहा है। अकसर, लोग कहते हैं, “चोर की दाढ़ी में तिनका”। चोर और उसकी दाढ़ी दोनों को अप्रस्तुत यानी अनुपस्थित मानकर कहता है, चोर वहां हुआ तो वह अपने-आप प्रस्तुत हो जाता है।
अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराने की ‘अन्योक्ति’ की समर्थ शैली का इस्तेमाल साधारण आदमी की जरूरत की आवाज को धुंधला करने के गलत इरादे से किया जाना बढ़ता गया है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे आदमी अब भाषा से घिर गया है। जीवन में सत्य, शांति और सद्भाव की प्रतिष्ठा में भाषा बहुत कमजोर पक्ष बनकर रह गई है।
राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है, कुछ लोग पहले सुपरमैन बनना चाहते हैं, फिर देवता बनने की बात करने लगते हैं, जबकि भगवान अपने को ‘विश्व-रूप’ कहते हैं। संघ प्रमुख के बयान पर ‘गंभीर चर्चा’ होना तय है। कुछ लोगों में यह प्रवृत्ति होती है। यह सामान्य बात है। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत किस की बात कर रहे हैं! कहनेवाले ने कह दिया। सुननेवाले ने सुन लिया। समझनेवाले ने समझ लिया। समझ लिया और ठीक ही समझा। लेकिन जिन्हें इस ‘समझ’ से अ-सुविधा हो सकती है, वे इस समझ को बदलने लगते हैं। इस तरह से भिन्नार्थ समझानेवालों को भी स्पष्टता से रोका नहीं जा सकता है। क्योंकि, यह सामान्य प्रवृत्ति कई व्यक्तियों पर लागू की जा सकती है! इस अन्योक्ति शैली का प्रयोग दो-तीन कारणों से होता है। पहला कहनेवाले के मन में कोई स्पष्ट लक्ष्य न हो।
दूसरा जिस के बारे में कहा जा रहा है उसे लज्जित या प्रभावित होने से बचाने के लिए सार्वजनिक रूप से उस पर कोई आरोप लगाना न चाहता हो। तीसरा और सब से बड़ा कारण यह होता है कि जिसके बारे में जो कहा गया है, उसके बारे में सीधा कहने का साहस न हो या पकड़ में आने से अपने बचाव का रास्ता उपलब्ध रखकर कहना चाहता हो! इसके अलावा अन्योक्ति शैली अपनाने के मिले-जुले कारण भी हो ही सकते हैं! सवाल यह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्यों अन्योक्ति शैली में यह सब कहा! सार्वजनिक रूप से यह सब कहने की जरूरत ही क्या थी! कहना जरूरी था तो अकेले में या सीमित दायरे में कहते। सार्वजनिक रूप से कहना जरूरी था तो साफ-साफ नाम लेकर कह सकते थे। नहीं कहा, तो लोग अपने-अपने तरीके से मतलब निकालते रहें, उन की बला से!
भारतीय जनता पार्टी के नेतागण राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। क्या राहुल गांधी का तात्पर्य वैसा ही था, जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता कह रहे हैं! यदि ऐसा है तो यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसकी जांच-पड़ताल होना जरूरी है। यदि राहुल गांधी का तात्पर्य वैसा नहीं है, तो फिर इसे फंसाने के उद्देश्य से राहुल गांधी के खिलाफ ‘राजनीतिक अफवाह’ घोषित किया जाना चाहिए। इस तरह के मामलों पर कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के अफवाह से उकसावे में पड़नेवाले तत्व को ‘किक’ मिल जाने की आशंका को भी बिल्कुल निराधार नहीं कहा जा सकता है। इस तरह राजनीतिक बतकुच्चन या बकैती का क्या मतलब! मतलब है मूल मुद्दों को गैर-मुनासिब राजनीतिक उलझाव में डालना। नागरिक समाज के अगुआ लोगों को सावधानी से इस पूरी प्रक्रिया को समझना चाहिए। ऐसे मामलों में ‘निष्पक्ष पक्षपात’ के परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के बड़े ‘प्रवक्ता’ राहुल गांधी, कांग्रेस, वाम और मुसलमान की किसी मिलीभगत की तरफ बार-बार इशारा करते रहते हैं। ऐसा करने के पीछे उन का इरादा एक ही साथ ‘चार शिकार’ करना है। जाहिर है कि ये ‘चार शिकार’ ऐसे हैं जिन से अंतिम संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और उसकी दक्षिण-पंथी राजनीति को करना ही होगा। ऐसा लगता है कि यह ‘राहुल गांधी, कांग्रेस, वाम और मुसलमान’ को एक सेट में डालना, फिर उन के खिलाफ एक साथ घृणा का वातावरण बनाकर उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता समाप्त करने की किसी नाजायज मुहिम का हिस्सा है। पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र यानी न्याय-पत्र में मुस्लिम लीग की छाप देखने-दिखाने की कोशिश की गई। यह दाव चला नहीं। अब इस सेट में ‘वाम’ को फिर से डालकर राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस राजनीतिक प्रयोग की सफलता से विभिन्न स्तर के मतदाताओं को अपने पक्ष में समेट लेने में वह कामयाब हो जायेगी।
इस बार के आम चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी संसद में सबसे बड़ा संसदीय दल तो बन गई, लेकिन अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। सरकार बनाने के लिए दस साल से अनमने पड़े राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहारे की जरूरत पड़ गई। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के हाथ में सरकार के अस्तित्व की चाभी पड़ गई। नरेंद्र मोदी का एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ मेल-जोल भरे, विश्वसनीय, सम्मानजनक और अच्छे राजनीतिक संबंध नहीं रहे हैं। अभी भी मेल-जोल से अधिक तोल-मोल के ही संबंध हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सब के साथ हिलमिल रहने की शैली भूल गई। हालांकि राम-भक्तों को सावधान खुद राम-भक्त तुलसीदास ने ही किया था, ‘तुलसी या संसार में भांति-भांति के लोग। सबसे हिलमिल चलियो नदी नाव संयोग।’
एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन से सरकार तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई। लेकिन इन का रिश्ता! तेरा-मेरा रिश्ता क्या! बेर-केर का संग! इधर बेर के डाल डोले, उधर केर के पत्ते फटे! सर्वसत्तावादी नरेंद्र मोदी को तो अब ‘सत्ता में सहयोगी लेकिन राजनीति में विरोधी’ सत्ता-समर्थकों का सहारा लेना पड़ा है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के प्रमुख, जब-न-तब ‘उपदेशित’ कर देते हैं! जरा-सा कमजोर क्या पड़े कि अपनी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी वाणी में दम लौट आया है। यह तो नरेंद्र मोदी की राजनीतिक बुद्धि का ही कमाल था कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का नेता चुने जाने के चक्कर और टक्कर में पड़े बिना, आनन-फानन में खुद को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के संसदीय दल का नेता चुनवा लिया।
भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच जैसे आनुषंगिक संगठनों की भी सांगठनिक चेतना जैसे नई हवा-पानी पाकर जाग उठी है! राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के अन्य नेतागण के विभिन्न बयान तो अपनी जगह झलक दिखलाते ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी खीझ राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के नेताओं पर निकालते रहते हैं। यहां तक तो ठीक, लेकिन खीझ निकालते-निकालते बतकुच्चन या बकैती में उस जगह पहुंचना ठीक नहीं, जहां सचमुच बड़ा खतरा हो सकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का कांग्रेस-मुक्त भारत का नारा तो कांग्रेस के राजनीतिक बहिष्कार से ही शुरू हुआ था न।
गंगा-जमुनी संस्कृति तो भारत की मूल शक्ति है। लेकिन यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि बहिष्करण की प्रवृत्ति भी भारत के एक अंश की ‘पारंपरिक-चेतना’ में सक्रिय रहती आई है। कहना न होगा कि बहिष्कारिणी प्रवृत्ति शक्ति से जुड़कर, भारत की गंगा-जमुनी संस्कृति में जहर घोलने पर आमादा हो जाती है। कभी इस बहाने तो, कभी उस बहाने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की हवा बनाने की कोशिश होती रहती है। लेकिन यह ऊपरी बात है। यह बात मजहबी परिप्रेक्ष्य के कारण तुरंत आंख में पड़नेवाली, तीखी और अधिक चुभन भरी होती है। असल में इन दिनों इस व्यवस्था में समस्त गरीब लोगों का आर्थिक बहिष्कार हो रहा है। कभी अतिक्रमण हटाने के नाम पर, तो कभी शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर। ऐसा लगता है कि गरीब लोगों को सभ्यता की चौहद्दी से ही बहिष्कृत कर दिया जायेगा! हालात ऐसे हैं, जैसे घर के ‘कुछ लोगों’ के लिए सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री जुटाते-जुटाते बाकी लोगों के लिए आटा का ही जुगाड़ बिगड़ जाये।
भारत के एक अंश की ‘पारंपरिक-चेतना’ में सक्रिय बहिष्करण की प्रवृत्ति और शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने तो 4 जनवरी 1925 को ‘बहिष्कृत हितकारिणी संघटना’ की स्थापना की थी। 27 सितम्बर 1925 को डॉ केशव बलिराम हेडगेवार ने ब्रिटिश हुकूमत की नजर से बचने के लिए राजनीतिक क्रिया-कलाप से परहेज करते हुए “अस्पृश्यता निवारण एवं हिंदुओं के सैनिकीकरण” के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ की स्थापना की थी। ‘बहिष्कृत हितकारिणी संघटना’ ने अपना महत्त्वपूर्ण काम किया और इस की चेतना को संवैधानिक प्रावधानों में जगह भी मिली। राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ ने “हिंदुओं के सैनिकीकरण” का काम तो पूरी तत्परता से किया, लेकिन व्यापक समाज में “अस्पृश्यता निवारण” और गैरबराबरी को दूर करने के लिए क्या किया यह तो वही जाने! कहने का आशय यह है कि बहिष्करण की नीति, कोई नई नीति नहीं है। हां, बहिष्करण की नीति के खिलाफ जनता के संघर्ष में साथ ‘खाते-पीते’ लोगों के होने की नीति में अ-भूतपूर्व शिथिलता कुछ हद तक नई बात जरूर है।
उम्मीद की जानी चाहिए कि भाषा से घिरे लोगों में हर प्रकार की बहिष्करण की नीति के खिलाफ संघर्ष करते हुए लोगों के साथ खड़े होने का हौसला है। राजनीतिक अफवाह नहीं, न्यायपूर्ण शांति और सद्भाव सब का हक है। भाषा के घेराव के अंधकार से बाहर लोकतंत्र का भरपूर उजाला है। बस ‘खाते-पीते’ लोगों का भाषा के घेराव से बाहर निकलना जरूरी है।
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)