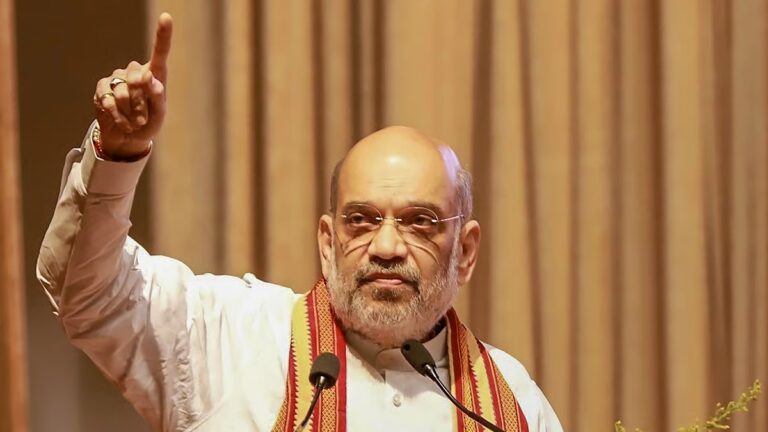इस लेख का शीर्षक आपको अटपटा लग सकता है। भारत के कुछ खास किस्म के बुद्धिजीवियों को इन दिनों लिबरल कहने-कहलाने का चलन बढ़ा है। हम लोग जब विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे तो ऐसे लोगों को आमतौर पर प्रगतिशील बुद्धिजीवी कहा जाता था।ऐसे लोगों का भला संघ-विचाधारा से जुड़े केरल के शीर्ष भाजपा नेता ओ. राजगोपाल से भला क्या रिश्ता हो सकता है? लेकिन रिश्ता है। प्रकृति में होने वाली क्रिया-प्रतिक्रिया की तरह समाज की घटनाओं का भी एक-दूसरे से रिश्ता होता है, चाहे वे जितना अलग-अलग दिखें। देश के एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार में छपे अपने इंटरव्यू में केरल के शीर्ष भाजपा नेता ओ राजगोपाल ने एक सवाल के जवाब में अपने सूबे की भाजपा राजनीति की चुनौतियों पर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उनसे पत्रकार ने सवाल कियाः ‘भाजपा केरल की राजनीति में अपनी जगह बनाने में विफल क्यों रही है?’ ओ. राजगोपाल ने इस सवाल का जवाब दियाः केरल अलग ढंग का राज्य है। यहां 90 फीसदी साक्षरता है (राजगोपाल ने कम बताया, आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यह 96.2 फीसदी है)। लोगों को लगता है, वे तर्कशील हैं। राज्य में 55 फीसदी हिन्दू और 45 फीसदी अल्पसंख्यक हैं। ये पहलू असर डालते हैं। इसीलिए केरल की किसी अन्य प्रदेश से तुलना नहीं हो सकती। फिर भी भाजपा यहां धीरे-धीरे बढ़ रही है।’ (इंडियन एक्सप्रेस, 23मार्च,2021).
ओ राजगोपाल कोई मामूली नेता नहीं हैं। भारतीय संसद को मैंने लंबे समय तक ‘कवर’ किया। इस नाते एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनसे मिलने और बातचीत के मौके भी मिले। मंत्री के तौर पर वह बहुत सक्रिय रहते थे। केरल के अब तक के संसदीय इतिहास में वह भाजपा के इकलौते विधायक हैं। 2016 के चुनाव में उन्होंने तिरुवनंतपुरम की नेमम सीट से चुनाव जीता था। वामपंथियों के गढ़ केरल में उनका चुनाव जीतना असाधारण घटना थी। केंद्र की वाजपेयी सरकार में वह केंद्रीय संसदीय राज्यमंत्री भी थे। उन दिनों वह राज्यसभा से सांसद थे। भाजपा के लिए वह इतने मूल्यवान थे कि पार्टी ने उन्हें किसी अन्य प्रदेश से निर्वाचित कराकर राज्यसभा में भेजा था। वह यूपी-बिहार-मध्य प्रदेश के ज्यादातर भाजपा नेताओं से अलग नजर आते हैं। मैंने उन्हें संसद में कभी उत्तेजित या असंयत होते नहीं देखा। एनडीए-1 दौर में वह एक शिष्ट और सहज भाव वाले मंत्री माने जाते रहे। राजगोपाल जैसा बड़ा भाजपा नेता अगर केरल में अपनी पार्टी की प्रभावी-राजनीतिक मौजूदगी न होने के कारणों पर ऐसा कोई बयान देता है तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।
उनके बयान का निहितार्थ है कि केरल चूंकि पढ़े-लिखे और समझदार लोगों का प्रदेश है। इसलिए वहां भाजपा का विस्तार यूपी-बिहार-मध्य प्रदेश आदि जैसे प्रदेशों की तरह आसानी और जल्दी से नहीं हो पा रहा है। आबादी में भी विविधता कुछ ज्यादा है। यह सब मुश्किलें हैं। पर धीरे-धीरे भाजपा बढ़ रही है। राजगोपाल साहब ऐसा दावा कर रहे हैं। दिलचस्प बात है कि केरल में संघ-भाजपा दशकों से काम कर रहे हैं। कुछ जिलों में उनकी सांगठनिक ताकत भी बढ़ी है। पर राज्यव्यापी स्तर पर उनके साथ आज तक बड़ी जनशक्ति नहीं जुटी। मेरे हिसाब से भी इसके पीछे बड़ा कारण केरल के समाज का अपेक्षाकृत शिक्षित और समावेशी होना है। एक पत्रकार के रूप में मैने केरल की राजनीतिक गतिविधियों, खासकर चुनाव के दौरान को भी दो-तीन बार ‘कवर’ किया है, इसलिए अपने निजी अनुभव की रोशनी में कहना चाहूंगा कि राजगोपाल जी की साक्षरता वाले पहलू के साथ अपेक्षाकृत समावेशी समाज की बात भी जोड़ना चाहिए। साक्षरता और अपेक्षाकृत समावेशी होना केरल की खास विशिष्टता है। यूपी-बिहार-मध्य प्रदेश या पूरे हिंदी-भाषी क्षेत्र को देखें तो इसके मुकाबले निश्चय ही केरल बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वर्ण-व्यवस्था का कर्मकांडी-विभाजन ही नहीं, उसका वैचारिक आतंक भी वहां नहीं दिखाई देता। इसी केरल में एक समय वह यूपी-बिहार से भी ज्यादा क्रूर रूप में मौजूद था।
केरल के समाज और राजनीति का यह विशिष्ट चेहरा तीन कारणों से विकसित हुआ। वहां के सामाजिक सुधार आंदोलनों, ईसाई मिशनरियों और फिर समाज और शासन में कम्युनिस्टों के प्रभाव चलते। इनमे दो का ज्यादा असर रहा-सामाजिक सुधार आंदोलनों और वामपंथियों का। वामपंथियों को वहां के सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भी प्रभावित किया। यहां तक कि एक दौर के कुछ राजा-महराजा भी इस सुधार आंदोलनों से प्रभावित हुए। नारायण गुरू(1856-1928) और अय्यनकाली(1863-1941) दो ऐसे बड़े समाज सुधारक एवं बौद्धिक व्यक्तित्व उभरे, जिनकी सामाजिक सोच ने केरल को बदलने में बहुत अहम् भूमिका निभाई। ये दोनों पिछड़े और अत्यंत उत्पीड़त समाजों में पैदा हुए और अपनी मानवतावादी शिक्षाओं से समाज को नयी दिशा दी। जिस केरल को पहली बार देखकर स्वामी विवेकानंद ने एक पागलखाने की संज्ञा दी और वहां के समाज में जात-पांत आदि रोष प्रकट किया, वह केरल अपने समाज-सुधार आंदोलनों के प्रभाव में अंदर ही अंदर बदलता रहा। उसका नतीजा कुछ समय बाद दिखने लगा। एक समय केरल में शासकीय किस्म की नौकरियां सिर्फ ब्राह्मणों को मिलती थीं। इसमें भी तमिल ब्राह्मणों की बहुतायत थी। ट्रावनकोर राज में पहली बार सन् 1891 में उत्पीड़ित समाजों ने आरक्षण के लिए आंदोलन छेड़ा। बाद के दिनों में इड़वा या ईषव, मुस्लिम और ईसाई लोगों के एक हिस्से ने सेवा के अलावा राजनीतिक-प्रशासनिक निकायों में भी हिस्सेदारी की मांग की। ऐसे आंदलनों को उस दौर के कई समाज-सुधारकों, लेखक और बुद्धिजीवियों का भी समर्थन मिला। इन आंदोलनों का ही असर था कि ट्रावनकोर राज में पहली बार 14जून, 1936 को आरक्षण लागू होने का ऐलान किया गया। जातियों-समुदायों की संख्या के हिसाब से उनके स्थान तय किये जाने लगे। एक कमेटी की रिपोर्ट के बाद सन् 1952 में ट्रावनकोर-कोचीन स्टेट में 45 फीसदी आरक्षण का ऐलान हुआ। इसमें ओबीसी के लिए 35 फीसदी आरक्षण था और शेष दलितों को। ओबीसी में आज के हिन्दू समझे जाने वालों के अलावा मुस्लिम और ईसाई समुदायों के पिछड़े लोग भी लाभार्थी के तौर पर शामिल किये गये थे। बाद के दिनों में सकारात्मक कार्ररवाई के स्वरूप को और सुसंगत बनाया जाता रहा। इस पृष्ठभूमि की चर्चा मैंने इसलिए कि हिंदी-भाषी क्षेत्र के अंग्रेजी में लिखने-पढ़ने वाले बुद्धिजीवियों, खासकर ‘लिबरल’ कहलाने वालों को यह सच बताया जा सके कि दक्षिण के राज्यों-केरल और तमिलनाडु आदि में समाज के समावेशी स्वरूप का विकास वहां के समाज सुधार आंदोलनों, उसमें लेखकों-बुद्धिजीवियों की सक्रिय भूमिका और सकारात्मक कार्रवाई के प्रशासकीय कदमों से संभव हुआ।
बाद के दिनों में वामपंथी आंदोलनों का प्रभाव बढ़ा। स्वतंत्रता के बाद जब केरल में कम्युनिस्टों की सरकार बनी तो उनका सबसे प्रमुख एजेंडा था-भूमि सुधार और शिक्षा सुधार। उन्हें लगा कि इन दो बड़े कदमों से वे समाज में गैर-बराबरी को कम कर सकते हैं और साथ में समाज को सभ्य, सुंदर और समावेशी भी बना सकते हैं। इन कदमों के आगे बढ़ाने के प्रयासों के क्रम में ही ईएमएस नंबूदिरिपाद की अगुवाई वाली पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार को सन् 1959 में केंद्र ने बर्खास्त कर दिया। ऐसी बर्खास्तगी जम्मू कश्मीर में सन् 1953 में ही हो चुकी थी। तब सूबे के प्रधानमंत्री शेख मो. अब्दुल्ला थे। उन्हें भूमि सुधार जैसे कदमों के चलते हटाया ही नहीं गया, जेल भी भेजा गया। लेकिन कश्मीर में सुधार कार्यक्रमों को आगे बढाने वालों के पास केरल की तरह सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन की ताकत नहीं थी। केरल में सिलसिला चलता रहा। कुछ वर्ष बाद फिर से वामपंथियों की सरकार बनी और उसने बड़े पैमाने पर सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। शिक्षा, कृषि व्यवस्था और स्वास्थ्य-हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कदम उठाये गये। शासकीय संस्थानों में भी समाज में उत्पीड़ित रहे हिस्सों की भागीदारी बढ़ती रही। इससे समाज भी बदलता रहा।
उत्तर के हिंदी-भाषी राज्यों में क्या हुआ? यूपी-बिहार-मध्यप्रदेश आदि में ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया गया। इन राज्यों में आजादी के बाद बनी कांग्रेसी सरकारों ने मुकम्मल भूमि सुधार की हर संभावना को रोका। बिहार की सरकारें इसके लिए सबसे कुख्यात रहीं। सरकारी सेवाओं में उत्पीड़ित समुदायों की वाजिब हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई। शुरू में बहुत मुश्किल से दलित-आदिवासियों के आरक्षण के प्रावधानों को अमलीजामा पहनाया गया। कानूनी प्रावधान होने के बावजूद उन्हें तहत नौकरियों में रोका गया। लंबे समय तक उन्हें शिक्षा से वंचित रखकर आरक्षण का फायदा उठाने से वंचित किया जाता रहा। उत्तर के हिंदी भाषी राज्यों में आजादी के चालीस-बयालीस साल तक शूद्रों(ओबीसी) को आरक्षण से वंचित रखा गया। मंडल आयोग की सिफारिशें आईं तो उसे भी दबा दिया गया। एक गैर-कांग्रेसी अपेक्षाकृत कमजोर—वीपी सिंह सरकार ने इसे सन् 1990 में लागू करने का ऐलान किया। सन् 1992 में बड़ी-बड़ी बाधाओं के बाद उसे किसी तरह लागू किया गया। आज तक उसके लक्ष्य हासिल नहीं किये जा सके। इससे हिंदी भाषी क्षेत्रों में पिछड़े लोगों को समुन्नत कर गैर-बराबरी कम करने और समावेशी समाज बनाने का सपना भी पिछड़ता रहा।
इस पूरे दौर और प्रक्रिया में हमारे समाज के लिबरल और कथित प्रगतिशील बुद्धिजीवियों की क्या भूमिका रही? अगर मैं अनुमान के आधार पर कहूं तो इनमें 99 फीसदी लोग उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों, अन्य संस्थानों और सरकारी सेवाओं में पिछड़ों को आरक्षण देने के विचार के विरोध में थे। वे नहीं चाहते थे कि दलित-आदिवासियों की तरह आरक्षण ने पाने वालों की एक और श्रेणी सामने आये! कारपोरेट-हिंदुत्वा की सत्ता के मौजूदा दौर में आज जिन-जिन बुद्धिजीवियों को व्यवस्था या सत्ता-विरोधी, पब्लिक इंटैलेक्चुअल, प्रोग्रेसिव या ग्रेट लिबरल आदि जैसी उपाधियों से नवाजा गया है, उनमें 90 फीसदी से ज्यादा लोग नब्बे के दशक में हिंदी-भाषी राज्य़ों के विभिन्न नगरों या देश की राजधानी में चलाये जा रहे आरक्षण-विरोधी अभियान के सक्रिय तौर पर साथ थे या आरक्षण के विरोध में अंग्रेजी के छोटे-बड़े अखबारों में लेख आदि लिखा करते थे। इनमें ऐसे अनेक लोग आज भी सक्रिय जीवन में हैं और कुछ दिवंगत हो चुके हैं, जो बीएचयू से जेएनयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लखनऊ विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश, राजस्थान या यहां तक कि बंगाल के शिक्षण संस्थानों में दलित-आदिवासी और बाद में आरक्षण के दायरे में लाये गये शूद्र समाजों(ओबीसी) से निकले इक्का-दुक्का प्रतिभाशाली युवाओं को प्रतिष्ठित संस्थानों में नौकरी पाने से वंचित करने की रणनीति बनाने में जुटे दिखते थे। नियुक्तियां सिर्फ उच्च हिंदू जाति या कुलीन मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच से ही होती थीं। यदा-कदा कभी अन्य श्रेणियों के कुछ लोगों पर कृपा कर दी जाती।
यह कोई कल्पित बात नहीं कर रहा हूं। अगर भरोसा न हो तो सन् 1990 से सन् 2002 के बीच केंद्रीय सेवाओं, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायपालिका, मीडिया और सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्त किये गये शूद्र समाजों(ओबीसी) के लोगों की संख्या का सरकारी आंकडा खंगाल कर देख लीजिये। शुरू से आरक्षण के दायरे में लाये गये दलित-आदिवासी भी तब तक ऐसी सेवाओं में संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत कम थे।
अपने-अपने समाजों और सूबों को बदलने में उत्तर के हिंदी भाषी राज्यों का राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व ही नहीं विफल रहा, बुद्धिजीवियों और विद्वानों ने भी अपने समाज को निराश किया। उनकी ये नाकामी किसी बाहरी कारण से नहीं थी। इसके पीछे वे स्वयं थे। अच्छे-अच्छे शब्दों और ज्ञान की चमक दिखाते रहने के बावजूद उन्होंने उत्पीड़ित समाजों को न्याय और हिस्सेदारी दिलाने के विचार का साथ क्यों नहीं दिया? सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने साथ नहीं दिया, उन्होंने इस विचार का विरोध भी किया। कथित प्रोग्रेसिव और आज के लिबरल बताये जाने वाले ऐसे बुद्धिजीवियों में वे तमाम लोग शामिल हैं, जिनकी किताबें और अखबारी कॉलम पढ़कर पिछली दो-तीन पीढियां जवान हुई हैं। इन राज्यों में समयानुसार न तो भूमि-सुधार होने दिया गया और न समाज को समावेशी बनाने के लिए लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने दी गई। नतीजतन अंतर्विरोध बढ़ते रहे। समाज में अलगाव, स्थगन और टकराव बढ़ता रहा। इसी आक्रोश में हिंदी क्षेत्रों में दलित-ओबीसी के बीच से नया नेतृत्व उभरा। किसी ने अपने को मंडलवादी तो किसी ने बहुजनवादी कहा। कुछ ने अपने आपको ‘सामाजिक न्याय’ आदि की वैचारिकी से जोड़ने की कोशिश की। इनमे कई लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहे। कुछ आज भी हैं। पर इनके पास कोई बड़ा ‘विजन’ नहीं था। समाज को बदलने की कई सुसंगत वैचारिकी नहीं थी। उनमें ज्यादातर आज पराजित होकर पस्त पड़े हैं। कुछ अब भी अपनी खोई सत्ता पाने की कोशिश में हैं। पर सत्ता पाने से क्या होगा? विचारहीन लोगों का झुंड सत्ता में आकर सिर्फ अपने लिए मलाई खोजेगा या थोड़े-बहुत कॉस्मेटिक बदलाव की बात सोचेगा। ऐसे कदमों से हिंदी-भाषी सूबों को केरल क्या, तमिलनाडु भी नहीं बनाया जा सकेगा! हिंदी-भाषी सूबे नहीं बदलेंगे तो भारत भी नहीं बदलेगा। फिर दक्षिण के कुछ सूबों के अपेक्षाकृत बेहतर परिदृश्य को भी खराब और गंदला करने की कोशिश की जायेगी। इसलिए भारत का सुंदर भविष्य चाहते हैं तो हिंदी सूबों की सोचिये कि इन्हें सुखी, सुंदर और समावेशी कैसे बनाया जाय! भयानक गैर-बराबरी, बेरोजगारी और बेहाली से उन्हें उबारा जाय? उत्तर के हिंदी-भाषी राज्यों में आज संघ-भाजपा के प्रसार और प्रभाव के पीछे सबसे बड़ा कारण है-इन इलाकों में अशिक्षा, अज्ञान और बेहाली का बढ़ता अंधेरा। इस अंधेरे को बरकरार रखने में उन कथित लिबरल बौद्धिकों को भी अपनी भूमिका की शिनाख्त करनी चाहिए। हिंदी-भाषी क्षेत्र के हे विद्वतजनों, कृपया आप ऐसे महा-विद्वानों को ‘पब्लिक इंटैलेक्टुअल’ कहकर पब्लिक का मजाक मत उड़ाइये।