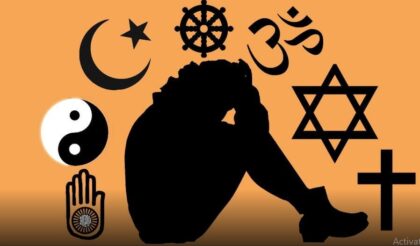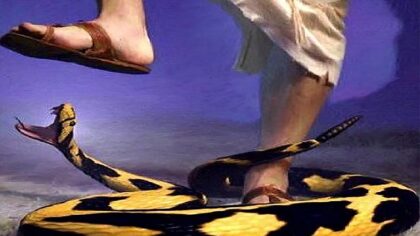समाज में नैतिकता, विवेक और इंसानियत की मान्यताओं को संजोने की हमारी कोशिशें हमेशा से ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। लेकिन जब समाज का एक वर्ग इन मूल्यों को महज औजार की तरह इस्तेमाल कर अपने लाभ के लिए उन्हें विकृत कर देता है, तब मानवीय रिश्तों और सामाजिक संरचना में एक गहरी विकृति जन्म लेती है।
इस शोषणकारी वर्ग का मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे समाज की संस्कृति, विचारधारा और मूल्यों पर भी अपना अधिकार जमाते हैं। उनकी बनाई इस वैचारिक संरचना में समाज का उत्पीड़ित वर्ग भ्रमित रहता है।
अपने वास्तविक शोषण को पहचान नहीं पाता और बार-बार उसी व्यवस्था को बनाए रखने में ही अपना हित समझता है, जो वास्तव में उसके ही खिलाफ काम करती है।
हॉवर्ड फास्ट का एक उपन्यास है, ‘फ़्रीडम रोड’। इस उपन्यास में एक संवाद है: “तुम उनको सही बात नहीं समझा सकते। उन्होंने विवेक व बुद्धि को दूषित कर दिया है। यदि हम उन्हें समझने में गलती नहीं करते, यदि हम उन्हें इंसान समझने की मूर्खता नहीं करते, यदि हम उन पशुओं के सम्मुख शिष्टता, सत्य और न्याय को सजाकर पेश न करते तो आज हमें ये दिन न देखने पड़ते।”
स्पष्ट है कि शोषणकारी व्यवस्था ने नैतिकता, विवेक और न्याय की अवधारणाओं को अपने लाभ के लिए मोड़ दिया है। इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य अपने लाभ के लिए समाज के अन्य वर्गों को भ्रम में रखना और असंगठित बनाए रखना है, ताकि वे अपनी शोषणपूर्ण स्थिति को न समझ सकें और संगठित होकर प्रतिरोध न कर सकें।
इस प्रकार के समाज में ही मिथ्या चेतना की स्थिति उत्पन्न होती है, जहां उत्पीड़ित वर्ग अपने वास्तविक हितों और शोषण के रूप को समझने में असमर्थ रहता है।
सत्ताधारी वर्ग समाज में अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए केवल आर्थिक नियंत्रण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अपनी शक्ति को सांस्कृतिक और वैचारिक क्षेत्रों में भी स्थापित करता है।
सत्ताधारी वर्ग ने समाज में ऐसी संरचना बना दी है जहां साधारण व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर को समझने की बजाय, सत्ताधारी वर्ग की परिभाषित नैतिकताओं को ही अपनाने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि समाज के निम्न और उत्पीड़ित वर्ग अपनी वास्तविक स्थिति को समझ ही नहीं पाते और शोषण के इस जाल में बंधे रहते हैं।
वास्तव में यह व्यवस्था एक दुष्चक्र है। जहां एक ओर समाज का वंचित वर्ग नैतिकता, सत्य और न्याय के भ्रम में रहता है, वहीं दूसरी ओर शक्ति संपन्न वर्ग अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा में लगा रहता है।
इस वर्ग के लिए “सही” और “गलत” का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि उनके सभी प्रयास मात्र अपने लाभ की ओर केंद्रित होते हैं। विवेक और नैतिकता का स्थान मुनाफे और प्रभुत्व ने ले लिया है।
मिथ्या चेतना की इस स्थिति में, जनता का एक बड़ा हिस्सा अपने असली हितों से भटककर उन मूल्यों और मान्यताओं का समर्थन करने लगता है, जो उनके खिलाफ ही काम करती हैं। उदाहरण के लिए, समाज में ‘समृद्धि का सपना’ जैसे विचार का प्रसार किया जाता है, जिससे साधारण लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि सत्ताधारी वर्ग का समर्थन करना ही उनकी समृद्धि का मार्ग है।
यह मिथ्या चेतना, सत्ताधारी वर्ग के वैचारिक प्रभुत्व का ही परिणाम होती है, जिसमें वे आमजन की सोच को नियंत्रित कर लेते हैं। इस प्रकार जनता यह समझने में असमर्थ हो जाती है कि उनके संघर्ष का असली कारण क्या है और वे इस व्यवस्था में सुधार की आशा में लगे रहते हैं, जो कि वास्तव में उनके खिलाफ ही काम कर रही होती है।
सत्ताधारी वर्ग का एक और उद्देश्य होता है, समाज को असंगठित बनाए रखना। उन्होंने समाज को इस प्रकार विभाजित कर रखा है कि लोग एक-दूसरे के ही साथ प्रतिस्पर्धा में फंसे रहते हैं और अपने असली शत्रु को पहचान नहीं पाते।
इस असंगठित स्थिति में, समाज के उत्पीड़ित वर्ग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर सकते, जिससे सत्ताधारी वर्ग को अपना प्रभुत्व बनाए रखने में आसानी होती है।
इस विभाजन की प्रमुख वजह यह भी है होती है कि सत्ताधारी वर्ग समाज के भीतर ही ऐसी वैचारिक संरचना का निर्माण करके रखता है, जहां उत्पीड़ित वर्ग के भीतर ही विरोधाभास और संघर्ष उत्पन्न होते रहते हैं।
समाज की यह स्थिति उस मानसिक दासता को दर्शाती है, जहां सत्ताधारी वर्ग के लाभ के लिए नैतिकता और सत्य जैसे मूल्यों का कोई स्थान ही नहीं है। समाज के सामान्य व्यक्ति अपने अधिकारों की समझ से दूर रहते हैं, क्योंकि उनकी सोच को एक विशेष प्रकार के ‘भ्रम’ में ढाला गया होता है।
इसी भ्रम में लोग इस विचार को सच्चाई मान लेते हैं कि नैतिकता, विवेक और सच्चाई केवल शब्दों तक सीमित हैं, जिनका वास्तविक जीवन में कोई महत्व नहीं है। इस स्थिति में समाज की उत्पादक जनता इसी भ्रम में जीती है कि वे उस व्यवस्था में ही न्याय पा सकते हैं, जो उन्हें निरंतर शोषित करती है।
शोषणकारी व्यवस्था से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका यह है कि समाज के उत्पीड़ित वर्ग अपनी प्रास्थितिक चेतना को जागरूक करें। उन्हें यह समझना होगा कि वे जिस नैतिकता और विवेक की अवधारणाओं में विश्वास रखते हैं, वह सत्ताधारी वर्ग द्वारा गढ़े गए सिद्धांत मात्र हैं, जो उनके शोषण को बनाए रखने के लिए रचे गए हैं।
जब तक जनता अपने असली हितों को नहीं पहचानती और इस मिथ्या चेतना से बाहर नहीं निकलती, तब तक वे इस व्यवस्था में शोषण का शिकार होते रहेंगे।
समाज के उत्पीड़ित वर्ग को अपने वास्तविक शत्रु को पहचानने की आवश्यकता है, ताकि वे संगठित होकर इस व्यवस्था का विरोध कर सकें। उन्हें यह समझना होगा कि सत्ताधारी वर्ग के साथ संवाद या नैतिकता की अपील से कोई परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि उनकी नैतिकता मुनाफे और सत्ता पर आधारित है, न कि मानवीय गुणों पर।
अतः उत्पीड़ित वर्ग के सामने एकमात्र विकल्प यही है कि वे इस वैचारिक दासता से मुक्त होकर एक संगठित समाज का निर्माण करें, जो उनके वास्तविक हितों की रक्षा कर सके।
समाज में नैतिकता और अनैतिकता का प्रश्न हमेशा से मानव सभ्यता का केंद्रीय विषय रहा है। यह सवाल मात्र किसी व्यक्ति के आचरण का नहीं है, बल्कि उस सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे का है, जिसमें व्यक्ति पला-बढ़ा और जीवित रहता है।
व्यक्ति के व्यवहार को उसकी स्वतंत्र इच्छा या चरित्र का परिणाम मान लेना समाज की जटिलताओं को सरल बनाकर देखने जैसा है। इसके बजाय, यह महत्वपूर्ण है कि हम व्यक्ति के आचरण को उस पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में समझें, जो उसे प्रभावित करता है।
व्यक्ति अपने परिवेश से परे स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसकी नैतिकता उस समाज के नियमों, मूल्यों और ढांचे से गहराई से प्रभावित होती है, जिसमें वह रहता है। अर्थात् मनुष्य की स्वतंत्रता उसकी सामाजिक स्थिति से तय होती है। व्यक्ति का व्यवहार किसी शून्य में नहीं घटित होता, बल्कि उस ढांचे में होता है जो उसके आस-पास मौजूद है।
जब कोई व्यक्ति अनैतिक व्यवहार करता है, तो यह आवश्यक नहीं कि वह उसके मूल स्वभाव की पहचान हो; बल्कि यह उस व्यवस्था की एक अभिव्यक्ति हो सकती है जो उसे ऐसे कदम उठाने पर मजबूर करती है।
जो वर्ग या समुदाय आर्थिक तंगी, सामाजिक बहिष्कार और असमानता के शिकार होते हैं, उनके पास जीवन यापन के लिए अनैतिक साधनों को अपनाने के अलावा बहुत कम विकल्प बचते हैं। आवश्यकता नैतिकता को दरकिनार कर सकती है, यह कठोर सच्चाई है, जिसे समझना जरूरी है।
समाज की मौजूदा आर्थिक संरचना में संसाधनों का असमान वितरण केंद्रीय मुद्दा है। एक तरफ वे लोग हैं, जिन्हें ‘विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग’ कहा जा सकता है, जिनके पास प्रचुर मात्रा में धन, शक्ति और संसाधन होते हैं। उनके लिए नैतिकता एक सुविधा बन जाती है, क्योंकि उनके अस्तित्व पर कोई संकट नहीं होता।
दूसरी ओर ‘उत्पादक वर्ग’ है, जो समाज के आर्थिक पहिए को चला रहा है, लेकिन स्वयं आर्थिक तंगी का शिकार है। इस वर्ग को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कई बार ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं, जिन्हें समाज अनैतिक मानता है। लेकिन जो उनके जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का साधन बनते हैं।
नैतिकता सिर्फ उन लोगों के लिए प्रासंगिक है जिनके पास विकल्प हैं। जब समाज में असमानता इतनी गहरी हो कि एक वर्ग को विलासिता में नैतिक आदर्शों का पालन करने का मौका मिले और दूसरे वर्ग को अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़े, तब नैतिकता का यह विभाजन स्वाभाविक है।
आर्थिक असमानता और शोषण की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वे न सिर्फ व्यक्ति के भौतिक जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि उसकी मानसिकता और सोच को भी ढालती हैं। यहां प्रश्न उठता है:
“क्या नैतिकता तब भी प्रासंगिक है, जब भूख और अभाव की जंजीरें व्यक्ति को जकड़ लें?” यह प्रश्न हमें उस विचार की ओर ले जाता है जो मानती है कि नैतिकता और अनैतिकता के प्रश्न को तभी सही ढंग से उठाया जा सकता है, जब सभी के पास समान अवसर हों और उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें।
समाज का वर्तमान ढांचा ऐसे असंतुलन पैदा करता है, जहां एक वर्ग विलासिता और अधिकारों का लाभ उठाता है, जबकि दूसरा वर्ग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करता है।
इस स्थिति में अनैतिकता को केवल व्यक्तिगत दोष मानना, उस ढांचे की गहराई से नासमझी होगी, जिसने इस असमानता को जन्म दिया है। असमानता ही अनैतिकता की जननी है और जब तक हम इस असमानता को दूर नहीं करेंगे, तब तक समाज में व्याप्त नैतिक संकट बना रहेगा।
वास्तविक नैतिकता समानता में निहित होती है। जब सभी लोगों के पास समान अवसर होंगे, तब नैतिकता केवल एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का आदर्श नहीं होगी, बल्कि समाज का मूल सिद्धांत बन जाएगी। इस समाज में अनैतिकता और बेईमानी की गुंजाइश कम होगी, क्योंकि कोई भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अनैतिक कार्य करने को मजबूर नहीं होगा।
इसलिए, बेईमानी या अनैतिकता का प्रश्न व्यक्ति का नहीं, उस ढांचे का है, जिसमें व्यक्ति जी रहा है। जब तक समाज में असमानता बनी रहेगी, तब तक नैतिकता का यह संकट भी जारी रहेगा। जिस समाज में जितनी अधिक असमानता होगी, अनैतिकता भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी।
(मनोज अभिज्ञान स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)