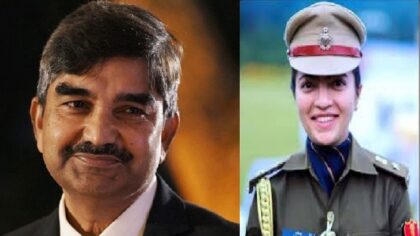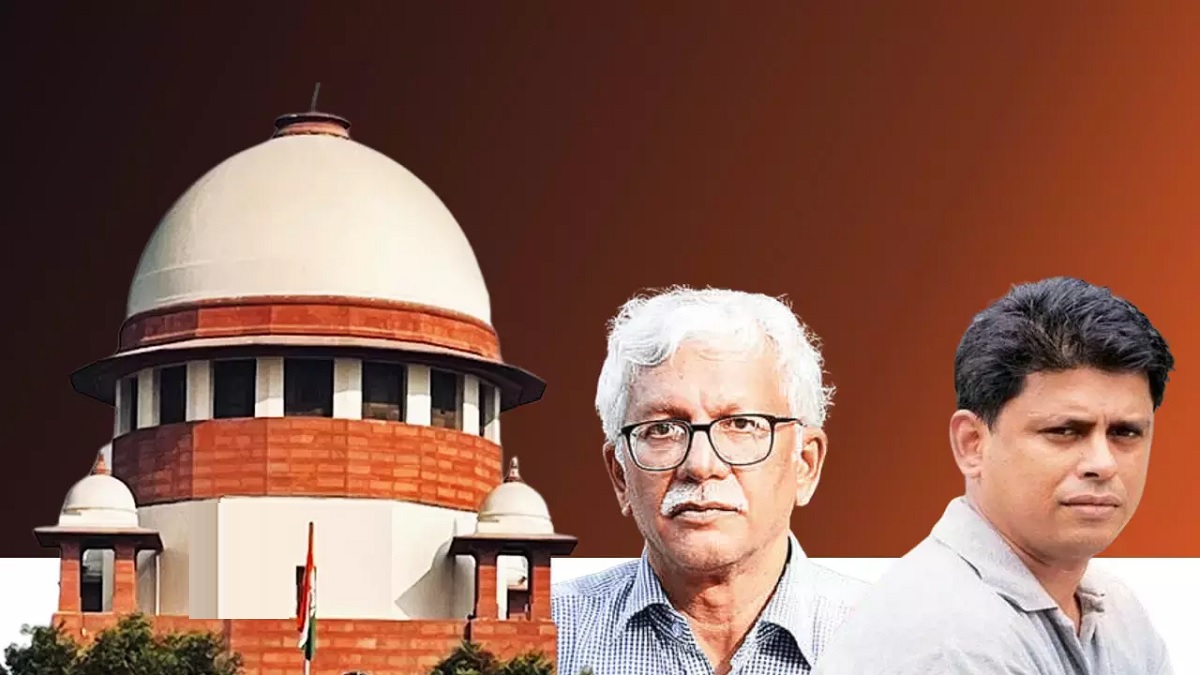न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली पीठ ने 28 जुलाई को श्री गोंसाल्वेस और श्री फरेरा को अपने मोबाइल फोन की लोकेशन स्थिति 24 घंटे सक्रिय रखने का आदेश दिया। अदालत के निर्देशानुसार “उनके फोन जांच अधिकारी (आईओ) के फोन से जोड़े जाएंगे, जिससे वह किसी भी समय अपीलकर्ताओं की सटीक लोकेशन की पहचान कर सकें।”
शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो अभियोजन पक्ष “इस अदालत को किसी भी प्रकार से पुनः संदर्भित किए बिना प्रत्येक या किसी भी अपीलकर्ता की जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है।”
गोंसाल्वेस और फरेरा पर 2018 से भीमा कोरेगांव मामले में यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। उनके साथ, इस साजिश मामले में 14 अन्य आरोपियों को भी यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किया गया था।
स्टेन स्वामी का जेल में खराब स्वास्थ्य स्थिति और भारतीय राज्य द्वारा खराब चिकित्सा उपचार के कारण निधन हो गया। इनमें से कुछ को विभिन्न शर्तों पर जमानत दी गई है, जो अदालतें लगाती हैं।
खास आपराधिक अधिनियमों के तहत जमानत की शर्तों पर ताजा बहस सुप्रीम कोर्ट के फ्रैंक विटस बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य एनडीपीएस मामले के निर्णय के बाद शुरू हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभय एस. ओका ने आरोपियों द्वारा दायर याचिका में जमानत की शर्तों को चुनौती देने के लिए अनुमति दी।
इस लेख में, मैं उस याचिका के एक भाग पर चर्चा करूंगा, जिसमें जांच एजेंसी को ‘गूगल पिन लोकेशन’ साझा करने की शर्त को चुनौती दी गई है ताकि मामले के जांच अधिकारी को उनकी लोकेशन उपलब्ध हो सके।
भारत का दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले में जमानत प्राप्त करने के प्रावधान प्रदान करता है, कुछ मामलों में यह अधिकार है और अन्य मामलों में यह न्यायिक विवेक पर निर्भर करता है।
CrPC की धारा 439 हाईकोर्ट और सत्र न्यायालय को ऐसे मामलों में जमानत देने की शक्ति देती है, जिनमें सात साल से अधिक या आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हो सकती है।
धारा 439 की भाषा स्पष्ट है “कि किसी भी अपराध के आरोपी और हिरासत में व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, और यदि अपराध धारा 437 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रकृति का है, तो वह आवश्यक उद्देश्यों के लिए कोई भी शर्त लगा सकता है।”
हमें धारा 437(c) को धारा 439 के साथ पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि इन दोनों धाराओं को आम तौर पर पढ़ने से ऐसे मामलों में जमानत की शर्तों की स्पष्ट तस्वीर मिलती है, जिनमें सात साल से अधिक की सजा होती है। उपधारा (c) यह व्यक्त करती है कि अदालत न्याय के हित में ऐसी अन्य शर्तें भी लगा सकती है जो उसे आवश्यक लगें।
कानून जमानत देने या अस्वीकार करने के दौरान न्यायालय के विवेक का उचित उपयोग करने की अपेक्षा करता है।
लाइव लोकेशन साझा करने जैसी शर्त लगाने के औचित्य पर गहराई से चर्चा करने से पहले, मुझे एनडीपीएस के इस विशेष मामले पर चर्चा करनी होगी, जिसमें माननीय अदालत ने जमानत देने के लिए कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधात्मक शर्तों की ओर इशारा किया।
यदि हम एनडीपीएस की धारा 37 की भाषा को पढ़ें, तो यह बताती है कि इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को केवल तभी जमानत दी जा सकती है जब यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार हो कि वह निर्दोष है या उसने अपराध नहीं किया है।
इसी प्रकार, विशेष अधिनियम यूएपीए की धारा 43(D)(5) का सामान्य पढ़ना जमानत के विचार को खारिज करता है, जिसका अर्थ है कि विधायिका ने निर्दोषता की धारणा को जानबूझकर नकार दिया है।
अपने आदेश में, न्यायमूर्ति ओका ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय कुनाल कुमार तिवारी बनाम बिहार राज्य का उल्लेख किया कि “इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि धारा 437(3) के खंड (c) के तहत न्याय के हित में ऐसी शर्तें लगाने की अनुमति है।
लेकिन ऐसी शर्तें मनमानी, कल्पनाशील या प्रावधान की सीमा से बाहर नहीं होनी चाहिए। ‘न्याय के हित’ वाक्यांश का अर्थ है ‘न्याय का अच्छा प्रशासन’ या ‘परीक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना’ और व्यापक अर्थ को शामिल करने से बचना चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करना है।
यह पैराग्राफ दंड प्रक्रिया संहिता के उद्देश्य के साथ खड़ा है, जो यह मानता है कि जब तक आरोपी दोषी साबित नहीं होता, वह निर्दोष है।”
गिरफ्तारी योग्य अपराध में जमानत देने के लिए न्यायाधीश को उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है; उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करे। लेकिन क्या इसका मतलब पुलिस के सामने अपराध स्वीकार करना है?
नहीं। जमानत की शर्तें लगाने का उद्देश्य शर्तों के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। जमानत शर्तें लगाते समय, जमानत पर रिहा किए गए आरोपी के संवैधानिक अधिकारों को केवल आवश्यक सीमा तक ही प्रतिबंधित किया जा सकता है।
यहां तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के बाद जेल की सजा काट रहे आरोपी को भी संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत सभी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।
जीवन का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को गारंटी दी गई है, और यहां तक कि राज्य भी इस अधिकार का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं रखता।
जेल में रहते हुए भी, आरोपी अपने सभी मौलिक अधिकारों का आनंद उठाता है, जिसमें गोपनीयता का अधिकार भी शामिल है। न्यायमूर्ति ओका ने कहा, “अदालत आरोपी पर यह शर्त नहीं लगा सकती कि वह अपनी हर गतिविधि और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की सूचना पुलिस को लगातार देता रहे”।
“जमानत शर्तों का उद्देश्य आरोपी की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखना नहीं हो सकता। यह अंततः आरोपी के गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा।”
इस निर्णय ने राज्य के सकारात्मक दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर एक मार्ग प्रशस्त किया है, विशेष रूप से विशेष आपराधिक कानूनों में। विभिन्न विशेष अधिनियमों के तहत कई विचाराधीन कैदी हैं, जो जमानत में इसी तरह की शर्तों का सामना कर रहे हैं।
इसका कारण यह है कि आरोपी पर ऐसी कठोर जमानत शर्तें लगाकर उसकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखना उसे जमानत पर रिहा होने के बावजूद किसी प्रकार के कारावास में रखने के बराबर होगा। ऐसी शर्तें जमानत की शर्त नहीं हो सकतीं।
वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा के मामले में, माननीय अदालत ने जमानत शर्तों का विस्तार करते हुए यह विचार प्रस्तुत किया कि विशेष अदालत जमानत की शर्तों का विस्तार कर सकती है, जो पहले से ही काफी कठिन थीं।
(निशांत आनंद कानून के छात्र हैं)