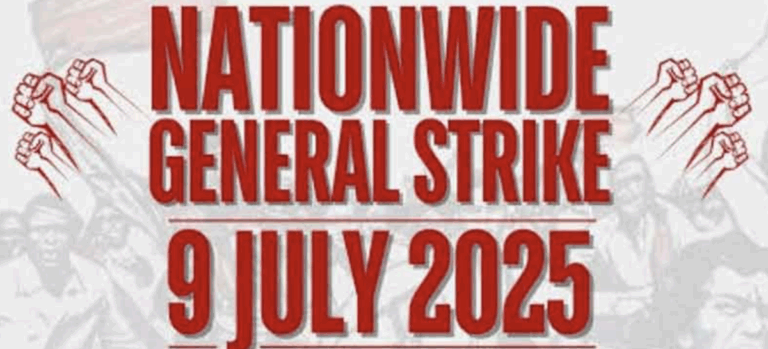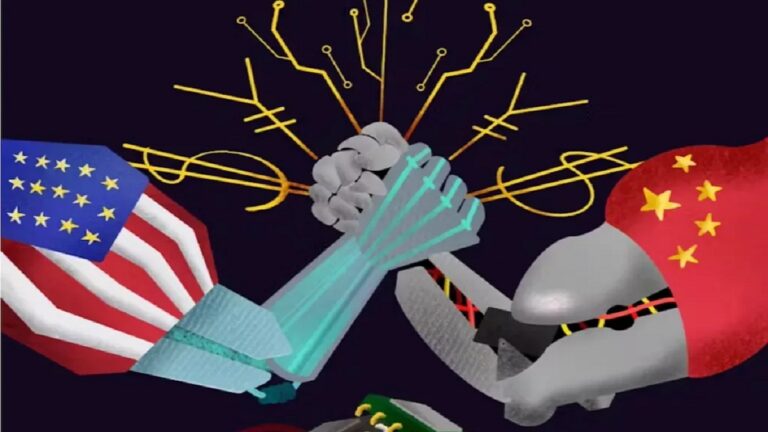जब कोई सामाजिक व्यवस्था केवल संसाधनों पर नहीं, बल्कि श्रम, शरीर, सोच और आत्म-संवेदना पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती है, तब उसके विरुद्ध होने वाला संघर्ष केवल राजनीतिक क्रांति नहीं रह जाता-वह समग्र सांस्कृतिक विद्रोह बन जाता है। भारत का जाति-आधारित समाज इसी प्रकार की व्यवस्था है, जिसमें उत्पीड़न का स्रोत केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और मानसिक स्तरों पर फैला हुआ है।
इस व्यवस्था में सामाजिक संरचना केवल ऊँच-नीच के अंतर से तय नहीं होती, बल्कि श्रम के बँटवारे और उसकी वैधता से भी जुड़ी होती है। यही कारण है कि भारतीय क्रांति की ज़मीन को समझने के लिए केवल वर्ग-संघर्ष की रूढ़ परिभाषाओं से काम नहीं चल सकता। हमें जाति और वर्ग को समग्र द्वंद्वात्मक एकता के रूप में देखना होगा-जहाँ दोनों एक-दूसरे के पूरक, विरोधी और उत्पाद हैं।
जाति को यदि केवल धार्मिक या सांस्कृतिक संरचना मान लिया जाए, तो हम उसे नैतिक दोष के रूप में देखेंगे-जैसे समाज के विकास में एक रुकावट, जिसे सामाजिक सुधारों और संवैधानिक उपायों से दूर किया जा सकता है। पर यह दृष्टिकोण न केवल अधूरा है, बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि यह जाति की उस भौतिक जड़ को छुपा देता है जो उत्पादन-संबंधों से जुड़ी हुई है।
जाति भारतीय समाज में केवल पूजा-पद्धति, विवाह, खानपान और आचरण की बात नहीं है; वह यह तय करती है कि कौन श्रम करेगा, कौन नियंत्रण रखेगा, कौन अधिकार भोगेगा, और कौन जीवनभर सेवा करता रहेगा। यह वर्गीय विभाजन का विशिष्ट भारतीय रूप है-एक प्रकार का ‘बंद वर्ग’ (closed class), जो जन्म पर आधारित है और परिवर्तन की सभी संभावनाओं को जन्म से ही रोक देता है।
यही वह बिंदु है जहाँ मार्क्सवाद और अंबेडकरवाद की टकराहट नहीं, बल्कि संवाद शुरू होता है। मार्क्स का वर्ग-संघर्ष सिद्धांत हमें बताता है कि ऐतिहासिक भौतिकता का निर्माण उत्पादन के साधनों पर अधिकार के आधार पर होता है। जो उत्पादन करता है और जो उस पर नियंत्रण रखता है, उनके बीच का संघर्ष ही ऐतिहासिक विकास का इंजन है।
लेकिन भारत में यह संघर्ष उस रूप में सामने नहीं आता जैसा यूरोप में आया। यहाँ उत्पादन पर नियंत्रण का निर्धारण पूंजी या श्रम के कौशल से नहीं, बल्कि जन्म से होता है। यहाँ एक बालक को उसके जन्म के क्षण से ही उसकी भूमिका, श्रम, अधिकार और यहाँ तक कि मृत्यु का भी वर्ग निर्धारित कर दिया जाता है। इस जन्मसिद्ध निर्धारण ने वर्ग-संघर्ष को जातिगत अवतार में ढाल दिया है।
अंबेडकर ने इसी यथार्थ को समझा और बताया कि जाति कोई सामाजिक ग़लती नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रणाली है, जो न केवल सामाजिक, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक असमानता को स्थायित्व देती है। उनकी दृष्टि में जाति का उन्मूलन केवल भेदभाव मिटाने का प्रयास नहीं है; यह व्यवस्था की चेतना को चुनौती देने वाला संघर्ष है। वे सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करते हैं, जो केवल संवैधानिक अधिकारों से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय से संभव है। उनके यहाँ ‘न्याय’ केवल अवसर की समानता नहीं है-यह शक्ति के स्रोतों के पुनर्वितरण की बात है।
जब हम जाति को इस भौतिक संदर्भ में देखते हैं, तो वह ‘सुपर-स्ट्रक्चर’ और ‘इकोनॉमिक बेस’ के बीच की पारंपरिक मार्क्सवादी विभाजन रेखा को धुंधला कर देती है। जाति धर्म, शिक्षा, विवाह जैसी ऊपरी संस्थाओं में तो है ही, पर वह खेत, कारखाने, श्रम, उत्पादकता और संपत्ति के बँटवारे में भी घुसी हुई है।
इसका मतलब है कि जाति केवल विचारधारा नहीं, बल्कि आर्थिक यथार्थ है-वह ऐसी परिघटना है जो संस्कृति और उत्पादन, परंपरा और संपत्ति, विचार और वस्तु-इन सबके बीच की सीमा रेखा को मिटा देती है। इसीलिए भारत में क्रांति की परिभाषा को जाति के बिना समझना न केवल अनुचित है, बल्कि प्रायः असंभव भी है।
यह भी सत्य है कि जाति और वर्ग दो भिन्न अवधारणाएँ हैं-एक जन्म आधारित, दूसरी श्रम आधारित; एक धार्मिक वैधता पर टिकी हुई, दूसरी भौतिक आवश्यकताओं पर; एक स्थिरता चाहती है, दूसरी गतिशीलता। लेकिन भारतीय समाज में यह दोनों एक-दूसरे में समाहित हो गए हैं।
जब किसी जाति को सैकड़ों वर्षों तक भूमि से वंचित रखा जाता है, जब श्रम का कोई विशिष्ट प्रकार केवल एक जाति के लिए नियत कर दिया जाता है, जब शिक्षा और ज्ञान की पहुंच भी जातियों के अनुसार नियंत्रित की जाती है-तो यह केवल सामाजिक असमानता नहीं रह जाती, बल्कि आर्थिक दासता का धार्मिक रूप बन जाती है।
इसलिए जाति और वर्ग को द्वैध सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक-दूसरे के अंत:संबंधित रूपों के रूप में देखना आवश्यक है। यह द्वैत हमें उस दर्शन की ओर ले जाता है, जो केवल वस्तुगत नहीं, बल्कि चेतनागत भी है। यह द्वंद्वात्मक दृष्टि हमें बताती है कि भारतीय क्रांति की जमीन पर आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक उत्पीड़न एक ही ताने-बाने में बुने हुए हैं। इन्हें अलग करके देखा जाए तो हम या तो ‘शुद्ध आर्थिक क्रांति’ की कल्पना करेंगे, जो जाति को उपेक्षित करती है, या फिर ‘शुद्ध सामाजिक सुधार’ की योजना बनाएंगे, जो उत्पादन संबंधों को अछूता छोड़ देती है। दोनों ही रास्ते हमें अधूरी मुक्ति की ओर ले जाते हैं।
भारतीय क्रांति तब ही पूर्ण होगी जब वह आर्थिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक, व्यक्तिगत और सामूहिक-इन सभी स्तरों पर हस्तक्षेप करेगी। यह क्रांति खेत की मेड़ से लेकर मंदिर की वेदी तक जाएगी; स्कूल की किताबों से लेकर शादी के मंडप तक; भाषा के व्याकरण से लेकर जीवन की परिभाषा तक। यह वह विद्रोह होगा जिसमें जाति को सिर्फ मिटाया नहीं जाएगा, बल्कि उसकी जगह नए मूल्य, नए संस्कार, और नए संबंध बनाए जाएँगे।
इस समग्र समझ को केवल दर्शन में नहीं, भारत के हालिया अतीत में जमीन पर भी रूपांतरित किया गया है। भोजपुर के खेतों में जब अहीर, चमार, पासी और कोइरी जातियों के युवाओं ने हथियार उठाए, तो उन्होंने केवल ज़मींदारी नहीं, जातिवादी प्रभुत्व को भी ललकारा। उनके नारों में वर्ग और जाति एक हो गए-“जो ज़मीन को जोतेगा, वही ज़मीन का मालिक होगा!” यह आंदोलन केवल भूमि सुधार नहीं था; यह सामाजिक पुनर्गठन था, जिसमें भूमि के साथ-साथ अस्मिता का भी पुनर्वितरण हुआ।
नक्सलबाड़ी आंदोलन ने इस चेतना को और व्यापक रूप में सामने रखा। वहाँ विद्रोह केवल राजनीतिक नहीं था; वह सांस्कृतिक पुनर्रचना थी। गीत, नाटक, त्यौहार, अनुष्ठान-सबको क्रांति के हथियार बनाए गए। महिलाओं ने शिशुओं को पीठ पर बाँधकर बंदूक उठाई-यह दृश्य केवल सैन्य साहस का नहीं, बल्कि मातृत्व और विद्रोह के गहरे एकत्व का प्रतीक था। वहाँ जातियों का अस्तित्व था, पर जातिवाद का नहीं-क्योंकि नेतृत्व दलित, आदिवासी, और पिछड़े समुदायों के हाथों में था। वहाँ जनसंस्कृति गढ़ी जा रही थी, जो संस्कृतिकरण के ब्राह्मणवादी आदर्शों को नकारती थी। यह सांस्कृतिक क्रांति थी-ऐसी धारा जिसमें पूजा-पद्धति का पुनर्लेखन हुआ, और खेत की भाषा, मज़दूर का गीत, और दलित की आँखों का सपना नई चेतना की नींव बने।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि नक्सलबाड़ी और भोजपुर के आंदोलनों को सैन्य दृष्टि से भले ही असफल कहा गया हो, पर वे भारतीय क्रांति की बुनियाद को सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से स्थापित कर गए। उन्होंने यह दिखा दिया कि जाति कोई ‘मिथक’ नहीं, बल्कि वर्गीय प्रभुत्व का वास्तविक रूप है; और जब तक हम केवल उसे ‘सुधारने’ की कोशिश करते रहेंगे, वह रूप बदलकर वापिस आती रहेगी। केवल वही संघर्ष जाति को समाप्त कर सकता है, जो उत्पादन के साधनों, सांस्कृतिक प्रतीकों, और सामाजिक सत्ता के सभी रूपों को एकसाथ बदलने की आकांक्षा रखता हो।
आज जब जाति की राजनीति फिर से केवल पहचान और आरक्षण के दायरे में सिमट रही है, यह ज़रूरी हो गया है कि हम उस व्यापक दार्शनिक समझ को पुनः जीवित करें, जो जाति को न केवल सामाजिक असमानता के रूप में, बल्कि वर्ग संघर्ष के स्थानीय रूप के रूप में देखती है। जब तक खेत का मालिक नहीं बदलेगा, जब तक संस्कृति का नेतृत्व नहीं बदलेगा, जब तक सोच की भाषा नहीं बदलेगी-तब तक जाति का अंत संभव नहीं।
मार्क्स के वर्गहीन समाज का स्वप्न और अंबेडकर का सामाजिक लोकतंत्र-दोनों एक ही ध्रुव की ओर इशारा करते हैं: ऐसा समाज जहाँ मनुष्य को उसकी जाति या वर्ग से नहीं, बल्कि उसकी चेतना, गरिमा और स्वतंत्रता से परिभाषित किया जाए। यही वह साझा बिंदु है जहाँ दोनों चिंतनधाराएँ मिलती हैं-और यहीं से भारतीय क्रांति की दार्शनिक यात्रा शुरू होती है।
(मनोज अभिज्ञान स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)