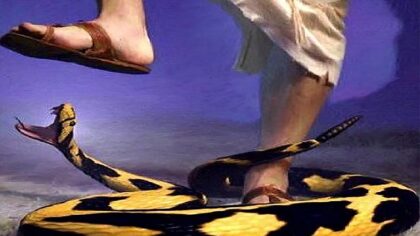आज 25 जनवरी भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। सच पूछा जाये तो मतदाता ही किसी संविधान सम्मत लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश का स्व-परिभाषित मालिक होता है। मतदाताओं के लिए यह आदर्श अवसर है कि वह अपने बल का अनुमान करे और देश की चिंता करे, अपने प्रतिनिधि के चाल-चरित-चेहरा के मूल्य-निर्धारण के प्रति सचेत होने का संकल्प ले। 2011 से शुरू हुए इस अवसर का इस्तेमाल केंद्रीय चुनाव आयोग नागरिकों को अधिक जागरूक बनाने की कोशिश कर सकता है, क्या आज इस मामले में किसी तरह की ईमानदार कोशिश की उम्मीद की जा सकती है! भारत में मतदाताओं को बांटने और बेड़ाबंदी के लिए कैसे-कैसे तौर-तरीके अपनाये जाने लगे हैं, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। नई वैश्विक परिस्थिति में भारत को नये सिरे से देश की अनसुनी आवाजों के मर्म और भारतीयों के भविष्य पर विचार किया जाये, यह बहुत ही जरूरी है।
आजादी के इतने दिन बाद भी भारत के लोगों के लिए सभ्य समाज और बेहतर जीवनयापन की संभावनाओं के द्वार बंद क्यों है! क्या भारत संसाधनिक अभाव से ग्रस्त है! क्या भारत के ‘अपने लोगों’ के द्वारा ‘अन-आत्मीय बना दिये गये भारत के अन्य लोगों’ के बीच दुश्मनी के कारण यह स्थिति बनी हुई है! भारत दुर्दशा की बात को राष्ट्र विरोधी कहकर वास्तविक स्थिति से ‘मुंह चुराना’ दुर्दशा को बढ़ावा ही देता रहा है।
विचारधारा का राजनीति में महत्व है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। यूरोपीय औद्योगिक क्रांति के दौरान विकसित पूंजीवादी विचारधारा के समानांतर मार्क्सवादी विचारधारा का विकल्प विकसित हो गया। न सिर्फ विकल्प विकसित हो गया बल्कि इस विकल्प के आधार पर सोवियत संघ का गठन भी हो गया। विश्व-युद्ध के होने को रोका तो नहीं जा सका और युद्ध की समाप्ति के बाद भी शीत-युद्ध जारी रहा। दुनिया दो खेमों या कहा जा सकता है कि दुनिया दो ध्रुवीय बन गई। ऐसी वैश्विक परिस्थिति में भारत को आजादी मिली।
विभाजन के दुख-दर्द के साथ नव-स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के सामने कई चुनौतियां थी। भारत ने इन चुनौतियों का सामना किया और निर्गुट आंदोलन भी चलाया। भारत के पास अगर कोई बल था तो बस नैतिक बल था। एक हद तक नैतिक बल से वह अपनी राजनीतिक कमजोरी की क्षतिपूर्ति कर लेता था। यह वह दौर था जब विचारधाराओं के टकराव के बीच भारत सहित दुनिया के कई देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, कुछ हद तक कामयाब भी हो रहे थे। अमेरिका से भारत के खड़े होने में कोई खास मदद नहीं मिल पा रही थी, लेकिन सोवियत संघ की तरफ से लगातार समर्थन मिला।
सोवियत संघ की उपस्थिति के कारण पूंजीवादी नीतियों में भी मानुस तत्वों की रणनीतिगत सक्रिय उपस्थिति बनी रही, नतीजा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शोषण तंत्रिका स्थगित बनी रही। हालांकि उपनिवेश की राजनीति के अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का काम करना मुश्किल हो गया तो उसी समय से भूमंडलीकरण कि प्रक्रिया शुरू कर दी गई। व्यापार और प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौता (General Agreement on Trade and Tariff, GATT) 1948 से शुरू हुआ। लेकिन इस समझौता में तीव्रता से प्राण का संचार हुआ, सोवियत संघ के ढांचागत विख्यात के बाद।
आठवां दौर (1986-93 ई.) उरूग्वे राउण्ड के नाम से विख्यात है। यह आठवां दौर गैट के इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसमें गैट के महानिदेशक आर्थर डंकेल के उदारीकरण के प्रस्ताव पर दुनिया के 117 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना हो गई। भारत के अतिरिक्त 85 देशों ने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की सहमति पर हस्ताक्षर किये थे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के माध्यम से विभिन्न देशों के मध्य व्यापार में अधिक विस्तार संभव हुआ। इसने भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया है। अर्थात विभिन्न जटिल कारणों से सोवियत संघ के बिखराव में पड़ जाने के कारण दुनिया एक ध्रुवीय हो गई।
इस पृष्ठ-भूमि को ध्यान में लेने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आज जब उदारीकरण-निजीकरण-भूमंडलीकरण (उनिभू) की धारा में दिख रहे भाटा के समतुल्य प्रभाव को संतुलित दृष्टि से समझना कुछ आसान हो। अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के महामहिम राष्ट्रपति बनने की संभावना के साथ ही कई तरह की आशंकाएं भी हवा में तैरने लगी। अब, डॉनल्ड ट्रंप का शासन-काल प्रारंभ हो चुका है। अमेरिका की नीतियों का प्रभाव पूरी दुनिया की शासकीय नीतियों पर पड़ता है।
पेरिस समझौता से निकलने और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अमेरिका के बाहर हो जाने के बाद पर्यावरण संकट को काबू करने की ताकत के कम होने के साथ-साथ पर्यावरण संकट से उत्पन्न बीमारियों से जूझने में अक्षमता बढ़ जायेगी।मनमर्जी से कभी इधर, कभी उधर होना निर्गुट रणनीति नहीं मानी जा सकती है। पिछले दिनों भारत की विदेश नीति में कभी इधर, कभी उधर की ‘मनमर्जी नीतियां’ ही अपनाई। इस चक्कर में अपने लगभग सभी पड़ोसियों से इस के रिश्तों में खराश आ गया। एक जमाने में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की नीतियों का विरोध करनेवाले का एक दूसरे को देख रहे हैं। अब क्या किया जाये!
उदारीकरण-निजीकरण-भूमंडलीकरण (उनिभू) के पलटने का स्वागत किया जाये! रोजगार, ग्राम-उद्योग पर चोट और गरीबी उन्मूलन, आय-संतुलन के नाम पर वोट आर्थिक उदारीकरण की रणनीति का हिस्सा रही है। उदारीकरण-निजीकरण-भूमंडलीकरण (उनिभू) का सब से ज्यादा विरोध वाम-पंथ से जुड़े ट्रेड यूनियनों और उस से जुड़े मजदूरों ने किया था। उदारीकरण-निजीकरण-भूमंडलीकरण (उनिभू) ने तो ‘ट्रेड’ को ही निष्क्रिय और नष्ट कर दिया तो यूनियनों की कौन पूछे!
लेकिन भरोसे की बात यह है कि लगातार की शासकीय कोशिशों के बावजूद किसानी और उस की अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों का संघर्ष अभी जारी है। इस संघर्ष का नतीजा क्या होगा, कुछ भी कहना मुश्किल है। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के संघर्ष की व्याख्या और उस के विश्लेषण का दायित्व इतिहास पर छोड़ दिया जायेगा या छटे हुए औद्योगिक मजदूर और जागरूक मतदाताओं के इस संघर्ष से जुड़ने पर इस संघर्ष की व्याख्या और इस का सही-सही विश्लेषण वर्तमान कर लेगा इस पर भारत के लोगों के भविष्य का बहुत कुछ निर्भर करेगा।
किसानी और मजदूरों के मुद्दों पर दक्षिण-पंथी राजनीति का व्यवहार तो साफ-साफ दिख ही रहा है, वाम-पंथी और वाम-झुकाव लिये बीच की राजनीति की तरफ से खास और कारगर पहल होना अभी भी इंतजार में ही है। लौटती हुई उदारीकरण-निजीकरण-भूमंडलीकरण (उनिभू) की प्रक्रिया के दौर में उस से उत्पन्न खतरों के प्रति वाम-पंथी और वाम-झुकाव लिये बीच की राजनीति को अधिक सावधान रहना चाहिए। क्या वे सावधान हैं! क्या पता!
लौटती हुई उदारीकरण-निजीकरण-भूमंडलीकरण (उनिभू) के तात्कालिक खतरे क्या दिख रहे हैं? अभी प्रकट इस के दो खतरे तो साफ-साफ दिखते हैं। पहला अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर अंधराष्ट्रवाद का ग्रहण लगेगा और देश के अंदरूनी मामलों में ‘देश भक्ति’ के नाम पर ध्रुवीकरण का नया औजार विकसित हो जायेगा। ‘देशभक्ति’ की नुमाइश और पैमाइश का नया सिलसिला शुरू हो जायेगा।
इस शासन-काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के ‘ऊंच-नीच’ पर आधारित सांस्कृतिक-राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह से भारत की समतामूलक आकांक्षावाली गंगा-जमुनी संस्कृति का विचारधारात्मक विनाश करने में लगी रही, यह बहुत ही निराशाजनक है। इस में कोई संदेह नहीं है कि मतदाताओं के ध्रुवीकरण की कोई भी प्रक्रिया राजनीतिक शक्ति की संस्कृति-संहार (culturicide) की नीतियों से ही निकलती है।
बाहर-भीतर दोनों ही जगह आबो-हवा बहुत रुखड़ा है। डॉनल्ड ट्रंप का चुनाव निश्चय ही अमेरिका के लोगों का अपना फैसला है लेकिन इस का प्रभाव पूरी दुनिया की न सिर्फ सरकारों और व्यवसायियों पर पड़ेगा बल्कि साधारण जन की जीवनयापन शैली पर भी पड़ेगा, पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा भी पड़ेगा। लेकिन भारत क्या करे!
जागरूक मतदाता और नागरिक समाज सरकार या सत्ता की भूखी राजनीतिक पार्टियों के भरोसे जान की भीख मांगते हुए हाथ-पर-हाथ धर कर न बैठे, बल्कि तुलनात्मक दृष्टि से जन-हितैषी राजनीति की पहचान कर उस का सक्रिय समर्थन करने का साहस संजोना शुरू करे और पहला अवसर मिलते ही अपनी मतदाता शक्ति की चयन कुशलता का इस्तेमाल करे।
‘मतदान’ का अर्थ साधारण दान नहीं है; मतदाता चुनावों में अपनी संप्रभुता पांच वर्ष के लिए अपने जन-प्रतिनिधि को अंतरित करता है। आज 25 जनवरी मतदाता दिवस है। जागरूक मतदाता ही लोकतंत्र का रक्षक और रक्षा-कवच है। भीतर संभल जाये तो बाहर भी जरूर संभल जायेगा, ऐसा है विश्वास! और हां, भारत के लोग भारत की अनसुनी आवाजों का मर्म न समझ पायें तो अपने ‘भविष्य’ को शायद ही सकारात्मक आयामों से जोड़ सकें और बेहतर जीवनयापन का अवसर इस दौर में हासिल कर सकें।
(प्रफुल्ल कोलख्यान स्वतंत्र लेखक और टिप्पणीकार हैं)