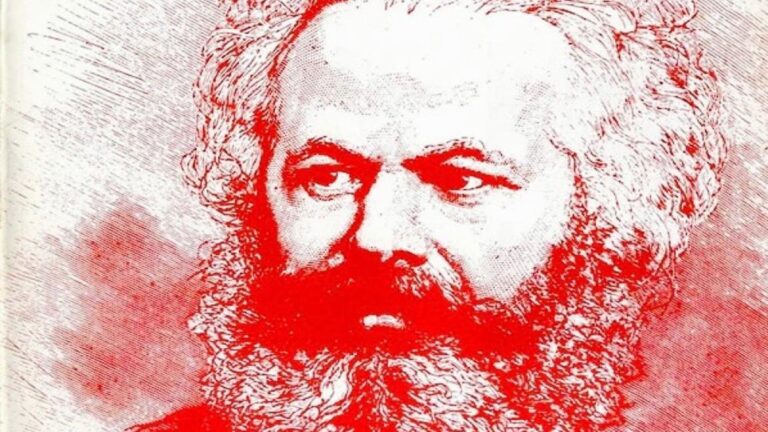धर्मनिरपेक्षता का विचार आधुनिक समय में विकसित हो रहे लोकतांत्रिक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। 1947 के बाद, भारत ने एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में एक लिखित संविधान अपनाया, जिसकी विचारधारा ने धर्मनिरपेक्षता को राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ के रूप में चिन्हित किया। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता के विचार को विकसित करने में न्यायपालिका की भूमिका उल्लेखनीय रही है, जिसने अल्पसंख्यकों के सुरक्षित धार्मिक कर्मकांड को करने के लिए एक सहज मार्ग प्रदान किया।
लेकिन “अनिवार्य धार्मिक प्रथा” (Essential Religious Practice, ERP) के विचार ने, जिसमें भारतीय न्यायपालिका ने धर्मों की मूल धारणाओं और प्रथाओं में हस्तक्षेप किया, जो किसी विशेष धर्म को परिभाषित करती हैं, एक नई बहस को जन्म दिया। यह लेख ERP के पीछे के मूल विचार और इसके प्रभावों को लोगों के धार्मिक जीवन के संदर्भ में चर्चा करेगा।
संविधान के व्याख्याकार के रूप में न्यायपालिका की भूमिका ने कभी-कभी धर्म के व्याख्याकार के रूप में खुद को बदल दिया है, जिससे यह ऐतिहासिक गलतियां करने की ओर अग्रसर हुई है। इन गलतियों ने धर्म के वस्तुनिष्ठ विकास को रोकते हुए धर्म को अतीत की परिधियों में बांध दिया। विशेष रूप से हिजाब प्रतिबंध, सबरीमाला फैसला और अन्य मामलों में लिए गए फैसलों ने यह स्पष्ट किया है कि ERP के सिद्धांतों के आधार पर की गई व्याख्याएं सही व्याख्या से भटक गईं हैं क्योंकि ERP व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपनी तरह से धर्म का पालन करने की सीमा को कम करता है और धर्म का अभ्यास करने की स्वतंत्रता पर एक संकीर्ण धार्मिक किताबों और तार्किकता पर सीमा लगाता है।
अनिवार्य धार्मिक प्रथा (Essential Religious Practice)
भारतीय संविधान अपने प्रत्येक नागरिक को धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का अर्थ है कि जिन आधारों पर राज्य किसी व्यक्ति (नागरिक) के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है, जैसे- सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिकता और स्वास्थ्य।
हालांकि, न्यायिक व्याख्या के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह व्याख्या की कि हर धार्मिक प्रथा अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षित नहीं है, बल्कि केवल अनिवार्य धार्मिक प्रथाएं (ERP) ही संविधान के तहत संरक्षित हैं। ऐसा करके, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को केवल पाठ्य सामग्री के आसपास धार्मिक रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया।
ERP की रूपरेखा यह निर्धारित करने के लिए एक त्रि-आधारित परीक्षण की मांग करती है कि कोई प्रथा अनिवार्य धार्मिक प्रथा है या नहीं। पहला, यह जांचना कि दावा धार्मिक है या नहीं; दूसरा, क्या यह विश्वास के लिए ‘अनिवार्य’ है; और तीसरा, यदि यह अनिवार्य है, तो क्या यह संविधान में उल्लिखित प्रतिबंधों को पूरा करता है।
ERP के तहत इन मानकों को लागू करना व्यावहारिक रूप से असंभव है, क्योंकि यह व्यक्ति की धार्मिक प्रथा को अपनाने की स्थिति को ध्यान में नहीं रखता है। ERP का मूल विचार व्यक्ति को एक ऐसी पहचान के रूप में नहीं देखता है, जो धर्म का अपना व्यक्तिगत अर्थ रख सकता है।
संविधान के निर्माताओं के दावे के अनुसार, भारतीय संविधान ने यूरोप और अमेरिका के मुकाबले धर्मनिरपेक्षता का एक अभिनव मॉडल अपनाया, जिसमें यह धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा का वादा करता है, और साथ ही सामाजिक कल्याण विधियों को लागू करने और समानता का वादा पूरा करने का प्रयास करता है। समय-समय पर संविधान के कई टिप्पणीकारों ने समाज के धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में लिखा है, जब वे संविधान की धर्मनिरपेक्षता को समझने की कोशिश करते हैं।
एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में, राज्य यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि लोग किसी धर्म का पालन न करें, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह स्वयं धर्मनिरपेक्ष प्रकृति में बना रहे।
एजेंसी या अनुशासन का प्रश्न
अक्टूबर 2022 में, सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने हिजाब प्रतिबंध के मामले में विभाजित निर्णय दिया। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जहां माननीय उच्च न्यायालय ने सरकारी संस्थानों में हिजाब प्रतिबंध को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट में, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले से सहमति व्यक्त की और कहा कि सार्वजनिक वर्दी का विचार शिक्षा के लिए अनिवार्य है और इसके बिना शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और निजता जैसे अधिकार ‘योग्य सार्वजनिक स्थानों’ में या तो अप्रासंगिक हैं या केवल कमजोर रूप से लागू होते हैं। न्यायमूर्ति गुप्ता ने बार-बार अनुशासन के विचार को संवैधानिक मूल्यों के ऊपर रखा। उनके अनुसार, नागरिकों के बीच बंधुत्व विकसित करने के लिए ड्रेस एक ऐसा माध्यम है जो संप्रदायवाद को हतोत्साहित करता है।
न्यायमूर्ति गुप्ता ने लिखा: “अनुशासन एक ऐसा गुण है जिसे छात्र स्कूलों में सीखते हैं। स्कूल के नियमों की अवहेलना अनुशासन के विपरीत होगी, जो उन छात्रों से स्वीकार्य नहीं है जो अभी वयस्कता तक नहीं पहुंचे हैं। इसलिए, उन्हें भाईचारे और बंधुत्व के माहौल में बढ़ना चाहिए, न कि विद्रोह या अवज्ञा के वातावरण में।” (पैरा-188, गौतम भाटिया, डिसिप्लिन ऑफ फ्रीडम)
यदि मैं गलत नहीं हूं, तो राज्य ने अपने प्रारंभ से ही कर्तव्यों के गीत गाए हैं। लेकिन, न्यायपालिका के लिए यह विचार लंबे समय तक इतना गंभीर नहीं था। अब, न्यायपालिका का अधिकार-आधारित से कर्तव्य-आधारित दृष्टिकोण में स्थानांतरण केवल एक समस्या नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र के बुनियादी ताने-बाने के लिए एक चेतावनी संकेत है।
यदि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ें जो सामुदायिक भौतिक संसाधनों पर केंद्रित है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान देश की आर्थिक प्रणाली पर कट्टर दृष्टिकोण में विश्वास नहीं करता है और हर सरकार को समाज के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार की आर्थिक नीति बनाने और लागू करने का अधिकार है। उसी फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया कि नीति निर्माण कार्यपालिका का कर्तव्य है और न्यायपालिका को राज्य के आर्थिक हस्तक्षेप के व्यापक क्षेत्र से दूर रहना चाहिए।
इसी न्यायपालिका ने एक भी शब्द नहीं कहा जब नया भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम (LARR) और वन अधिकार संशोधन संसद द्वारा पारित किया गया। ये कानून आदिवासियों की सामूहिक भूमि को समाज के भौतिक संसाधनों और राष्ट्रीय हित के नाम पर छीन लेते हैं। क्या यह आर्थिक कट्टरता नहीं है कि न्यायपालिका ने कॉर्पोरेट्स और विदेशी निवेशकों को हमारे संसाधनों की लूट के लिए खुला हाथ दे दिया? क्या यह जनता से छुपा हुआ है कि समान अवसरों की खोज में नव-उदारवादी बाजार ढांचे ने अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को बढ़ा दिया है? क्या यह न्यायपालिका की आर्थिक कट्टरता नहीं है, जो बड़े कॉर्पोरेट्स के मुनाफे के शोषण के लिए आसान श्रम कानूनों को वैधता प्रदान करती है?
“नियम मेरे हैं, अदालत मेरी है, फिर भी मैं एक ऐसा खिलाड़ी हूं जो मेरे बनाए नियमों पर आवाज नहीं उठाएगा। क्योंकि जिस समय आप अपनी स्थिति का दावा करेंगे, मैं व्याख्या बदल दूंगा।”
मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य पहले ही एक कल्याणकारी राज्य से एक नव-उदारवादी राज्य में बदल चुका है, जहां भूमि और उद्योगों पर बड़ी शक्तियों का नजदीकी गठजोड़ है। लेकिन न्यायपालिका जो आगे बढ़ रही है, वह अंततः लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और उनके अस्तित्व की आवाज़ उठाने के सभी रास्ते बंद कर देगी।
फ्रांस और नागरिक अधिकारों का नया प्रश्न
2024 के ओलंपिक खेल पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुए, जहां खेलों के उद्घाटन से पहले 24 सितंबर 2023 को नागरिक अधिकारों की एक नई बहस शुरू हुई। खेल मंत्री एमेली ओडिया-कास्टेरा ने घोषणा की कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
हालांकि फ्रांसीसी खेल प्राधिकरणों ने “उत्कृष्टता, सम्मान और मित्रता” जैसे ओलंपिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच और स्पोर्ट एंड राइट्स अलायंस जैसे समूहों ने हेडस्कार्फ़ पहनने वाले राष्ट्रीय खिलाड़ियों पर प्रतिबंध को “भेदभावपूर्ण पाखंड” कहा। इस निर्णय का सीधा प्रभाव फ्रांस की मुस्लिम खिलाड़ियों, जैसे बास्केटबॉल खिलाड़ी सलिमाता सिल्ला और हेलेन बा पर पड़ा है, जो पहले प्रतियोगिताओं के दौरान हिजाब पहन चुकी हैं।
फ्रांस, जो आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों और राज्य का जनक है, जहां लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, अब वही फ्रांसीसी राज्य कुशल और योग्य खिलाड़ियों को उनके पहनावे के कारण सीधे प्रतिबंधित कर रहा है। भारतीय न्यायपालिका को जो बदलाव स्वीकार करने की आवश्यकता है, वह अल्पसंख्यक विरोधी प्रतिक्रिया के साथ फासीवादी विचारधारा का उभार है।
एजेंसी के तर्क को ERP के संदर्भ में आगे बढ़ाना
एक तरफ, हिजाब प्रतिबंध के मामले को संवैधानिक मूल्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया था: महिला छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और उनके चुनाव का अधिकार। और दूसरी तरफ, इस मामले को ERP (अनिवार्य धार्मिक प्रथा) परीक्षण के आधार पर रखा गया, जो वास्तव में एजेंसी के विचार को मिटा देता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार, जो इस संदर्भ में उल्लिखित हैं, सबसे पहले व्यक्ति और उसकी स्वतंत्र पहचान के विचार पर निर्भर करते हैं, चाहे वह विश्वास करे या न करे। लेकिन जब हम गेंद को ERP के न्यायालय में फेंकते हैं, तो चर्चा का मूल आधार – मुस्लिम छात्रों की इच्छा – समाप्त हो जाती है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्तिपरक और सामान्य विचार के खिलाफ लड़ने के लिए हमने एक और व्यक्तिपरक और कम वस्तुनिष्ठ विचार को चुना।
न्यायमूर्ति धूलिया ने इस मुद्दे को अंतरात्मा और चुनाव की स्वतंत्रता के आधार पर सही ढंग से रखा और इस मुद्दे में ERP के किसी भी ठोस आधार की सराहना नहीं की। धूलिया ने यह स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक रूप से ERP पद्धति का उपयोग सामूहिक धार्मिक अधिकारों और किसी विशेष समुदाय की संपत्ति के मामलों में किया गया है। लेकिन इस मामले में, मुस्लिम महिला छात्रों के व्यक्तिगत अधिकार खतरे में हैं।
धर्म में व्यक्ति के विचार को आगे बढ़ाते हुए, न्यायमूर्ति धूलिया ने लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर इशारा किया कि ERP सिद्धांत वास्तव में धार्मिक असहमति और धार्मिक बहुलवाद की संभावना को मिटा देता है। धूलिया के लिए प्राथमिक प्रश्न यह तय करना है कि यह एजेंसी का मामला है या धर्म का मामला।
जहां न्यायमूर्ति धूलिया ने इस मामले को सही ढंग से रखा, वहीं न्यायमूर्ति हेमंत ने प्रश्न का आधार धार्मिक ग्रंथों में खोजने के लिए सैकड़ों पृष्ठों के कुरान का उपयोग किया। ERP का “भूत” वह प्रचलित तत्व था जो न्यायमूर्ति हेमंत के मन में हर समय गूंजता रहा, लेकिन न्यायमूर्ति धूलिया ने सही स्थिति ली और किसी भी कट्टरता का दावा किए बिना, एक व्यक्ति द्वारा लोकतांत्रिक निर्णय के विचार, यानी एजेंसी, के साथ खड़े रहे।
(निशांत आनंद कानून के छात्र हैं)