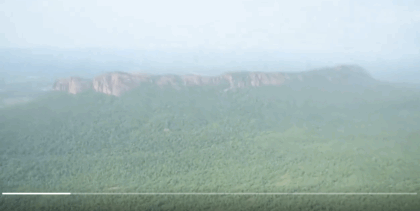क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा? दुनिया इस अटकल में उलझी हुई है। पाकिस्तान तो ऐसी आशंकाओं से बुरी तरह घिरा हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में कहा- ‘हमने अपने बलों की चौकसी बढ़ा दी है, क्योंकि यह (युद्ध) अवश्यंभावी है।’ बाद में पाकिस्तान के न्यूज चैनल समा टीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा- ‘युद्ध क्षितिज पर मंडरा रहा है। हमें इसके लिए दिमागी तौर पर तैयार रहना है।’ ये दोनों ही बातें उन्होंने 28 अप्रैल को कहीं।
हालांकि उसी रोज बाद में आसिफ ने सफाई दी। कहा- मेरे बयान का गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। मेरी बात का मतलब यह नहीं है कि अगले दो या तीन दिन में लड़ाई शुरू हो जाएगी। मेरा मतलब सिर्फ यह था कि अगले कुछ दिन निर्णायक हैं।
आसिफ ने बयान संभवतः कुछ देशों के दबाव में बदला। संभवतः उनसे कहा गया कि वे माहौल को और ना भड़काएं। इसका बात का संकेत खुद आसिफ का अगला बयान है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने खाड़ी देशों, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देशों से संपर्क किया है और उन्हें स्थिति की जानकारी दी है। कहा- ‘अरब खाड़ी के कुछ देशों ने भारत और पाकिस्तान दोनों से बात की है।’ आसिफ ने खाड़ी देशों का नाम नहीं लिया, मगर उनका इशारा सऊदी अरब, कतर और ईरान की तरफ था।
(https://www.dawn.com/news/1907228/pakistan-is-prepared-for-anything-india-might-try)
गौरतलब है कि ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने भारत और पाकिस्तान के नेताओं से बात की। ईरान ने औपचारिक रूप से दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। कुछ खबरों में बताया गया कि ऐसी ही पहल सऊदी अरब, मिस्र और कतर ने भी है। यहां कुछ बातें ध्यान खींचती हैः
- अमेरिका ने, जो पहले स्वंयभू मध्यस्थ के रूप में सामने आता था, इस बार अपने को विवाद से दूर दिखाने की कोशिश की है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों उनके करीबी हैं और वे आपस में विवाद का निपटारा कर लेंगे।
- ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों ने भी लगभग तटस्थता बनाए रखी है।
- रूस ने इस मसले में प्रत्यक्ष रूप से अपनी कोई भूमिका बनाने की कोशिश नहीं की है।
- अपेक्षा के मुताबिक ही चीन ने पाकिस्तान की ‘संप्रभुता और सुरक्षा’ के प्रति अपना समर्थन जताया है। उसने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। चीन ने पहलगाम की घटना की “निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय जांच” कराने की पाकिस्तान की उस मांग का भी समर्थन किया है।
तुर्किये उपरोक्त देशों की तरह बड़ी ताकत नहीं है। बहरहाल, उसने खुल कर पाकिस्तान का समर्थन किया है (https://x.com/RT_com/status/1916893280958132330). ऐसी खबरें हैं कि उसने भारत से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की है। (https://x.com/timesofindia/status/1916832270255792643)
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 अप्रैल को पहलगाम की घटना पर चर्चा की। वहां सर्व-सम्मति से पारित प्रस्ताव में पहलगाम में आतंकवादी हमले की निंदा की गई। कहा गया कि अपने सभी रूपों में आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है। (https://press.un.org/en/2025/sc16050.doc.htm). मगर इस प्रस्ताव में किसी आतंकवादी संगठन या उनके संरक्षक के रूप में पाकिस्तान का उल्लेख नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि चीन की मदद से पाकिस्तान इस प्रस्ताव की भाषा को सामान्य एवं नरम रखने में कामयाब हुआ।
पाकिस्तान इस समय 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्य के रूप में चीन का प्रभाव जग-जाहिर है। मगर प्रश्न यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे पश्चिमी “दोस्त” देशों और “भारत के खास दोस्त” रूस इस रूप में प्रस्ताव को पारित करने में सहायक क्यों बने? उन्होंने इस पर जोर क्यों नहीं दिया कि पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में आम सैलानियों पर हुए बर्बर हमले के दोषियों का नाम लेकर उल्लेख किया जाए? आखिर हमले के बाद भारतीय जांच एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंच चुकी थीं कि हमला लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुट ने किया है, जिसे पाकिस्तान सरकार का संरक्षण हासिल है।
बेशक, दुनिया भर के देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की है। उन्होंने मारे गए लोगों के परिजनों और भारत के प्रति अपनी सहानुभूति भी जताई है। मगर हमले को अंजाम देने वाले समूह या उनके संरक्षक देश के मामले में उन्होंने उतना ही स्पष्ट रुख क्यों नहीं लिया है? यह आतंकवाद के प्रति उनके अस्पष्ट रुख और दोहरे पैमाने को जाहिर करता है या फिर भारत अपना पक्ष उनके सामने रख पाने में नाकाम रहा है? ये सवाल बेहद अहम हैं, क्योंकि इस मामले में आगे क्या होगा, उसका इससे गहरा संबंध है।
भारत सरकार ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद से सख्त पैगाम भेजने का रुख अख्तियार किया। इस सिलसिले में,
- 1960 में हुई सिंधु जल संधि को लंबित अवस्था में डालने का एलान हुआ
- सरहद पर स्थित अटारी चौकी को बंद करने का फैसला हुआ
- कहा गया कि सार्क वीजा रियायत योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की इजाजत नहीं दी जाएगी
- नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, सेना, नौ सेना और वायु सेना सलाहकारों को भारत से निकाल दिया गया। साथ ही इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में तैनात अपने सलाहकारों को वापस बुला लेने की घोषणा की गई
- और, दोनों स्थानों पर स्थित उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटा कर 30 करने का निर्णय हुआ।
इनके अलावा सेना की युद्ध तैयारी की खबरें मीडिया में छा गईँ। यही वह पृष्ठभूमि है, जिस कारण पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ‘युद्ध के अवश्यंभावी’ होने की बात कही। असल में भारत ने जो इरादा दिखाया है, उसके मद्देनजर ‘पाकिस्तान को सख्त सबक’ सिखाना ही अब माकूल विकल्प रह गया है। और यह सिर्फ सांकेतिक कार्रवाइयों से नहीं हो सकता। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट हमले के बाद अब किसी भी कार्रवाई का महत्त्व तभी होगा, जब उसका दायरा और स्तर उनसे ज्यादा हो। तो यह कार्रवाई क्या होगी? अथवा, यह क्या हो सकती है?
हमने ऊपर विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाओं का उल्लेख इन्हीं सवालों के संदर्भ में किया है। यह अनुमान लगाने के लिए कि अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हमले से आगे जाकर कार्रवाई करता है, तो उसे कैसी वैश्विक प्रतिक्रियाओं का सामना करना होगा। फिलहाल, उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर अनुमान यही लगता है कि भारत शायद ही किसी शक्तिशाली देश से सक्रिय समर्थन की उम्मीद कर सकता है। जबकि पाकिस्तान कम-से-कम चीन और तुर्किये के समर्थन पर भरोसा करके अवश्य चल सकता है।
इनमें चीन का रुख महत्त्वपूर्ण है। इसलिए कि चीन आज एक बड़ी सैनिक ताकत है और उसके पास रक्षा उत्पादन की ऐसी क्षमता है, जिससे वह पाकिस्तान के लिए गोला-बारूद और सैन्य उपकरणों की लगातार सप्लाई कर सके। यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि चीन के पाकिस्तान में गहरे हित हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन-पाकिस्तान इकॉनमिक कॉरिडोर (सीपैक) परियोजना पर उसने अरबों डॉलर का निवेश किया है। इस परियोजना के जरिए उसने आम इन्फ्रास्ट्रक्चर के अलावा बंदरगाह और हवाई अड्डों का भी निर्माण किया है। सीपैक परियोजना का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद है। समझा जाता है कि इन सबकी रक्षा में चीन का अपना स्वार्थ है।
असल में, 2019 के बाद से बने समीकरणों के बीच चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य तालमेल की खबरें सुर्खियों में रही हैं। इसीलिए कुछ रक्षा विशेषज्ञों की राय है कि अब की परिस्थितियों में पाकिस्तान से युद्ध असल में पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ “टू फ्रंट” युद्ध में बदल सकता है। (https://www.youtube.com/watch?v=29COT3qxfIc). वैसे, अधिक संभव यही है कि चीन प्रत्यक्ष युद्ध में शामिल ना हो। मगर उसका कूटनीतिक और सैन्य साजो-सामान का समर्थन पाकिस्तान को मिलेगा, यह संभावना मजबूत है।
इसलिए आकलन का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या भारत एक साथ पाकिस्तान और चीन दोनों की साझा रणनीति का मुकाबला करने को लेकर आश्वस्त है? इस सिलसिले में वह किस देश के समर्थन पर भरोसा कर सकता है? अतीत में पाकिस्तान के साथ युद्धों के दौरान रूस का खुला समर्थन भारत के साथ रहा। मगर अब रूस और चीन के बीच बनी धुरी को देखते हुए उसके समर्थन को लेकर आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। रूस चीन के विरुद्ध जाकर कोई कदम उठाएगा, इसकी संभावना आज न्यूनतम समझी जाती है। इसकी एक बड़ी वजह चीन पर बनी रूस की आर्थिक एवं तकनीकी निर्भरता भी है। फिर चूंकि भारत ने अमेरिका से संबंध को अपनी प्राथमिकता बनाए रखा है, तो उसका असर भी रूस के रुख पर पड़ सकता है।
आम तौर पर गुजरे दो दशकों और खास तौर पर एक दशक में बने समीकरणों के आधार पर स्वाभाविक अपेक्षा यही होनी चाहिए कि अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देश ऐसे टकराव में भारत का पूरा समर्थन करेंगे, जिसमें चीन की सहानुभूति भारत के विरोधी पक्ष के साथ है। मगर फिलहाल ठोस रूप में यह भी फलीभूत होता नहीं दिखता, क्योंकि फिलहाल ‘पश्चिम’ की प्राथमिकताएं बदली हुई हैं। डॉनल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका अंतरराष्ट्रीय विवादों से दूर रहने की नीति पर चल रहा है। ट्रंप की प्राथमिकता ‘अमेरिका को फिर से महान’ बनाना है, जिस मकसद से उन्होंने पूरी दुनिया के खिलाफ व्यापार युद्ध का एलान कर रखा है। इसमें उन्होंने भारत जैसे ‘रणनीतिक सहयोगी’ और यूरोपीय देशों जैसे अपने सैन्य गठबंधन (नाटो) के सहभागी देशों को भी बख्शा है।
ट्रंप प्रशासन की निगाह में भारत का अतिरिक्त महत्त्व सिर्फ इतना है कि उसने व्यापार युद्ध में अमेरिका के खिलाफ जवाबी कदम उठाने का इरादा नहीं दिखाया है और चीन के साथ अमेरिका के बढ़ते टकराव में भारत का समर्थन अमेरिका के लिए लाभदायक हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कारण ट्रंप प्रशासन भारत को सैन्य एवं कूटनीतिक समर्थन देगा। ट्रंप के अस्थिर सोच और बदलते रुख के बीच इस बारे में कोई ठोस अनुमान लगाना कठिन है। मगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर भारत- पाकिस्तान विवाद पर अभी तक ट्रंप प्रशासन का जो रुख सामने आया है, उससे बहुत भरोसा नहीं बंधता।
ट्रंप काल का एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि ‘साझा पश्चिम’ (Collective West) की अवधारणा पर विराम लग गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका और यूरोपीय देशों को मिला कर ‘साझा पश्चिम’ की अवधारणा बनी थी। यह हकीकत है कि तब से ट्रंप काल के पहले तक ये देश आम तौर पर साझा हस्तक्षेप कर वैश्विक मामलों में पश्चिम की महत्त्वपूर्ण भूमिका बनाए रखते थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद तो यह भूमिका निर्णायक महत्त्व की हो गई थी। मगर ट्रंप ने ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति पर अमल करते हुए इस अवधारणा को फिलहाल ध्वस्त कर दिया है। वे अमेरिकी वर्चस्व की पुनर्स्थापना की कीमत सभी देशों से वसूलने की राह पर चल रहे हैं और इन ‘सभी’ में यूरोप भी शामिल है।
इस घटनाक्रम का नतीजा यह हुआ है कि यूरोपीय देश आज अपने लिए अलग सहारे ढूंढ रहे हैं। इसमें उनकी निगाह जिन स्थलों पर टिकी है, उनमें चीन भी है। चीन के बड़े बाजार और निवेश क्षमता का लाभ उठाने के लिए अपने पहले के कई रुख पर वे समझौता करते दिख रहे हैं। यह अनायास नहीं है कि चीन के शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों के कथित दमन का मुद्दा अब सुर्खियों से गायब हो गया है। इसी तरह चीन में मानव अधिकारों के हनन और बाल श्रमिकों के शोषण जैसे मुद्दे भी कहीं पृष्ठभूमि में चले गए हैँ। ऐसे में यूरोपीय देश चीन के हितों के खिलाफ किसी नए मुद्दे पर उत्साह दिखाएंगे, इसकी संभावना कम है।
ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, यूएई आदि जैसे देशों की सक्रियता को इसी संदर्भ में देखना उचित होगा। वैसे भारत से इन देशों के संबंध बेहतर हैं, इसके बावजूद तथ्य यह है कि वे सभी इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के सदस्य हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। उनसे यह अपेक्षा व्यावहारिक नहीं है कि वे पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत का समर्थन करेंगे। दरअसल, ऐसे चयन की नौबत ना आए, इसी मकसद से उन्होंने बीच-बचाव की पहल की है।
तो यह वो अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति है, जिसमें भारत को अपना अगला कदम तय करना है। भारत को आकलन करना है कि इन परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान को निर्णायक सबक कैसे सिखाया जाए? फिलहाल जो माहौल बन चुका है, उसमें इस लक्ष्य को हासिल किए बिना कदम वापस खींचा गया, तो उसे भारत की कमजोरी के रूप में देखा जाएगा। ऐसा संकेत या संदेश कोई ग्रहण करे, यह भारत के हित में बिल्कुल ही नहीं होगा। मगर कदम आगे बढ़ाने का निर्णय भी जलिटताओं से भरा हुआ है। स्पष्टतः यह भारत सरकार का कड़ा इम्तिहान है।
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं)