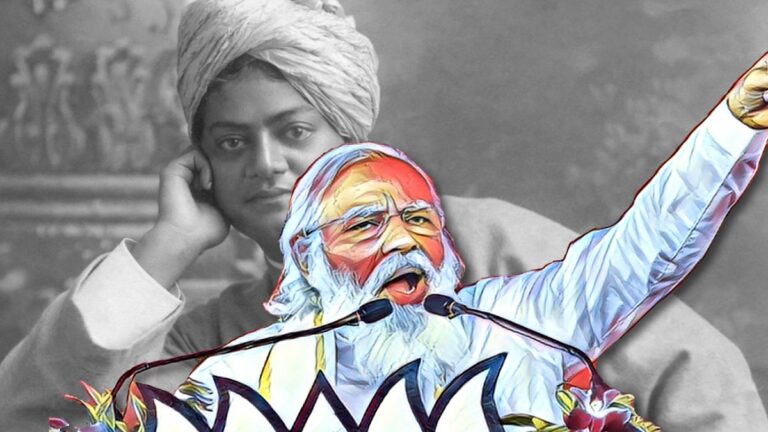अमेरिका के उप-राष्ट्रपति जेडी वांस की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में ध्यान भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर रहा। मोदी- वांस वार्ता के बाद ह्वाइट हाउस ने एक बयान में दावा किया कि बीटीए से दोनों देशों के सामने एक नए और आधुनिक समझौते पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर आया है, जिसमें ध्यान दोनों देशों में नौकरियां पैदा करने और नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित होगा। कहा गया- बीटीए का मकसद द्विपक्षीय व्यापार और आपूर्ति शृंखला (सप्लाई चेन) को संतुलित और पारस्परिक लाभ के नजरिए से आपस में जोड़ने पर है।
ह्वाइट हाउस ने कहा- ‘भारत के अमृत काल और अमेरिका के स्वर्ण युग की दृष्टियों से प्रेरित बीटीए से दोनों देशों में मजदूरों, किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर विकसित होने की उम्मीद है।’
भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा- ‘हम पारस्परिक लाभदायक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें व्यापार, तकनीक, रक्षा, ऊर्जा एवं जनता के स्तर पर आदान-प्रदान शामिल हैं।’
कूटनीतिक भाषा में किस तरह के छद्म होते हैं और उनके जरिए किस तरह सच्चाई से अलग झलक पैदा की जाती है, अगर उसे समझना हो, तो ये दोनों बयान इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण समझे जाएंगे। आखिर भारत के सामने इस समझौता वार्ता में शामिल होने की मजबूरी इसलिए आई है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तय कायदे एक झटके से बदल दिए। उनका प्रशासन तमाम देशों से अधिकतम लाभ झटकने के नजरिए से बातचीत कर रहा है। तो उस हाल में भारत के श्रमिक वर्ग का हित कैसे सध सकेगा?
डॉनल्ड ट्रंप ने आयात शुल्क युद्ध (टैरिफ वॉर) के जरिए भूमंडलीकरण के दौर की समाप्ति का एलान कर दिया है। उस दौर में निर्यात केंद्रित उत्पादन तमाम विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का केंद्रीय पक्ष रहा। अमेरिका ने इस नीति को सफल बनाने के लिए अपना बाजार उपलब्ध कराया। इससे अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं को सस्ती सामग्रियां प्राप्त हुईं। उत्पादक देशों को विदेशी मुद्रा (यानी डॉलर) प्राप्त हुई, जिसका अपने भंडार में होना भूमंडलीकरण के दौर में और भी महत्त्वपूर्ण हो गया था।
लेकिन अब अमेरिका ने अपने बाजार के चारों ओर टैरिफ की दीवार खड़ी कर दी है। द्विपक्षीय व्यापार वार्ता का मकसद इसी दीवार के बीच कुछ खिड़कियां हासिल करना है। मगर इसके लिए अमेरिका ऐसी कठिन शर्तें लगा रहा है, जिसे अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने माना, तो भारत की अंदरूनी अर्थव्यवस्था के बहुत सारे हिस्से डगमगा जाएंगे।
ट्रंप प्रशासन ने यह तो आरंभिक दौर में स्पष्ट कर दिया कि टैरिफ वॉर असल में सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है। बल्कि अमेरिकी बाजार में जगह पाने के लिए अनिवार्य है कि बाकी सभी देश अपने बाजार में संरक्षण के मौजूद रहे-सहे प्रावधानों को भी कम-से-कम अमेरिकी कंपनियों के मामले में खत्म कर दें। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने इन्हें non-tariff बाधाएं कहा। ट्रंप ने इसे non-tariff cheating यानी गैर-टैरिफ धोखाधड़ी कहा है। उनकी निगाह में जिन देशों ने यह ‘धोखाधड़ी’ की है, उनमें भारत प्रमुख है।
काफी समय तक तो ट्रंप प्रशासन ने इसे स्पष्ट नहीं किया कि गैर-टैरिफ रुकावटों के तहत वह किन बातों को शामिल कर रहा है। मगर 20 अप्रैल को खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आठ प्रकार की कथित non-tariff cheating की सूची जारी की। इसमें शामिल हैः
- करेंसी मैनिपुलेशन (मुद्रा की विनिमय दर कृत्रिम रूप से तय करना)
- वैल्यू ऐडेड टैक्स (वैट)। ट्रंप ने कहा है कि यह टैरिफ और निर्यात सब्सिडी की भूमिका निभाता है
- डंपिंग (लागत मूल्य से कम दाम पर वस्तु का निर्यात करना)
- निर्यात सब्सिडी एवं अन्य सरकारी सब्सिडी
- संरक्षणात्मक कृषि प्रतिमान (मसलन, जैविक हेरफेर से तैयार- genetically engineered कृषि उत्पादों के आयात पर रोक। ऐसा प्रावधान खासकर यूरोपियन यूनियन में है)
- संरक्षणात्मक तकनीकी प्रतिमान (मसलन, जापान में होने वाला कथित bowling ball test. यह ट्रंप का आरोप है, जबकि सचमुच जापान में आयातित कारों का कोई ऐसा टेस्ट होता है, इसके प्रमाण मौजूद नहीं हैं)
- बौद्धिक संपदा की जालसाजी, चोरी और नकल। ट्रंप का दावा है कि इससे हर साल अमेरिका को इन कारणों से एक ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता है)
- अमेरिका में टैरिफ से बचने के लिए ट्रांसशिपिंग का इस्तेमाल (यानी किसी अन्य देश में ले जाकर या वहां उत्पादन कर अमेरिका को निर्यात)
(https://x.com/KobeissiLetter/status/1914071619297001875)
इनमें से कम-से-कम तीन ऐसे मुद्दे हैं, जो भारत के संदर्भ में लागू होते हैं। इन्हें बीटीए वार्ता में अमेरिका एजेंडे पर ला चुका है। भारत अगर इन पर समझौता करता है, तो उसका क्या असर होगा, इस पर ध्यान देः
- निर्यात सब्सिडी एवं अन्य प्रकार की सरकारी सब्सिडी। यह मुद्दा भारत के उद्योग एवं कृषि दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव (पीएलआई) भारत में ऐसे उत्पादन के लिए दी है, जिसका मकसद निर्यात बढ़ाना है। उदाहरण के लिए इस स्कीम का लाभ उठा कर एपल कंपनी ने अपने आईफोन की असेंबलिंग बड़े पैमाने पर भारत में शुरू की है। ट्रंप की शर्त मानी गई, तो मोदी सरकार को ऐसी योजनाओं को वापस लेना होगा।
मगर इसकी ज्यादा मार कृषि क्षेत्र पर पड़ेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदारी कृषि सब्सिडी की श्रेणी में ही आती है। इसके अलावा किसानों को खाद, बिजली एवं आदि कई सुविधाओं पर सब्सिडी दी जाती है। ट्रंप प्रशासन चाहता है, इन सबको खत्म किया जाए, ताकि इनसे भारतीय कृषि को जो संरक्षण हासिल है, वह समाप्त हो और अमेरिकी कृषि उत्पाद विक्रेता कंपनियों के लिए भारतीय बाजार पूरी तरह खुल जाए। ट्रंप प्रशासन की इस मांग पर भारत सहमत हुआ, तो भारत के दुग्ध उद्योग के लिए भी वह घातक कदम होगा।
- भारत में अनेक जीएम खाद्यों (genetically engineered) के आयात पर रोक है। इसकी वजह इन खाद्यों की सुरक्षा को लेकर संदेह है। मगर अमेरिकी कृषि कंपनियों का यह बड़ा कारोबार है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि इन कंपनियों के कारोबार की राह में कोई रुकावट ना रहे।
- बौद्धिक संपदा की कथित चोरी, नकल और जालसाजी खत्म करने की ट्रंप की मांग का सीधा असर भारत के औषधि उद्योग पर पड़ेगा। भारत की औषधि निर्माता कंपनियां जेनरिक दवाओं का उत्पादन कर पाती हैं, क्योंकि उन्हें भारत के पेंटेंट कानून के तहत संरक्षण हासिल है। इन दवाओं का एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अलावा खुद अमेरिका में बहुत बड़ा बाजार है। यही वजह है कि ये दवाएं सस्ती पड़ती हैं। अमेरिकी दवा कंपनियों की लंबे समय से शिकायत है कि सस्ती दवाएं उपलब्ध होने का असर उनकी ब्रांडेड दवाओं पर पड़ता है। इसलिए वे भारत के इस कारोबार को चौपट कराना चाहती हैं। ट्रंप उनके हितैषी की भूमिका निभा रहे हैं।
- ट्रंप प्रशासन को खास परेशानी उन देशों से है, जिन पर अमेरिका कृत्रिम रूप से अपनी मुद्रा की कीमत डॉलर की तुलना में कम रखने का आरोप लगाता है। इससे विश्व व्यापार में उन देशों के निर्यात सस्ते हो जाते हैं। भारत पर यह आरोप नहीं है। भारत के बारे में धारणा तो यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपने हस्तक्षेप से रुपये की कीमत डॉलर की तुलना में उससे ज्यादा बनाए रखता है, जितना सामान्य रूप से होना चाहिए। इसलिए यह अमेरिका के लिए फिलहाल मुद्दा नहीं है, मगर जिस तेजी से डॉलर की कीमत गिर रही है, उससे आगे चल कर करेंसी मैनिपुलेशन के इस पक्ष पर भी वह आपत्ति कर सकता है।
बहरहाल, करेंसी मैनिपुलेशन वाले मुद्दे को अभी छोड़ दें, तब भी उपरोक्त तीन मामलों में अमेरिकी मांगों को मानना भारतीय अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए मारक साबित असर होगा। क्या मोदी सरकार उन क्षेत्रों के हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका से बीटीए को अंजाम दे पाएगी? अभी तक के अनुभव से इसकी संभावना कम नजर आती है। निम्नलिखित घटनाक्रमों पर गौर करेः
- जिन देशों ने अमेरिकी टैरिफ की मार से बचने के लिए सबसे पहले द्विपक्षीय वार्ता की पहल की, उनमें जापान भी है। मगर जापान की पहली विस्तृत वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं हुई। क्यों? इस बारे में जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने सार्वजनिक बयान दिया। कहा- ‘हम अमेरिका की हर मांग नहीं मान सकते। अगर जापान ने सब कुछ स्वीकार कर लिया, तो हम अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा नहीं कर पाएंगे।’
इशिबा की यह टिप्पणी भारत के संदर्भ में खास महत्त्वपूर्ण है- “हम विभिन्न उपायों को अपना कर जापान के कृषि की रक्षा करते रहे हैं। इनमें टैरिफ और आयात को सीमित रखने संबंधी नियम शामिल हैं। हमें यह संरक्षण अवश्य जारी रखना होगा। और हमें अवश्य ही अपने उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।”
- मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम ने 21 अप्रैल को एलान किया कि ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत में अंतिम समझौते तक नहीं पहुंचा जा सका है।
(https://x.com/KobeissiLetter/status/1914322721447571688)
- वियतनाम ने भी द्विपक्षीय वार्ता से टैरिफ मसले का हल निकालने की कोशिश की। इसके लिए वियतनाम का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका गया। मगर वहां हुई वार्ता सिर्फ टैरिफ और कथित गैर-टैरिफ रुकावटों तक सीमित नहीं रही। ट्रंप प्रशासन ने शर्त रख दी कि वियतनाम को अमेरिका और चीन के बीच में से किसी एक को चुनना होगा। (https://www.msn.com/en-us/money/markets/with-tariff-gambit-trump-pushes-vietnam-to-choose-between-us-and-china/ar-AA1CGMAc?ocid=BingNewsSerp)
- जाहिर है, बात आगे नहीं बढ़ी। वियतनामी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इससे नाराज वियतनाम ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हाल में हुई यात्रा के दौरान उनके स्वागत का स्तर बढ़ा दिया। उधर वियतनाम की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ने 50 साल बाद यह खुलासा किया कि अमेरिका के खिलाफ वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के तीन लाख सैनिकों ने अपना योगदान दिया था। वियतनाम उस युद्ध में हुई अमेरिका की शर्मनाक हार की 50वीं सालगिरह धूमधाम से मना रहा है। 30 अप्रैल को इस मौके पर होने वाली परेड में पीएलए की एक टुकड़ी भी भाग लेने वाली है।
- जो शर्त ट्रंप प्रशासन ने वियतनाम के सामने रखी, वही उसने यूरोपियन यूनियन (ईयू) के सामने भी रखी है। (https://www.ft.com/content/70294411-3738-45cd-b582-c60c238593d1). ईयू ने आरंभ में ही अपने यहां अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क शून्य कर देने की पेशकश कर समाधान निकालने की कोशिश की थी। मगर यह ट्रंप प्रशासन को मंजूर नहीं हुआ। ट्रंप प्रशासन की निगाह में ईयू के सिलसिले में वैट, जीएम खाद्यों पर रोक, अमेरिकी टेक कंपनियों संबंधी विनियमन आदि बड़े मुद्दे हैं। इसीलिए ईयू के अधिकारी व्यापार समझौता होने को लेकर बहुत आशान्वित नहीं हैं। खबर है कि समझौता ना होने की स्थिति के लिए ईयू ने जवाबी कार्रवाई की पूरी योजना बना रखी है।
जब तजुर्बा यह है, तो आखिर भारत सरकार की उम्मीदों का आधार क्या है? वह भारतीय हितों की पूरी सुरक्षा करते हुए बीटीए को संपन्न कर पाएगी, ऐसे दावों का आधार क्या है? और अगर बीटीए नहीं हो सका, तो उस हाल के लिए भारत सरकार की योजना या तैयारी क्या है? ये सारे सवाल इस समय वक्त बेहद अहम हैं।
जब से ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ा है, इसके स्वरूप और इसके संभावित परिणामों को लेकर विश्व स्तर पर विस्तृत चर्चा हुई है। ट्रंप के कट्टर समर्थकों को छोड़ कर अमेरिका में भी यह किसी की समझ नहीं है कि ट्रंप की योजना कामयाब हुई, तो उससे अमेरिका के आम उपभोक्ताओं और श्रमिक वर्ग का कोई लाभ होगा। ट्रंप का टैरिफ वॉर अर्थशास्त्र के नियमों के इतने विरुद्ध है कि पहले तो उसके कामयाब होने की संभावना न्यूनतम है। मगर चर्चा के लिए मान भी लिया जाए कि इसमें उसे सफलता मिल जाती है, तब भी उससे आम अमेरिकी श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। इससे अधिक से अधिक यह हो सकता है कि ट्रंप प्रशासन बिना सरकारी ऋण का बोझ बढ़ाए अति धनी वर्ग के लिए टैक्स छूट की योजना पर अमल कर पाए।
भारत ने ट्रंप प्रशासन की शर्तों को मानते हुए करार किया, तो उससे भी अधिकतम यही होगा कि भारत के बड़े पूंजीपतियों के लिए अमेरिकी बाजार की खिड़कियां खुली रहेंगी। मगर उससे दोनों देशों के ‘मजदूरों, किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर विकसित होने’ की जताई गई उम्मीद एक अययार्थ धारणा गढ़ने की कोशिश के अलावा कुछ और नहीं है। वैसे ह्वाइट हाउस ने इस सिलसिले में ‘भारत के अमृत काल और अमेरिका के स्वर्ण युग’ का उल्लेख कर उचित ही किया है। हकीकत यही है कि इन दोनों सपनों में श्रमिक वर्ग के हितों की कोई वास्तविक चिंता शामिल नहीं रही है।
वैसे अनेक देशों के अनुभव को देखते हुए यह साफ है कि मोदी सरकार ने भारत के कृषि, डेयरी (दुग्ध) और औषधि उद्योग आदि जैसे क्षेत्रों के हितों की न्यूनतम चिंता भी की, तो उसका अनुभव जापान या ईयू से अलग नहीं रहेगा। वैसी स्थिति में बीटीए का संपन्न होना बेहद टेढ़ी खीर साबित होगा। इसलिए बेहतर यह होता कि भारत सरकार बीटीए के पीछे भागने के बजाय भूमंडलीकरण के बाद के दौर की तैयारियों में जुटती। वह घरेलू बाजार के विस्तार और अपने उद्योग-धंधों को मजबूत संरक्षण देने की योजना पर काम करती। यह तो साफ है कि इसके अलावा सभी वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने का कोई और विकल्प अब मौजूद नहीं रह गया है।
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं)