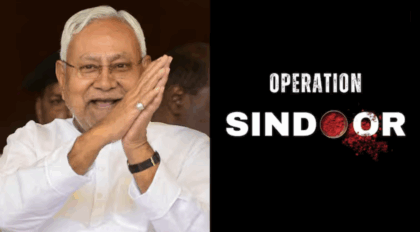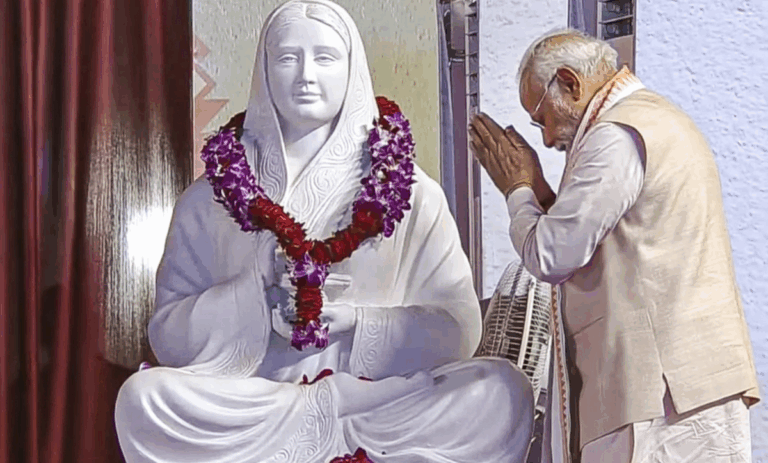25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, अड़तालीस साल बीत गए हैं, लोग अब भी पूछते हैं- कैसा था वह समय?
यदि आज 2023 में, आपको समझना है कि आपातकाल में ज़िंदगी कैसी थी, जाइए और थोड़ा समय बिताइए कभी जम्मूृ-कश्मीर कहलाने वाले राज्य में। एक पर्यटक के तौर पर या तीर्थयात्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर, जो समझना चाहता है कि क्षेत्र के लोगों का जीवन कैसा है।
5 अगस्त, 2019 से जब जम्मू-कश्मीर के लोगों को अनुच्छेद 370 के तहत मिले अधिकार रातों-रात छीन लिए गए और एक पूर्ण राज्य केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल गया, तब से उस क्षेत्र खासकर कश्मीर में एक तरह से आपातकाल के ही हालात हैं।
जरा सोचिए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के यह कदम उठाने के साथ ही इसका विरोध करने वाले सभी राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
मीडिया, जिसके लिए सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण वैसे भी कभी राह आसान नहीं रही, पूरी तरह शांत हो गया। इंटरनेट निलंबित कर दिया गया, जिससे पत्रकारों के लिए खबरें देना असंभव सा हो गया। उनसे सवाल किए गए, उन्हें डराया-धमकाया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया।
धीरे-धीरे बचा-खुचा स्वतंत्र मीडिया भी खदेड़ दिया गया। जिन पत्रकारों ने सवाल करने की हिम्मत की, उन पर जन सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मामले दर्ज किए गए।
चार कश्मीरी पत्रकार अब भी जेल में हैं और दर्जन से अधिक को या तो कश्मीर छोड़ना पड़ा या सावधानी का दामन थामना पड़ा क्योंकि उनके सिर पर गिरफ़्तारी या पूछताछ की तलवार हमेशा लटकी रहती है। यहां तक कि देश छोड़ने का विकल्प भी मौजूद नहीं है क्योंकि कइयों ने खुद को बिना पूर्व सूचना के नो-फ्लाई सूची में पाया है।
कई प्रमुख कश्मीरी पत्रकार अब अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों के लिए लिखते हैं क्योंकि उनकी खबरों को कुछ स्वतंत्र डिजिटल समाचार मंचों को छोड़कर मुख्यधारा का मीडिया मुश्किल से ही हाथ लगाता है।
कश्मीर में अखबार तभी बचे रह सकते हैं, अगर वह सरकार के कहे अनुसार चलें क्योंकि अब वह पूरी तरह से सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर हैं। वरिष्ठ पत्रकार वेद भसीन के शुरू किये और अब बेटी अनुराधा द्वारा संचालित सबसे पुराने अंग्रेजी अखबार ‘कश्मीर टाइम्स’ को श्रीनगर कार्यालय बंद करने पर मजबूर किया गया, जब लीज़ बिना कोई सफाई दिए रद्द कर दी गई।
पत्रकारों के लिए मुलाकात का एक महत्वपूर्ण अड्डा, श्रीनगर में कश्मीर प्रेस क्लब, भी मनमाने तरीके से बंद कर दिया गया।
2020 में एक मीडिया नीति लाई गई जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन या पत्रकार को दंडित किया जाना था जिसने ऐसी कोई खबर दी, जिसे सरकार “भ्रामक” या “गलत” मानती हो। दूसरे शब्दों में सरकारी नीतियों या कार्यक्रमों की आलोचना करने वाली कोई सामग्री प्रकाशित नहीं की जा सकती।
यह सब उससे अलग कैसे है, जो 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद हुआ?
उस समय भी विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया और जेल में डाला गया। अधिकांश आपातकाल की पूरी अवधि तक जेल में ही रहे।
प्रेस शांत हो गया क्योंकि प्रेस सेन्सरशिप लागू की गई। कोई भी प्रकाशन जो सेन्सरशिप ‘दिशानिर्देशों’, जो लगातार बदले जा रहे थे या उनमें नई बातें जोड़ी जाती थीं, का उल्लंघन करता था, उसे बंद कर दिया जाता था। आपको केवल उन दिशा-निर्देशों का पालन करना होता था।
अगर प्रमुख अखबारों के पत्रकार, जो उन्होंने जमीनी स्तर पर खुद देखा था, खबर देना चाहें तो नहीं दे सकते थे क्योंकि उनके प्रकाशन वह खबर प्रकाशित ही नहीं करते। उनके पास एक ही विकल्प था कि किसी तरह जुटाई गई जानकारी बाहर भेजो ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छप सके।
आपातकाल की घोषणा के कुछ सप्ताह में देश को डर ने ऐसा जकड़ लिया कि कोई प्रतिरोध या राजनीतिक गतिविधि नहीं हो सकी। ऐसी गतिविधि भूमिगत होने लगी। आपातकाल के विरोधियों, जो किसी तरह गिरफ्तार होने से बच गए थे, को सम्प्रेषण के ऐसे तरीके ढूंढने पड़े कि पकड़ में न आ सकें।
आपातकाल की अवधि यानि 20 महीनों तक, देश के एक हिस्से के लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है। उत्पीड़न की पूरी वास्तविकता हमें तब पता चली जब सेन्सरशिप हटाया गया और चुनाव हुए और इंदिरा गांधी नीत कांग्रेस सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
बहुत जल्दी अनुच्छेद 370 हटाने को चार साल हो जाएंगे। क्या कश्मीर में कुछ बदला है?
हालांकि कुछ राजनीतिक नेता रिहा किए गए हैं, उनकी पूर्व राज्य संचालन में कोई भूमिका नहीं है क्योंकि विधानसभा ही नहीं है। सामान्य राजनीतिक गतिविधि जैसे आम सभा या रैली करना असंभव है। राजनीतिक पार्टियां अपने लोगों तक ऐसे तरीकों से पहुंचने को मजबूर हैं, जो अधिकारियों, जो सीधे दिल्ली से आदेश लेते हैं, का ध्यान न खींचें।
और मीडिया का क्या? 5 अगस्त 2019 से पहले कई बड़े कश्मीरी पत्रकार मुख्यधारा के मीडिया के लिए खबरें करते थे। उनकी खबरों में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं और हालात के बारे में आम लोगों की राय शामिल होती थी। वह विपक्षी नेताओं के विचार भी छापते थे भले वह विचार दिल्ली में सत्तारूढ़ ताकतों को पसंद न हों।
आज, क्षेत्र से समाचार छनकर आते हैं। जो हम देखते या पढ़ते हैं वह सुरक्षा बलों के पर्चे होते हैं या फिर पर्यटन के बारे में वाहवाही करते लेख। ऐसा लगता है जैसे अतीत में हम जिन मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में पढ़ते थे, गायब हो गए हैं।
इस तरह, जम्मू-कश्मीर में भले औपचारिक तौर पर आपातकाल की घोषणा नहीं की गई हो, पिछले चार सालों में क्षेत्र के लोगों ने जो देखा-जिया है वह 1975-77 के आपातकाल के समय से अलग नहीं है।
ज्यादा चिंतनीय बात यह है कि बाकी भारत में देश के इस हिस्से में लोगों को उनके बुनियादी लोकतान्त्रिक अधिकारों से वंचित किए जाने पर कोई आक्रोश नहीं है।
अधिनायकवाद को तब उपजाऊ जमीन मिलती है जब नागरिकों को लोकतान्त्रिक अधिकारों के उल्लंघन के प्रति उदासीन बना दिया जाता है, जब लोग यह भ्रम पालने लगते हैं कि जो एक क्षेत्र में हो रहा है, वह दूसरे क्षेत्र में नहीं हो सकता और जब वह यह प्रचार पचा जाते हैं कि भारत अब भी “लोकतंत्र की मां’’ है।
हमें यह पहचानने की जरूरत है कि जो कश्मीर में हुआ है, इस सरकार की तरफ से किया गया एक प्रयोग है, यह देखने के लिए कि नागरिकों को उनके बुनियादी अधिकार मना करने के मामले में वह कहां तक जा सकते हैं। आपातकाल घोषित करने की जरूरत ही क्या है जब आपका काम उसके बिना भी चल सकता है?
(मुंबई की वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा का यह लेख ‘नेटवर्क ऑफ वुमन इन मीडिया, इंडिया’ की वेबसाइट से साभार लिया गया है। अंग्रेजी लेख का अनुवाद महेश राजपूत ने किया है।)