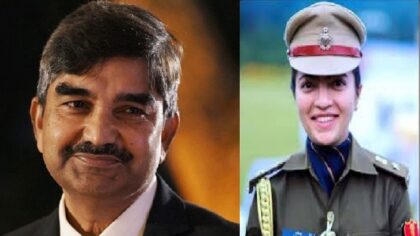जब आस्था को आधार बनाकर किसी विवादित ढांचे को गिराने की कार्रवाई को अपनी जीत के तौर पर देखा जाने लगता है, भले ही उसे अपराध की श्रेणी में गिना जाता हो, तो हमारे देश का ताना-बाना पूरी तरह से बिखर जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर रोक लगाकर सही कदम उठाया है।
तथ्य यह है कि मौजूदा सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, जो कि एक चिंता का विषय है। उनकी चुप्पी को उन लोगों के द्वारा मौन सहमति मान ली जाती है, जिन्हें इस बात का भय है कि अदालतों को उस एजेंडे को पूरा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसके चलते 6 दिसंबर, 1992 के दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो सका।
अतीत की कब्र खोदने के लिए अदालत जाने वालों का इरादा एक ऐसे माहौल को तैयार करने का है, जो एक खास राजनीतिक एजेंडे का पक्षपोषण करता करता है, जिसमें धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। (सी आर शशिकुमार)
“दोगुनी मेहनत और संकट खड़ा करने के परिणामस्वरूप; आग धधकने लगती है और देगची में उबाल आने लगता है।” यह एक तरह की ज़हरीली शराब है जब धर्म और उसके साथ भावनात्मक मंत्र राजनीतिक फायदे की खातिर विभाजन को जन्म देते हैं।
जब हम भारत के लोगों ने खुद के लिये भारत का यह संविधान तैयार किया, तो हमने कुछ बुनियादी सिद्धांतों को अंगीकार किया था, जो हमारे गणतंत्र की नींव के तौर पर हैं। यही कारण है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना नागरिकों के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, और इसके साथ ही नागरिकों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को भी बरकरार रखती है।
इसका आशय यह है कि इस देश के नागरिक को अपनी आस्था, अपने विश्वास में स्वतंत्रता रखने का हक है, जो कि एक अविभाज्य अधिकार है। इसके अनुसार पूजा करने का अधिकार हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में अंतर्निहित है। यह भारत में चलन में जारी सभी धर्मों के ऊपर लागू होता है, और जो हमारे बहु-सांस्कृतिक समाज का आधार-स्तंभ रहा है।
जब आस्था के आधार पर किसी कथित विवादित ढांचे को ढहा देने के कुकृत्य को अपनी जीत के तौर पर गिना जाने लगता है, भले ही इसे अपराध की श्रेणी में क्यों न गिना जाये, तो ऐसे में हमारे देश का ताना-बाना छिन्न-भिन्न हो जाता है। हमारे देश का इतिहास बर्बर आक्रमणों की बाढ़ से भरा पड़ा है, और उस दौर में तब कानून के शासन की अवधारणा प्रबल नहीं थी।
यदि अतीत की उन कथित ऐतिहासिक गलतियों को लेकर ऐसी शिकायतों के लिए अब उन लोगों से इसका प्रतिशोध लिए जाने की मांग की जाती है, जिनका इन कृत्यों से कोई लेना-देना नहीं है, तो वर्तमान हमारे गणतंत्र के फलने-फूलने के लिए एक असहज स्थान बन जाता है।
वर्तमान में रह रहे हमारे लाखों नागरिकों को अतीत के कथित बर्बर कृत्यों के लिए भला कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? ऐसे राजनीतिक एजेंडे जो हमारे गणतंत्र के नागरिकों को ऐसे कथित ऐतिहासिक गलतियों के लिए निशाना बनाकर उन्हें प्रताड़ित करने पर आमादा हैं, उनका कोई संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं है।
6 दिसंबर 1992 का दिन कई लोगों के लिए विजय दिवस के तौर पर था, लेकिन एक विशेष धर्म को मानने वालों के लिए यह एक त्रासदी के रूप में रहा। इस अशांत जल को शांत करने और भविष्य में इस प्रकार की किसी संवैधानिक वहशत को खत्म करने के लिए, संसद ने 1991 में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान), अधिनियम 1991 (“1991 का अधिनियम”) को लागू करने का फैसला लिया था।
अपनी अंतर्वस्तु में, यह कानून इस बात को निर्धारित करता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन पूजा स्थलों का जो चरित्र था, उसमें उसके बाद से कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भारत स्वतंत्र हुआ और 26 नवंबर 1950 को हमारे संविधान को अंगीकार किया गया, तो हमारे संविधान, हमारे गणराज्य ने संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता का भरोसा दिया था।
इसमें कहा गया है कि “सभी व्यक्ति समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता के हकदार हैं और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार के हकदार हैं।”
सैकड़ों वर्ष पूर्व किये गये कृत्यों के लिए अतीत के घावों को फिर से कुरेदने के हालिया प्रयास, वर्तमान का खलनायकीकरण करने और सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले साबित हो रहे हैं। हर दूसरे दिन, हम देखते हैं कि अदालतों को एक विशेष समुदाय के पूजा स्थलों के खिलाफ संदिग्ध ऐतिहासिक दावों के लिए युद्ध के मैदान के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है।
ये दावे ऐसे संदिग्ध दावों पर आधारित हैं कि वास्तव में मौजूद संरचनाएं उस स्थान को मलबे में तब्दील कर बनाई गई हैं जहां अन्य धर्म के पूजा-पाठ का पालन किया जा रहा था। ऐसी याचिकाएं अपने आप में ऐसी हरकतें हैं जो संविधान के उन मूल्यों के साथ असंगत भावनाओं को भड़काने का काम कर रही हैं जिन्हें हमने अंगीकार किया हुआ है।
12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के जरिये ऐसी सभी याचिकाओं पर रोक लगा दी है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है।
न्यायालय के पास इस बात को साबित करने का कोई कानूनी आधार नहीं है कि ऐसे कृत्य वास्तव में कथित ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं। वास्तव में, किसी तथ्य के अस्तित्व का न्यायिक निर्धारण करने के लिए न्यायालय द्वारा किया गया ऐसा प्रयोग अपने आप में घातक साबित हो सकता है और नए विवाद को जन्म देता है।
ऐसे स्थानों पर इबादत करने वाले लोग खुद को निशाना बनाए जाने के रूप में अनुभव करने लगते हैं। जबकि दूसरे लोग उनकी बेचैनी को अपनी जीत समझने लगते हैं। इससे भय और अनिश्चितता दोनों का माहौल बनता चला जाता है।
ऐसे सभी दावों पर जिस तेजी से न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये हैं और जिस तेजी से सरकारी एजेंसियां कार्रवाई पर उतारू हो जाती हैं, उससे पता चलता है कि यह एक साधारण मुकदमेबाजी से कहीं अधिक है।
कुछ मुकदमे इस आधार पर दायर किए गए हैं कि संबंधित पूजा स्थल एक संरक्षित स्मारक है और इसलिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा 15 के तहत इसकी पहुंच से इनकार नहीं किया जा सकता है।
हालांकि, धारा 13 के तहत वही अधिनियम इस बात को निर्धारित करता है कि सरकार द्वारा बनाए गए पूजा स्थल या तीर्थ का उपयोग उसके चरित्र के साथ असंगत किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, धारा 16 के संदर्भ में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 की धारा 13 में निर्धारित किए गए नियमों को निर्धारित करता है।
यह पूजा स्थलों के संबंध में है, जिनका रखरखाव सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 25 किसी भी स्थिति में, सभी पूजा स्थलों को उनके चरित्र को बदले जाने से बचाव प्रदान करता है, चाहे उनका रखरखाव सरकार द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं।
इसलिए, क़ानून के आधार पर किए गए कोई भी दावे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं।
यह तथ्य कि वर्तमान सरकार इस मुद्दे पर साधे हुए है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। उनकी चुप्पी को उन लोगों के द्वारा मौन सहमति मान लिया जाता है, जो इस बात से आशंकित हैं कि अदालतों को उस एजेंडे को पूरा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसके नतीजे के तौर पर 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था।
अतीत की कब्र खोदने के लिए अदालत का रुख करने वालों का इरादा एक ऐसे माहौल को निर्मित करने का है जो एक खास राजनीतिक एजेंडे का समर्थन करता है, जिसमें धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। बहुसंख्यकवाद की जीत इसका मकसद है।
मेरे विचार में, एक खास राजनीतिक दल के समर्थन के बल पर अदालत का रुख करने का इरादा एक बहुसंख्यक वोट बैंक के निर्माण से जुड़ा हुआ है, जो जाति और पंथ से परे जाकर एक ऐसी शक्ति के बतौर कायम हो जाए जो धर्म के आधार पर “हम” और “उन” में अंतर पैदा कर सके।
इसके साथ ही कुछ लोगों के द्वारा नफरत फैलाने वाले भाषणों और अन्य लोगों द्वारा नफरत की बेलगाम अभिव्यक्ति के साथ मिलकर यह उस आंदोलन का हिस्सा बन जाता है, जिसकी शुरुआत आडवाणी की रथयात्रा के साथ हुई थी।
यदि हमारी राजनीति ने हमारे गणतंत्र के संवैधानिक मूल्यों को अपनाया होता, तो ऐसी घटनाएं कभी भी देखने को नहीं मिलतीं। 1991 के अधिनियम की भी कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे कानून के अस्तित्व में होने के चौबीस वर्ष बाद भी हम अतीत के उन घावों को फिर से ताजा करने पर उतारू हैं, जिन्हें संविधान ने अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया हुआ है।
धर्म को एक राजनीतिक औजार के तौर इस्तेमाल करना असल में गणतंत्र की अवधारणा के लिए अभिशाप बन गया है। धर्म को अपने घर चारदीवारी के भीतर और समुदाय की भलाई के लिए पालन करना और इसे पनपने देना सबसे उचित है।
साभार: इंडियन एक्सप्रेस, इस लेख के लेखक कपिल सिब्बल, राज्यसभा के सांसद होने के साथ-साथ देश के जाने-माने वकील हैं।