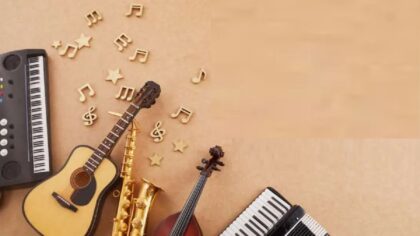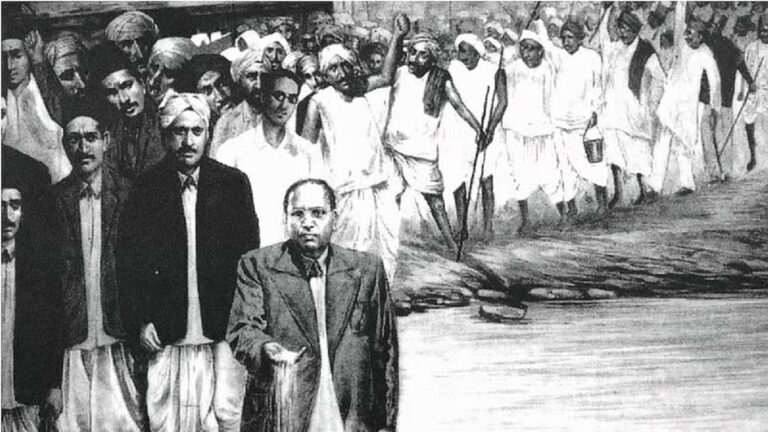औद्योगिक क्रान्ति की शुरूआत तथा पूंजीवादी व्यवस्था के जन्म के समय मज़दूरों का अमानवीय शोषण होता था। काम के घंटे तय नहीं थे। दस से पंद्रह घंटे काम करने पर भी मज़दूरी कम मिलती थी, लेकिन महिला कामगारों की स्थिति उससे भी ज़्यादा खराब थी।
औरत होने के कारण उन्हें दोहरी गुलामी झेलनी पड़ती थी। पुरुषों से कम वेतन तो था ही, मातृत्व लाभ जैसी कोई स्थिति नहीं थी। कामगारों के शोषण के ख़िलाफ़ बड़े आंदोलन चले, इससे काफ़ी हद तक मज़दूरों की स्थिति में सुधार हुआ। काम के घंटे निश्चित हुए।
मज़दूरी वेतन आदि में भी काफ़ी हद तक सुधार हुआ, इसका फ़ायदा महिला कामगारों को भी मिला। काफ़ी हद तक महिला-पुरुष कामगारों के वेतन में समानता आई। ये सब मज़दूरों के विशेष रूप से कम्युनिस्टों के आंदोलन के कारण हुआ, परन्तु नब्बे के दशक में दुनिया भर में नव उदारवादी नीतियां लागू होने के बाद स्थितियां बदलने लगीं।
बड़े पूंजीपतियों तथा कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए श्रम कानूनों को शिथिल कर दिया गया। निजीकरण की अवधारणा के कारण स्थायी मज़दूरों की जगह ठेके पर मज़दूर रखे जाने लगे, जिससे कम वेतन पर असीमित काम करवाया जा सके। इन नीतियों से सबसे खराब प्रभाव महिला कामगारों पर पड़ा। यह प्रवृत्ति तीसरी दुनिया के देशों से लेकर विकसित दुनिया के देशों में भी देखी जा रही है।
अभी हाल में ‘अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन’ द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें विश्व श्रम शक्ति में लैंगिक असमानता और अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रही औरतों की समीक्षा की गई है। इस रिपोर्ट से यह और भी स्पष्ट होता है कि ‘बराबरी’ के नारे से विश्व स्तर पर स्थापित हुई पूंजीवादी ढांचे में आज हर कार्य क्षेत्र में कैसे औरतों के साथ भेदभाव होता है।
आंकड़ों के मुताबिक़ इस समय विश्व स्तर पर कुल कामगारों में औरतों की संख्या बहुत कम है। केवल 39.5 प्रतिशत औरतें ही काम पर लगी हुई हैं। उत्तरी अमेरिका में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत और दक्षिण एशिया में 34 प्रतिशत है।
अगर हम भारत की बात करें, तो हालांकि रिपोर्ट 37.7 प्रतिशत औरतों के काम पर लगे होने की बात करती है, लेकिन इससे पहले जारी हुई अन्य रिपोर्टों के मुताबिक़ भारत में यह आंकड़ा बहुत कम है। कुल श्रम शक्ति में औरतों की संख्या का कम होना दर्शाता है कि कैसे बहुसंख्यक औरतों को आज इक्कीसवीं सदी में भी घरों की रसोई तक ही सीमित रखा गया है।
कुल कामगारों में औरतों की संख्या कम होने के कई कारण हैं-
- पहला पूंजीवादी व्यवस्था सस्ती से सस्ती श्रम शक्ति चाहती है, ताकि इसका शोषण करके अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमा सके, इसीलिए इस व्यवस्था में औरतों, बच्चों,प्रवासी मज़दूरों आदि की भयंकर लूट होती है और अक्सर उन्हें क़ानून द्वारा निर्धारित नियमों के तहत मज़दूरी और अन्य सुविधाएं भी नहीं मिलतीं।
- भारत में भी औरतों, बाल मज़दूरों और प्रवासी मज़दूरों के श्रम को पूंजीपतियों द्वारा लूटा जाता है, लेकिन दूसरी ओर अनुभवहीन या कम अनुभवी होने के कारण आर्थिक मंदी या सुस्ती का सबसे पहला शिकार भी अक्सर औरत मज़दूर ही बनती हैं।
- कोरोना काल के बाद स्पष्ट देखा जा सकता है कि बेरोज़गारी की सबसे ज़्यादा मार औरत मज़दूरों पर पड़ी है और वह श्रम बाज़ार से बाहर कर दी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि औरतें इस वजह से बेकार हो गई हैं, बल्कि औरतों और मर्दों के बीच जो काम का बंटवारा है, उसके कारण सामाजिक उत्पादन में शामिल औरतें अपनी श्रम शक्ति का बड़ा हिस्सा ऐसे कामों में ख़र्च करती हैं, जिसके एवज़ में उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता।
- घर में खाना बनाना, बच्चों, बुज़ुर्गों की देखभाल करना और घर संभालना आदि आज भी उनका मुख्य काम माना जाता है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक़ अगर इस काम को भी अर्थव्यवस्था में शामिल कर लिया जाए तो यह कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 40% बनेगा। ज़्यादातर औरतों के लिए ये काम का बोझ वे बेड़ियां हैं, जो उन्हें घर की चारदीवारी के अंदर बंद करके सामाजिक उत्पादन में हिस्सा लेने से रोकती हैं।
- औरतों की श्रम शक्ति में घट रही हिस्सेदारी का दूसरा कारण आज के पूंजीवादी भारत में आज भी औरतों के प्रति सामंती मानसिकता का गहराई तक बैठे होना है। बेटी घर की इज्ज़त होती है, बाहर काम करने वाली औरतें चरित्रहीन बन जाती हैं या बिगड़ जाती हैं, जैसे विचार आज भी बड़ी गिनती में आबादी के मनों में घर किए बैठे हैं।
- तीसरा कारण यह भी है कि इस समाज में क़दम-क़दम पर औरतों को भद्दी टिप्पणियों, छेड़छाड़ और शोषण का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारी औरतें बहुत सोच-विचार करके ही कहीं काम करने के लिए तैयार होती हैं और काम करने के लिए कुछ ख़ास पेशे ही चुनती हैं। ये सारी बातें केवल भारत में ही नहीं, बल्कि छोटे या बड़े रूप में विश्व के लगभग सभी मुल्क़ों में ही देखने को मिलती हैं।
- औरतों की कम हुई हिस्सेदारी का चौथा कारण कोरोना काल के बाद दसियों लाख की गिनती में लड़कियों की पढ़ाई छुड़वाकर उनका जबरन विवाह किया जाना भी है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 37% लड़कियां कोरोना काल के बाद कभी भी वापस स्कूल नहीं गईं। ज़ाहिर है कि इनमें से बहुत-सी लड़कियों को आगे पढ़ने या रोज़गार करने का मौक़ा भी नहीं मिला और उनको ब्याह दिया गया।
कुल श्रम शक्ति में कम हिस्सेदारी के अलावा इस रिपोर्ट के आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि औरतों की ज़्यादातर हिस्सेदारी कुछ ख़ास क्षेत्र के कामों में होती है। उदाहरण के तौर पर स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल जैसे काम, अध्यापन, दफ़्तरी कामकाज, नर्सिंग आदि में औरतों की भूमिका 90% के लगभग है।
अगर हम विज्ञान,तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित आदि की बात करें, तो यहां औरतों की गिनती नाममात्र है। केवल 38 फ़ीसदी औरतें कंप्यूटर क्षेत्र में काम कर रही हैं और केवल 24 फ़ीसदी लड़कियां इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। इसका कारण यही है कि इन तकनीकी विषयों के लिए ख़ास महारत चाहिए होती है, जिसके लिए अक्सर पढ़ाई की मियाद भी लंबी होती है।
लेकिन हमारे समाज में औरतों पर रोज़गार के अलावा घर की ज़िम्मेदारी, बच्चों के पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी आदि भी डाली जाती है। ये सब अतिरिक्त ज़िम्मेदारियां निभाते हुए उनके लिए ऐसी महारत और लंबी अवधि वाली पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है।
दूसरा, शिक्षा के निजीकरण के कारण इन क्षेत्रों में काम करने के लिए जो शिक्षा चाहिए, वह बहुत महंगी है। भारत जैसे पिछड़े मुल्क़ों में जहां लड़कियों को जल्दी ब्याह देने की प्रथा है, जहां सोच यह है कि लड़की ने ब्याह करके ससुराल जाना है, उसकी कमाई भी साथ ही जाएगी, जबकि लड़के की कमाई घर में ही रहेगी, इसलिए ऐसी महंगी पढ़ाई आमतौर पर लड़कों को ही ज़्यादा करवाई जाती है।
ऐसा करके भी ऐसी शिक्षा तक और नतीजतन इन क्षेत्रों तक औरतों की पहुंच सिमटकर रह जाती है। अगर घरेलू काम का समाजीकरण कर दिया जाए।
बढ़िया बालघर, बेहतरीन मेसों आदि के ज़रिए घर की ज़िम्मेदारियों को अधिक से अधिक समाज की ज़िम्मेदारियां बना दिया जाए और हर स्तर की पढ़ाई मुफ़्त हो तो लाज़िमी ही औरतों को भी पढ़ने-लिखने और काम करने के लिए बराबर का माहौल मिलेगा और अलग-अलग कामों की जो बांट इस पूंजीवादी व्यवस्था ने बनाकर रखी है, यह भी ख़त्म होगी।
समाजवादी सोवियत यूनियन और समाजवादी चीन की उन्नत मिसालें हमारे सामने हैं, जहां समाजवादी सरकार ने शिक्षा मुफ़्त करके घरेलू कामों का बड़े स्तर पर समाजीकरण करके औरतों को सही अर्थों में चूल्हे-चौके और अन्य ग़ैर-ज़रूरी ज़िम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था, जिसके कारण औरतें हर क्षेत्र में आगे बढ़ी थीं।
तनख़्वाह के अंतर के अलावा औरतों की स्थिति काम के क्षेत्र की गुणवत्ता के मामले में भी भेदभाव वाली है।
संगठित क्षेत्र के मुक़ाबले ग़ैर-संगठित क्षेत्र में औरतों की हिस्सेदारी अधिक है। संगठित क्षेत्र को आमतौर पर अधिक टिकाऊ रोज़गार माना जाता है, जहां मज़दूरों को एक हद तक थोड़ी-बहुत सुविधाएं भी हासिल हो जाती हैं, जबकि ग़ैर-संगठित क्षेत्र में मज़दूर आमतौर पर बिना किसी रोज़गार सुरक्षा के बिना किसी सुविधा के काम करते हैं।
विश्व स्तर पर 58 फ़ीसदी औरतें ग़ैर-संगठित क्षेत्र में काम करती हैं। इस मामले में भी औरतों की हालत मर्द मज़दूरों से अधिक बदतर है। पूंजीपतियों द्वारा औरतों की सस्ती श्रम शक्ति को असुरक्षित ग़ैर-संगठित कामों के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ा जाता है।
अगर हम भारत की बात करें, तो आंकड़ों के मुताबिक़ लॉकडाउन के बाद संगठित क्षेत्र की तुलना में औरतों की हिस्सेदारी ग़ैर-संगठित क्षेत्र में बढ़ी है। साल 2018-19 में कुल कामगार औरतों का लगभग 59 फ़ीसदी (39 फ़ीसदी कृषि और 20 फ़ीसदी घरेलू काम-धंधे में) ग़ैर-संगठित क्षेत्र के धंधों में लगा हुआ था, जो 2021 में बढ़कर 67% हो गया।
इस ग़ैर-संगठित क्षेत्र में काम करने वाली औरतें अक्सर ही आर्थिक लूट के साथ-साथ शारीरिक शोषण, गाली-गलौच आदि का भी शिकार होती हैं। औरत मज़दूरों से अक्सर काम तो मर्द मज़दूरों के बराबर लिया जाता है, लेकिन तनख़्वाह उनके मुक़ाबले में बहुत कम दी जाती है।
नव उदारवादी नीतियों ने औरतों के शोषण को भयानक रूप से बढ़ा दिया है। भूमंडलीकरण की नीतियों तथा मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था में दुनिया के बड़े कॉरपोरेट उन देशों में अपने सामान का निर्माण करा रहे हैं, जहां श्रम कानून बहुत शिथिल हैं तथा बहुत कम वेतन पर मज़दूरों से काम करवाया जा सकता है।
चीन, वियतनाम, दक्षिणीकोरिया, बांग्लादेश तथा अफ्रीका के अनेक देश इसके उदाहरण हैं। इन देशों में सस्ते माल बनाने के लिए मज़दूरों का उसी तरह शोषण हो रहा है, जैसे की पूंजीवाद के प्रारम्भिक समय में जब औद्योगिक क्रान्ति हुई थी, तब हो रहा था।
निश्चित रूप से महिला कामगारों की स्थिति इन सभी देशों में और भी ज़्यादा खराब है। भूमंडलीकरण की नीतियों के विरोध में बड़ा वैश्विक आंदोलन ही इन हालातों को बदल सकता है।
(स्वदेश कुमार सिन्हा लेखक व स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)