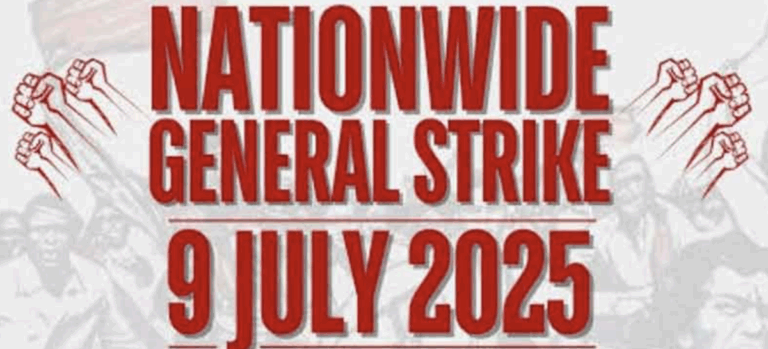भारतीय आज़ादी के इतिहास को ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ने के आदी हम लोगों के लिए कोरेगांव परिघटना और बाबा साहब द्वारा उसके महत्त्व के रेखांकन को समझना बहुत मुश्किल है।
फिलहाल दो तीन बातें, सत्तावन की क्रान्ति के असफल हो जाने के बाद जो नए सिरे से राष्ट्रवाद का उभार हुआ, यह नव मध्यवर्ग अपने को सत्तावन से सायास अलग करता था। इनमें सम्बन्ध ढूंढने की काफी कवायद की गयी पर अलगाव के ही बिंदु ज्यादा हैं।
सत्तावन की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का एक वर्ग यह भी मानता है कि वह सफल होती तो पुराने रजवाड़ों का शासन कोई बेहतर नहीं होता। इसे न मानने वाले और सत्तावन की क्रांति को जनविद्रोह मानने वाले वाम और दक्षिण दोनों खेमों में बहुतायत में हैं।
सत्तावन की क्रांति से अंग्रेजों ने ये सबक लिया कि भारत के सामाजिक ढाँचे में न्यूनतम छेड़छाड़ की जाए तो राज करना सुभीते का काम रहेगा।
जो नवमध्यवर्ग उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरा, उसे भारत का स्वर्णिम अतीत वाला इतिहास यूरोपीय इतिहासकारों ने ही उसे थमाया था। यूरोपीय इतिहास दृष्टि अपना स्वर्ण युग ग्रीस में ढूंढती थी, हमारे लिए ये काम वैदिक युग ने किया और यूरोपीय अन्धकार युग हमारे यहाँ इस्लाम से जुड़ा मध्यकाल बन गया। अब मजेदार यह है कि कट्टर पुनरुत्थानवादियों से लेकर सुधारवादियों तक दोनों अक्षांश पर खड़े स्वतंत्रतासेनानी अपने-अपने कारणों से अंग्रेज़ी शासन के प्रति शुक्रगुजार दिखाई देते हैं। यूरोपीय इतिहास बोध से रचित राष्ट्र की अवधारणा एक सामुदायिक अवधारणा बनने के लिए अभिशप्त थी और तमाम छोरों पर खड़े स्वतंत्रता सेनानियों के यहां उनकी जाति, धर्म, वर्ग की सीमाओं से गढ़ी राष्ट्र की छवि और बहुत असुविधाजनक चिंतन मिलता है। अमूमन राष्ट्रवादी इतिहास लेखन (जिसमें एक बड़ा हिस्सा मार्क्सवादियों का था) ने इन असुविधाजनक तथ्यों की चयनित उपेक्षा ही की है। उत्तर औपनिवेशिक और सबाल्टर्न इतिहासकारों की नई पीढ़ी ने पिछले तीन दशकों में इस पर काम किया है। ध्यान रहे, यह ‘पाप’ मार्क्सवादियों ने नहीं बल्कि उनके प्रतिरोध में उभरी इतिहास लेखन की नई शाखा ने किया है।
बहरहाल, समाज सुधार बनाम राजनीतिक स्वतंत्रता, इनकी समानांतरता या किसी एक की प्राथमिकता के सवाल पूरे स्वतंत्रता आन्दोलन की बहसों में दिखाई देते हैं, चाहे हम उन्हें अपनी सुविधानुसार न सुनते आये हों। महाराष्ट्र इन बहसों की सबसे उर्वर भूमि रहा है। याद रहे, सत्तावन की क्रांति के बरअक्स ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई पहला लड़कियों का स्कूल खोल रहे थे। अब यह कोई संयोग नहीं है कि ‘पहले राजनीतिक स्वतंत्रता’ के आग्रही सवर्ण अभिजात पुरुष ही दिखाई देते हैं। शारदा एक्ट से लेकर पूना पैक्ट तक ‘राजनीतिक स्वतंत्रता’ के आग्रही इन सवर्ण स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिगामी भूमिका ही दिखती है।
इन सब ध्रुवों की उपेक्षा करने वाला चतुर इतिहासकार ‘वरशिपिंग फाल्स गॉड्स’ लिखता है जिसमें आंबेडकर को अंग्रेजों का समर्थक साबित करता है। वैसे जैसा मैंने पहले लिखा इतिहास के एक ख़ास मोड़ तक अंग्रेजों के प्रति स्वाभाविक शुकराना और उनके सहयोग से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रवृत्ति सुधारवादियों और पुनरुत्थानवादियों, दोनों में ही दिखती है। अतः यदि शौरी की तरह बेईमान उखाड़-पछाड़ करनी होती तो किसी को भी अँगरेज़ समर्थक साबित किया जा सकता था।
स्वतन्त्र भारत के शुरुआती चार दशकों तक सशक्त रहा मार्क्सवादी इतिहास लेखन यदि कोई चयनित उपेक्षा करता भी रहा था तो उसका कारण मुख्यतः एक सदिच्छा ही माना जा सकता है। एक समन्वित राष्ट्रवाद का स्वरूप गढ़ने की कोशिश। समन्वित राष्ट्रवाद में वर्चस्वशाली स्वर ही प्रमुखता पाते हैं अतः एक समय के बाद उसका प्रतिरोधी स्वर आता ही है। अतः एक मायने में यह मंथन अपरिहार्य भी है और अच्छा भी। बस, डर है तो यह कि व्हाट्सएप इतिहास लेखन के द्रुतगामी दौर में यह मंथन बेहद विकृत रूप ले सकता है।
( हाँ, एक आख़िरी बात, जब मैं पुनरुत्थानवादी और समाजसुधारकों के दो मोटा-मोटी विभाजन करके अपनी बात कह रहा हूँ तो इसमें पुनरुत्थानवादी खेमे से आशय नए-नए उगे संघी स्वतंत्रता सेनानियों से नहीं है। वे स्वतंत्रता संग्राम में कहीं नहीं थे।)
(हिमांशु रविदास अध्यापक हैं और ये लेख उनके फेसबुक वाल से साभार लिया गया है।)