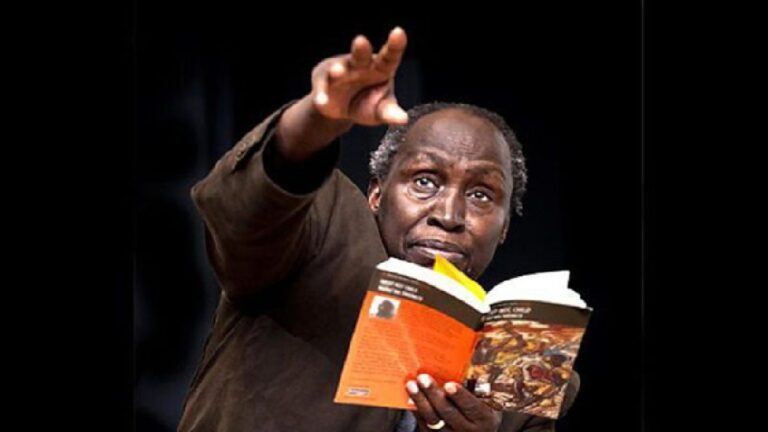मानसून सत्र में जब विपक्ष प्रधानमंत्री से संसद में आकर बयान देने का आग्रह कर रहा था तब काफी हंगामे के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हम बहस के लिए तैयार हैं, आप क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने भी एक बात कही; वह विपक्ष की ओर मुखातिब होते हुए बोले कि बयान कौन देगा, यह आप तय नहीं करेंगे। इसके बाद तो काफी हंगामा होता रहा। एक सांसद को मानसून सत्र से ही बर्खास्त कर दिया गया। कई को चेतावनी दी गई और अंततः विपक्ष एकजुट होकर संसद परिसर में धरने पर बैठ गया।
पिछले नौ सालों में संसद में इस तरह के कई दृश्य पैदा हुए। सांसदों को निलंबित करना, उनके भाषणों की कांट-छांट करना, सांसदों, खासकर विपक्ष द्वारा धरना देना, विरोध मार्च निकालना आदि घटनाएं निरंतर बनी हुई हैं। यह सब नये संसद भवन के उद्घाटन के दौरान भी हुआ। आमतौर पर इस दृश्य को आम घटना की तरह देखा और पेश किया जाता रहा है। कुछ मीडिया प्लेटफार्म इसे अभूतपूर्व बताकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन, यदि इसे ध्यान से देखा जाय तो यह एक पैटर्न की तरह है जो लगातार बढ़ता गया है।
सबसे पहले तो यह समझना है कि संसदीय लोकतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार बना है और यह उसी के अनुसार चलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तब यह संवैधानिक उसूलों का उलघंन करता है और इससे निश्चय ही वह जमीन तैयार होती है जिसमें संविधान आधारित लोकतंत्र क्षरित होता जाता है। संविधान का अनुच्छेद 74, 75 और 76 और इनकी उपधाराएं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उसके अधिकार आदि को तय करती हैं। इसी संदर्भ में केंद्र शासित राज्यों और राज्यों के संबंध में भी संविधान के अनुच्छेद इन मसलों की कार्यकारी और संरचनागत व्यवस्था देते हैं।
नागरिक शास्त्र की बेहद प्राथमिक किताबें भी बताती हैं कि संसद में बहुमत हासिल दल को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। यह प्रधानमंत्री देश की आंतरिक और बाह्य दोनों ही मसलों और प्रमुख निर्णयों के लिए उत्तरदायी होता है। यदि मसला बड़ा हो तब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी मुख्य हो जाती है। यह बड़े मसले आंतरिक सुरक्षा से लेकर आपदा आदि तक के हैं; वे निर्णय भी हैं जिनसे देश की जनता पर निर्णायक असर पड़ रहा हो।
ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह का यह कहना कि वह चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष तैयार नहीं है, इन प्रावधानों का सीधा उलघंन है। प्रधानमंत्री देश में हैं और संसद से बाहर बयान भी दे रहे हैं लेकिन संसद में बयान नहीं दे रहे हैं। पहली बात, मसला सिर्फ बयान देने का नहीं है। मणिपुर में लगभग तीन महीनों से चल रहे दो समुदायों के बीच खूनी जंग, जिसमें प्रशासन व्यवस्था अनुपस्थिति हो चुकी है और राजनीतिक व्यवस्था काम ही नहीं कर पा रही है, लोगों का जीवन और उसकी गरिमा नष्ट हो रही है; इस पर सिर्फ बयान और चर्चा ही नहीं, इसमें प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी तय होनी है। इसमें सिर्फ गृहमंत्री की जिम्मेदारी ही नहीं राज्य के मसलों में प्रधानमंत्री की संवैधानिक जिम्मेदारी भी तय होनी है और इसके लिए उचित कदम उठाने हैं।
प्रधानमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद का अस्तित्व नहीं होता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच प्रधानमंत्री होता है और उसी के द्वारा ही सरकार के द्वारा निर्णय और प्रस्ताव राष्ट्रपति तक पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री के बिना दल के बहुमत का भी कोई अर्थ नहीं होता। प्रधानमंत्री यदि इस्तीफा दे दे तब दल को एक नया नेता चुनना होता है और उसे संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से एक बार संसद में अपना बहुमत और राष्ट्रपति की मंजूरी और उससे शपथ लेना होता है।
पिछले 9 सालों में जब प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के निर्णय और उनकी गलतियों को लेकर जिस तरह संसद में व्यवहार किया जा रहा है उसमें जिम्मेदारी तो दूर की बात, उस पर बयान देना भी गवारा न करने का चलन बढ़ता हुआ दिख रहा है। यदि आप नोटबंदी को याद करें; तब आप को प्रधानमंत्री नोटबंदी से जुड़े बड़े-बड़े दावे आम सभाओं में करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वह संसद में बोलते हुए नहीं दिखते हैं। वह आरोप लगाते हुए जरूर मिल जायेंगे कि विपक्ष उन्हें बोलने नहीं दे रहा है; विपक्ष भ्रष्ट है इसलिए उसे नोटबंदी से दिक्क्त है…आदि। वह विदेश में जाकर बोल आये लेकिन संसद इस मसले पर जो बहस चाहता था, वह नहीं हो पाया। इस निर्णय की प्रक्रिया आज भी कोई नहीं जान पाया।
इसी तरह कोविड-19 को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा अचानक किया गया लाॅकडाउन था। यह मसला भी देश को बर्बादी की कगार पर ले जाना वाला निर्णय था जिसमें लोगों का जीवन-मरण जुड़ा था। लोग पैदल चलकर मरते और बर्बाद होते रहे, उद्योग बर्बादी के मुहाने पर पहुंच गये, लेकिन यह मसला भी संसद में बहस से कमोबेश दूर ही रहा। एक साल तक चले किसानों पर प्रधानमंत्री का रुख और संसद के प्रति बेरुखी और अभी हाल में खेल जगत में महिलाओं के शोषण को लेकर महिला पहलवान खिलाड़ियों के प्रर्दशन पर इसी तरह का रवैया हम देख चुके हैं।
यदि प्रधानमंत्री के संसद और मंत्रिपरिषद के प्रति व्यवहार को देखें, तो उसमें संवैधानिक प्रावधानों और परम्पराओं का निहायत अभाव ही नहीं, उसे न मानने का बढ़ता हुआ रुख दिखेगा। मसलन, चीन के मसले पर जब वह संसद में बोल रहे थे, उनके तथ्य और जो मीडिया और अन्य स्रोतों से जो तथ्य सामने आ रहे थे, उससे वे मेल नहीं खा रहे थे। इसी तरह मणिपुर को लेकर जो बयान मीडिया में दिया वह भी बेहद भ्रामक है। जैसे मणिपुर की महिला संबंधी घटना को राजस्थान आदि राज्यों से जोड़कर देखना। इस बयान से मणिपुर की वास्तविक स्थिति का पता ही नहीं चलता, जैसा वहां की गवर्नर, पुलिस बल, पार्टियां, संगठन और मीडिया बता रहे हैं।
इस संदर्भ में एक और मसले पर जरूर ध्यान देना चाहिए, और वह है विपक्ष के सांसदों की सदस्यता और उपस्थिति को लेकर जिस तरह से दोनों सदन के अध्यक्ष महोदय रुख अख्तियार कर रहे हैं, वह बेहद चिंता की बात है। यह निश्चित रूप से संसदीय लोकतंत्र की परम्परा, जिसे एक प्रावधान की तरह देखने का रिवाज है; पर गंभीर हमला है।
यदि बहुमत दल का नेतृत्व संवैधानिक उसूलों पर सरकार बनाने में कामयाब हो जाये और फिर खुद उस संरचना से बाहर जाकर उन्हीं संवैधानिक अधिकारों पर काम करने लगे, उत्तरदायित्व को दरकिनार करने लगे और प्रधानमंत्री खुद की मंत्रिपरिषद के काम पर भी दावा करने लगे; तब संविधान के ज्ञाताओं को जरूर इस पर नजर डालनी होगी और इसकी व्याख्या करनी होगी।
कई प्रबुद्ध लोगों को लगता है कि खुद को एक कद्दावर नेता के रूप में पेश कर जनता में अपनी इमेज को एक अवतारी रूप में रखकर चलने की वह रणनीति है जिससे उस नेता के नाम से वोट मिले। यह कथित निर्णयकारी व्यक्तित्व का मुजाहरा है। ‘एक अकेला सब पर भारी’ इसका नारा है। निम्न-बुर्जआ समाज और भुखमरी की ओर बढ़ रहे गरीब-किसानों में ऐसे व्यक्तित्व कई बार आकर्षक विकल्प बनते हैं और इस व्यक्तित्व को गढ़ने में सट्टेबाज पूंजीपतियों और गांव के सूदखोरों और पतित भू-स्वामियों से खूब समर्थन भी मिलता है।
कई बार ऐसी स्थितियां भयावह शक्ल ले लेती हैं और इस तरह के व्यक्तित्व वाला राजनेता ऐसी सनक का शिकार हो जाता है जो उपरोक्त वर्गों के लिए सहायता करता तो दिखता है लेकिन पूरे देश को कत्लगाह में बदल देता है, पूंजी और श्रम की उत्पादक क्षमता को खा जाता है और इस सबकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेता है। 1942-44 का जर्मनी इसका एक क्लासिक उदाहरण है। जहां संसद को प्रक्रिया में बेकार बना दिया गया और संसद का प्रयोग तभी किया गया जब इसकी जरूरत हुई और इसे तब नष्ट कर दिया गया जब इसकी जरूरत रह ही नहीं गई थी।
भारत में जिस तरह से संसदीय लोकतंत्र चल रहा है उसके सामने कई खतरे आ खड़े हुए हैं। विपक्ष इस संसद को लेकर चिंतित है। लेकिन, उसकी असफलता इसमें है कि सरकार को वह उसकी जिम्मेदारियों के प्रति जबाबदेह नहीं बना पा रहा है। वह प्रधानमंत्री की असफलता के आधार पर उनके निर्णय की क्षमता पर सवाल नहीं बना पा रहा है। संसद में आकर बयान देने से कतराने को लेकर जनता में एक गैर-जिम्मेदार प्रधानमंत्री की इमेज नहीं बना पा रहा है।
विपक्ष प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की कार्यशैली को संविधान के परिप्रेक्ष्य में रखकर लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौती का अब भी एक मसला नहीं बना पा रहा है। विपक्ष की यह असफता एक घातक निर्णय तक जा सकती है और इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विपक्ष जन और राष्ट्रविरोधी रुख ले रहा है। सांसद और विपक्ष के एक महत्पूर्ण नेता को संसद से बाहर कर देने के पीछे की कहानी में कोर्ट के निर्णय के पहले झूठी खबर के सहारे संसद और संसद के बाहर एक ओपिनियन बनाया गया।
इसी तरह हाल ही में बंगाल में हुए चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर यह माहौल बनाया जा रहा था कि तृणमूल पार्टी लोकतंत्र के अनुकूल है भी या नहीं; हालांकि इस बहस को जल्द ही तिलांजली दे दी गई। महाराष्ट्र में विपक्ष मुक्त सरकार बनाकर एक उदाहरण पेश किया जा चुका है। ऐसे में, संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष का अर्थ तभी तक है, जब तक वह प्रधानमंत्री को संवैधानिक उसूलों के सामने खड़ा करे और उन ताकतों को बेनकाब करे जो प्रधानमंत्री जैसे पद को संविधान, संसद, मंत्रिपरिषद और यहां तक कि जन के ऊपर बैठा रहा है। यह वह एक रास्ता है जिससे संसदीय लोकतंत्र का बहुसंख्यावाद एक अहम् ब्रह्मास्मि में बदलने से रुक सकेगा।
(अंजनी कुमार पत्रकार हैं।)