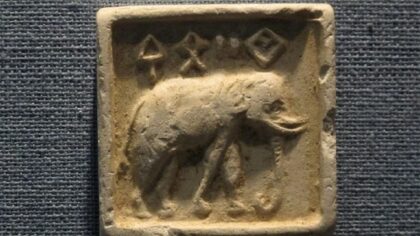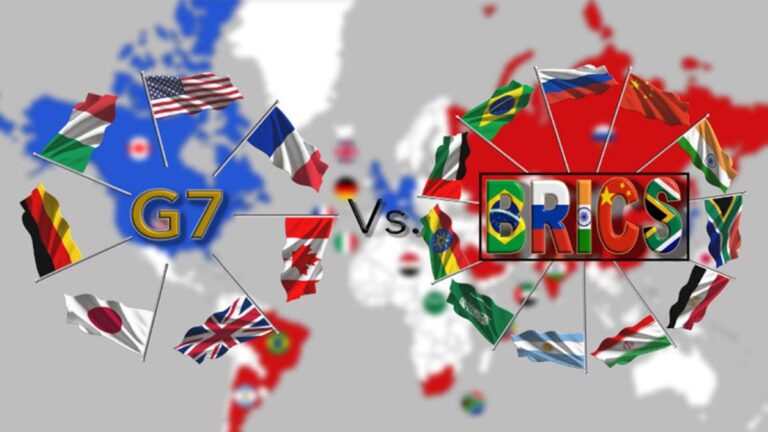आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की ताजा रिपोर्ट जारी होने पर मीडिया में खुशनुमा सुर्खियां बनीं कि आखिरकार देश में बेरोजगारी की दर बेहद निम्न हो गई है। बताया गया कि 2022-23 और 2023-24 के बीच बेरोजगारी दर सिर्फ 3.2 प्रतिशत रही, जो 2017-18 के बाद सबसे निम्न दर है।
इस तरह ये धारणा पेश की गई कि कोरोना महामारी से आवीजिका पर जो मार पड़ी थी, भारत उससे उबर गया है।
ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पीएलएफएस यानी पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे सबसे 2017-18 में ही किया गया था। इसके पहले की सरकारों के दौर में हर पांच साल पर रोजगार-बेरोजगारी सर्वे होता था। इस सर्वे में 2011-12 में बेरोजगारी दर 2.2 प्रतिशत रही थी।
ताजा सर्वे में यह भी बताया गया है कि देश में श्रम शक्ति भागीदारी दर (एलएफपीआर) में वृद्धि हुई है। अब यह 61 प्रतिशत हो गया है। यानी देश में हर 100 से 61 फीसदी लोग श्रम बाजार में हैं या तो उन्हें रोजगार मिला हुआ है या वे रोजगार की तलाश में हैं।
इन 61 फीसदी लोगों के बीच 3.2 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। श्रम बाजार में मौजूद बाकी सभी लोगों को रोजगार देने में अर्थव्यवस्था कामयाब रही है।
तो जाहिर है, ताजा आंकड़ों के जरिए यह धारणा बनाने का प्रयास भी हुआ है कि मोदी सरकार की नीतियां देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान ढूंढने में कामयाब हैं। किसी देश में सचमुच 3.2 प्रतिशत बेरोजगारी दर हो, तो उसे कुल मिला कर एक सफल अर्थव्यवस्था कहा जाएगा।
ऐसी हर कहानी के साथ यह संदेश देने की कोशिश भी की जाती है कि भारत की ‘सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था’ सबके लिए खुशहाली ला रही है। आज मीडिया का रुझान यह है कि सरकार आंकड़ों को जिस रूप में पेश करना चाहती है, अपनी खबरों में वे उनको उसी रूप में पेश करते हैं।
मोटी सुर्खियां बन जाती हैं। उनसे धारणा बन जाती है। कुछ गंभीर अंग्रेजी अखबारों में बाद में जरूर बारीकियों में जाने की कोशिश की जाती है, जिससे असल कहानी उभर कर सामने आती है। लेकिन तब तक आम जन मानस में सुर्खियों से बनी धारणा टिकाऊ हो चुकी होती है।
ताजा पीएलएफएस के संदर्भ में भी यही हुआ है। सर्वे के आधार बेरोजगारी दर के निम्न होने की कहानी प्रचारित की गई है। लेकिन इसी सर्वे के अंदर जाकर रोजगार की प्रकृति देखी जाए, तो कुछ और कहानी उभरती है।
बनी सुर्खियों और उनके अंदर की हकीकत पर आइए, एक नज़र डालते है।
लेकिन उसके पहले यह बात जरूर याद कर लेनी कि नई सरकार ऐसे काम को भी रोजगार की श्रेणी में शामिल करने की शुरुआत कर चुकी है, जिनमें किसी तरह का वेतन नहीं मिलता।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक:
- देश के श्रम बाजार में मौजूद 3.2 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं।
- लेकिन जिन लोगों ने सेंकडरी या उससे ऊपर की डिग्री हासिल कर रखी है, उनके बीच बेरोजगारी की दर 7.1 फीसदी है। यानी शिक्षित लोगों में बेरोजगारी दर आज भी खासी ऊंची है।
यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि जिन लोगों को काम मिला हुआ है, उनके रोजगार की प्रकृति क्या हैः
- कुल रोजगार प्राप्त लोगों में 58.4 फीसदी लोग स्वरोजगार की श्रेणी में हैं। 2017-18 में यह संख्या 52.2 प्रतिशत थी। यह ध्यान में रखना चाहिए कि आम तौर पर स्वरोजगार स्थायी नौकरी ढूंढ पाने में नाकामी के बाद व्यक्ति का सहारा बनता है। सामान्यतः स्वरोजगार किसी तरह गुजारा करने के प्रयास का दूसरा नाम है।
- कुल रोजगार प्राप्त लोगों में 21.7 प्रतिशत लोग घरेलू उद्यम में हेल्पर का काम करते हैं। जाहिर है, इन लोगों को कोई नियमित वेतन नहीं मिलता। 2022-23 के बाद यह संख्या बढ़ गई है। तब 18.3 प्रतिशत लोग इस रूप में काम कर रहे थे।
- उधर नियमित वेतन प्राप्त कर्मियों की संख्या सिर्फ 21.7 प्रतिशत है। 2017-18 में ऐसे कर्मियों की संख्या 22.8 फीसदी थी। यानी ऐसे रोजगार में गिरावट आई है। जबकि सामान्य परिभाषा में रोजगार का मतलब ऐसे ही काम को समझा जाता है, जिसमें नियमित आमदनी सुनिश्चित हो और न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाएं प्राप्त हों।
- 19.8 प्रतिशत लोग दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं।
सर्वे के आधार पर सुर्खी बनी है कि महिलाओं की श्रम बाजार में भागीदारी बढ़ कर अब 31.7 प्रतिशत हो गई है। लेकिन नियमित वेतन वाले रोजगार में इनमें से बहुत कम महिलाएं हैं। 67.4 प्रतिशत महिलाएं स्वरोजगार श्रेणी में हैं।
2017-18 में यह संख्या 51.9 फीसदी थी। 36.7 प्रतिशत महिलाएं तो हेल्पर के रूप में काम कर रही हैं। यह संख्या भी पांच साल में बढ़ गई है।
द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है- “सर्वे के मुताबिक, वेतनभोगी काम में महिलाओं की हिस्सेदारी गिरी है। अब ज्यादा महिलाएं स्वरोजगार में हैं। ये या तो unpaid हेल्पर के रूप में काम करती हैं, या उन्होंने अपना उद्यम शुरू किया है। यह विकल्पों के अभाव का सूचक है।”
पारिवारिक उद्यम में ऐसे कर्मियों की संख्या भी बढ़ी है, जिन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। ताजा सर्वे के मुताबिक कृषि क्षेत्र में सहयोग करने वाले (हेल्पर) लगभग 100 फीसदी कर्मी unpaid हैं। गैर-कृषि क्षेत्र में ऐसे कर्मियों की संख्या 17.9 प्रतिशत है।
भारत के रोजगार बाजार की संभवतः सबसे बड़ी समस्या बड़ी संख्या में श्रमिकों का अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने को मजबूर होना रही है। यह समस्या अधिक गंभीर होती जा रही है।
2023-24 इस क्षेत्र में 73.2 प्रतिशत श्रमिक काम कर रहे थे। 2017-18 में इसमें 68.2 फीसदी श्रमिक काम करते थे। जाहिर है, पांच साल में अधिक लोग इस क्षेत्र में काम करने को मजबूर हुए हैं, जहां वेतन कम मिलता है और जहां कोई सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती।
यह दुनिया भर का अनुभव है कि नियमित वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली सबसे ज्यादा नौकरियां मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में मिलती हैं। लेकिन भारत में यह सेक्टर गतिरुद्ध बना हुआ है।
दरअसल, 2021-22 की तुलना में स्थिति बदतर हो गई है। तब कुल श्रमिकों के बीच 11.6 प्रतिशत मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे थे। अब इनकी संख्या 11.4 फीसदी ही है।
तो कुल मिलाकर ताजा पीएलएफएस से तस्वीर यह उभरती है कि भारत में अच्छी, नियमित वेतन वाली नौकरियां बढ़ नहीं रही हैं। नतीजतन, अधिक लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं या स्वरोजगार कर रहे हैं, जहां घर के कई सदस्य unpaid हेल्पर के रूप में काम करते हैं।
यह अफसोसनाक है कि वर्तमान सरकार ने ऐसे काम को भी रोजगार की श्रेणी में गिनना शुरू किया। सिर्फ यह दिखाने के लिए कि श्रम बाजार में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है और बेरोजगारी दर गिर रही है, रोजगार की समझ को सिर के बल खड़ा कर दिया गया है।
मीडिया के बड़े हिस्से में आम तौर इस समझ पर सवाल नहीं उठाए जाते। बल्कि सरकार की मंशा के मुताबिक ऐसी सुर्खियां बनाई जाती हैं, जो गुमराह करने वाली होती हैं- बल्कि यह कहना चाहिए कि जिनका मकसद हकीकत पर परदा डालना होता है।
देश की अर्थव्यवस्था का उत्तरोत्तर वित्तीयकरण (financialization) होता जा रहा है। इसके बीच मैनुफैक्चरिंग का जाल फैलना लगातार कठिन होता जा रहा है। जो मैनुफैक्चरिंग इकाइयां लगती हैं, वो भी पूंजी-केंद्रित (capital intensive) होती हैं, इसलिए उनमें-खासकर अकुशल कर्मियों के लिए कम ही रोजगार पैदा होता है।
औपचारिक रोजगार की जो संभावना बनती है, वह भी आउटसोर्सिंग की वजह से जमीन पर नहीं उतर पाती। ओटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का बढ़ता उपयोग नई परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं।
इन चुनौतियों का कैसे मुकाबला किया जाए, इन पर ईमानदारी और गंभीरता से विचार करने के बजाय सरकार ने आंकड़े गढ़ने और आंकड़ों को संदर्भ से काट कर पेश करने का रास्ता अख्तियार किया हुआ है।
मीडिया का बड़ा हिस्सा इसमें सहायक बना हुआ है। नतीजतन, हकीकत के उलट सुर्खियां बनती हैं और उनसे विकट स्थिति के बीच खुशनुमा माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक स्तर पर ये प्रयास सफल भी हो जाता है।
(इस लेख में दिए गए सारे आंकड़े अंग्रेजी अखबारों में छपे विश्लेषणों के आधार पर हैं।)
(सत्येंद्र रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में रहते हैं)