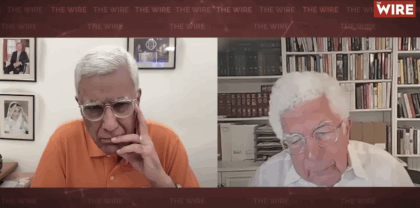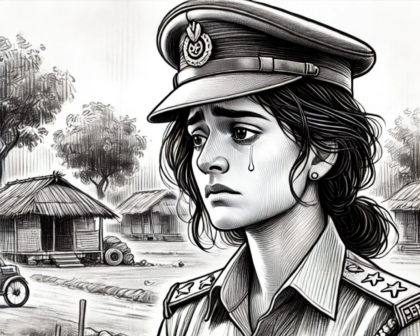वर्तमान वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य में विचारधाराओं का अनोखा और चिंताजनक बदलाव देखा जा रहा है। जहां एक ओर आर्थिक असमानता, शोषण और भेदभाव लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं इनसे लड़ने वाली वामपंथी विचारधारा का प्रभाव कम होता दिख रहा है।
दूसरी ओर, दक्षिणपंथी संगठनों को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है और तर्कवाद, वैज्ञानिक सोच तथा सेकुलर मूल्यों के कमजोर होने की प्रवृत्ति सामने आ रही है।
यह विरोधाभास और भी गहराता है जब भारत जैसे देश में उन वर्गों में धार्मिकता और पुरातनपंथ का प्रभाव बढ़ता दिखता है, जो सदियों से शोषण और उत्पीड़न का शिकार रहे हैं। इसके साथ ही, भारत का उच्च और निम्न मध्यवर्ग, जिसमें पेशेवर, सरकारी अधिकारी और शैक्षिक वर्ग शामिल हैं, दक्षिणपंथी विचारों की ओर झुकाव दिखा रहा है।
ज्योतिष, वास्तु, धार्मिक अनुष्ठान और प्रवचनकर्ताओं की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिससे यह सवाल उठता है: आखिर यह वैचारिक और सांस्कृतिक बदलाव क्यों हो रहा है? क्या यह सामाजिक असुरक्षा का परिणाम है या स्वाभाविक चक्रीय परिवर्तन?
वर्तमान वैश्विक और भारतीय समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनके पीछे की अंतर्निहित प्रक्रियाओं को समझने के लिए हमें गहरे दार्शनिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत है।
सवाल उठता है कि आखिर क्यों वामपंथी या समानता पर आधारित विचारधाराएं कमजोर होती दिख रही हैं, क्यों धार्मिकता और पुरातनपंथ का प्रभाव समाज के शोषित तबकों में बढ़ रहा है और क्यों दक्षिणपंथी विचारों को आज इतना जनसमर्थन मिल रहा है?
विचारधाराएं स्थायी या अपरिवर्तनीय नहीं होतीं, बल्कि वे समाज में मौजूद आर्थिक संरचनाओं और उत्पादन संबंधों पर आधारित होती हैं। विचारधारा (Ideology) किसी भी समाज में शासक वर्ग के हितों की अभिव्यक्ति होती है।
जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधनों का नियंत्रण होता है, वही वर्ग अपने हितों को समाज के लिए सामान्य और प्राकृतिक मान्यता दिलाने की कोशिश करता है।
विचारधाराएं समाज की आर्थिक आधारभूत संरचना (economic base) से उत्पन्न होती हैं, जो कि उत्पादन के साधन और उत्पादन संबंधों से संबंधित होती है। यह आर्थिक आधार एक अधिरचना (superstructure) को जन्म देता है, जिसमें राजनीतिक, कानूनी और सांस्कृतिक संस्थाएं शामिल होती हैं, जिनके माध्यम से शासक वर्ग की विचारधारा प्रचलित होती है।
जैसे-जैसे उत्पादन के साधनों और आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन होता है, वैसे-वैसे विचारधाराएं भी बदलती हैं। इस संदर्भ में, विचारधाराएं ऐतिहासिक रूप से परिवर्तनीय होती हैं और सामाजिक बदलाव के साथ विकसित होती हैं।
इस विचार को हम ऐतिहासिक भौतिकवाद (Historical Materialism) के सिद्धांत के रूप में समझ सकते हैं, जो बताता है कि इतिहास में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव मुख्य रूप से आर्थिक बदलावों द्वारा संचालित होते हैं, और इन बदलावों के साथ-साथ विचारधाराएं भी बदलती हैं।
वर्तमान वैश्विक आर्थिक प्रणाली पूंजी के नियंत्रण और उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण पर आधारित है। इसके परिणामस्वरूप श्रम और उत्पादन के बीच गहरा विभाजन हुआ है। जहां एक ओर धनी वर्ग और बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुनाफे में बढ़ोतरी कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर समाज का बड़ा हिस्सा गरीबी और शोषण का शिकार हो रहा है।
ऐसे में, जिन विचारधाराओं का उदय आर्थिक समानता के लिए और शोषण के खिलाफ संघर्ष के रूप में हुआ था, वे कमजोर पड़ने लगीं क्योंकि इन संगठनों में विचारधारात्मक विभाजन हुए और कई बार नेतृत्व आत्मकेंद्रित हो गया।
इसके अतिरिक्त पूंजीवादी व्यवस्था ने सरकारों और संस्थानों पर इतना प्रभुत्व जमा लिया कि जिन विचारों को बदलने की जरूरत थी, वे उन्हीं के द्वारा नष्ट कर दिए गए।
मीडिया और सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों ने भी विचारधारात्मक संघर्ष को कमजोर करने में भूमिका निभाई। उपभोक्तावाद और सामाजिक प्रतिष्ठा की चाह ने संघर्षशील विचारधाराओं को हाशिए पर धकेल दिया।
लोग अब अपनी आर्थिक और सामाजिक परेशानियों के समाधान के लिए ठोस वैचारिक आंदोलनों के बजाय व्यक्तिगत समस्याओं में उलझते जा रहे हैं।
धार्मिकता और पुरातनपंथ का प्रभाव विशेष रूप से उन सामाजिक तबकों में बढ़ा है जो इस व्यवस्था के शोषण का शिकार रहे हैं। यह परिघटना दर्शाती है कि लोग धार्मिकता और परंपराओं में सांत्वना की तलाश करते हैं, खासकर जब उन्हें अपने जीवन में अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है।
धर्म और पुरातनपंथ ने हमेशा से समाज के गरीब और शोषित तबकों के लिए सांस्कृतिक आश्रय प्रदान किया है। जब समाज की संरचनाएं उन्हें न्याय नहीं दिला पातीं या जब उनकी संघर्षशील विचारधारा का विघटन हो जाता है, तो वे धार्मिक और पुरातनपंथी प्रवचनों में अपने सवालों का उत्तर ढूंढते हैं।
धार्मिकता आसान जवाब देती है-सर्वशक्तिमान या नियति का हाथ मानकर अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करना। पुरातनपंथी कथाएं और धार्मिकता सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का माध्यम बनती हैं और यह जुड़ाव उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक असुरक्षा के समय में भावनात्मक सहारा प्रदान करता है।
धार्मिक और पुरातनपंथी तत्वों का राजनीतिक दुरुपयोग भी महत्वपूर्ण कारण है कि यह विचारधारा मजबूत हो रही है। धर्म का उपयोग दक्षिणपंथी ताकतों द्वारा सामूहिक भावनाओं को नियंत्रित करने और उनके वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
आज दक्षिणपंथी संगठनों को वैश्विक स्तर पर जनसमर्थन मिल रहा है। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि वैज्ञानिक तर्क, तार्किकता और प्रबोधन के मूल्यों के विकास के बजाय यह ध्रुवीकरण प्रतिगामी कदम प्रतीत होता है।
दक्षिणपंथी विचारधारा का मुख्य आधार सांस्कृतिक पहचान और परंपरा का संरक्षण है। यह विचारधारा लोगों को यह समझाने का प्रयास करती है कि उनके सामाजिक और आर्थिक संकटों का समाधान बाहरी ताकतों (जैसे अन्य धर्म, समुदाय या प्रवासियों) से लड़ने में है।
यह सरल और स्पष्ट समाधान की अपील करता है, जबकि तार्किक और प्रबोधनवादी दृष्टिकोण अधिक जटिल होते हैं और लंबी प्रक्रिया की मांग करते हैं।
जब समाज में आर्थिक संकट बढ़ता है, तब लोग अपनी सामाजिक पहचान और सांस्कृतिक जड़ों से चिपकने लगते हैं। ऐसे में दक्षिणपंथी विचारधाराएं सुरक्षा का आश्वासन देती हैं और एक सामूहिक ‘दुश्मन’ की पहचान कराकर लोगों को एकजुट करती हैं।
दक्षिणपंथी विचारधारा अक्सर राष्ट्रवाद का सहारा लेकर सामूहिक पहचान को मजबूत करती है। यह विचारधारा विभिन्न सामाजिक और जातीय वर्गों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करके अपनी ताकत बढ़ाती है, जिससे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकता है।
यह समझना जरूरी है कि भारत का उच्च मध्यवर्ग और निम्न मध्यवर्ग, जो शिक्षक, डॉक्टर, वकील और नौकरशाह हैं, दक्षिणपंथी विचारधाराओं की ओर आकर्षित क्यों हो रहा है।
इस पर गहनता से विचार करते समय तत्कालीन जर्मनी के उदाहरण को ध्यान में रखना उपयोगी होगा, जहां उच्च शिक्षित वर्ग हिटलर के प्रति आकर्षित हो गया था।
समाज की संरचना मुख्य रूप से आर्थिक शक्तियों और वर्ग विभाजन पर आधारित होती है। राज्य, शासक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए एक टूल होता है और जब कोई समाज आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता का सामना करता है, तो शासक वर्ग अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए वैचारिक और सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करता है।
इस संदर्भ में, मध्यवर्ग की भूमिका विशेष होती है, क्योंकि यह वर्ग अक्सर अपने आर्थिक हितों को संरक्षित करने के लिए शासक वर्ग की विचारधारा का समर्थक बन जाता है।
भारत का उच्च और निम्न मध्यवर्ग, विशेष रूप से वे लोग जो शिक्षित और अपेक्षाकृत सुरक्षित नौकरियों में हैं, आज की अस्थिर आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में अपनी स्थिति को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है।
इस असुरक्षा का स्रोत वैश्विक पूंजीवाद के परिणामस्वरूप बढ़ती आर्थिक विषमता और नौकरी बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा है।
जब इस वर्ग को लगता है कि उनकी स्थिति खतरे में है, वे दक्षिणपंथी विचारधाराओं की ओर झुकते हैं, जो उन्हें सरल समाधान और स्थिरता का वादा करती हैं।
दक्षिणपंथी विचारधारा सांस्कृतिक पहचान, परंपरा और धर्म के आधार पर सुरक्षित भविष्य का सपना दिखाती है, जिसमें उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति संरक्षित रहेगी।
तत्कालीन जर्मनी में, हिटलर का उदय भी इसी प्रकार के सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा के माहौल में हुआ था। जर्मनी की पराजय और महान आर्थिक मंदी के बाद, वहां का उच्च शिक्षित वर्ग-जो प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर और नौकरशाहों से मिलकर बना था-हिटलर की विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ।
इस वर्ग ने हिटलर की उन बातों में अपनी उम्मीद देखी, जो जर्मनी की पुरानी महानता, सांस्कृतिक शुद्धता और स्थिरता को पुनःस्थापित करने का वादा करती थीं। यह वर्ग अपने सामाजिक और आर्थिक पतन के डर से सांस्कृतिक श्रेष्ठता और राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित हुआ, जिसे हिटलर ने अपने फासीवादी एजेंडे के माध्यम से बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।
यह समझा जा सकता है कि जर्मनी के उच्च शिक्षित वर्ग ने हिटलर के फासीवाद का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अपनी वर्गीय स्थिति को बचाने के लिए शासक वर्ग के विचारों को अपनाया। पूंजीवादी संकट के समय, शासक वर्ग ने राष्ट्रवाद और नस्लीय श्रेष्ठता का उपयोग करके अपने नियंत्रण को बनाए रखा और जनता को विभाजित किया।
जर्मनी में, शासक वर्ग ने मध्यवर्ग की आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का फायदा उठाया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान बाहरी दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में है।
भारत में भी यह प्रक्रिया इसी प्रकार से कार्य कर रही है। जब मध्यवर्ग के लोग आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव का सामना करते हैं, तो वे दक्षिणपंथी विचारधाराओं की ओर आकर्षित होते हैं, जो उन्हें सांस्कृतिक गौरव, परंपराओं की पुनर्स्थापना और धार्मिक श्रेष्ठता का वादा करती हैं।
दक्षिणपंथी ताकतें इस वर्ग को यह विश्वास दिलाती हैं कि उनकी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का कारण बाहरी तत्व हैं, चाहे वह जातीय, धार्मिक या सांस्कृतिक स्तर पर हो।
इस प्रकार, वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक प्रतीकों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि यह उन्हें सुरक्षा का आभास देता है। इस वर्ग के लोग अपनी श्रेणी में बने रहने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में वे उस विचारधारा का समर्थन करने लगते हैं जो शासक वर्ग की स्थिति को मजबूत करती है।
इस तरह यह देखा जा सकता है कि मध्यवर्ग अपनी सामाजिक असुरक्षा के कारण अक्सर दक्षिणपंथी विचारधाराओं की ओर आकर्षित होता है।
यह प्रक्रिया न केवल समाज के आर्थिक ढांचे से जुड़ी है, बल्कि शासक वर्ग द्वारा संचालित वैचारिक उपकरणों के माध्यम से भी चलती है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करके लोगों की असुरक्षाओं का फायदा उठाते हैं।
यह असमानता और वर्ग संघर्ष का परिणाम है, जहां शोषित वर्ग अपनी वास्तविक स्थिति को पहचानने में विफल रहता है और शासक वर्ग की वैचारिक और सांस्कृतिक हेजेमनी को स्वीकार कर लेता है। यह पूरी परिघटना केवल चक्रीय परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह गहरा सामाजिक संकट है।
समाज में बढ़ती असुरक्षा और आर्थिक असमानताएं दक्षिणपंथी विचारधाराओं के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर रही हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए नई दृष्टि और संगठित वैचारिक संघर्ष की आवश्यकता है।
असली सवाल यह है कि क्या हम इस संकट को पहचान कर इसे बदलने के लिए तैयार हैं या इसे चक्रीय प्रक्रिया मानकर इसके समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे?
(मनोज अभिज्ञान स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)