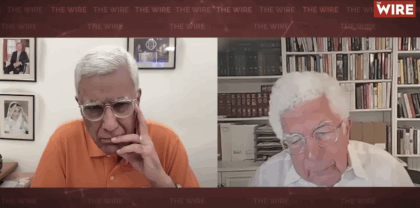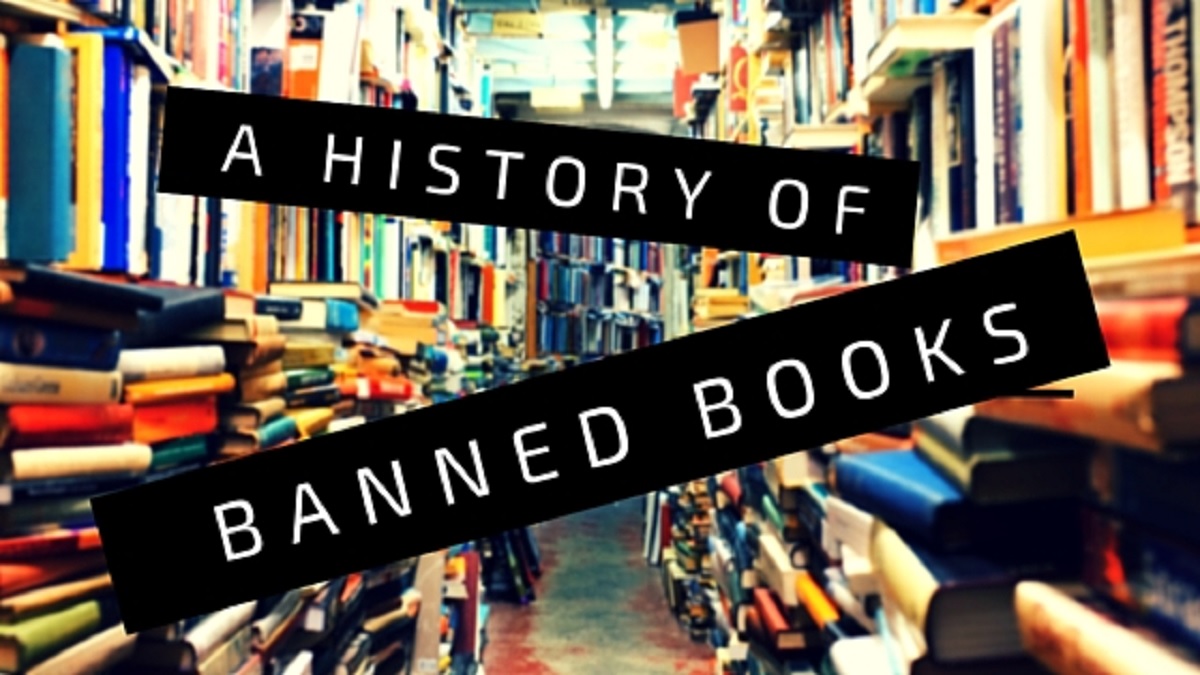हमारे संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, जिसे उस अनुच्छेद के ठीक बाद स्पष्ट किया गया है जो स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इतिहास में तथ्यों की वैधता को उसकी वस्तुनिष्ठता तक पहुंचने के लिए बहस के कई स्तरों से गुजरना पड़ता है।
लेकिन तथ्य, उपयुक्त जांच प्रक्रियाओं और सत्य को ठोस बनाने के अन्य आधुनिक उपकरणों के माध्यम से वैधता प्राप्त करते हैं, जो मानव सभ्यता के संघर्ष के साथ विकसित हुए हैं।
पुस्तक प्रतिबंध का इतिहास वर्ग समाज के विकास से जुड़ा है, न केवल विश्व स्तर पर बल्कि विशेष रूप से भारत में भी। प्राचीन काल में, दास मालिकों का इतिहास उन साहित्य को जलाने का रहा है, जो यथास्थिति या धर्म की रूढ़िवादी प्रकृति को चुनौती देते थे।
नास्तिकता को “ईश्वर विरोधी” के रूप में लेबल किया गया और इसे बड़ी क्रूरता के साथ दंडित किया गया। इसी तरह, सामंती युग के दौरान, वे साहित्य जो राजा या राजवंश की प्रभुता को चुनौती देते थे, उन्हें राज्य द्वारा सेंसर किया गया या अक्सर सार्वजनिक समारोहों में पुस्तकों को जलाने का आयोजन किया गया।
आधुनिक ‘लोकतांत्रिक’ राज्य भी पुस्तकों और साहित्य की ओर इसी प्रवृत्ति को अपनाता है, लेकिन अब यह आरोपों के माध्यम से किया जाता है, जैसे कि ईशनिंदा फैलाना, राज्य विरोधी होना, या समाज की आर्थिक स्थिति के खिलाफ होना (यह आरोप नवउदारवाद के साथ नया उभरा है)।
इतिहास में साहित्य पर दो प्रकार के प्रतिबंध रहे हैं, राज्य द्वारा और समाज द्वारा। लेकिन साहित्य और राज्य का आगमन समानांतर रहा है, और पुस्तकों पर प्रतिबंध का इतिहास भी राज्य जितना ही पुराना है। बहुत कम लोग जानते हैं कि लेनिन कानून के छात्र थे, जिन्होंने कानून की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए और रूस में टॉप किया।
लेकिन उन्होंने कानून को राज्य की प्रभुत्व के दूसरी ओर से देखा। लेनिन के अनुसार, राज्य वर्गों की प्रभुत्व है, और राज्य के उदय के साथ ही संघर्ष शोषित और शासक वर्गों के बीच संघर्ष बन गया।
प्राचीन भारत में चार्वाक के साहित्य को ब्राह्मणवादी शासक वर्ग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। चार्वाक को सार्वजनिक रूप से उनके कार्यों के साथ जला दिया गया। आज जो चार्वाक के कार्य पढ़े जाते हैं, वे उनके अनुयायियों और कुछ टीकाकारों द्वारा संरक्षित किए गए हैं।
चार्वाक की विचारधारा ने ब्राह्मणवादी दर्शन के छह रूढ़िवादी स्कूलों को चुनौती दी और किसी भी ईश्वर या पुनर्जन्म के विचार को अस्वीकार कर दिया। चार्वाक का भौतिकवाद केवल प्रत्यक्ष अनुभव को स्वीकार करता था।
यह विचार बहुत ही उत्तेजक है कि कोई व्यक्ति दो हजार साल पहले भौतिकवाद की बात कर रहा था और मानव जीवन में किसी भी बाहरी पारलौकिक हस्तक्षेप को अस्वीकार कर रहा था।
कल्पना कीजिए कि अगर कानून भौतिकवाद (चार्वाक के सिद्धांत) के आधार पर बनाए गए होते, तो समाज का विश्वास तंत्र एक अलग वास्तविकता में काम करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चार्वाक को उनके ब्राह्मण प्रतिद्वंद्वियों ने उनके साहित्य सहित जला दिया।
पुस्तकों पर प्रतिबंध और दार्शनिकों की हत्या की प्रवृत्ति व्यापक थी। चीन में, कानूनवादी विचारधारा, जो सामंती शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, ने कन्फ्यूशियस के साहित्य को जलाया, क्योंकि कन्फ्यूशियस दास शासक अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे।
फ्रांस में, वोल्टेयर, दिदेरो, रूसो और मोंटेस्क्यू के साहित्य का बड़े पैमाने पर सामंती शासकों द्वारा प्रतिबंधित किया गया। फ्रांस की क्रांति के समय, इन पुस्तकों को भूमिगत रूप से प्रसारित किया गया, क्योंकि फ्रांसीसी शासक अभिजात वर्ग इसे उन साहित्यिक रचनाओं के रूप में मानते थे, जो समाज के रूढ़िवादी मूल्यों पर आघात करती थीं।
यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो पुस्तकें दो सौ साल पहले राज्यों द्वारा प्रतिबंधित की गई थीं, वे आज की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से हैं। फ्रांसीसी राज्य ने इन ‘खराब किताबों’ को जलाने के समारोहों का आयोजन किया। राजद्रोह और ईशनिंदा राज्य द्वारा क्रांतिकारी साहित्य को प्रतिबंधित करने के पुराने हथकंडे थे।
औपनिवेशिक भारत में प्रतिबंधित साहित्य
1876 का ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कंट्रोल एक्ट, 1897 का देशद्रोह विधेयक, 1907 का देशद्रोही सभाओं का अधिनियम, 1908 का अखबारों (अपराधों के लिए उकसावा) अधिनियम और भारतीय दंड कानून संशोधन अधिनियम, 1910 का भारतीय प्रेस अधिनियम, 1915 का डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, 1918 का कुख्यात रॉलेट एक्ट और 1931 का भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियां अधिनियम) एक के बाद एक लागू किए गए।
इन कानूनों के तहत स्वदेशी, देशभक्ति से संबंधित गीत, कविताएं, लेख और बड़ी संख्या में पुस्तकें प्रतिबंधित कर दी गईं। लंदन की इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी में प्रतिबंधित पुस्तकों की पूरी सूची उपलब्ध है।
1962 में भारत सरकार ने उन पुस्तकों को जलवा दिया जो चीन के सीमा विवाद और दावों का समर्थन करती थीं। नक्सलबाड़ी आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में पुस्तकें प्रतिबंधित की गईं। सीपीआई (एमएल) और अन्य कम्युनिस्ट संगठनों से जुड़े पत्र-पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाकर भारतीय राज्य ने जनता को क्रांतिकारी साहित्य से अनभिज्ञ बनाए रखने का प्रयास किया।
सलिल त्रिपाठी ने 1947 के बाद भारत में पुस्तकों पर प्रतिबंध के विषय में एक विस्तृत कार्य प्रकाशित किया, जिसमें उन विषयों का विस्तृत विवरण है जो प्रतिबंध लगाने के आधार बने।
उदाहरण के लिए, गुजराती में अनूदित पुस्तक ‘स्त्री’ (द वुमन ऑफ रोम) की कहानी एक महिला के इर्द-गिर्द थी जो कलाकारों के लिए नग्न पोज देती है और अंततः एक यौनकर्मी बन जाती है। उस समय के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने इसे अश्लील बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया।
स्थानीय अदालत ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि केवल नग्न मॉडल का चित्रण या बिना कपड़ों की मूर्ति को प्रदर्शित करना किसी कृति को अश्लील नहीं बनाता। न्यायाधीश डेव ने अपने फैसले में कहा कि हमें समय के साथ चलना चाहिए और उन मूल्यों से चिपके नहीं रहना चाहिए जो वर्तमान समय के अनुरूप नहीं हैं।
इसके बाद, बड़ौदा की स्थानीय अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने लेडी चैटरलीज लवर पर प्रतिबंध को पलटने की अपील खारिज कर दी, जो पहले यूके में प्रतिबंधित थी। 1960 में यूके सरकार ने इस पुस्तक से प्रतिबंध हटा लिया और स्वीकार किया कि इसके विषयों पर समाज में चर्चा की जा सकती है।
लेकिन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने अपीलकर्ता के दावे को खारिज कर दिया और हिकलिन टेस्ट के आधार पर कहा कि क्या कोई विशेष पाठ ‘अनैतिक प्रभावों से किसी गंदी मानसिकता को भ्रष्ट और खराब’ करने की संभावना रखता है।
कोर्ट ने तर्क दिया कि चैटरलीज जैसी पुस्तकें भारत की क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों को ऐसी रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित करेंगी और “हमारे पूरे साहित्य को विकृत कर देंगी क्योंकि अश्लीलता लाभ देती है और सच्ची कला को लोकप्रिय समर्थन बहुत कम मिलता है।”
एन. राधाकृष्णन बनाम भारत संघ के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रचनात्मक अभिव्यक्ति को दबाया या चुप नहीं कराया जा सकता और बौद्धिक स्वतंत्रता को नष्ट नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पुस्तकों पर प्रतिबंध की संस्कृति विचारों के स्वतंत्र प्रवाह को प्रभावित करती है और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और भाषण का अपमान है। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने कहा कि रचनात्मक कार्य को परिपक्व दृष्टिकोण, वस्तुनिष्ठ सहनशीलता और स्वीकृति की भावना के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
यह स्पष्ट करते हुए कि अनुच्छेद 19(2) प्रासंगिक है, कोर्ट ने कहा कि किसी पाठ को खंडित तरीके से पढ़ने के बजाय उसे संपूर्ण रूप में पढ़ा जाना चाहिए।
पसंदीदा पुस्तकों को पढ़ने और किसी विषय पर अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार मौलिक अधिकारों के दायरे में आता है। आधुनिक गरिमा और स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा सीधे अभिव्यक्ति और उस विचार की स्वतंत्रता से जुड़ी है जो कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय के बारे में सोचता है।
लेकिन यदि ज्ञान के स्रोत को उसी राज्य द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाए जिसे जनता ने चुना है, तो क्या होगा? यदि राज्य का पूरा प्रचार बिना किसी अन्य पक्ष की सच्चाई को जाने ही गूंजता रहे, तो क्या होगा? प्रतिबंध के माध्यम से, राज्य उस चीज़ को रोकने का प्रयास करता है जो ‘वास्तविक चरित्र को उजागर कर सकती है।’
स्वतंत्रता का आनंद लेने से वंचित होने की भावना ने अधिकारों के जन्म को जन्म दिया। जब हर चीज़ को स्वाभाविक रूप से आनंदित किया जाता है, तो मानव में वंचित होने की कोई भावना नहीं होती। यह भावना तब उत्पन्न होती है, जब कुछ लोगों को उन अधिकारों का आनंद लेने से वंचित कर दिया जाता है, जबकि अन्य लोग स्वतंत्रता और अधिकारों का एकाधिकार बनाए रखते हैं।
साहित्यिक प्रतिबंधों के ऐतिहासिक विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जिस भी राज्य ने अपने शासन में साहित्य पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, वही साहित्य मानव सभ्यता के अगले चरण का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया।
आज का कमजोर हो रहा आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य और उभरता हुआ फासीवादी राज्य एक नई स्थिति पैदा कर रहा है, जहां गैर-राज्य अभिनेता (आधुनिक राज्य की शब्दावली में) मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और बौद्धिकों के खिलाफ ‘कंगारू न्याय’ कर रहे हैं।
गौरी लंकेश, पानसरे, दाभोलकर-हमारे पास कई उदाहरण हैं, जहां कट्टर भीड़ को गैर-राज्य अभिनेता के रूप में बौद्धिकों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया।
हम मानव विकास की सबसे उन्नत सभ्यता हैं, इसलिए हमें इस तरह से कार्य करना चाहिए और अपने मस्तिष्क को वास्तविकता की धार से और अधिक तेज़ करना चाहिए।
(निशांत आनंद कानून के छात्र हैं)