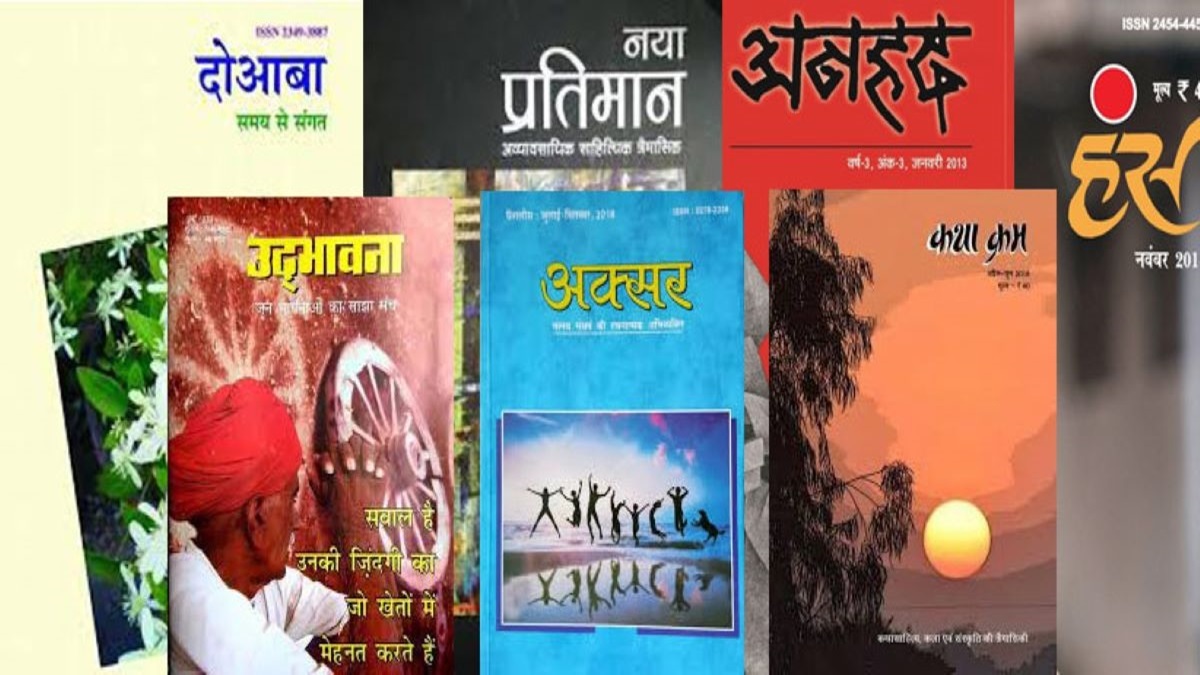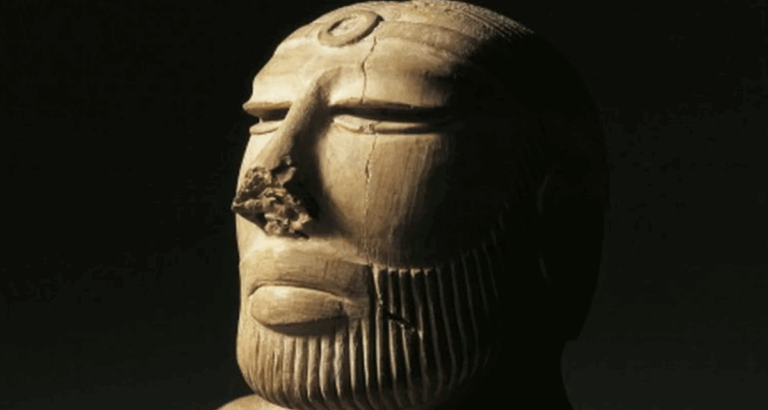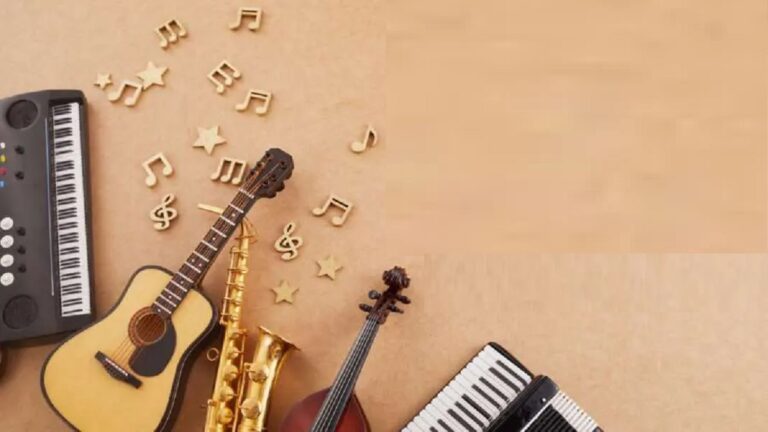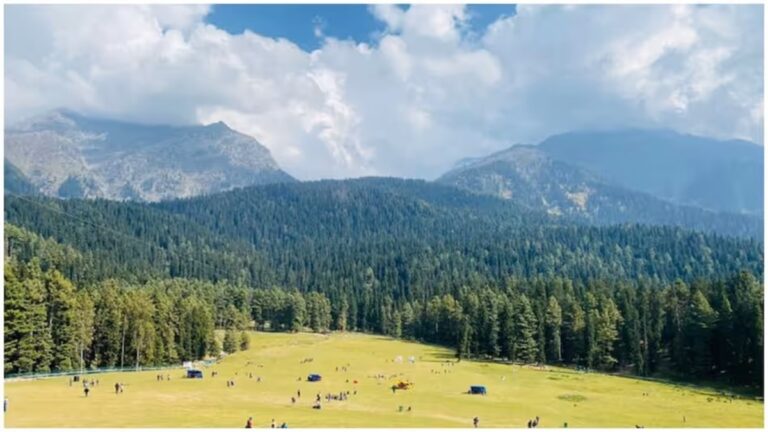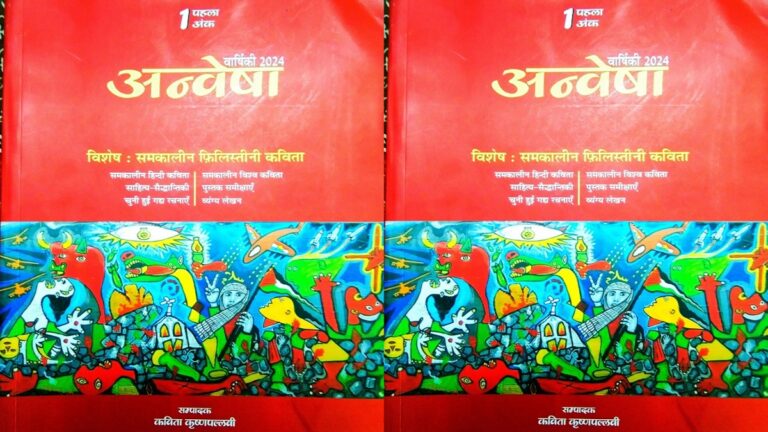जैसा कि विदित है, हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में भारतेंदु युग 1873 से 1900 तक माना जाता है। इस युग के एक छोर पर भारतेंदु की हरिश्चंद्र मैगजीन थी और दूसरी ओर नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा अनुमोदित सरस्वती। उन्नीसवीं शताब्दी के इन 27 वर्षों का आदर्श भारतेंदु की पत्रकारिता थी। कविवचनसुधा (1867), हरिश्चंद्र मैगजीन (1874), श्री हरिश्चंद्र चंद्रिका (1874), और बालाबोधिनी (स्त्रीजनों की पत्रिका, 1874) के रूप में भारतेंदु ने इस दिशा में पथप्रदर्शन किया। उनकी टीका-टिप्पणियों से अधिकारी तक घबराते थे।
कविवचनसुधा के “पंच” पर रुष्ट होकर काशी के मजिस्ट्रेट ने भारतेंदु के पत्रों को शिक्षा विभाग के लिए लेना भी बंद करा दिया था। इसमें संदेह नहीं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी भारतेंदु पूर्णतः निर्भीक थे और उन्होंने नए-नए पत्रों को प्रोत्साहन दिया। हिंदी प्रदीप, भारतजीवन आदि अनेक पत्रों का नामकरण भी उन्होंने ही किया था। उनके युग के सभी पत्रकार उन्हें अग्रणी मानते थे।
भारतेंदु के बाद इस क्षेत्र में जो पत्रकार आए, उनमें प्रमुख थे: पंडित रुद्रदत्त शर्मा (भारतमित्र, 1877), बालकृष्ण भट्ट (हिंदी प्रदीप, 1877), दुर्गाप्रसाद मिश्र (उचित वक्ता, 1878), पंडित सदानंद मिश्र (सारसुधानिधि, 1878), पंडित वंशीधर (सज्जन-कीर्ति-सुधाकर, 1878), बद्रीनारायण चौधरी “प्रेमधन” (आनंद कादंबिनी, 1881), देवकीनंदन त्रिपाठी (प्रयाग समाचार, 1882), राधाचरण गोस्वामी (भारतेंदु, 1882), पंडित गौरीदत्त (देवनागरी प्रचारक, 1882), राज रामपाल सिंह (हिंदुस्तान, 1883), प्रतापनारायण मिश्र (ब्राह्मण, 1883), अंबिकादत्त व्यास (पीयूषप्रवाह, 1884), बाबू रामकृष्ण वर्मा (भारतजीवन, 1884), पं. रामगुलाम अवस्थी (शुभचिंतक, 1888), योगेशचंद्र वसु (हिंदी बंगवासी, 1890), पं. कुंदनलाल (कवि व चित्रकार, 1891), और बाबू देवकीनंदन खत्री एवं बाबू जगन्नाथदास (साहित्य सुधानिधि, 1894)। 1895 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इस पत्रिका से गंभीर साहित्य समीक्षा का प्रारंभ हुआ और इसलिए हम इसे एक निश्चित प्रकाशस्तंभ मान सकते हैं। 1900 में सरस्वती और सुदर्शन के अवतरण के साथ हिंदी पत्रकारिता के इस दूसरे युग का समापन हो गया।
इन 27 वर्षों में हमारी पत्रकारिता अनेक दिशाओं में विकसित हुई। प्रारंभिक पत्र शिक्षा प्रसार और धर्म प्रचार तक सीमित थे। भारतेंदु ने सामाजिक, राजनीतिक, और साहित्यिक दिशाएँ भी विकसित कीं। उन्होंने ही बालाबोधिनी (1874) नाम से पहला स्त्री-मासिक पत्र चलाया। कुछ वर्ष बाद महिलाओं को स्वयं इस क्षेत्र में उतरते देखा गया-भारतभगिनी (हरदेवी, 1888), सुगृहिणी (हेमंतकुमारी, 1889)।
आज वही पत्र हमारी इतिहास-चेतना में विशेष महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने भाषा, शैली, साहित्य, अथवा राजनीति के क्षेत्र में कोई अप्रतिम कार्य किया हो। साहित्यिक दृष्टि से हिंदी प्रदीप (1877), ब्राह्मण (1883), क्षत्रिय पत्रिका (1880), आनंद कादंबिनी (1881), भारतेंदु (1882), देवनागरी प्रचारक (1882), वैष्णव पत्रिका (पश्चात् पीयूषप्रवाह, 1883), कवि व चित्रकार (1891), नागरी नीरद (1883), साहित्य सुधानिधि (1894), और राजनीतिक दृष्टि से भारतमित्र (1877), उचित वक्ता (1878), सारसुधानिधि (1878), भारतोदय (दैनिक, 1883), भारतजीवन (1884), भारतोदय (दैनिक, 1885), शुभचिंतक (1887), और हिंदी बंगवासी (1890) विशेष महत्वपूर्ण हैं।
इन पत्रों में हमारे उन्नीसवीं शताब्दी के साहित्य रसिकों, हिंदी के कर्मठ उपासकों, शैलीकारों, और चिंतकों की सर्वश्रेष्ठ निधि सुरक्षित है। यह क्षोभ का विषय है कि हम इस महत्वपूर्ण सामग्री को पत्रों की फाइलों से उद्धार नहीं कर सके। बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, सदानंद मिश्र, रुद्रदत्त शर्मा, अंबिकादत्त व्यास, और बालमुकुंद गुप्त जैसे सजीव लेखकों की कलम से निकले हुए न जाने कितने निबंध, टिप्पणियाँ, लेख, पंच, हास-परिहास, और स्केच आज हमें अलभ्य हो रहे हैं। आज भी हमारे पत्रकार उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने समय में तो वे अग्रणी थे ही।
बीसवीं शताब्दी की पत्रकारिता हमारे लिए अपेक्षाकृत निकट है और उसमें बहुत कुछ पिछले युग की पत्रकारिता की विविधता और बहुरूपता मिलती है। उन्नीसवीं शताब्दी के पत्रकारों को भाषा-शैली के क्षेत्र में अव्यवस्था का सामना करना पड़ा था। उन्हें एक ओर अंग्रेजी और दूसरी ओर उर्दू के पत्रों के सामने अपनी वस्तु प्रस्तुत करनी थी। उस समय हिंदी में रुचि रखने वाली जनता बहुत छोटी थी। धीरे-धीरे परिस्थितियाँ बदलीं और हम हिंदी पत्रों को साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करते पाते हैं।
इस शताब्दी में धर्म और समाज सुधार के आंदोलन कुछ पीछे पड़ गए और जातीय चेतना ने धीरे-धीरे राष्ट्रीय चेतना का रूप ग्रहण कर लिया। फलस्वरूप, अधिकांश पत्र साहित्य और राजनीति को लेकर चले। साहित्यिक पत्रों के क्षेत्र में पहले दो दशकों में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती (1903-1918) का नेतृत्व रहा। वस्तुतः इन बीस वर्षों में हिंदी के मासिक पत्र एक महान साहित्यिक शक्ति के रूप में सामने आए।
शृंखलित उपन्यास और कहानी के रूप में कई पत्र प्रकाशित हुए-जैसे उपन्यास (1901), हिंदी नाविल (1901), उपन्यास लहरी (1902), उपन्यास सागर (1903), उपन्यास कुसुमांजलि (1904), उपन्यास बहार (1907), उपन्यास प्रचार (1912)। केवल कविता अथवा समस्यापूर्ति को लेकर अनेक पत्र उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में निकलने लगे थे और वे चलते रहे। समालोचना के क्षेत्र में समालोचक (1902) और ऐतिहासिक शोध से संबंधित इतिहास (1905) का प्रकाशन भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं।
परंतु सरस्वती ने “मिसलेनी” के रूप में जो आदर्श रखा, वह अधिक लोकप्रिय रहा। इस श्रेणी के पत्रों में कुछ ही पत्रों का नाम लिया जा सकता है, जैसे भारतेंदु (1905), नागरी हितैषिणी पत्रिका (बाँकीपुर, 1905), नागरी प्रचारक (1906), मिथिला मिहिर (1910), और इंदु (1909)। सरस्वती और इंदु दोनों हमारी साहित्य-चेतना के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हैं और एक तरह से हम उन्हें उस युग की साहित्यिक पत्रकारिता का शीर्ष मणि कह सकते हैं। सरस्वती के माध्यम से आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी और इंदु के माध्यम से पंडित रूपनारायण पांडेय ने जिस संपादकीय सतर्कता, अध्यवसाय, और ईमानदारी का आदर्श हमारे सामने रखा, वह हमारी पत्रकारिता को एक नई दिशा देने में समर्थ हुआ।
आधुनिक युग (1921) के बाद हिंदी पत्रकारिता का नया काल आरंभ होता है। इस युग में हम राष्ट्रीय और साहित्यिक चेतना को साथ-साथ पल्लवित पाते हैं। इसी समय हिंदी का प्रवेश विश्वविद्यालयों में हुआ और कुछ ऐसे कृती संपादक सामने आए, जो अंग्रेजी की पत्रकारिता से पूर्णतः परिचित थे और हिंदी पत्रों को अंग्रेजी, मराठी, और बंगला के पत्रों के समकक्ष लाना चाहते थे। फलस्वरूप, साहित्यिक पत्रकारिता में एक नए युग का आरंभ हुआ।
राष्ट्रीय आंदोलनों ने हिंदी की राष्ट्रभाषा की योग्यता को पहली बार घोषित किया। जैसे-जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों का बल बढ़ा, हिंदी के पत्रकार और पत्र अधिक महत्व पाने लगे। 1921 के बाद गांधीजी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन मध्यवर्ग तक सीमित न रहकर ग्रामीणों और श्रमिकों तक पहुँचा। इसके प्रसार में हिंदी पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सच तो यह है कि हिंदी पत्रकार राष्ट्रीय आंदोलनों की अग्रिम पंक्ति में थे और उन्होंने विदेशी सत्ता से डटकर मोर्चा लिया। विदेशी सरकार ने अनेक बार नए-नए कानून बनाकर समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया, परंतु जेल, जुर्माना, और अनेकानेक मानसिक व आर्थिक कठिनाइयाँ झेलते हुए भी हमारे पत्रकारों ने स्वतंत्र विचार की दीपशिखा जलाए रखी।
1921 के बाद साहित्य क्षेत्र में जो पत्र आए, उनमें प्रमुख हैं: स्वार्थ (1922), माधुरी (1923), मर्यादा, चाँद (1923), मनोरमा (1924), समालोचक (1924), चित्रपट (1925), कल्याण (1926), सुधा (1927), विशाल भारत (1928), त्यागभूमि (1928), हंस (1930), गंगा (1930), विश्वमित्र (1933), रूपाभ (1938), साहित्य संदेश (1938), कमला (1939), मधुकर (1940), जीवन साहित्य (1940), विश्वभारती (1942), संगम (1942), कुमार (1944), नया साहित्य (1945), पारिजात (1945), हिमालय (1946) आदि।
वास्तव में, हमारे मासिक पत्रों की साहित्यिक प्रौढ़ता और विविधता में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता। हिंदी की अनेक प्रथम श्रेणी की रचनाएँ मासिक पत्रों द्वारा ही पहले प्रकाश में आईं और अनेक श्रेष्ठ कवि व साहित्यकार पत्रकारिता से भी संबंधित रहे। हमारे मासिक पत्र जीवन और साहित्य के सभी अंगों की पूर्ति करते रहे हैं और अब विशेषज्ञता की ओर भी ध्यान जाने लगा है। साहित्य की प्रवृत्तियों की जैसी विकासमान झलक पत्रों में मिलती है, वैसी पुस्तकों में नहीं मिलती। वहाँ हमें साहित्य का सक्रिय, सप्राण, गतिशील रूप प्राप्त होता है।
राजनीतिक क्षेत्र में इस युग में जिन पत्र-पत्रिकाओं की धूम रही, वे हैं: कर्मवीर (1924), सैनिक (1924), स्वदेश (1921), श्रीकृष्ण संदेश (1925), हिंदू पंच (1926), स्वतंत्र भारत (1928), जागरण (1929), हिंदी मिलाप (1929), सचित्र दरबार (1930), स्वराज्य (1931), नवयुग (1932), हरिजन सेवक (1932), विश्वबंधु (1933), नवशक्ति (1934), योगी (1934), हिंदू (1936), देशदूत (1938), राष्ट्रीयता (1938), संघर्ष (1938), चिनगारी (1938), नवज्योति (1938), संगम (1940), जनयुग (1942), रामराज्य (1942), संसार (1943), लोकवाणी (1942), सावधान (1942), हुंकार (1942), और सन्मार्ग (1943), जनवार्ता (1972)। इनमें से अधिकांश साप्ताहिक हैं, परंतु जनमन के निर्माण में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है।
जहाँ तक पत्र-कला का संबंध है, वहाँ तक हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि तीसरे और चौथे युग के पत्रों में धरती और आकाश का अंतर है। एक समय तक पत्र-संपादन वास्तव में उच्च कोटि की कला थी। राजनीतिक पत्रकारिता के क्षेत्र में आज (1921) और इसके संपादक स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराड़कर का लगभग वही स्थान है, जो साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी को प्राप्त है। सच तो यह है कि आज ने पत्र-कला के क्षेत्र में एक महान संस्था का कार्य किया और उसने हिंदी को बीसियों पत्र-संपादक और पत्रकार दिए।
आधुनिक साहित्य के अनेक अंगों की भाँति हमारी पत्रकारिता भी नई कोटि की है और उसमें मुख्यतः हमारे मध्यवर्ग की सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, और राजनीतिक हलचलों का भास्वर प्रतिबिंब है। वास्तव में, पिछले 140 वर्षों का सच्चा इतिहास हमारी पत्र-पत्रिकाओं से ही संकलित हो सकता है। बंगला के कलेर कथा ग्रंथ में पत्रों के अवतरणों के आधार पर बंगाल के उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यवर्गीय जीवन के आकलन का प्रयास हुआ है। हिंदी में भी ऐसा प्रयास वांछनीय है।
द्विवेदी युग के साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं, वही उस साहित्य का असली रूप है। 1921 के बाद साहित्य बहुत कुछ पत्र-पत्रिकाओं से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, परंतु फिर भी विशिष्ट साहित्यिक आंदोलनों के लिए हमें मासिक पत्रों के पृष्ठ ही उलटने पड़ते हैं। राजनीतिक चेतना के लिए तो पत्र-पत्रिकाएँ हैं ही।
हिंदी में साहित्यिक पत्रिकाओं का लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। दरअसल, हिंदी में लघु पत्रिका आंदोलन की शुरुआत छठे दशक में व्यावसायिक पत्रिकाओं के जवाब में हुई। इस आंदोलन का श्रेय हम हिंदी के वरिष्ठ कवि विष्णुचंद्र शर्मा को दे सकते हैं। उन्होंने 1957 में बनारस से कवि का संपादन-प्रकाशन शुरू किया था। कालांतर में और भी कई लघु पत्रिकाएँ व्यक्तिगत प्रयासों और प्रकाशन संस्थानों से निकलीं, जिन्होंने हिंदी साहित्य की तमाम विधाओं को न केवल समृद्ध किया, बल्कि उनका विकास भी किया।
बेनेट कोलमैन एंड कंपनी तथा हिन्दुस्तान टाइम्स लिमिटेड की पत्रिकाएँ-धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, सारिका, कादम्बिनी, दिनमान, और माधुरी जैसी बड़ी पूँजी से निकलने वाली पत्रिकाओं के मुकाबले अणिमा, कहानी, नई कहानियाँ, कल्पना, लहर, वातायन, बिन्दु, क्यों, तटस्थ, वाम, उत्तरार्ध, आरम्भ, ध्वज भंग, सिर्फ, हाथ, कथा, आलोचना, कृति, क ख ग, माध्यम जैसी पत्रिकाएँ बड़े प्रतिष्ठानों से नहीं, बल्कि लेखकों के व्यक्तिगत, निजी प्रयासों से छोटे पैमाने पर निकलीं।
उस समय ऐसी पत्रिकाओं की जैसे झड़ी-सी लग गई: समझ, आवेग, सनीचर, अकविता, आकंठ, इबारत, जारी, ज़मीन, आइना, कंक, अब, आमुख, तेवर, धरातल, आवेश, आवेग, धरती, वयं, संबोधन, ओर, संप्रेषण जैसी पत्रिकाएँ निकलीं, जो सीमित संसाधनों, व्यक्तिगत प्रयासों, या लेखक संगठनों की देन थीं। इन पत्रिकाओं का मुख्य स्वर साम्राज्यवाद-विरोध था और ये शोषण, धार्मिक कट्टरता, लैंगिक असमानता जैसी प्रवृत्तियों के विरुद्ध खड़ी दिखाई देती थीं। एक समय तो ऐसा भी आया, जब मुख्यधारा के बहुत-से लेखकों ने पारिश्रमिक का मोह छोड़कर बड़ी पत्रिकाओं के लिए लिखना बंद कर दिया और वे केवल इन लघु पत्रिकाओं के लिए ही लिखते रहे।
लघु पत्रिका (लिटिल मैगजीन) आंदोलन मुख्य रूप से पश्चिम में प्रतिरोध (प्रोटेस्ट) के औजार के रूप में शुरू हुआ था। यह प्रतिरोध राज्य सत्ता, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, या धार्मिक वर्चस्ववाद-किसी के भी विरुद्ध हो सकता था। लघु पत्रिका आंदोलन की विशेषता उससे जुड़े लोगों की प्रतिबद्धता और सीमित आर्थिक संसाधनों में तलाशी जा सकती थी। अक्सर बिना किसी बड़े औद्योगिक घराने की मदद लिए, व्यक्तिगत अथवा छोटे सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप निकलने वाली ये पत्रिकाएँ अपने समय के महत्वपूर्ण लेखकों को छापती रही हैं।
भारत में भी सामाजिक चेतना के बढ़ने के साथ-साथ बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लघु पत्रिकाएँ प्रारंभ हुईं। 1950 से 1980 तक का दौर हिंदी की लघु पत्रिकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। यह वह दौर था, जब नई-नई मिली आजादी से मोहभंग शुरू हुआ था और बहुत बड़ी संख्या में लोग विश्वास करने लगे थे कि बेहतर समाज बनाने में साहित्य की निर्णायक भूमिका हो सकती है।
एक दौर ऐसा भी आया, जब बड़े घरानों की पत्रिकाओं में छपना शर्म की बात समझा जाता था और लघु पत्रिकाओं में छपने का मतलब साहित्यिक समाज की स्वीकृति की गारंटी होता था। इन्होंने रचनाशीलता का एक अलग ही माहौल बनाया। इनमें से अधिकांश में दृष्टि थी, रचना-विवेक था, और इन्हें लेखकों का अकुंठित सहयोग प्राप्त था।
लघु पत्रिकाएँ घटनाओं की जड़ तक पहुँचकर सच्चाई को उजागर करने का काम कर रही थीं। इनसे एक ओर जहाँ नवलेखन पल्लवित होता था, वहीं सामान्य जन की आशा-आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलती थी। लोग पारिश्रमिक देने वाली और लेखक को स्टार बनाने वाली पत्रिकाओं में छपने की जगह इनमें छपना गौरव की बात समझते थे। सारी बड़ी बहसें इन्हीं छोटी पत्रिकाओं में चलीं। आज जो भी लिखा जा रहा है, उसके प्रकाशन का मंच यही पत्रिकाएँ हैं।
आज के समय में मुख्यधारा की पत्रिकाएँ और अखबार कॉर्पोरेट जगत व साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव में समाहित हो रहे हैं। इस वजह से देश के चौथे स्तंभ के प्रति पाठकों में संशय उत्पन्न हो रहा है। कुछ लोगों ने हर काल में पत्रकारिता को अपने अनुसार परिभाषित करने या संचालित करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ पत्रकारों ने अपनी साख बचाने के लिए सत्ता-शीर्ष से कभी समझौता नहीं किया। पत्रकारिता पर सत्ता का दबाव कल भी था और आज भी है।
पत्रकारिता यदि जनसरोकार से जुड़ी हो, तो उसे कोई चाहकर भी दबा नहीं सकता, लेकिन आज स्थिति चिंताजनक है। पत्रकारिता को तहस-नहस करने की सुनियोजित कोशिश चल रही है। बहुत हद तक यह हो भी चुका है। मुख्यधारा की पत्रकारिता अनर्गल प्रलाप बन चुकी है। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक उपाय खोजने होंगे। आज सोशल मीडिया का बड़ा नेटवर्क है, लेकिन वह जनसरोकारों से पूरी तरह लैस नहीं है।
ऐसी स्थिति में लघु पत्रिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। लघु पत्रिकाएँ पिछलग्गू विमर्श का मंच नहीं हैं। लघु पत्रिका का चरित्र सत्ता के चरित्र से भिन्न होता है। ये पत्रिकाएँ मौलिक सृजन का मंच हैं। आज नैतिक पतन के दौर में लघु पत्रिकाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। रचनाकार वैचारिक लेखन से दूर होते जा रहे हैं, जो समाज के लिए चिंता का विषय है। साम्प्रदायिकता का सवाल हो, धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न हो, अथवा वैश्वीकरण का प्रश्न हो, हमारी व्यावसायिक पत्रिकाएँ सत्ता-विमर्श को ही परोसती रही हैं। सत्ता-विमर्श व उसके पिछलग्गूपन से इतर लघु पत्रिकाएँ अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता, संघर्षशीलता, और सकारात्मक सृजनशीलता की पक्षधर हैं।
लेकिन इन लघु पत्रिकाओं की सीमाएँ भी हैं:
- प्रसार बहुत कम (वैसे, अगर संतोष करना चाहें, तो यह तथ्य कि टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट और न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स की भी 7-8 हजार प्रतियाँ ही छपती हैं।)
- संपादकीय दृष्टि का अभाव
- रचनाओं का अभाव
- संपादक की महत्वाकांक्षा
- व्यावसायिक/आर्थिक विवशताएँ
मई 2022 में समकालीन जनमत पत्रिका में साथी कौशल किशोर का लघु पत्रिकाओं पर एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका एक अंश उद्धृत करना प्रासंगिक लगता है। वे कहते हैं: “यह समय है, जब लघु पत्रिकाओं में भी बदलाव दिखता है। वाम-जनवादी दिशा और तेवर की जगह अस्मिता-विमर्श, साम्प्रदायिकता का सवाल, उपभोक्तावाद, बाजारवाद आदि ले रहे हैं। विचार की जगह बाजार प्रधानता ग्रहण करता है। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पुरस्कारों आदि की ऐसी नकली होड़ शुरू हुई, जिसने मध्यवर्गीय महत्वाकांक्षा, व्यक्तिवाद, अवसरवाद जैसी पराई प्रवृत्तियों को बढ़ाने का काम किया। वस्तुपरकता का पहलू कमजोर हुआ। रचनाकारों में आत्मपरकता, आत्मश्लाघा, आत्मप्रशंसा, आत्मप्रचार बढ़ा। इस दौर की अधिकांश पत्रिकाएँ व्यक्तिगत प्रयासों से निकली हैं/निकल रही हैं। सामूहिकता की भावना, यानी जनवाद का पक्ष कमजोर हुआ है।”
ऐसे में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार आवश्यक है:
- स्वतंत्र रूप से निकलने वाली पत्रिकाओं और सरकारी संस्थानों/अकादमियों से निकलने वाली पत्रिकाओं में क्या कोई विशेष अंतर है? अगर नहीं है, तो इसके क्या कारण हैं?
- साहित्यिक पत्रिकाओं के चरित्र को देखें। जहाँ कुछ के पास संसाधनों का घोर अभाव है, उनके लिए एक-एक अंक के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कहीं न कहीं उनका कमिटमेंट और जुनून है, जिसकी वजह से पत्रिकाएँ निकलती हैं। वहीं, कुछ के पास संसाधनों और विज्ञापनों की कोई कमी नहीं। वे कलेवर में साहित्यिक दिखती हैं, लेकिन संचालन में व्यावसायिक हैं। बहुत कुछ इनका नजरिया बकौल धूमिल ‘विरोध में हाथ भी उठा रहे और काँख भी ढकी रहे’ रहता है। ऐसी पत्रिकाओं के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या हो?
- क्या आज की पत्रिकाओं का एक ही चेहरा है? उनके बीच क्या फर्क है या किया जाना चाहिए? इनके बीच क्या कोई विभाजन रेखा है?
- साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं के स्वरूप व चरित्र में आए बदलाव को देखते हुए क्या वर्तमान में उन्हें ‘लघु’ नाम देना उचित है? लघु से हमारा आशय क्या है? इनकी प्रतिबद्धता क्या हो?
ढेरों सामान्य, एकरस, और बड़े नामों को बांड बनाकर भुनाने वाली, विज्ञापनों से धन बटोरने वाली, सरकारी कृपा पर निर्भर रहने वाली, एक समूह के हितों को संपुष्ट करने वाली, यशकामी-महत्वाकांक्षी, अवसरवादी संपादकों की व्यक्तिगत कुंठाओं को ढोने वाली, सजावटी शो-रूम पत्रिकाओं की भीड़ में निस्पृह रहकर पत्रिका निकाल पाना एक अत्यंत दुरूह कर्म है।
मैंने भी एक प्रयास किया और अपने अनुभव से जाना कि ऐसे प्रयासों में लोगों का सहयोग भी अत्यल्प होता है। अधिकांश लोग लघु पत्रिका प्रकाशन की कठिनाइयों को नहीं समझते। उनकी समझ स्टीरियोटाइप होती है। उनके सामने एक उत्पाद भर होता है, जैसे कि कोई व्यावसायिक उत्पाद हो। दोनों में अंतर करने की दृष्टि और क्षमता वहाँ नहीं दिखती। संवेदनशीलता की कमी भी झलकती है। हिंदी में ऐसे पाठकों की कमी है, जो पत्रिका खरीदने को नैतिक दायित्व समझते हों। बड़े-बड़े साहित्यकार और हिंदी के अधिकांश प्राध्यापक पत्रिका खरीदना अपनी तौहीन मानते हैं।
आज राष्ट्रीय एवं वैश्विक कारणों से न तो लघु पत्रिकाएँ निकालने वालों के मन में पुराना जोश बाकी है और न ही उनमें छपना पहले जैसी विशिष्टता का अहसास कराता है। फिर भी, लघु पत्रिकाओं में छपी सामग्री का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। हिंदी साहित्य के बहुत-से विवाद, आंदोलन, और प्रवृत्तियों को निर्धारित करने वाली सामग्री और महान रचनाएँ इन लघु पत्रिकाओं के पुराने अंकों में समाई हुई हैं। इनमें से बहुत-सी सामग्री कभी पुनर्मुद्रित नहीं हुई। साहित्य के गंभीर पाठकों और शोधार्थियों के लिए इनका ऐतिहासिक महत्व है। अब भी लघु पत्रिकाएँ सामाजिक व राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए साहित्यिक चेतना जगाने का काम कर रही हैं।
(शैलेन्द्र चौहान लेखक-साहित्यकार हैं और जयपुर में रहते हैं)