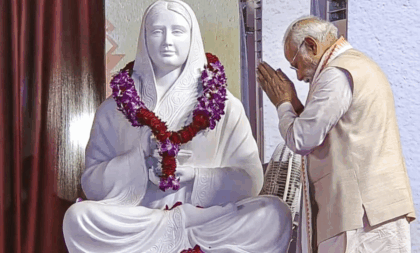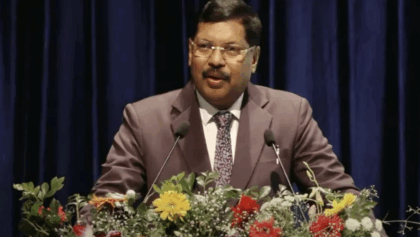इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के संभावित प्रकोप को देखते हुए देश में 2022 में होने वाले चुनाव टाल दिए जाएं। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस कथन की कानूनी पड़ताल के पचड़े में न पड़ते हुए, इसका निर्णय, भारत निर्वाचन आयोग के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि संविधान के अंतर्गत, देश में, चुनाव कराने, टालने और संशोधित करने की सारी शक्तियां आयोग के पास हैं। अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा भी है कि इस विषय पर राज्यों से विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। कल क्या होगा, यह अभी नहीं बताया जा सकता है। फिलहाल तो इस महामारी ने बच्चों की शिक्षा पर क्या असर डाला है इस बिंदु पर चर्चा करते हैं।
देश मे कोरोना की आमद 30 जनवरी 2020 में केरल में मिले एक मरीज से हुयी और धीरे धीरे 2020 के खत्म होते होते कोरोना ने देश में तबाही के कई मंज़र दिखा दिए। इसका व्यापक असर, न केवल उद्योगों और व्यापार पर पड़ा, बल्कि इसका एक बड़ा असर स्कूलों पर, बच्चों की मानसिक स्थिति और उनकी मनोदशा पर भी पड़ा है। लगभग, दो वर्ष से महामारी के कारण, पूरे भारत के अधिकांश स्कूल बंद चल रहे हैं। बच्चे घरों में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूली छात्रों की सामान्य दिनचर्या, जिसमें केवल क्लासरूम में प्रत्यक्ष पढ़ाई ही नहीं शामिल होती है, बल्कि स्पोर्ट्स, हॉबी विकास, अन्य शिक्षणेत्तर गतिविधियां भी होती हैं, बाधित हो गयी हैं। अचानक हुए इस परिवर्तन ने सभी राज्यों, वर्गों, जाति, लिंग और सभी क्षेत्रों के बच्चों की एक बड़ी संख्या को प्रभावित किया है। बच्चे एक प्रकार के कैदखाने में कैद हो गए हैं। विशेषकर, उन घरों में जो एकल परिवार के हैं और छोटे छोटे फ्लैटों में पहले ही एक प्रकार के आइसोलेशन में जी रहे हैं। संयुक्त परिवारों और बड़े घरों में तो थोड़ी बहुत, राहत है, पर एकल परिवार और कामकाजी दंपतियों के परिवार के बच्चों पर इस महामारी जन्य कैदखाने का बेहद प्रतिकूल असर पड़ा है।
इस सम्बंध में यूनिसेफ द्वारा एक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन पर सुजॉय घोष जो अर्थव्यवस्था और उसके राजनीतिक असर पर अक्सर लिखते रहते हैं ने इंडियन पोलिटिकल डिबेट वेबसाइट पर एक गम्भीर लेख लिखा है। हाल ही में किए गए यूनिसेफ के उक्त अध्ययन के अनुसार, स्कूलों के बंद होने से 286 मिलियन छात्र, जिनमें 48 प्रतिशत लड़कियां हैं, और जो पूर्व-प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ती हैं, प्रभावित हुयी हैं। महामारी के दौरान, भारत में, स्कूलों के अचानक बंद हो जाने के कारण, पारंपरिक कक्षा आधारित भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली अब एक अनियोजित ऑनलाइन आधारित शिक्षा प्रणाली के रूप में स्थानांतरित हो गई है। अनियोजित इसलिए कि, न तो हम मानसिक रूप से और न ही तकनीकी रूप से ऑनलाइन शिक्षा की इस अचानक आ पड़ी, चुनौती से निपटने के लिये, तैयार थे। अचानक होने वाला यह अप्रत्याशित तकनीकी बदलाव न केवल छात्रों को, डिजिटल रूप से विभाजित कर रहा है, बल्कि उनके सीखने की क्षमता, और उनकी समग्र प्रगति (सामाजिक और सांस्कृतिक कौशल, फिटनेस, आदि) को भी धीमा कर दे रहा है। सामूहिकता न केवल तरह तरह से सीखने की क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि वह तरह तरह की होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिये बच्चों को मानसिक रूप से तैयार भी करती है। बच्चों पर, उनकी सीखने की क्षमता और विविधता के अलावा, स्कूली शिक्षा की अनुपस्थिति का, बच्चों और किशोरों के समग्र विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ेगा।
कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों के बंद होने के कारण छात्रों के सीखने की क्षमता, लर्निंग कैपेसिटी, पर क्या प्रभाव पड़ा है, का आकलन करने के लिए, यूनिसेफ ने देश के छह राज्यों, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आंकड़े जुटाए और उनका मूल्यांकन और अध्ययन किया। यह अध्ययन, “कोविड के संदर्भ में स्कूल बंद” प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष यह भी है कि, “छात्र स्कूल बंद होने पर स्व-अध्ययन पर समय तो अधिक व्यतीत कर रहे हैं पर सीख कम रहे हैं, जबकि, स्कूल में कम समय बिताते हैं और, अधिक सीखते हैं।” यानी स्कूलों में वे कम समय के बावजूद, अधिक मात्रा में और अधिक तेजी से पाठ्यक्रम सीखते हैं। जबकि घरों में स्वअध्ययन यानी ऑनलाइन पर अधिक समय देने के बावजूद, अधिक नहीं सीख पा रहे हैं। यह अंतर सामूहिक और एकल अध्ययन के गुणदोष का है। अध्ययन में आये आंकड़ों के अनुसार, 97% छात्र प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे पढ़ाई और सीखने में व्यतीत करते हैं। लेकिन प्रति दिन 3-4 घंटे की पढ़ाई स्कूल की प्रत्यक्ष पढ़ाई की मात्रा से कम है। साथ ही, स्कूल खुलने के बाद भी, छात्र आमतौर पर होमवर्क, ट्यूशन और अन्य स्व-निर्देशित, चीजों के सीखने की गतिविधियों पर समय बिताते ही हैं। सामूहिकता सीखने की क्षमता, लालसा और उत्कंठा को बढ़ा देती है, जबकि एकल अध्ययन, नीरस और उबाऊ हो जाता है। यह अध्ययन स्कूली बच्चों पर है, न कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति वालों पर।
अब अगर हम ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और नेट की पहुंच क्षमता का आकलन करें तो पाएंगे कि, हम में से अधिकांश अपने देश में भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक वर्गों में ‘डिजिटल हैव नॉट्स’ की तरह ही हैं। डिजिटल हैव नॉट्स यानी वे इलाके जो नेटवर्क और अन्य सायबर सुविधाओं में पिछड़े हैं। इस अध्ययन के अनुसार, उपरोक्त छह राज्यों में, 10 प्रतिशत छात्र स्मार्ट फोन, फीचर फोन, टीवी, रेडियो, या लैपटॉप / कंप्यूटर आदि किसी भी उपकरण से वंचित हैं। यह मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों की व्यथा है, जहां स्कूल और शिक्षक तो हैं पर ऑनलाइन पढ़ाई के लिये आवश्यक उपकरण नहीं हैं। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि, जनता तक प्रौद्योगिकी की पहुंच अभी दूर की बात है। यह भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि कई इलाकों में दूरस्थ शिक्षण संसाधनों, ऑनलाइन सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद, सर्वेक्षण किए गए छह राज्यों में 40 प्रतिशत छात्रों ने स्कूलों के बंद होने के बाद से किसी भी प्रकार के दूरस्थ या ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग नहीं किया। जब ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग न करने वाले छात्रों से पूछा गया कि, उन्होंने ऑनलाइन शिक्षण उपकरणों का उपयोग क्यों नहीं किया, तो 73 प्रतिशत छात्रों ने, इसे सीखने की सामग्री या संसाधनों के बारे में जागरूकता की कमी का होना बताया।
उपरोक्त अध्ययन, दो महत्वपूर्ण समस्याओं का संकेत देते हैं। एक, ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों का सामर्थ्य और दूसरे इनके प्रति, जागरूकता। माता-पिता या अभिभावकों के एक समूह के लिए, एक मुख्य बाधा डिवाइस और इंटरनेट (डेटा) पाने की क्षमता और सामर्थ्य है, यानी वे ऑनलाइन पढ़ाना तो चाहते हैं पर उनमें इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है कि ऑनलाइन शिक्षा के लिये, ज़रूरी उपकरण खरीद सकें। वहीं दूसरी ओर, एक अन्य समूह, ऐसे माता-पिता और अभिभावकों का है, जो अपने बच्चों के लिए उपकरण और इंटरनेट दोनों का खर्च, आसानी से वहन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण उपकरण और प्रक्रिया के उपयोग के बारे में, उनमें पर्याप्त जागरूकता का अभाव है।
यूनिसेफ ने इस अध्ययन में, ऑनलाइन स्कूली शिक्षा की प्रभावशीलता को अपने अध्ययन का एक प्रमुख बिंदु रखा है। यूनिसेफ के इस अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार, “माता-पिता और शिक्षक दोनों महसूस करते हैं कि छात्र स्कूलों की तुलना में दूरस्थ (ऑनलाइन अध्ययन के लिए, दूरस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है) शिक्षा के माध्यम से कम सीखते हैं। 5 से 13 वर्ष की आयु के छात्रों के 76 प्रतिशत और 14 से 18 वर्ष की आयु के 80 प्रतिशत, किशोरों के बारे में इस अध्ययन की रिपोर्ट है कि छात्र स्कूलों में जितना, सीखते हैं, उसकी तुलना में ऑनलाइन शिक्षा में वे कम सीख रहे हैं। अध्ययन के अनुसार, 67 प्रतिशत शिक्षक यह मानते हैं कि यदि स्कूल खुले रहते तो, जितना छात्र स्कूलों में जाकर पढ़ते सीखते हैं, उसकी तुलना में छात्र, अपनी समग्र सीखने की क्षमता में पिछड़ रहे हैं। खासकर प्राथमिक स्कूलों के छात्र इसमें अधिक नुकसान में हैं।
सीखने की क्षमता में कमी के अतिरिक्त, स्कूल बंद होने के कारण, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है। जैसे-जैसे छात्र अपने घरों में, महामारी जन्य आइसोलेशन में कैद होते गए, वे अपने मित्रों और शिक्षकों से दूर होते गए। साथ ही महामारी में आने वाली बुरी खबरों का असर जो घर के बड़ों पर पड़ा, उनके तनाव से भी बच्चों और किशोरों के मन मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। माता-पिता की नौकरियों पर असर पड़ा, कुछ महामारी के ग्रास बन गए तो, इसका असर पड़ा, और घर मे लगातार महामारी जन्य नकारात्मकता ने बच्चों को मानसिक रूप से रुग्ण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घर के जबरिया थोपे गए एकांत और हमउम्र मित्रों के अभाव के कारण उपजी संवादहीनता ने, बच्चों के सीखने की क्षमता और स्वाभाविक जिज्ञासु भाव को बहुत अधिक प्रभावित किया है। अध्ययन से यह पता चलता है कि, 5 से 13 वर्ष की आयु के एक तिहाई छात्रों और लगभग आधे किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर खराब असर या बहुत ही खराब असर पड़ा है। अध्ययन के दौरान परिवारों से साक्षात्कार भी लिये गये। उनके अनुसार, “सामाजिक अलगाव, सीखने में व्यवधान और परिवार की वित्तीय असुरक्षा खराब मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख कारण हैं।”
देश में, स्कूल फीडिंग प्रोग्राम (मुख्य रूप से सरकारी स्कूलों में), मिड डे मील (एमडीएम) के कई लाभ हैं जैसे कि, कक्षा में भूख से बचना, स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना और सबसे प्रमुख, कुपोषण को दूर करना है। अब, देश भर में स्कूल बंद होने के कारण, ‘स्कूल फीडिंग कार्यक्रम अब योजना (एमडीएम पोर्टल) के तहत नामांकित 115.9 मिलियन बच्चों को बहुत जरूरी मुफ्त दोपहर का भोजन प्रदान नहीं कर सका।’ इसलिए, सीखने के अलावा, स्कूली शिक्षा की अनुपस्थिति का भी बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। कोरोना की स्थिति तुलनात्मक रूप से थोड़ी बेहतर हुयी तो, माता-पिता और सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में सोचना शुरू कर ही दिया था, कि, कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के मामले बढ़ने लगे। बच्चों का टीकाकरण अभी नही हुआ है और संक्रमण का खतरा उठाना भी उचित नहीं है तो स्कूलों को खोलने की योजना पर सरकारें जो सोच रही थीं, उन पर फिर ग्रहण लग गया।
यूनिसेफ की रिपोर्ट ने एक और तथ्य की ओर इशारा किया है कि, ‘लगभग 8 प्रतिशत छात्र स्कूल खुलने के बाद, अगले तीन महीनों में या उसके बाद स्कूल नहीं लौट सकेंगे। उनमें से अधिकांश (60%) स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण स्कूल नहीं लौट पाएंगे। इस त्वरित मूल्यांकन रिपोर्ट ने यह भी उजागर किया कि ‘स्कूल बंद होने के एक बड़े झटके के रूप में, कुछ बच्चे वापस लौटने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। वे पूरी तरह से स्कूल छोड़ सकते हैं। 10 प्रतिशत परिवारों का कहना है कि वे बच्चों को वापस स्कूल भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते जबकि 6 प्रतिशत का कहना है कि उन्हें जीने योग्य आय अर्जित करने के लिए, अपने बच्चों की मदद की आवश्यकता है।’ पश्चिम बंगाल में एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया है कि महामारी के दौरान स्कूल जाने वाले बच्चों के बाल श्रम में 105% की वृद्धि हुई है। महामारी के दौरान ‘सेव द चिल्ड्रन’ द्वारा इसी तरह के एक सर्वेक्षण में शामिल 62 प्रतिशत परिवारों, जिसमें क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों में 67 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 55 प्रतिशत हैं, के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुयी है।
महामारी का व्यापक असर देश की आर्थिकी पर पड़ा है। 2016 में हुयी नोटबन्दी के कारण 31 मार्च 2020 तक देश की जीडीपी में 2 प्रतिशत गिरावट आ चुकी थी और फिर जब महामारी का दौर आया तो, लम्बे समय तक चलने वाले रुक रुक के लॉक डाउन, कामगारों के व्यापक और देशव्यापी विस्थापन ने, देश की बेरोज़गारी दर को और बढ़ा दिया जिससे मंदी जैसे हालात पैदा हो गये। इसका सीधा असर, लोगों की जीवन शैली पर पड़ा और बच्चों की शिक्षा इससे बुरी तरह से प्रभावित हुयी। लोगों के पास, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिये धन की कमी हुयी तो शिक्षा जो सरकार की प्राथमिकता में तो वैसे भी नहीं है, अब इन विपन्न होते परिवारों में भी प्राथमिकता से धीरे धीरे बाहर होने लगी। इसका प्रभाव आगे चल कर उन गरीब परिवारों पर अधिक पड़ेगा, जिन्हें बजट की कमी का सामना बराबर करना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप, गरीब होते परिवारों के बच्चे स्कूल छोड़ देंगे और अपने माता-पिता की कमाई में मदद करने के लिए आर्थिक गतिविधियों में लग जाएंगे। यह स्पष्ट है कि बच्चे जितने अधिक समय तक स्कूल से बाहर रहते हैं, वे उतने ही कमजोर होते जाते हैं और उनके स्कूल लौटने की संभावना भी कम होती जाती है।
सरकार को शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को गम्भीरता से लेना होगा। देश मे सरकारी स्कूली शिक्षा की बात करे तो उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। निजी स्कूल ज़रूर बहुत हैं और अब भी खुल रहे हैं, पर वे दिन पर दिन महंगे भी होते जा रहे हैं और तरह तरह के शुल्कों के कारण, एक सामान्य वेतनभोगी या निम्न मध्यवर्ग की पहुंच के बाहर भी हैं। ऐसे स्कूलों के फीस ढांचे पर सरकार का या तो कोई नियंत्रण नहीं है या सरकार जानबूझकर उन्हें नियंत्रित करना ही नहीं चाहती है। ऐसी स्थिति में पढ़ाई की असल नींव जो स्कूली शिक्षा में पड़ती है, वह नहीं बन पा रही है। महामारी एक अस्थायी समस्या है। टीकाकरण और अन्य इलाज की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। स्थिति सामान्य होगी ही और स्कूल भी खुलेंगे। पर शिक्षा, कम से कम स्कूली शिक्षा तो सर्वसुलभ हो, यह देश और समाज की बेहतरी के लिये अनिवार्य है। ऑनलाइन शिक्षा, एक मज़बूरी भरा विकल्प है जो इस महामारी जन्य आफ़तकाल में स्कूल से आभासी रूप से जोड़े रखने का एक उपक्रम भर है। असल शिक्षा तो स्कूलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों में सामूहिक क्लास रूम में मिलती है न कि मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप के स्क्रीन पर।
( विजय शंकर सिंह रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं। )