कबीर और कबीरपंथ ब्रिटिश शोधकर्ता और लेखक एफ ई केइ (फ्रैंक अर्नेस्ट केइ) की मशहूर और ऐतिहासिक महत्व की किताब-कबीर एंड हिज फालोवर्स (1931) का हिंदी अनुवाद है। मूल पुस्तक अंग्रेजी में पहली बार एसोसिएशन प्रेस, कलकत्ता से छपी थी। अब तक इसका अनुवाद नहीं उपलब्ध नहीं था। पहली बार इसका अनुवाद मशहूर लेखक और विचारक कंवल भारती ने किया। इसे कबीर और कबीरपंथ के रूप में फारवर्ड प्रेस, दिल्ली ने जुलाई, 2022 मे प्रकाशित किया।
केइ एंग्लिकन चर्च के पादरी, मिशनरी और लेखक थे। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से एम. ए. और डी लिट् तक की शिक्षा अर्जित की थी। वह भारत में अनेक स्थानों पर पदस्थापित रहे। इंडियन एजूकेशन इन एनशियेंट टाइम्स(1918), ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर(1920) और कबीर एंड हिज फालोवर्स (1931)-उनकी तीन भारत-विषयक किताबें हैं। केइ का जन्म 1879 में और निधन 1974 में हुआ। वह ब्रिटेन में लंदन, हालैंड में एम्सटर्डम और भारत में शिमला, जबलपुर, मेरठ, भागलपुर सहित कई अन्य स्थानों पर रहे।
इस किताब में कुल 11 अध्याय हैं-कबीर का समय और परिवेश, किंवदंतियों में कबीर का जीवन, इतिहास के कबीर, कबीर का साहित्य, कबीर के सिद्धांत, कबीरपंथ का इतिहास और संगठन, कबीरपंथ का साहित्य, कबीरपंथ के धर्म-सिद्धांत, कबीरपंथ के संस्कार और कर्मकांड, कबीर से प्रेरित अन्य संप्रदाय, कबीर और ईसाइयत। पुस्तक में आठ पृष्ठों की द्वारका भारती लिखित भूमिका है-‘आइए, ऐतिहासिक कबीर से मिलें’।
इसके बाद फिर एक कंवल भारती की बहुत जरूरी अनुवादकीय टिप्पणी है-सात पृष्ठों की। इसमें किताब के विभिन्न अध्यायों के ब्योरे सहित उसका परिचय दिया गया है। मूल किताब छपने के 90 साल बाद हिंदी में पहला अनुवाद कंवल जी ने किया। अंग्रेजी में शोधपत्र की तरह छपी किताब को कंवल जी ने अपने अनुवाद से सहज और रोचक बनाया है। भूमिका में वह लिखते हैं कि डॉ. धर्मवीर ने अपनी किताबों में कबीर पर हजारी प्रसाद दिवेदी और राम चंद्र शुक्ल आदि की थीसिस को पूरी तरह खारिज किया है। उनका मानना है कि कबीर ने हिन्दू शास्त्रों और लोक-विश्वासों का आजीवन विरोध किया। हजारी प्रसाद जी का कबीर हिन्दू अवधारणाओं का ही कबीर है। पर धर्मवीर इसे निराधार साबित करते हैं।
समीक्षित पुस्तक : कबीर और कबीरपंथ
लेखक : एफ. ई. केइ
अनुवादक : कंवल भारती
प्रकाशक : फारवर्ड प्रेस, नई दिल्ली
मूल्य : 200 रुपए (अजिल्द)
केइ कबीर को कबीरपंथियों के कबीर से भिन्न पाते हैं। कबीरपंथियों ने कबीर को ईश्वर के समकक्ष रख दिया पर ऐसा करने से सतपुरुष की अवधारणा जिसे कबीर ने रखा, अपना महत्व खो देती है। कबीर साहित्य में जिस निरंजन शब्द का प्रयोग हुआ है-वह काल या समय ही है। सिखों में सतपुरुष ही सतनाम के रूप में आया है। भूमिका में कहा गया है कि कबीर उस भारतीय दर्शन के संवाहक नहीं हैं जिसके मूल में स्मृतियां, वेद और पुराण हैं। कबीर ने अपने जीवन में जो देखा-समझा, उसे लिखा और प्रतिपादित किया। कबीर अरबी भाषा का शब्द है,जिसका मतलब है-महान। टैगोर और अम्बेडकर ने भी कबीर की महानता स्वीकार की है।
किताब में एक जगह बीजक शब्द की उत्पत्ति बताई गयी है कि कबीर-समर्थकों ने उनके ग्रंथ को बीजक का नामकरण कैसे किया, कहां से आया यह शब्द? पूर्वी इलाके में जहां कबीर रहते थे-साधारण लोगों मे एक प्रथा थी कि वे अपनी कोई बहुमूल्य चीज जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ देते थे। उसे चिन्हित करने के लिए कुछ निशान भी बना देते थे। उस गुप्त निशान को बीजक कहा जाता था। कबीर की बहुमूल्य वाणी के संग्रह को इसी बहुमूल्यता के कारण बीजक नाम दिया गया।
ज्यादातर संत कवियों की तरह कबीर भी काफी घुमक्कड़ थे। इस किताब में किंवदंतियों के अनुसार कबीर ने बलख और बुखारा तक की यात्रा की थी। कबीर के बारे में सही तथ्य कहां से मिल सकते हैं-इस पर लेखक बताता है कि किंवदंतियों के साथ कबीर का वास्तविक वृत्तांत इतना मिला हुआ है कि दोनों को अलग-अलग करना मुश्किल है और अनुचित भी है। क्योंकि ऐसी किंवदंतियों में अतिशयोक्ति के बावजूद कबीर के जीवन और कर्म के बारे में बहुतेरी सच्चाइयां खोजी जा सकती हैं। दूसरा स्रोत माना है-आदिग्रंथ में शामिल पदों को। साथ में लेखक यह भी कहता है कि पूरे भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता कि कबीर के नाम से दर्ज वे सारे पद स्वयं कबीर के ही लिखे हैं। कबीर ने बहुत सारा लेखन रूपकों में किया है इसलिए उनके हर पद और विषय का शाब्दिक अर्थ या मतलब खोजना आसान नहीं है।
कबीर के जुलाहा (मुस्लिम) होने पर लेखक को कोई संदेह नहीं है। यह महज संयोग नहीं कि उनका नाम भी मुस्लिम परंपरा का शब्द है। बनारस गजेटियर कहता है कि कबीर बनारस के पास के आजमगढ के बेलहार गांव मे पैदा हुए थे। पर उनको बनारस का पैदा हुआ बताने वालों की संख्या ज्यादा है। उनके विवाहित होने या न होने पर विवाद है-लोई, कमाल और कमाली को कुछ लोग शिष्या-शिष्य बताते हैं तो बहुत सारे पत्नी और बाल-बच्चे। एक बात असंदिग्ध है कि वह एक लोअर क्लास मुस्लिम थे-जुलाहा। स्वयं कबीर ने ऐसा कहा है-
जोलाहे घरु आपना चीन्हा
घट ही रामु पछानां
कहतु कबीरु कारगह तोरी
सूतै सूत मिलाए कोरी
कबीर अपने समय के बेहद अलोकप्रिय व्यक्ति थे। उनके परिवार के लोगों ने भी उन्हें तिरस्कार योग्य समझा। अन्य लोगों ने भी उनके विचारों के कारण उकी उपेक्षा की। कभी-कभी गालियां भी मिलती थीं। इसका उनके पदो में वर्णन मिलता है। कबीर का विरोध करने वाले खासतौर पर ब्राह्मण थे। वे उनको नीची जाति का लंपट, आवारा और ईश्वर द्रोही कहते तो वह उनकी परवाह किये बगैर कहते कि ब्राह्मण अज्ञान के चलते आध्यात्मिक सत्य को नहीं जानते। इसीलिए वे समाज को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं-
तूं ब्रह्मनु मैं कासीक जुलहा
मुहि तोहि बराबरी कैसे कै बनहि
हमरे राम नाम कहि उबरे
बेद भरोसे पांडे डूब मरहि
मौलवियों पर भी उनका प्रहार देखें-
बहुतक देखे पीर औलिया पढ़ैं किताब कुराना
कै मुरीद तदबीर बतावै उनमें उहै जो ज्ञाना
बताते हैं कि एक बार कबीर ने मक्का जाने का भी मन बनाय़ा पर वे नहीं गये। संकीर्ण पंडित और संकीर्ण मुसलमान, दोनों उनके समान विरोधी थे। सुल्तान सिकंदर लोधी के समय वह बनारस छोड़कर मगहर चले गये। अपनी जान बचाने या सुल्तान के आदेश पर, इस बारे में ठोस तथ्य नहीं हैं। कबीर का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ बीजक ही है। बनारस, मिर्जापुर और गोरखपुर के इलाके में बोली जाने वाली भाषा में इसके पद लिखे गये हैं-
मेरी बोली पूरबी ताइ न चीन्है कोई
मेरी बोली सो लखै जो पूरब का होई
(बीजक, साखी-194)
पूरबिया भाषा में अरबी-फारसी और तुर्की के 200 से भी ज्यादा शब्द बीजक मे पाये गये हैं। बीजक के अनेक संस्करण हैं। पहला बनारस से 1868 में छपा था, जिसमें रीवा के महराजा विश्वनाथ सिंह की टीका भी है। एक पाठ 1911 में कानपुर से छपा-वह बनारस वाले से मिलता-जुलता है। बीजक के अलावा आदिग्रंथ है, जिसमें कबीर के पद मिलते हैं। यह सिखों का पवित्र ग्रंथ है। यह 1604 में सिख गुरु अर्जन के आदेश पर तैयार किया गया, जो सिखों के छठें गुरु थे। इसे दसवें गुरु के ग्रंथ से अलग करने के लिए आदिग्रंथ कहा जाता है।
कबीर की लोकप्रियता के बारे में केइ की मान्यता हैः ‘संभवतः कबीर के अलावा ऐसा कोई दूसरा कवि नहीं है, जिसके पद और दोहे उत्तर भारत के लोगों की जुबान पर इतने ज्यादा हों, सिवाय तुलसीदास के।’ (पृष्ठ-100) लेखक किताब के पांचवें अध्याय-‘कबीर के सिद्धांत’ में कबीर की विचारधारा का अध्ययन और विश्लेषण करता है। यह अध्याय कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है।
केइ की वस्तुनिष्ठता से हिंदी लेखकों को सीखना चाहिए कि कबीर का यह गंभीर अध्येता किस तरह कबीर की भक्ति में डूबे बगैर उनकी वैचारिकी को बहुत ईमानदारी से रेखांकित करता है। इसके लिए वह सिर्फ उनके पदों और दोहों का सहारा लेता है। उसका मानना है कि कबीर एक सशक्त कवि के अलावा एक व्यावहारिक धर्मगुरु सरीखे हैः ‘कबीर एक धार्मिक दार्शनिक से ज्यादा एक एक व्यावहारिक धर्मगुरु थे; इसलिए उनके विचारों में हमेशा एक परिपूर्ण संगति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनकी शिक्षा में रचनात्मकता का अभाव नहीं था और उनके सिद्धांत में सिर्फ नकारों का समावेश नहीं था, फिर भी निस्संदेह वे अपने समय की दोषपूर्ण व्यवस्थाओं के आलोचक ज्यादा थे और किसी नई व्यवस्था के सर्जक कम। शायद इसीलिए बाद में उनके अनुयायियों ने अपनी रचनाओं को कबीर का बताया ताकि वे उनकी शिक्षा में कमियों की पूर्ति कर सकें।(पृष्ठ-101-102)।
केइ के मुताबिक कबीर एक ईश्वर में यकीन करते थे। पर अपने ईश्वर के लिए वह कई शब्दों में का प्रयोग करते थे-जैसे-राम, हरि, गोविन्द, नारायण, अल्लाह और खुदा आदि। कबीर के लिए मूर्ति-पूजा का कोई मतलब नहीं था। वह उसका तीव्र विरोध करते थे। उनका विरोध मूर्तिपूजा तक ही सीमित नहीं था, वह समूचे कर्मकांड, अनुष्ठान, यज्ञ, उपवास, जनेऊ, खतना, कंठीमाला और शुद्धि आदि के भी विरोधी थे। पशुबलि की भी उन्होंने निंदा की। वेद, पुराण और कुरान जैसे तमाम धार्मिंक ग्रंथों में उनका कोई विश्वास नहीं था। केइ ने इस बारे में कबीर को कई बार उद्धृत किया है। उनमें कुछ की शुरुआती पंक्तियां यहां देखियेः
योग यज्ञ जप संयमा तीरथ व्रत दाना
नवधावेद किताब है झूठे के बाना
काजी तुम कौन किताब बखाना
माथे तिलकु हाथि माला बानां
लोगन रामु खिलउना जानां
कबीर ने योगी सन्यासियों की भी निंदा की है, जो उनके समय में बहुत बड़ी संख्या में थे। यथाः
जटा तोरि पहिरालै सेली। योग युक्ति कै गर्भ दुहेली।।
आसन उड़ाये कौन बड़ाई। जैसे काग चील्ह मड़राई।।
(बीजक, रमैनी-71)
कबीर वर्ण और जाति की व्यवस्था के घोर विरोधी थे। जिस तरह हिन्दू-मुसलमान के विभाजन को वह खारिज करते हैं, उसी तरह जाति-वर्ण के विभाजन को भी। केइ को वह अपने समय के सबसे बड़े मानववादी नजर आते हैं। सभी मनुष्य उन्हें एक ही ईश्वर के परिवार के सदस्य लगते हैं। इसलिए उन्हें परिवार में किसी तरह क विभाजन असह्य है। कबीर की वैचारिकी के कुछ पहलुओं से नास्तिक और तर्कवादी कुछ मायूस भी हो सकते हैं। यहां उन्हें कबीर की वैचारिकी की सीमा नजर आयेगी। इन सीमाओं की भी केइ ने चर्चा की है। उदाहरण के लिए केइ बताते हैं कि कबीर कर्म-पुनर्जन्म और मायाचक्र आदि की हिन्दू-धारणा को अपने ढंग से मानते हैं। ‘कबीर और सूफीवाद’ उपशीर्षक में केइ लिखते हैं-‘ निस्संदेह कबीर और सूफियों की शिक्षा में काफी समानता है।’ अपने इस मंतव्य के पक्ष में वह सिर्फ दलील नहीं, ठोस तथ्य भी देते हैं।
कबीर और कबीरपंथ से जुड़े ऐसे अनेक अनछुए पहलुओं पर केइ विचार करते हैं और तथ्यों और तर्कों की रोशनी में महत्वपूर्ण सामग्री पेश करते हैं। इस ब्रिटिश शोधकर्ता ने सचमुच कबीर पर जितनी मेहनत, शोध और चिंतन-मनन से काम किया है, उसके लेखन और मूल्यांकन में जिस तरह की वस्तुनिष्ठता है, वह अप्रतिम है। यह हम उत्तर-भारतीयों, खासकर हिंदी वालों के लिए अनुकरणीय भी है। कबीर पर एफ ई केइ की यह किताब जरूर पढ़ी जानी चाहिए। विख्यात लेखक और विचारक कंवल भारती ने इसका सहज और सुंदर अनुवाद और फारवर्ड प्रेस ने इसे प्रकाशित करके हिंदी पाठकों पर बड़ा उपकार किया है।
(उर्मिलेश वरिष्ठ पत्रकार हैं।)





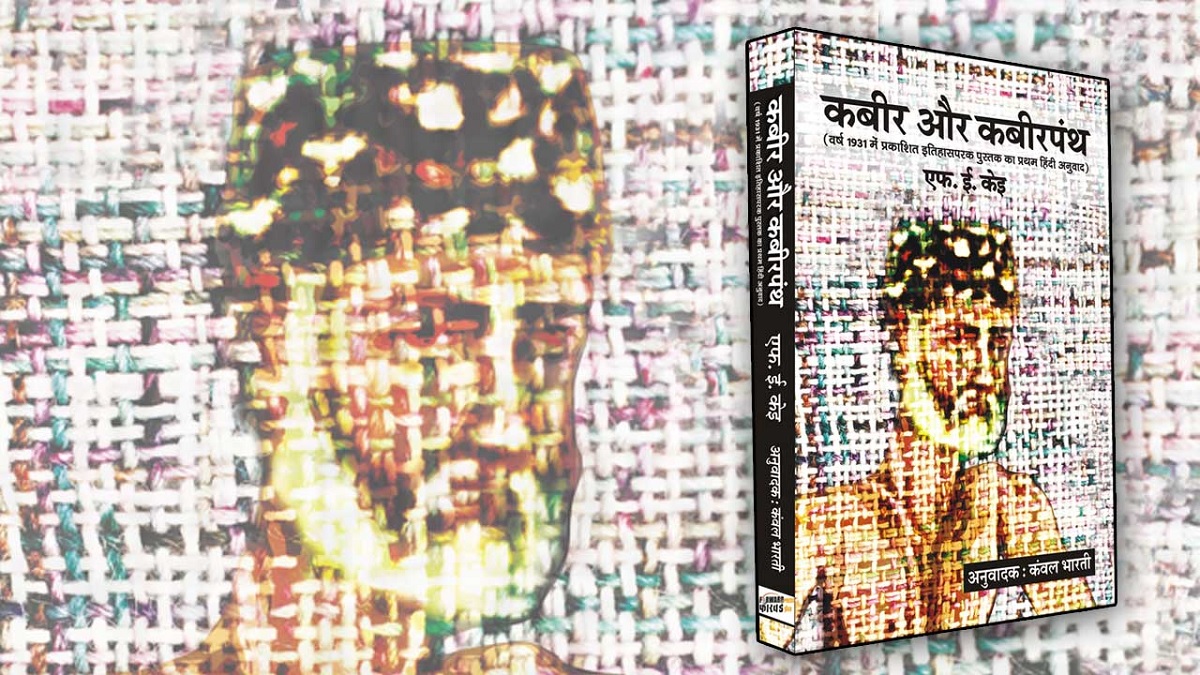
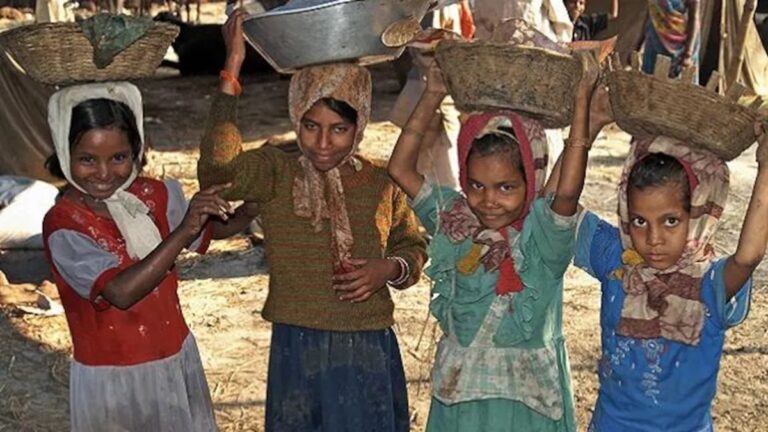
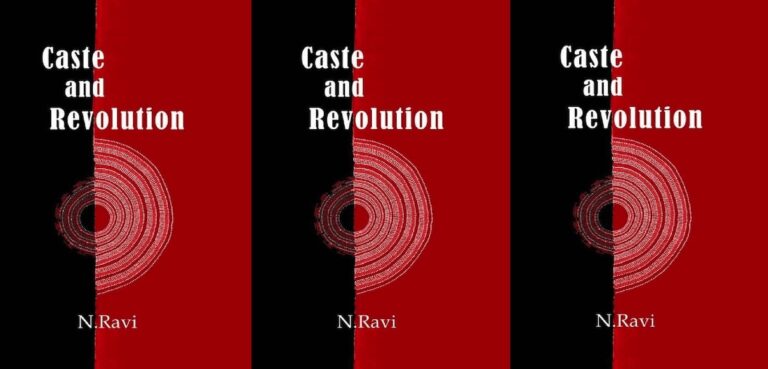



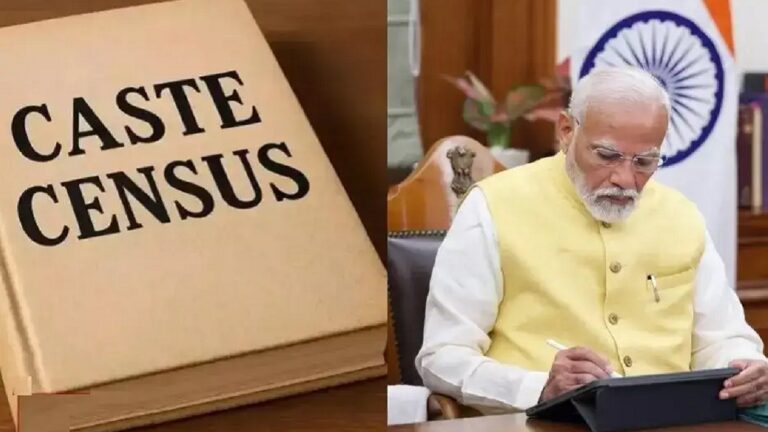


पठनीय
वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी की कबीर की पुस्तक पर लिखी समीक्षा पढ़ी
प्रतीत होता है कि समीक्षा बहुत जल्दी और अधूरेमन से लिखी गई है
एक जगह उन्होंने अनुवादक और भूमिका लेखक के शब्दों को परस्पर मिश्रित कर दिया है
फिर भी वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका बहुत मायने रखती है
अपना समय निकालने के लिए उनका आभार करना ही चाहिए