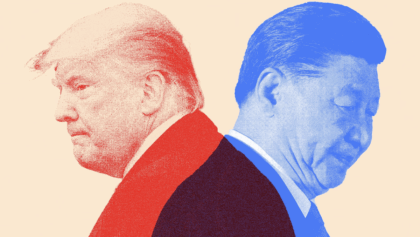उत्तराखंड। लेख के मूल विषय पर आने से पहले मैं पाठकों के सामने तीन घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। इन घटनाओं का जिक्र विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि कठ बद्दी जैसी परम्पराए। सुदूर इतिहास में होने वाली क्रूरताओं की छाया भर है।
उनके अनुसार अब उत्तराखंड आधुनिक नैतिकताओं के आधार पर चलता हैI लेकिन इन तीन घटनाओं का जिक्र इस बात को दिखाने के लिए किया जा रहा है कि कठ बद्दी मेले में अवैज्ञानिकता और अमानवीयता का जो विचार पैबस्त है, वह उत्तराखंड की अनेक गतिविधियों और वहां के लोगों के द्वारा लिए जाने वाले अनेक स्थानीय फैसलों में हर दिन दिखाई देता है।
भले ही एक समय था जब उनके द्वारा लिए जाने वाले फैसले कानून के खिलाफ नहीं माने जाते थे, लेकिन आज उनके द्वारा लिए जाने वाले अनेक फैसले भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के खिलाफ हैं। लेकिन छुआछूत के मामले में उत्तराखंड के जातिवादी लोग संविधान के खिलाफ जाने से कब घबराते हैं!
पहली घटना 1984 की है। मैं स्कूल के फाइनल एग्जाम देने के बाद अपने गांव (दंडधार, पोस्ट ऑफिस भोन, जिला पौड़ी गढ़वाल,) गया हुआ था। उस समय गांव के लोग जिस ‘पन्दोले’ से पानी लेकर आते थे, वह गांव में मेरे घर से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर है।
मेरे गांव के दलित परिवार के घर से ‘पन्दोले’ की दूरी करीब दो किलोमीटर होगी। तो, एक दिन मैं गांव के कास्ट हिन्दू लोगों के साथ पन्दोले के पास बैठा हुआ था। मैं भी उन्हीं कास्ट हिन्दूज में से एक हूं। पन्दोले के पास कोई महिला कपड़े धो रही थी। कोई दांत मांज रहा था। कोई पानी भर रही थी। कोई पानी गर्म करने के लिए चूल्हा जला रही थी.
इस तरह पन्दोले के आसपास लोग अलग-अलग गतिविधियों में लगे हुए थे। तभी पन्दोले के ऊपर की पहाड़ी पर करीब 11 साल की एक लड़की खड़ी दिखाई दी। गांव में लगातार न रहने की वजह से मैं उस लड़की को नहीं पहचानता था। उस लड़की को न पहचान पाने की एक वजह जातिगत छुआछूत के कारण विकसित हो चुकी दूरियां भी थीं।
उसे देखते ही पन्दोले के आस-पास के कास्ट हिन्दू लोगों में हड़कंप सा मच गया। वह हड़कंप मेरी समझ से दूर था। कोई किसी को गगरा हटाने की सलाह दे रही थी। कोई किसी से कपड़ा हटाने को कह रहा था। कोई अपने बच्चे को रास्ते से हट जाने के लिए कह रही थी।
जब पन्दोले के पास से इंसानों समेत सारा सामान हटा लिया गया, तब जाकर ‘कास्ट हिन्दूज’ ने उस लड़की को आवाज देकर नीचे आने के लिए कहा। उस अपमानजनक स्थिति में जीने को अभिशप्त वह छोटी सी बच्ची धीरे-धीरे चलती हुई पन्दोले तक पहुंची।
जिस समय वह पन्दोले से बहते पानी से अपने गगरे को धो रही थी, उस समय उसे चारों तरफ से सुनाई दे रहा था कि “छींटे मत मार, छींटे मत मार”। गगरा धोने के बाद जब उसका 12-15 किलो का गगरा पानी से भर गया, तो वह खामोशी से मदद के लिए बारी-बारी से सब की ओर देखने लगी।
क्योंकि छुआछूत को मानने कि मेरी ट्रेनिंग ज्यादा गहरी नहीं हो पाई थी, इसलिए उसकी मदद करने के लिए जैसे ही मैं उठने को हुआ, लोगों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। वह लड़की, छुआछूत के मामले में, उन अमानवीय लोगों से, रोज ही मानवीय होने की उम्मीद करती और उसे रोज ही निराशा का मुंह देखना पड़ता था। मदद न तो मिलनी थी, न ही मिली।
अब उसने अपने गगरे से आधा पानी गिराया। उसे लगा कि वह इतना वजन बिना किसी की मदद के जमीन से सिर तक उठा सकती है। जितने पानी के लिए ‘कास्ट हिन्दूज’ को 3 किलोमीटर चलना होता था, उतने ही पानी के लिए उस लड़की को आठ किलोमीटर चलना पड़ता था।
वो एक धार्मिक आदेश था जिसे ‘कास्ट हिन्दूज’ मान रहे थे।वो सामूहिक अमानवीयता का एक सबूत था।
दूसरी घटना 2017 की है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार और लेंसडॉन के बीचों-बीच दुगड्डा के पास एक गांव है। उस गांव का नाम है फतेहपुर। इस गांव के मोटे तौर पर तीन हिस्से हैं। एक हिस्से में केवल ब्राह्मण रहते हैं। नदी के पार वाले हिस्से में मुसलमान रहते हैं और सड़क के किनारे वाले हिस्से में दलित और अन्य लोग रहते हैं।
इस गांव के ब्राह्मण टोले में मैंने 2017 से 2021 के आखिरी दिनों तक एक मकान किराए पर ले रखा था। दिल्ली से हर महीने 5-7 दिनों के लिए मैं यहां आता और रहता। एक दिन जब मैं और मेरी पत्नी वहां थीं, तो मकान मालकिन और उसके पति भी आ गये। हमारे बीच बातें होने लगीं।
बातों के दौरान मैंने मकान मालकिन से पूछा कि क्या इस गांव में अभी भी जातिवाद और छुआछूत माना जाता है। मकान मालकिन ने बहुत ही सहज भाव से उत्तर दिया कि नहीं अब वो सब कौन मानता है। अब तो सब बराबर हो गए हैं। उनका उत्तर सुनकर मैंने उनसे पूछा कि भुली अगर मैं “डूम” होता तो क्या आप यह मकान मुझे किराए पर दे देतीं?
मेरा प्रश्न सुनकर वे पति और पत्नी बिल्कुल खामोश हो गए। तो लोग जातिगत भेदभाव और छुआछूत दोनों को मानते हैं। लेकिन अक्सर, बदले हुए जमाने पर गुस्सा निकालने के लिए यह झूठ भी कहते चलते हैं कि अब कौन मानता है!
तीसरी घटना 2021 की है। 2021 के आखिरी दिनों में मैं देहरादून के विकासनगर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए एक प्लॉट की तलाश कर रहा था। मेरे साथ दिल्ली से ही मेरे दो साथी और थे। एक साथी बिहार के ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी पत्नी अनुसूचित जनजाति की हैं।
ये साथी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और उनकी पत्नी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। प्लॉट की तलाश में हम कई डीलर्स के पास गये। वे हमें अपनी-आपनी प्रॉपर्टी दिखाकर उसकी विशेषताएं बताते। पहले डीलर ने अपनी प्रॉपर्टी की विशेषताएं बताने के दौर में कहा कि हमारी प्रॉपर्टी साफ सुथरी है।
हमें लगा की साफ सुथरी का मतलब यह है कि उनकी प्रॉपर्टी में कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। फिर भी बात को स्पष्ट करने के लिहाज़ से मैंने उनसे “साफ सुथरी” का मतलब पूछा। बात को साफ करते हुए उन्होंने समझाया कि “साफ सुथरी” का मतलब यह है कि वे अपनी जमीन मुसलमान, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को नहीं बेचते।
हम जिस भी डीलर के पास गए हमें यह बात हर बार सुनने को मिली। उन डीलर्स की बात सुनने के बाद मेरे प्रोफेसर मित्र ने मेरा पड़ोसी बनने का सपना त्याग दिया। मैं देहरादून के होरावाला में मकान बना चुका हूं।
मकान बन जाने के बाद भी मैंने अपने स्तर पर आसपास के जमीनधारी लोगों से पूछा कि क्या वे किसी शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जमीन बेचने को तैयार हैं। लेकिन, अफसोस कि अभी तक, कहीं से भी सकारात्मक उत्तर नहीं मिल सका है।
बावजूद इसके मैं जिनके लिए जमीन खोज रहा हूं, उनमें से एक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और दूसरे दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरी के प्रोफेसर हैं। जमीनधारियों को अपने मित्रों के पद और काम बताने के बाद भी मैं असफल रहा हूं।
1984 से 2021 तक लगभग तीन दशक के तीन तथ्य आपके सामने रखे। मैं ऐसे सैकड़ों तथ्य आपके सामने रख सकता हूं। क्या कोई बदलाव दिखाई देता है? सामाजिक लोकतंत्र तो छोड़ ही दीजिए। जो कानून, राजनैतिक लोकतंत्र की निशानी हैं, उत्तराखंड के लोग उसे भी अपनाने को तैयार नहीं हैं। इस पृष्ठभूमि में उत्तराखंड के कठ बद्दी मेले पर मेरी निम्लिखित टिप्पणी प्रस्तुत है-
उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में एक उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव पर टिप्पणी के बहाने यह इशारा किया जाएगा कि कैसे संस्कृति और परंपरा की आड़ में अवैज्ञानिकता और अमानवीयता को जीवित रखने के प्रयास जारी हैं। यह उत्सव, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में एक मेले के रूप में मनाया जाता है।
इस मेले को “कठ बद्दी” मेले के नाम से जाना जाता है। कठ बद्दी यानि काठ का बादी। तो “काठ का बादी” से ही पहला सवाल यह निकलता है कि ये “बादी” कौन है, जिसे काठ का बनाया गया है?
दूसरा सवाल निकलता है कि क्या संस्कृति क्रूर भी होती है ?
तीसरा सवाल यह कि क्या लोग अपने अमानवीय और अत्याचारी होने पर शर्मिंदा होने की बजाय, अत्याचार का उत्सव मनाकर खुश हो सकते हैं?
दरअसल कठ बद्दी मेले के बारे में लिखने का ख्याल मुझे उत्तराखंड के कवि मोहन मुक्त की एक कविता पढ़कर आया। मोहन मुक्त का एक काव्य संग्रह है “हम खत्म करेंगे”। इस संग्रह में एक कविता है “प्रिय पुल बनाने वालो”। इस कविता में मोहन मुक्त ने उत्तराखंड की एक दलित जाति का जिक्र किया है।
वह जाति है “बादी”। यह कविता बहुत ही मार्मिक है और उत्तराखंड के सवर्णों द्वारा, उत्तराखंड के दलितों पर किए गये शोषण की कई परतों को हमारे सामने रखती है।
इस कविता के अंत में मोहन मुक्त ने बादी जाति पर सवर्णों द्वारा किये गये जुल्मों के इतिहास के दो रेफरेंस दिये हैं। उन्होंने यमुनादत्त वैष्णव की किताब “कुमाऊं का इतिहास” से एक लम्बा उद्धरण दिया है। कुमाऊं के खस मानव समुदाय के इतिहास पर केन्द्रित यह किताब 1877 में प्रकाशित हुई थी।
दूसरा रिफरेन्स उन्होंने 1882 में प्रकाशित और Atkinson द्वारा लिखित Gazetteer of the Himalayan Districts of the North-Western Provinces का दिया है। Atkinson कुमाऊं क्षेत्र में सिविल सर्वेंट थे। अपने Gazetteer में Atkinson ने सवर्णों द्वारा, बादी जाति पर किये जाने वाले जुल्मों को दर्ज किया है।
कठ बद्दी मेले का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हुए मैंने अपने चैनल के लिए एक विडियो बनाया है। इस वीडियो को अब तक ग्यारह हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मोहन मुक्त ने मशवरा दिया कि मैं इस विषय को एक लेख के रूप में भी सामने लाऊं।
कठ बद्दी मेले में हवा में तनी हुई करीब 100-125 मीटर लंबी रस्सी पर फिसलता हुआ एक पुतला होता है। रस्सी दो खंबों के सहारे बंधी होती है। रस्सी का एक सिरा ऊंचाई पर और दूसरा सिरा ढलान की तरफ होता है। पुतले के फिसलना शुरू करते ही रस्सी के आसपास और नीचे खड़े लोगों में उत्साह देखते ही बनता है।
वे खुशी से नाचते हैं। चिल्लाते हैं। झूमते हैं। जैसे-जैसे पुतला हवा में दूरी कम करता जाता है, वैसे-वैसे लोगों की ख़ुशी बढ़ती जाती है। ऊंचाई पर हवा में तनी रस्सी से फिसलता हुआ पुतला, जैसे ही रस्सी के निचले सिरे पर पहुंचता है लोग खुशी से पागल हो उठते हैं।
फिसलने के दौरान पुतले को पहनाये गये कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे हैं। एक बात जो कठ बद्दी मेले के सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियोज में दिखाई नहीं देती, वो ये कि फिसलते हुए पुतले के बीच वाले भाग में कितनी गर्मी पैदा हो रही होगी।
पुतले के शरीर का वह भाग जिस पर उसे रस्सी पर टिकाया गया है। क्या वह भाग जल रहा होगा? उसमें से धुआं निकल रहा होगा? आप सोचिए और शर्मिंदा हो जाइए। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है वह आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा।
अगर गर्मी पैदा होने कि बात समझ नहीं में आ रही है तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोर-जोर से रगड़कर उन्हें अपने गालों पर लगाओ। क्या हथेलियों के घर्षण से गर्मी पैदा हुई। अगर हथेलियों के घर्षण से गर्मी पैदा हो रही है तो भारी पुतले के हवा में तनी रस्सी पर करीब 80 KM प्रति घंटे की रफ़्तार से फिसलते हुए कितनी गर्मी पैदा हो रही होगी?
ये कौन लोग हैं जो ख़ुशी मनाते हैं?
ये कौन लोग हैं जिनके लिए यह उत्सव है?
रस्सी पर फिसलता पुतला जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है क्या वे वही लोग हैं जो नीचे खड़े खुशियां मना रहे हैं?
अब सोशल मीडिया पर तैर रहे कठ बद्दी मेले के वीडियोज में एक परिवर्तन कर देते हैं। काल्पनिक परिवर्तन, जो अभी तो कल्पना है, लेकिन इतिहास में सच हुआ करता था। हवा में तनी 100-125 मीटर लंबी रस्सी पर, पुतले की जगह किसी इंसान को बिठाते हैं।
कल्पना में कोशिश करके देखते हैं कि कोई इंसान उस रस्सी पर फिसलने के लिए तैयार हो जाए। मैंने कोशिश की, लेकिन मेरी कल्पना में कोई भी इंसान तैयार नहीं हो रहा है। क्या आपकी कल्पना में कोई तैयार हुआ? क्या कहा, नहीं हो रहा है? आपकी कल्पना में भी कोई तैयार नहीं हो रहा है?
कोई तो होगा जांबाज युवक ! नहीं। कोई नहीं। फिर भी, क्या आप उस रस्सी पर अपने बेटे को बिठाना चाहोगे? अपने भाई को? क्या कहा, नहीं! अपने पिता को बिठाना चाहोगे? क्या कहा, उनको भी नहीं बिठाना चाहोगे। तो इस रस्सी पर किस इंसान को बिठाया जाए?
क्या उत्तराखंड के किसी ब्राह्मण को बिठाया जाए? सुना है उस पर भगवान की कृपा कुछ ज्यादा होती है! तो क्या भगवान की कृपा का कवच पहन कर उत्तराखंड का ब्राह्मण उस रस्सी पर बैठना चाहेगा? क्या कहा, नहीं! तो उसे भगवान की कृपा पर भरोसा नहीं है। तो सवाल अपनी जगह पर जस का तस बना हुआ है कि रस्सी पर किस इंसान को बिठाया जाए?
अब आपकी कल्पना उस इंसान की तरफ बढ़ चुकी है जिसे इस रस्सी पर बिठाया जा सकता है। लगता है आपने सही आदमी की पहचान कर ली है। आपने पहाड़ के ठाकुरों, राजपूत की भीड़ की तरफ इशारा कर दिया है। इन्हें तो तलवारबाजी का और बहादुरी का बहुत अभिमान है।
क्या इनमें से कोई हवा में तनी रस्सी पर बिना सुरक्षा कवच के और बिना सुरक्षा साधनों के फिसलना चाहेगा? क्या कहा! राजपूत और ठाकुर डर रहे हैं।
फिर कौन इंसान हो सकता है जिसे इस रस्सी पर बिठाया जाए? अरे! आप सब की निगाहें उस आदमी की तरफ क्यों मुड़ गई है? अरे! ये क्या! आप सब ने मिलकर उसको पकड़ लिया है। अरे! देखो वो छूटने के लिए छटपटा रहा है। अरे! ये क्या, आपने तो हिंसा शुरू कर दी।
उसे रस्सी पर बिठाने के लिए आप उसे पीट रहे हैं। ये क्या, आप कह रहे हैं कि आपके देवता को खुश करने के लिए किसी को तो रस्सी पर फिसलना होगा। किसी को तो अपनी जान की बाज़ी लगानी होगी। किसी को तो अपनी जान कुर्बान करनी होगी। लेकिन यह आदमी है कौन, जिसे आप सब ने मिलकर दबोच रखा है। और लो! आपने उसे रस्सी पर बिठा ही दिया है।
हवा में तनी रस्सी पर फिसलते हुए उसके पैर सीधे रहें, इसके लिए आपने उसके दोनों पैरों में भारी वजन की बोरियां बांध दी हैं। उसके पैरों पर 20-30 किलो का वजन बांधने से पहले, आपने उसके नीचे लकड़ी का एक पटरा रख दिया है।
वो आदमी अब अपने 70 किलो वजन के साथ, पैरों पर 30 किलो तक का वजन लटकाए लकड़ी के एक पटरे पर बैठा है। करीब-करीब मौत के मुंह में जाने को मजबूर।
ये मजबूर आदमी किसका बेटा है? ये किसका भाई है? किसका पिता है? ये किसका पति है? इस समय जब भीड़ ने इसे कैद कर लिया है, ठीक इसी समय उसके परिवार में दुःख और भय का वातावरण होगा।
क्या ये उस भीड़ में से किसी का अपना है, जो अपने देवता को खुश करने के लिए 100 किलो वजन के साथ उसे रस्सी पर फिसलने के लिए मजबूर कर रही है। इस भीड़ का उस मजबूर व्यक्ति के साथ रिश्ता क्या है? यह रिश्ता शोषक और शोषित का है। ये रिश्ता उत्पीड़क और उत्पीड़ित का है। ये रिश्ता उत्तराखंड के सवर्ण और दलित का है।
यमुनादत्त वैष्णव ने अपनी किताब कुमाऊं का इतिहास में लिखा है कि- “जब घाटी में खेती की उपज कम होने लगती, किसी महामारी से पशु मरने लगते या बारिश नहीं होती तो ऐसे में देवी देवताओं को खुश करने के लिए उनकी पूजा करने की जरूरत पड़ जाती थी”।
“बारिश के देवता को संतुष्ट करने के लिए गांव के वादी को बुलाया जाता था। बादी समुदाय के लोगों को सबसे नीची जाति का माना जाता था। बारिश लाने के लिए बादी को अपने प्राणों की बाजी लगाकर घाटी की सबसे ऊंची चोटी से नदी की पैंदी तक तने हुए एक रस्से पर फिसलना होता था। इस तरह की पूजा पद्धति 18 वीं सदी के अंत तक भी प्रचलित रही है।”
एटकिंसन ने अपने गजेटियर में इस पूजा पद्धति का वर्णन इन शब्दों में किया है। एटकिंसन ने लिखा कि- सूखे से जब खेती चौपट होने लगती है और पशु मरने लगते और जब चारों तरफ भूख के लक्षण दिखाई देने लगते, तब नाराज बारिश के देवता (दयो) को प्रसन्न करने के लिए एक समारोह किया जाता।
गांव के बादी को बुलाकर पहले पूजा पाठ किया जाता और उसके बाद एक बकरे की बलि दी जाती। एक रस्सा पहाड़ की चोटी पर से नीचे घाटी तक तान दिया जाता। बादी को चोटी की ओर से रस्सी के छोर पर लकड़ी की जीन पर बिठाया जाता। रस्सी के दोनों छोर खूंटों से बंधे रहते।
यह खूंटे जमीन में मजबूती के साथ गाड़ दिए जाते। काठ की जीन रस्सी पर आसानी से खिसक सके इसके लिए उसके नीचे बीच में रस्सी को अटकाए रखने के लिए गहरी नाली बनाई जाती। खिसकते समय बादी का संतुलन बना रहे इसके लिए बालू भर थैले दोनों और पैरों में बांध दिए जाते।
बादी जब रस्सी पर नीचे की ओर फिसलने लगता है तो काठ की जीन से धुएं का अंबार उठने लगता। चाहे रस्सी पर कितनी ही चिकनाई क्यों ना लगाई गयी हो, रस्से और पटरे के घर्षण से आग पैदा हो जाती थी।
बादी को रस्सी के टूट जाने का डर रहता था, इसलिए वह अपने हाथ की ही बटी रस्सी का उपयोग करता। यह रस्सी बाबिल नामक घास की बनी होती थी, जिसे बाबड़ भी कहा जाता है।
एटकिंसन लिखते हैं कि रस्सी के टूट जाने के अलावा भी बादी के ऊपर एक खतरा और मंडराता था। यदि बादी खिसकते समय रस्सी से नीचे गिर पड़ता था तो दर्शक समुदाय उसके गिरते ही अपनी तलवारों से उसके टुकड़े कर देते थे। बाद के दिनों में इस खेल में बादी कि हत्या करना वर्जित कर दिया गया था।
बादी के सफलतापूर्वक अपना कर्तव्य पूरा करने पर उसके द्वारा इस्तेमाल की गयी रस्सी को काटकर उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए जाते। एक-एक टुकड़ा प्रत्येक गृहस्थ अपने घर के दरवाजे के ऊपर टांकने के लिए अपने साथ ले जाता। बादी के बाल मुंडवा दिये जाते। उन बालों को भी किसान शुभ-शकुन मानकर अपने पास रखते।
बादी का जीवन खेतों की उर्वरता का साधन माना जाता। यह विश्वास किया जाता कि भूमि के बांझपन को बादी ने स्वयं ग्रहण कर लिया है। यह विश्वास इतना पक्का था कि उसके हाथ का छुआ हुआ बीज खेतों में नहीं बुवाया बोया जाता। यह मान लिया जाता कि उसका छुआ हुआ बीज अंकुरित नहीं होगा। (एटकिंसन. 1882 संस्करण . हिमालय डिस्ट्रिक्ट. पृष्ठ 834. यमुना दत्त वैष्णव की किताब कुमाऊं के इतिहास के पृष्ठ 304 और 305 पर उद्धरित)।
तो हमने देखा कि उत्तराखंड के सवर्ण, अपने अमानवीय में होने का प्रदर्शन कठ बद्दी जैसा उत्सव मना कर अब भी कर रहे हैं। उनकी संस्कृति और परंपराएं, उनके विश्वास अमानवीय थे, इस बात के लिए वे शर्मिंदा नहीं है। वे इस बात को छुपाना नहीं चाहते।
परंपराओं में अवैज्ञानिकता हो सकती है। उनमें अतार्किकता हो सकती है। लेकिन परम्पराओं में क्रूरता का होना एकदम ही अलग मामला है। उनमें क्रूरता का होना बुरी बात है, और उस क्रूरता का उत्सव मनाना तो और भी बुरी बात है।
मान लीजिए की कल से उत्तराखंड के दलित “कठ बद्दी” की तर्ज पर “कठ बामण” नाम से कोई त्यौहार मनाने लग जाएं। तब क्या होगा? क्या ब्राह्मणवादियों को “कठ बामण” जैसा कोई भी उत्सव स्वीकार होगा? क्या “कठ बामण” नाम के उत्सव में उन्हें अपने पर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हमला दिखाई देगा? उत्तराखंड के लोगों को इस तरह के सवालों पर चिंतन करना चाहिए।
उत्तराखंड के कठबद्दी मेले, एक क्रूर परंपरा की प्रदर्शनियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड देव भूमि है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि वो कैसे देवता थे, जो बादी के साथ की जाने वाली क्रूरता को देखकर भी मानवता के पक्ष में सक्रिय नहीं हुए?
संस्कृति पूजे जाने की वस्तु नहीं है, समझे जाने की वस्तु है। क्योंकि संस्कृतियां क्रूर भी होती हैं। क्रूरता को समझकर ही उसके खिलाफ लड़ा जा सकता है। अपनी ही संस्कृति के अमानवीय होने को समझना पहला कदम है।
(बीरेन्द्र सिंह रावत, शिक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं।)